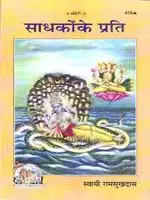|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> साधकों के प्रति साधकों के प्रतिस्वामी रामसुखदास
|
81 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है साधकों के प्रति....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
।।श्रीहरिः।।
निवेदन
हमारे परमश्रद्धेय स्वामीश्रीरामसुखदास जी महाराज अत्यन्त सरल एवं सुबोध
भाषा-शैली में प्रवचन दिया करते हैं। ‘साधकों के
प्रति’ नाम
से ‘कल्याण’ मासिक पत्रिका में आपके प्रवचन प्रकाशित
होते
हैं। प्रवचनों की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रवचनों की उपादेयता
के कारण यह महत्त्वपूर्ण प्रवचन-संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कहना
अतिशयोक्ति नहीं है कि इसे मनन पूर्वक पढ़ने से जीवन में व्यावहारिक एवं
पारमार्थिक अभूतपूर्व सहायता ही नहीं सफलता भी प्राप्त हो सकेगा। अतः
सर्वसाधारण से निवेदन है कि प्रस्तुत विषयको भलीभाँति हृदयंगम करने की
कृपा कर लाभ उठावें।
विनीत
प्रकाशक
प्रकाशक
प्रवचन-1
साधकों के प्रति—
साधक के लिये खास बात है—पराधीनता से रहित होना। शरीर, रुपये,
व्यक्ति, देश, काल आदिक की आवश्यकता अनुभव करना ही पराधीनता है। जीसके पास
अधिक रुपये, विद्या, बुद्धि, बल आदि हैं, वह संसार की अधिक सेवा कर सकता।
यह वहम हृदय से बिलकुल उठा देना चाहिये। साधकके पास दजितने रुपये, विद्या,
शक्ति आदि हैं, उतने से ही वह संसार की बड़ी-से-बड़ी सेवा कर सकता है। जो
अपने पास नहीं है, उसे देने की जिम्मेवारी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति
वस्तु से नहीं, त्याग से होती है।
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं की आवश्यकता अनुभव करना और उनका आश्रय से अपनी उन्नति मानना महान् भूल है। साधक को कभी स्वप्न में भी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिये। पासमें जो धन, जमीन, मकान, परिवार आदि हैं, उनके रहते हुए ही अन्तःकरण से उनकी आवश्यकता का मूलोच्छेदन कर देना चाहिये। ऐसा करने से साधककी उन्नति स्वतःसिद्ध है।
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना योगमार्ग, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग—तीनों ही मार्गों में महान् बाधक है। जीव स्वयं नित्य परिपूर्ण निर्विकार परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी यदि उत्पत्ति-विनाशशील जड़ वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव करता है, तो वह परमात्मा को जान ही कैसे सकता है ? अतः धनादि जड़ वस्तुएँ हमारी हैं और हमारे लिये आवश्यक हैं—यह भाव साधकको मनसे ही उठा लेना चाहिये।
मनुष्य के भीतर यह भाव रहता है कि जो वस्तु परिस्थिति, योग्यता आदि अभी नहीं है, वह मिल जाय तो मेरी उन्नति हो जायगी। वह उत्पत्ति-विनाशशील जड़ वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानता है। जैसे, उसके पास धन नहीं है, तो धन कमाकर लखपति-करोड़पति बननेपर वह सोचता है कि मैंने बड़ी भारी उन्नति कर ली है, वह पढ़ा-लिखा नहीं है तो पढ़-लिखकर विद्वान बन जानेपर सोचता है कि मैंने बड़ी उन्नति कर ली, इत्यादि। वास्तव में यह उन्नति नहीं है, अपितु महान् अवनति (पतन) है। जो वस्तु पहले नहीं थी, वह बादमें भी नहीं रहेगी। स्वयं नित्य-निरंतर रहनेवाला होनेपर भी अनित्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपनी उन्नति मानना अपने साथ महान् धोखा करता है। जो सदा से है और सदा रहेगी, उस अविनासी परमात्मा को प्राप्त करने में ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। जो वस्तु अभी नहीं है, उसे प्राप्त कर भी लेंगे तो वह कबतक हमारे साथ रहेगी। जो अभी नहीं है, वह अन्त में भी ‘नहीं’ में ही परिणति होगी।
ऐसी उत्पत्ति –विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने में बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन (पराधीन) होना है।
दूसरी खास बात यह है कि अपने में सद्गुण-सदाचारों की कमी दीखने पर भी साधक ऐसा भी न माने कि मुझमें सद्गुण-सदाचारों का अभाव है। सद्गुण-सदाचार ‘सत्’ हैं और दुर्गुण-दुराचार ‘असत्’ है। ‘असत्’ की तो सत्ता नहीं होती और ‘सत्’ का कभी अभाव नहीं होता —‘नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।’
(गीता 2/16)। उत्पत्ति-विनाशशील असत् का संग करने के कारण ही सत् प्रकट नहीं होता। अस्वाभाविक असत् (दुर्गुण-दुराचार) का त्याग कर दें, तो सते (सद्गुण-सदाचार) स्वतःसिद्ध हैं। सत् से विमुख हुए है, उसका अभाव नहीं हुआ है। असत् (दुर्गुण-दुराचारों) का त्याग करने का उपराय यह है कि साधक इन्हें अपने में कभी न माने। वास्तव में ये हमारे में हैं ही नहीं, रह सकते ही नहीं। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और प्राण भी पहले हमारे साथ नहीं थे और न ही आगे हमारे साथ रहेंगे। कारण कि ये सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएँ हैं और हम स्वयं अविनाशी परमात्मा के अंश हैं।—‘ममैवांशो जीवलोके’ (गीता 15/7) जड़ वस्तुएँ बदलती और आती-जाती हैं जबकि स्वयं (आत्मा) कभी नहीं बदलता और सदैव ज्यों-का-त्यों रहता है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाता है और जन्म-मरण के बन्ध से बँध जाता है। गीतामें आया है—
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं की आवश्यकता अनुभव करना और उनका आश्रय से अपनी उन्नति मानना महान् भूल है। साधक को कभी स्वप्न में भी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिये। पासमें जो धन, जमीन, मकान, परिवार आदि हैं, उनके रहते हुए ही अन्तःकरण से उनकी आवश्यकता का मूलोच्छेदन कर देना चाहिये। ऐसा करने से साधककी उन्नति स्वतःसिद्ध है।
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना योगमार्ग, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग—तीनों ही मार्गों में महान् बाधक है। जीव स्वयं नित्य परिपूर्ण निर्विकार परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी यदि उत्पत्ति-विनाशशील जड़ वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव करता है, तो वह परमात्मा को जान ही कैसे सकता है ? अतः धनादि जड़ वस्तुएँ हमारी हैं और हमारे लिये आवश्यक हैं—यह भाव साधकको मनसे ही उठा लेना चाहिये।
मनुष्य के भीतर यह भाव रहता है कि जो वस्तु परिस्थिति, योग्यता आदि अभी नहीं है, वह मिल जाय तो मेरी उन्नति हो जायगी। वह उत्पत्ति-विनाशशील जड़ वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानता है। जैसे, उसके पास धन नहीं है, तो धन कमाकर लखपति-करोड़पति बननेपर वह सोचता है कि मैंने बड़ी भारी उन्नति कर ली है, वह पढ़ा-लिखा नहीं है तो पढ़-लिखकर विद्वान बन जानेपर सोचता है कि मैंने बड़ी उन्नति कर ली, इत्यादि। वास्तव में यह उन्नति नहीं है, अपितु महान् अवनति (पतन) है। जो वस्तु पहले नहीं थी, वह बादमें भी नहीं रहेगी। स्वयं नित्य-निरंतर रहनेवाला होनेपर भी अनित्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपनी उन्नति मानना अपने साथ महान् धोखा करता है। जो सदा से है और सदा रहेगी, उस अविनासी परमात्मा को प्राप्त करने में ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। जो वस्तु अभी नहीं है, उसे प्राप्त कर भी लेंगे तो वह कबतक हमारे साथ रहेगी। जो अभी नहीं है, वह अन्त में भी ‘नहीं’ में ही परिणति होगी।
ऐसी उत्पत्ति –विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करके अपने में बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन (पराधीन) होना है।
दूसरी खास बात यह है कि अपने में सद्गुण-सदाचारों की कमी दीखने पर भी साधक ऐसा भी न माने कि मुझमें सद्गुण-सदाचारों का अभाव है। सद्गुण-सदाचार ‘सत्’ हैं और दुर्गुण-दुराचार ‘असत्’ है। ‘असत्’ की तो सत्ता नहीं होती और ‘सत्’ का कभी अभाव नहीं होता —‘नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।’
(गीता 2/16)। उत्पत्ति-विनाशशील असत् का संग करने के कारण ही सत् प्रकट नहीं होता। अस्वाभाविक असत् (दुर्गुण-दुराचार) का त्याग कर दें, तो सते (सद्गुण-सदाचार) स्वतःसिद्ध हैं। सत् से विमुख हुए है, उसका अभाव नहीं हुआ है। असत् (दुर्गुण-दुराचारों) का त्याग करने का उपराय यह है कि साधक इन्हें अपने में कभी न माने। वास्तव में ये हमारे में हैं ही नहीं, रह सकते ही नहीं। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और प्राण भी पहले हमारे साथ नहीं थे और न ही आगे हमारे साथ रहेंगे। कारण कि ये सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएँ हैं और हम स्वयं अविनाशी परमात्मा के अंश हैं।—‘ममैवांशो जीवलोके’ (गीता 15/7) जड़ वस्तुएँ बदलती और आती-जाती हैं जबकि स्वयं (आत्मा) कभी नहीं बदलता और सदैव ज्यों-का-त्यों रहता है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाता है और जन्म-मरण के बन्ध से बँध जाता है। गीतामें आया है—
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्।
कारणं गुणसंदोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।। (गीता 13/21)
कारणं गुणसंदोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।। (गीता 13/21)
‘प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य त्रिगुणात्मक पदार्थों
को
भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी-बुरी योनियों में
जन्म लेने का कारण है।’
तीसरी खास बात यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक सम्पत्ति वैभव पद, अधिकार, विद्या आदिकी अधिकता होनेसे आध्यात्मिक उन्नति अधिक होगी और इनकी कमी होने से आध्यात्मिक उन्नति कम होगी—ऐसी बात बिलकुल नहीं है; क्यों सांसारिक वस्तु चाहे अधिक हो या कम, उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना ही अर्थात् उसकी कामना और मममता का त्याग करना है। चाहे लाखों-करोड़ों रुपये हों, चाहें पाँच रुपये हों और चाहे कुछ भी न हो, भीतर से उनकी कामना ही त्याग करना है। त्याग करने में सभी समान हैं।
अमुक व्यक्ति ने बहुत त्याग किया और अमुक व्यक्ति ने थोड़ा त्याग किया तो इससे त्याग में क्या फर्क पड़ा ? त्याग तो दोनों का समान ही है। अधिकका त्याग करने की अपेक्षा कम का त्याग करने में सुगमता भी होगी। बोलने-बोलने में फर्क है ? पर न बोलने में क्या फर्क ? देखने-देखने में फर्क है, पर न देखने में क्या फर्क ? दो आदमी काम करें तो करने में फर्क होगा, पर न करने में क्या फर्क ? तात्पर्य यह कि सांसारिक वस्तुओं के रहते हुए तो फर्क है पर उनका त्याग करने में कोई फर्क नहीं। किसी के पास धन, जमीन मकान आदि अधिक हैं और किसी के पास ये कम हैं, पर इनसे रहित होने में सब बराबर हैं। जीनें में कई फर्क हैं पर ये कम हैं, पर इनसे रहित होने में सब बराबर हैं। जीने में कई फर्क हैं पर मरने में कोई फर्क नहीं, चाहें मनुष्य मरे या पशु-पक्षी। अतएव हमारे पास-धन-सम्पति कम है, विद्या कम है, योग्यता कम है, इसलिये हम पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकते—यह धारणा बिलकुल गलत है।
जड़ता से सम्बन्ध-विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चिन्मयता—(परमात्मतत्त्व-) की प्राप्ति सभी को स्वतः सिद्ध है पर जड़ता (उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं)-को महत्त्व देने से हम चिन्यमता से विमुख हुए हैं। अतः जड़ता से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। हृदय में धनादि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं का महत्त्व अंकित होने के कारण ही ऐसा भाव होता है कि हमारे पास बहुत धन है, इसलिये हम बड़े आदमी हैं अथवा हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम छोटे हैं। वास्तव में चाहें धनवान् हो या निर्धन, मन से धनकी इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान हैं। अतएव जैसी भी परिस्थिति, योग्यता आदि हमें मिली हुई है, उसी में साधक परमात्मतत्त्व का अनुभव कर सकता है।
मनुष्य-शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो सकता है, क्योंकि संसारकी कोई वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्णरूप से नहीं मिलती। परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्त्व की प्राप्ति में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य-शरीर मिल गया तो परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया।
तीसरी खास बात यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक सम्पत्ति वैभव पद, अधिकार, विद्या आदिकी अधिकता होनेसे आध्यात्मिक उन्नति अधिक होगी और इनकी कमी होने से आध्यात्मिक उन्नति कम होगी—ऐसी बात बिलकुल नहीं है; क्यों सांसारिक वस्तु चाहे अधिक हो या कम, उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना ही अर्थात् उसकी कामना और मममता का त्याग करना है। चाहे लाखों-करोड़ों रुपये हों, चाहें पाँच रुपये हों और चाहे कुछ भी न हो, भीतर से उनकी कामना ही त्याग करना है। त्याग करने में सभी समान हैं।
अमुक व्यक्ति ने बहुत त्याग किया और अमुक व्यक्ति ने थोड़ा त्याग किया तो इससे त्याग में क्या फर्क पड़ा ? त्याग तो दोनों का समान ही है। अधिकका त्याग करने की अपेक्षा कम का त्याग करने में सुगमता भी होगी। बोलने-बोलने में फर्क है ? पर न बोलने में क्या फर्क ? देखने-देखने में फर्क है, पर न देखने में क्या फर्क ? दो आदमी काम करें तो करने में फर्क होगा, पर न करने में क्या फर्क ? तात्पर्य यह कि सांसारिक वस्तुओं के रहते हुए तो फर्क है पर उनका त्याग करने में कोई फर्क नहीं। किसी के पास धन, जमीन मकान आदि अधिक हैं और किसी के पास ये कम हैं, पर इनसे रहित होने में सब बराबर हैं। जीनें में कई फर्क हैं पर ये कम हैं, पर इनसे रहित होने में सब बराबर हैं। जीने में कई फर्क हैं पर मरने में कोई फर्क नहीं, चाहें मनुष्य मरे या पशु-पक्षी। अतएव हमारे पास-धन-सम्पति कम है, विद्या कम है, योग्यता कम है, इसलिये हम पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकते—यह धारणा बिलकुल गलत है।
जड़ता से सम्बन्ध-विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चिन्मयता—(परमात्मतत्त्व-) की प्राप्ति सभी को स्वतः सिद्ध है पर जड़ता (उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं)-को महत्त्व देने से हम चिन्यमता से विमुख हुए हैं। अतः जड़ता से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। हृदय में धनादि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं का महत्त्व अंकित होने के कारण ही ऐसा भाव होता है कि हमारे पास बहुत धन है, इसलिये हम बड़े आदमी हैं अथवा हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम छोटे हैं। वास्तव में चाहें धनवान् हो या निर्धन, मन से धनकी इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान हैं। अतएव जैसी भी परिस्थिति, योग्यता आदि हमें मिली हुई है, उसी में साधक परमात्मतत्त्व का अनुभव कर सकता है।
मनुष्य-शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो सकता है, क्योंकि संसारकी कोई वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्णरूप से नहीं मिलती। परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्त्व की प्राप्ति में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य-शरीर मिल गया तो परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i