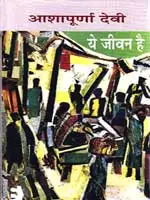|
कहानी संग्रह >> ये जीवन है ये जीवन हैआशापूर्णा देवी
|
372 पाठक हैं |
|||||||
इन कहानियों में मानव की क्षुद्र और वृहत् सत्ता का संघर्ष है, समाज की खोखली रीतियों का पर्दाफाश है और आधुनिक युग की नारी-स्वाधीनता के परिणामस्वरूप अधिकारों को लेकर उभर रहे नारी-पुरुष के द्वन्द्व पर दृष्टिपात है।
आत्महत्या
मैला बिछौना, तेल-मलिन तकिया और गद्दे से सीलन भरी बदबू फैल रही है...जैसे
सालभर उसे किसी ने धूप न दिखाई हो। ऐसी शय्या पर सोकर लाख टके का सपना तो देखा
जा सकता है, मगर दुर्लभ प्रेयसी का सपना? कभी नहीं!होस्टल का नहीं, घर का ही, बिस्तर मगर घर में भी यानी मोहन जैसे लोगों के घर में शायद इससे अच्छा कुछ सोचा नहीं जा सकता। सोने के लिए चार हाथ जगह मिल गयी, यही क्या कम है?
मगर एक बिछौने को छोड़कर और ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ स्वयं को बिलकुल निश्चिन्त समर्पित कर कल्पना की उड़ान भरी जा सके। दैनन्दिन जीवन के भीषण संघर्ष मे अपनी मानस-प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने का स्थान ही कहाँ!
जीवन-लीला नहीं, जीवन-युद्ध। ससार की तुलना अब किसी नैया से नहीं, बल्कि उस टूटी हुई बैलगाड़ी से की जा सकती है जिसके पहिये कीचड़ में फँस गये हैं। पहले ज़माने में लोग घर क्या बसाते थे-पचास रुपये माहवार में दस-बारह बच्चे पाल लेते, खिलाते-पिलाते, शादी-ब्याह करते, दान-ध्यान, तीर्थ-दर्शन, कुछ भी नहीं छूटता था।
आराम से लम्बी उम्र काटते, मरने में भी जल्दबाजी नहीं करते थे। राम नाम जपते, पूरे होश-हवास में स्वर्ग का रास्ता नापते थे। उस ज़माने में रक्तचाप वृद्धि से सड़क पर गिरकर लोगों की मृत्यु नहीं होती थी, जैसी मृत्यु मोहन के पिता की हुई। ऑफ़िस से लौटकर, ट्यूशन के लिए जाते समय गिर पड़े और उनकी साँसें उखड़ गयीं।
फिर भी मोहन के पिता को इस बीमारी का पता तिरपन वर्ष की उम्र में चला था, मोहन की तरह तेईस वर्ष में नहीं। बीमारी का कारण संघर्ष और कठिन आर्थिक संकट था। इतने पर भी मोहन जैसे क्षुब्ध और असन्तुष्ट नही थे, बल्कि इसके विपरीत थोड़े में ही वे सन्तुष्ट हो जाते।
छोटी-छोटी बातों पर खुशी जाहिर करते। उनके इस महत्त्वाकांक्षाहीन स्वभाव को देखकर मोहन का मन घृणा और वैराग्य से भर जाता, आज भी मोहन को सब कुछ याद है।
शायद उनके मानस-पटल पर किसी मानसी का वास नहीं था तभी तेलसिक्त तकिये पर सर रखते ही वे आराम से सो जाते!...बचपन से मोहन उन्हें ऐसे ही देखता आया है।
खैर, आज उनकी चर्चा अप्रासंगिक है। अन्तिम शय्या में तो उन्हें वह तेलसिक्त तकिया भी नसीब नहीं हुआ था। इसका अफसोस मोहन की माँ को होता रहता है, मगर मोहन को इस बात का कोई दुःख नहीं।
फुटपाथ पर मौत होने से थोड़ा-बहुत आडम्बर हुआ था लेकिन अपने उस दुर्गन्धपूर्ण सीलन भरे अन्धेरे कमरे के गन्दे बिस्तर पर बीमारी झेलकर मरने से क्या वह भी नसीब होता? ऊपर से मोहन की माँ और बहन के पास सोने का एकाध कण बचा था वह भी बिक जाता और मोहन के सर पर कर्ज का बोझ कुछ और भारी हो जाता।
यह सब बाते अगर उजागर हो जातीं तो मोहन का समाज में मुँह दिखाना मुश्किल हो जाता और उस पर 'नराधम', 'हृदयहीन', 'अकृतज्ञ', जैसे विशेपण इसी दिन काम आते।
पर सोचने-विचारने पर तो कोई रोक नहीं?
बस यही एक आज़ादी हमेशा आदमी को मिलती रहेगी। मोहन मन-ही-मन पिता की सद्विवेचना की तारीफ़ किये बिना नहीं रह पाता।
यह सब तो इतिहास बन चुका है अब।
फिलहाल मोहन ने अपने आपको एक देशी बैक मे साधारण मूल्य के किराये पर लगाया है। ऐसी उसकी धारणा है। यह नौकरी उसके भविष्य और जीवन की निर्धारक है ऐसा वह सोच भी नहीं सकता यह भाग्य की सामयिक विडम्बना ही तो है 'दासत्व शैतान' के आगे अपनी आत्मा को बेचेगा मोहन, कभी नहीं परिस्थिति की विवशता ही उसे अपने आपको किराये पर लगाने को मजबूर कर रही है। जिस प्रकार पिता की मृत्यु के बाद किराये पर दे दिये घर के दो कमरे।
सामयिक विडम्बना हो या जो भी हो, दस से पाँच तक ऑफिस तो करना ही पड़ता है। फिर तीन घण्टे और लग जाते है बी.कॉम की पढ़ाई जारी रखने में। बस थोड़ा-सा अवसर रात को ही मिल पाता।
अवसर मिल पाता नरक भोगने का।
उषा का चेहरा याद आते ही वह जल-भुन गया। ऐसी शय्या पर सोकर प्रेयसी का ध्यान-छिः छिः। मन-ही-मन जैसे अपने हाथों से उस मुस्कुराती छवि को मिटाकर उठ बैठा मोहन...। टूटा हुआ पंखा उठाकर जोर-ज़ोर से झलने लगा। हवा मिली या न मिली, शोर जोरो का होने लगा।
हर रात वह सोचता, सुबह उठकर चाहे कुछ करे न करे, एक पंखा जरूर खरीद लाएगा। पर सुबह उठकर इस तुच्छ वस्तु की याद ही नहीं रहती। पंखे के शोर से
तंग आकर मोहन उसे उठाकर फेंकने ही वाला था कि नीचे से जयन्ती ने कहना शुरु किया, ''लो, शुरू हो गया भैया का पंखा ठोकना। उफ्, दिन भर की मेंहनत रात को जरा सो सकूँ, वह भी नसीब नहीं।''
सारे परिवार को एक ही कमरे में सोना पड़ता था। कमरे किराये पर देने का यही अवश्यम्भावी परिणाम था जिसे सबने मान लिया था। गरीबी की अनेक असुविधाओं में सबसे बुरी यही लगती थी, फिर भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। महीने भर दौड़धूप कर और अपना खून-पसीना एक कर मोहन जो कमाकर लाता, प्लास्टर झरे ईंट की दीवारों से बने दो कमरे चुपचाप बैठकर कुछ वैसा ही कमा लेते थे तो फिर सहन न करे तो क्या करे?
ये कमरे तो खाते भी नहीं, पहनते भी नहीं। भोर में उनके लिये उठकर चूल्हा भी तो नहीं जलाना पड़ता। इस तुलना में तो मोहन की कीमत कम ही ठहरेगी। तभी तो निरुपाय होकर चुपचाप कमरे में बिछे बिछावन की कतार को रौंदकर वह अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता।
मगर जयन्ती के कटुभाषण से वह ऐसा तिलमिला उठता कि दिल करता एक रात घर में आग लगाकर कहीं निकल जाए।...
आश्चर्य की बात थी। कितने परिवार उजड़ गये देश के दंगे में...कितने सुखी और समृद्ध परिवार...मगर मोहन के इस टूटे-फूटे घर की एक ईंट तक नहीं हिली।
पंखे को फेंकने की इच्छा को दबाकर जयन्ती के कथन के प्रतिरोध-स्वरूप मोहन उसे जोर-ज़ोर से झलने लगा।
''देख रही हो माँ,'' जयन्ती झल्ला उठी, ''जानबूझकर और शोर मचा रहा है।''
''क्या करे वह भी,'' तरुलता की थकीहारी आवाज़ उस अँधेरे में जैसे राहत खोज रही होती, ''क्या करे बोल? इतनी गर्मी में बिना पंखा झले रहे भी कैसे? सारे दिन की मेंहनत के बाद...''
''नहीं रह सकता? क्यों हम आदमी नहीं हैं क्या? क्या दिन भर गद्दे बिछा-बिछाकर सोये रहते हैं हम? मरदों की मेंहनत, हुँ। दाई-महरी के काम से लेकर जूता सिलाई और चण्डीपाठ तक करना पड़ता तो समझते। दिन भर पंखे की तेज हवा के नीचे बैठकर वेसा शौक़िया काम तो सभी कर लेंगे।''
मोहन व्यंग्यभरी आवाज़ में बोल उठता, ''एक दिन काम बदल लेते हैं आपस में। वहाँ तो 'ए बी सी डी' लिखते ही कलम टूट जाएगी।''
तुरन्त मुखर होकर जयन्ती बोली, ''हाँ टूट जाएगी। मगर इसके लिए शर्म मुझसे तुम्हीं लोगों को होनी चाहिए, समझे? आसमान की ओर मुँह करके थूकोगे तो वह तुम्हारे ही मुँह पर गिरेगा, याद रखना।''
''क्यों नहीं रखूँगा! दिन-रात क्या कुछ नहीं याद रखता? ये थोड़ी-सी बात कैसे भूल जाऊँ?''
''ज्यादा बको नहीं भैया, जलन होती है, तनबदन में। पिताजी नहीं रहे, अब। हमें ठीक से रखने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी ही है, पता है?''
''खूब पता है।'' मोहन हँस पड़ता, ''सिर्फ ठीक से रखना। माँ के गठिया का
इलाज कराना, मुन्नी के पेट की बीमारी का इलाज कराना, शोभन को विलायत भेजना, और तेरी शादी के लिए एक राजकुमार ढूँढ़ लेना-ये सभी मेरी ही जिम्मेदारी है न!
''बिलकुल है!'' जयन्ती भी उठ बैठती। अँधेरे में भी पता चलता। ऐसे में भी उसकी बातें तीर की तरह चुभतीं।
''शर्म नही आती चिढ़ाते हुए? मगर आदमी होते तो शर्म से मिट्टी में मिल गये होते।''
''क्या! क्या शुरू हो गया?'' तरुलता झल्ला उठती। लेकिन उस झल्लाहट में गुस्सा कम असहायता ज्यादा होती। बेटी से निपट लेना उनके बस की बात नही फिर भी रोकना जरूरी था, इसलिए बोलीं-
''अरे कह लेने दो।'' मोहन की व्यंग्योक्ति धुरी की तीक्ष्ण धार की तरह झलक उठती। "कहने पर टैक्स तो नहीं है न। कोई सरकारी नियन्त्रण भी नहीं, बकने दो जितनी मर्जी।''
''मेरा मज़ाक़ उड़ाकर अपना दोष ढँक रहे हो भैया, पर जान लो दुनिया में एक तुम ही चालाक नहीं हो।''
''अच्छा बाबा, तू भी बड़ी चालाक है'', बड़ी मुश्किल से स्वर में प्रभुता लाती तरुलता-''अब तो सो जा। वह बेचारा दिन भर दफ्तर में मेहनत करने के बाद अपनी पढ़ाई करता है, ज़रा-सा सोया कि उलझ पड़ी उससे। गर्मी से परेशान हुआ जा रहा है, पंखा नहीं झलेगा तो और क्या करेगा? तेरी तो हर बात में जबर्दस्ती चलती है। इतना बड़ा लडका, इस खटाल में सो रहा है, यही कम तकलीफ़ है क्या?''
''कौन कहता है तकलीफ करने को? पाँच सो रुपये महीना लाये और रहे शान से! तुम तो सिर्फ भैया की तरफ़दारी करती हो! शोभन के बारे में सोचा है कभी? इतनी छोटी उम्र में क्या नहीं करता है घर के लिए? भैया कभी दो पैसे की चीज लाकर भी देता है हाथ में? जैसे विलायत से साहब आये। तुम्हारे यहाँ रहकर तुम्हें निहालकर रहे है। ये नवाबी मुझसे तो नहीं देखी जाती।''
"तेरी बातें भी किसी के कान में शहद नही घोलती, समझी, अब कृपाकर चुप रहेगी या पार्क में जाकर रात काटूँ,'' ठण्डी आवाज़ में मोहन कहता।
''जाओ न! किसने मना किया?" जयन्ती लेट जाती धम्म से। ''तुम्हारे लिए तो फिर भी पार्क का बेंच है, हमारे नसीब में तो श्मशान घाट के सिवा और कोई जगह नहीं।''
विक्षुब्ध तरुलता बोल उठीं, ''कैसी बातें करने लगी है आजकल। जब से इनका स्वर्गवास हुआ है, पता नहीं कैसी हो गयी है।''
''अच्छा? तो पिताजी के साथ मुझे भी क्यों नहीं विदा कर दिया? चैन की साँस तो लेती? ऐसी मुँहजली, उद्दण्ड, अलक्ष्मी को रखने की क्या जरूरत थी?'' तीखी आवाज में कम्पन आ जाता।
''अब क्या! शुरू कर दे आँसू टपकाना। जो जी में आये कह लिया और मुश्किल देखी तो आँसू बहाकर जीत गयी। औरत होना बुरी बात नहीं है।''
पंखा नीचे पटककर मोहन खाट से उतर जाता। छोटे भाई-बहनों के हाथ-पैर कुचलते हुए किसी तरह दरवाजे की ओर बढ़ता।
''कहाँ चल दिया?'' आर्त्तस्वर में तरुलता पूछतीं।
''डरो नहीं? श्मशान घाट की ओर नहीं,'' मोहन हँस पड़ता ''निश्चिन्त रहो, घूम-फिरकर इसी खटाल में लौट आऊँगा। जरा खुली हवा में घूमकर आता हूँ।''
''तभी तो कहती हूँ 'नवाब','' फिर जयन्ती की आवाज़ सुनाई पड़ती। ''इतने लोग इस कमरे में सो रहे हैं, इन्हीं को बीच रात में हवा खाने की जरूरत पड़ गयी।''
''जयी, फिर?'' तरुलता अचानक हाथ बढ़ाकर जयन्ती की चोटी खींच बैठती। शायद अधिक कायर लोग ही कभी-कभी निर्भीक होकर अचानक एक दुस्साहस का काम कर बैठते हैं। तभी तीक्ष्ण स्वर में बोलतीं, ''तब से बकी जा रही है, तुझे मौत क्यों नहीं आती, चुड़ैल?''
अँधेरे में जयन्ती हँसती, ''उफ, मेंरी चोटी छोड़ दो। मेंरे मरने से तुम्हें कुछ सुख मिलेगा क्या? कमर के दर्द से तो हिल भी नहीं पाती। नहीं तो मरकर एक बार देखने को जी करता है।''
''इतना आसान नहीं है,'' मोहन का तीक्ष्ण स्वर अँधेरे को चीरते हुए वार करता जयन्ती पर। ''मरना इतना आसान होता तो फिर क्या चिन्ता थी? इस घर में किसी भी जीने का हक नहीं, समझी? तुझे नहीं, मुझे नहीं, माँ को नहीं, शोभन, मुन्नी, किसी को भी नहीं। फिर भी जीना है। जीना नहीं जिन्दा रहना है। इस धरती के अन्न का भागीदार बनकर जिन्दा रहना है। दिन-रात भाग्य को कोसकर सर पीटकर भी जिन्दा रहना है। लानत है।''
फटी चप्पल में से आवाज निकलती और फिर धीमी होती जाती। मोहन बाहर चला जाता।
तरुलता हड़बड़ाकर उठतीं और दर्द से कराह उठतीं और फिर बेटी पर ही बरस पड़ती, ''कुलक्षणी कहीं की! तेरे ही कारण किसी दिन मेंरा बेटा आत्मघाती हो जाएगा।"
''आत्मघाती होना इतना आसान नहीं है माँ, सो जाओ चुपचाप।''
''तू तो कहेगी ही, माँ का दिल थोड़े ही है।'' निराश भाव से कहतीं, ''पता नहीं इतनी रात को किसलिए निकल गया...''
''क्यों सोचकर परेशान होती हो माँ, दो सिगरेट फूँककर अभी वापस आ जाएगा, देख लेना।''
बेटी की भविष्यवाणी उसे आश्वस्त नहीं कर पाती। पहले थोड़ा भुनभुनाती और फिर रोने लग जातीं तरुलता। मगर जयन्ती की भविष्यवाणी भी झूठी निकली। उस रात मोहन वापस नहीं आया, अगले दिन सुबह भी नहीं।
रुपये, ढेर सारे रुपये, अनगिनत रुपये चाहिए। पार्क की दीवार फॉदकर अन्दर एक बेंच पर लेटकर आकाश की ओर भावमग्न होकर देख रहा था मोहन। सिर्फ़ पाँच सौ रुपये महीना नहीं, ढेर सारे रुपये। घर की हर ईंट जैसे चीख-चीखकर यही सुना रही है-"रुपये चाहिए, रुपये।''
कितना भद्दा था जयन्ती के बोलने का ढंग? कैसा मैन तिरस्कार छिपा था माँ के चेहरे पर!
आँखों के आगे अब कहाँ है वह काले धब्बों में लिपटी झुकी हुई छत जहाँ से सारी कल्पनाएँ टकराकर लौट जाएँगी। तारों से झिलमिल खुले गगन को देखकर उसकी कल्पना बेलगाम हो गयी। कल्पना उसी ऐश्वर्य की, गिने-चुने रुपये नहीं, बल्कि इतने कि मुट्ठी भर-भरकर बरसा सके। उसी रुपये से मुँह बन्द होगा जयन्ती का। सुबोध-सुशील बने रहेंगे जिद्दी और अडियल सारे छोटे भाई-बहन, चुका सकेगा मातृऋण।...उद्धार कर सकेगा अपनी आत्मा का...खरीद सकेगा उषा को। क्यों नहीं? पैसे से क्या नहीं होता? उषा को भी पैसे से खरीदा जा सकता है। सुनने में कटु पर बात यही सच है। निर्लज्ज सच। सिर्फ धन चाहिए, काफी नहीं, उससे अधिक। काफी से भी अतिरिक्त।
यह धन अगर ऊपर से बरस पड़ता।...ऐसा होता तो मोहन के लिए चमत्कार हो जाता। पर ऊर्ध्यलोकवासी इतने मूर्ख तो नहीं। जब धन के बदले थोड़ा-सा शीतल समीर भेजने से ही तत्काल काम चल जाए तो बुरा ही क्या?
अपनी सारी माँगों, सारे प्रश्नों को भूलकर कुछ समय के लिए शान्त हो गया मोहन।
नींद खुली तो उषा की लाली फैली थी। उठकर इधर-उधर झाँका कि कहीं गिरा-पड़ा मिल जाए कोई धन...कोई कोना नहीं छोड़ा। बेंच के नीचे, झाड़ियों के पीछे कहीं कोई हज़ार का नोट ही मिल जाए।...मिलता तो आस्तिक हो जाता, सोचा था उसने...पर बन नहीं सका। दिन भर लक्ष्यहीन-सा टहलता रहा, पर रात बिताये कहाँ उस खटाल को छोड़कर? रातभर खुले मैदान में सोकर बिना नहाये, बिना खाये उसे बुखार-सा लग रहा था। फिर दफ्तर से कब तक अनुपस्थित रहता छू?
घर तो लौटना ही था। मगर घर में ऐसी अनहोनी उसका इन्तजार कर रही थी, उसे क्या पता था?
बिना रुपयों के मिले और बिना उनके खर्च किये ही जयन्ती का मुँह बन्द हो गया। दिन के उजाले में किवाड़ बन्दकर एक रस्सी को मरोड़-मरोड़कर अपने गले से ऐसा लिपटाया था कि उसका स्वर हमेंशा के लिए रुद्ध हो गया।
घर के दरवाजे पर आकर अपने घर को नहीं पहचान सका मोहन। कहाँ से इतने लोग जुट गये, यह भी हैरत की बात थी।
जीवन में कहीं कोई उत्सव का आयोजन नहीं इसीलिए क्या सन्तुलन बनाये रखने के लिए ही मृत्यु एक आडम्बर बनकर आ रही है उनके जीवन में? पहले पिताजी, फिर जयन्ती।
जयन्ती अब कभी नहीं बोलेगी। यह सोचकर ही बहुत हैरान हो गया मोहन। जयन्ती!
दर्द से परेशान तरुलता में दौड़कर आने की शक्ति नहीं थी इसीलिए बेटे को देखते ही रो पड़ी वहीं से। बेटी के प्रति कभी भी कोई कर्तव्य नहीं निभा पायीं...उसे खाने को नहीं मिला, पहनने को नहीं मिला, माँ के घर में दासवृत्ति करते-करते ही जीवन से ऊब गयी थी वह...इन्हीं बातों को रो-रोकर सुनाने लगीं वह। बोलीं, ''तंग आकर मेरी बेटी ने जान दे दी अपनी।''
तंग आकर? तंग होना जानती थी क्या जयन्ती, अनपढ़, मूर्ख, वाचाल जयन्ती, जो उषा जैसी लड़की के सामने खड़ी होने के लायक़ भी नहीं थी, उसके मन में घृणा इतनी प्रबल कि गले में फन्दा डाल ले!
जयन्ती जैसी लड़की का एक मन भी होता है? एक चिन्ताजगत भी होता है?
तंग आकर मोहन आत्मघाती नहीं हुआ, हुई जयन्ती। शायद जयन्ती के लिए ही सम्भव था। अनपढ़ अशालीन थी इसीलिए शायद भावावेग का प्रदर्शन भी इतना प्रबल था। सभ्य सुशिक्षित मोहन तो तंग आकर अधिक-से-अधिक एक रात पार्क की बेंच पर गुजार सकता था, अपने नैराश्य की कड़वाहट को छिपाने के लिए दिन भर निरुद्देश्य चक्कर काट सकता था-उससे अधिक कुछ नहीं।
वह शिक्षा और सभ्यता ही क्या जो मन की आग को वश में न कर सके।
किराये की मियाद बढ़ते-बढ़ते शायद एक दिन शैतान के हाथों ही आत्मा बिक जाएगी...मगर इसके लिए आत्महत्या करना?
छिः! जैसे किसी सस्ते नाटक का फीका पटाक्षेप!!
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i