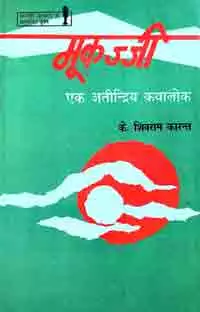|
जीवनी/आत्मकथा >> पगले मन के दस चेहरे पगले मन के दस चेहरेशिवराम कारंत
|
213 पाठक हैं |
|||||||
डॉ कारंत की यह आत्मकथा एक प्रकाश-स्तम्भ की तरह है। यह संघर्ष करना तो सिखलाती ही है, सफलता का आत्म-विश्वास भी पैदा करती है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दी पाठकों के नाम
भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली के प्रति मैं हार्दिक आभार
व्यक्त करता हूँ कि उसने मेरी आत्म कथा (एक प्रकार की) के हिन्दी में
प्रकाशन की दिशा में पहल की। यह योग संस्थान सवधानीपूर्ण चयन एवं उपयुक्त
मान्यता-पद्धति के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर निपुण लेखकों की खोज करने
और उन्हें राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा
है। समय-समय पर मेरी कुछ पुस्तकों के न्यासों, निजी प्रशंसकों एवं
संस्थाओं द्वारा हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किये जाते रहे हैं, किन्तु मैं
पाता हूँ कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा चुनी गयी पुस्तक ‘मकूज्जी’ ने मुझे सच्ची राष्ट्र व्यापी प्रतिष्ठा दिलायी है।
जो व्यापक प्रचार मुझे उससे प्राप्त हुआ है उसे मैं अपना अहोभाग्य मानता
हूँ। किन्तु इस तथ्य का अर्थ यह तो नहीं है कि वे मेरे लिए अतिरिक्त कष्ठ
उठाएँ। मेरा तात्पर्य यह है कि कि इससे उन्हें यह कैसे लगा कि मेरी
आत्माकथा भी बृहत्तर पाठक-वर्ग को रोचक प्रतीत होगी। बहरहाल, जिस भी योग्य
हो, यह कृति भारतीय ज्ञानपीठ के अतिरिक्त अनुग्रह के कारण हिन्दी पाठकों
के सामने है।
इस पुस्तक का नाम ‘पगले मन के दस चेहरे’ मैंने पाठक को जीवन के अपने क्षेत्रों में अपनी मानसिक साहसिकताओं का आभास देने के लिए तय किया है। अपने सार्वजनिक जीवन की चौथाई शताब्दी (1923-1948) पूर्ण हो जाने पर मैंने अनुभव किया कि कन्नड़ जनता को, जिसके बीच रहकर मैंने इतने लम्बे समय तक संघर्ष किया, अपनी आप बीती कह सुनाऊँ। अनेक लोगों ने मेरी आरम्भिक गति विधियों पर छींटाकशी की थी और मेरे निकट के लोगों तक ने महसूस किया था कि मैं हरफनमौला तो था, मगर किसी भी फन का उस्ताद नहीं। निश्चय ही दक्षता का दावा मेरा किसी भी दिशा में नहीं है।
सबसे पहले तो मैंने यह अन्वेषण करना चाहा कि मुझमें क्या-कुछ करने की क्षमता थी तदुपरान्त मैंने अपनी क्षमता का विस्तार अपने साथियों को जानने एवं उनकी सेवा करने के लिए किया। कन्नड़ में इस आत्मकथा का प्रथम संस्करण 1948 में प्रकाशित हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसका व्यापक स्वागत हुआ।
लगभग 1962 में इसकी सामग्री को अद्यतन करते हुए इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया।
छठे दशक में मैंने अपने अपने अतीत की झलकियाँ विषयानुसार प्रस्तुत करने की एक भिन्न पद्धति अपनायी। मैंने उनके शीर्षक इस प्रकार रखे-‘मैं और मेरा मूल स्थान’, ‘मैं और मेरा साहित्य’, ‘मैं और शिक्षा’ ‘मैं और नाटक’ आदि-आदि।
वे तीन भिन्न-भिन्न जिल्दों में स्मृति पलट शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुई है। तिथी क्रमानुसार आत्मकथा को विस्तार देने का मेरा कोई इरादा न था।
किन्तु कुछ मित्र उसमें भी रूचि रखते थे। अतः अपने जीवन का वर्णन बढ़ाते-बढ़ाते 1983 तक खींच लाने के लिए मैं बाध्य हो गया। सच, जीवन पथ में मेरी यह पर्याप्त लम्बी यात्रा है। यदि हिन्दी पाठक इस प्रकार की पुस्तक पढ़ने की रूचि दिखाएँगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह उनकी हृत्तन्त्री के कुछ तारों को अवश्य छेड़ेगी।
कोई मनुष्य अपने समकालीनों से और चाहता भी क्या है।
इस पुस्तक का नाम ‘पगले मन के दस चेहरे’ मैंने पाठक को जीवन के अपने क्षेत्रों में अपनी मानसिक साहसिकताओं का आभास देने के लिए तय किया है। अपने सार्वजनिक जीवन की चौथाई शताब्दी (1923-1948) पूर्ण हो जाने पर मैंने अनुभव किया कि कन्नड़ जनता को, जिसके बीच रहकर मैंने इतने लम्बे समय तक संघर्ष किया, अपनी आप बीती कह सुनाऊँ। अनेक लोगों ने मेरी आरम्भिक गति विधियों पर छींटाकशी की थी और मेरे निकट के लोगों तक ने महसूस किया था कि मैं हरफनमौला तो था, मगर किसी भी फन का उस्ताद नहीं। निश्चय ही दक्षता का दावा मेरा किसी भी दिशा में नहीं है।
सबसे पहले तो मैंने यह अन्वेषण करना चाहा कि मुझमें क्या-कुछ करने की क्षमता थी तदुपरान्त मैंने अपनी क्षमता का विस्तार अपने साथियों को जानने एवं उनकी सेवा करने के लिए किया। कन्नड़ में इस आत्मकथा का प्रथम संस्करण 1948 में प्रकाशित हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसका व्यापक स्वागत हुआ।
लगभग 1962 में इसकी सामग्री को अद्यतन करते हुए इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया।
छठे दशक में मैंने अपने अपने अतीत की झलकियाँ विषयानुसार प्रस्तुत करने की एक भिन्न पद्धति अपनायी। मैंने उनके शीर्षक इस प्रकार रखे-‘मैं और मेरा मूल स्थान’, ‘मैं और मेरा साहित्य’, ‘मैं और शिक्षा’ ‘मैं और नाटक’ आदि-आदि।
वे तीन भिन्न-भिन्न जिल्दों में स्मृति पलट शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुई है। तिथी क्रमानुसार आत्मकथा को विस्तार देने का मेरा कोई इरादा न था।
किन्तु कुछ मित्र उसमें भी रूचि रखते थे। अतः अपने जीवन का वर्णन बढ़ाते-बढ़ाते 1983 तक खींच लाने के लिए मैं बाध्य हो गया। सच, जीवन पथ में मेरी यह पर्याप्त लम्बी यात्रा है। यदि हिन्दी पाठक इस प्रकार की पुस्तक पढ़ने की रूचि दिखाएँगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह उनकी हृत्तन्त्री के कुछ तारों को अवश्य छेड़ेगी।
कोई मनुष्य अपने समकालीनों से और चाहता भी क्या है।
प्रस्तावना
क्षमा-याचना की आवश्यकता नहीं
ऐसी एक रचना के लिए प्रस्तावना लिखनी चाहिए
अथवा क्षमा
याचना करनी चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लिखना ही मेरी वृति होने
के कारण मुझे उसके बारे में क्षमा-याचना करने की आवश्यकता नहीं है। जिन
विषयों को मैं जानता हूँ उनके बारे में लिखना मेरी आदत-सी हो गयी है। यह
वह अधिकार है जो एक लेखक अपने आप को देता है। यह बिना किसी प्रत्यक्ष गुरू
के प्राप्त दीक्षा है। विश्व में जीनेवाले किसी भी व्यक्ति का यदि कोई
गुरू न भी हो तो भी वे सारे अनुभव, शिक्षा उसे विश्व से प्राप्त हो जाते
हैं। निसर्ग की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव, व्यक्ति के चैतन्य होकर
जीनेवाला प्रत्येक क्षण, लेखक की मनोवृति को सदा निरूपित करते रहते हैं।
वैसे दूसरे भी उस नियम के बाहर नहीं हैं। जन्म से ही मिलनेवाली यह शिक्षा
उसके जीवन के अन्त में ही समाप्त होती है। इन दोनों के बीच के दीर्घ या
अल्पावधि में, वह अपने लेखन की दीक्षा प्राप्त करता है। वैसे वह किसी एक
व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार भले ही न करे, पर सैकड़ों
व्यक्ति, सैकड़ों जीव और असंख्य घटनाएँ उसके लिए गुरु ही होते हैं। इनसे
परिपुष्ट, स्फूर्ति वाला एक लेखक अनेक कृतियों को जन्म दे सकता है। इनमें
अगर सौ खराब हों तो कुछ अच्छे भी होंगी। अच्छे बुरे के बीच की भी कुछ
कृतियाँ हो सकती हैं। मूलतः लेखक अथवा कोई भी कलाकार अपनी आत्मतृप्ति के
लिए अपने मन के भाव को व्यक्त करता है। वह मूकजीवी नहीं होता है। दूसरे
मानव भी मूक नहीं होते हैं। अतः उसकी कृतियाँ उसके समान ही अनुभव वाले
दूसरे व्यक्तियों और अनुभवापेक्षियों के लिए उपयोगी हो सकती हैं और
पर्याप्त रूप में सन्तोष भी दे सकती हैं। परन्तु कलाकार को पहला सन्तोष और
सबसे बड़ा सन्तोष उसकी कृति के निर्माण के समय ही मिलना चाहिए। लोगों की
पसन्द, आलोचना अथवा प्रशंसा से मिलनेवाला आनन्द तो एक पर्याय मात्र है।
उसी प्रकार निन्दा या उपेक्षा से मिलनेवाला दुख भी एक पर्याय ही उसकी
परवाह मुझे है ही नहीं। मेरा जीवन मेरे अधिकार की वस्तु है। मेरा जीवन
मेरा अपना है। उसका सुख सौन्दर्य, दर्द, पीड़ा और सौन्दर्य का अभाव ये सब
मेरे हैं। दूसरे उसमें भाग लेना चाहें तो अच्छा, उसे स्वीकार करें तो
अच्छा, न भी करें तो अच्छा। मैंने जो जीवन बिताया वह मेरा है, केवल मेरा
है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों को तुच्छ समझता हूँ। इसका यह भी मतलब
नहीं कि उनकी आलोचना के सत्यांश की ओर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके
बिना कोई भी मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। फिर भी जिसने जो जीवन बिताया,
उसे उसके अलावा भला और कौन जान सकता है ? यह लेखन ही मेरे पगले मन के दस
चेहरे हैं। इस लेखन के बारे में यदि मुझे किसी से क्षँमा माँगनी हो तो
मेरे जीवन के साथ मुझे उठाकर, जिस जीवन-प्रवाह ने संचार किया उससे माँगनी
चाहिए।
एक अर्थ में मैंने अपने जीवन को अपना कहा है। परन्तु विस्तृत अर्थ में, सत्य देखनें चलें तो वह जीवन दूसरों का साथ घुला-मिला है। मैं समाज के जीवन का एक अंश हूँ न ! उसके सुख-दुःख मेरे हैं न ! मेरा सदा का जीवन समाज का हिस्सा है न !
एक अर्थ में मैंने अपने जीवन को अपना कहा है। परन्तु विस्तृत अर्थ में, सत्य देखनें चलें तो वह जीवन दूसरों का साथ घुला-मिला है। मैं समाज के जीवन का एक अंश हूँ न ! उसके सुख-दुःख मेरे हैं न ! मेरा सदा का जीवन समाज का हिस्सा है न !
सम्पूर्णता की बात नहीं
यह एक सम्पूर्ण आत्मकथा नहीं है। सम्पूर्ण तो
मैं भी नहीं
हूँ। सम्पूर्णता का एक अंश भी नहीं बन पाया हूँ। यह मैं जानता हूँ कि यह
विश्व ही सम्पूर्णता के लिए संघर्षरत है अतः सवर्ज्ञ पद को मैं वहन नहीं
कर सकता। दूसरे अर्थ में भी यह परिपूर्ण नहीं है। मैं अब ढलती उमर पर पाँव
रख चुका हूँ। अतः अपने जीवन के जिस समय यह वर्णन कर रहा हूँ, वहाँ तक का
ही वह चित्र उपस्थित कर सकता हूँ। पूरे जीवन का चित्र नहीं दिखा सकता।
मुझे सौ वर्ष जीने की इच्छा नहीं है। पर यह इच्छा अवश्य है कि दूसरों पर
शारीरिक रूप से एक भार बन कर न जीऊँ। यदि बाद में जीवित रहा तो शायद मेरी
स्थित वैसी ही हो सकती है जैसी ताण्डव मुनि के बेटे उसे काँवर से उठाकर
भटकते थे। दूसरों की सहायता न करनेवाले व्यक्ति को दूसरों पर बोझ नहीं
बनना चाहिए न !
लिखने की इच्छा
खैर, कोई भी मुझसे यह पूछ सकता है कि ऐसी
आत्मकथा लिखने का
पागलपन क्यों ? मैं पहले ही यह स्वीकार कर चुका हूँ कि मेरा मन पगला है,
तो यह प्रश्न ही व्यर्थ हो उठता है। कुछ वर्ष पहले मेरे मित्र नेगलूर
रंगनाथराय ने मुझसे कहा था, मैं जागीरदार की जीवनी लिख रहा हूँ, मैं आपसे
उसकी भूमिका लिखवाना चाहता हूँ वे दोनों ही मित्र हैं। ‘अच्छी
बात
है’ कहकर मैंने भूमिका के चार शब्द लिख दिये। बाद में उन्होंने
कहा,
‘‘मैं आपकी भी जीवनी लिखना चाहता हूँ। उसके लिये आप
सामग्री
दे सकेंगे ?’’ तब मैंने हँसकर कहा,
‘‘दूसरों की
लेखनी से हत्या कराने की इच्छा मुझे नहीं है। मैं अपनी हत्या अपने आप ही
कर लूँगा।’’ यह बात हुए कुछ ही साल हुए। मेरे कई
मित्रों ने
ही नहीं, पत्नी लीला ने भी मेरी जीवनी के बारे में लिखा है। मेरा एक गहरा
विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति की जीवनी बढ़िया लिखनी है तो लिखनेवाले का
और उस व्यक्ति का निकट का परिचय अवश्य होना चाहिए तभी वह सजीव बन पड़ेगी।
केवल पुरानी खोजों से लिखा जानेवाला जीवन-चरित्र एक व्यक्ति का केटेलॉग
मात्र हो सकता है। वह हमें तभी सरस लगा सकता है जबकि उसमें लेखक की
मनोवृति प्रतिबिम्बित हो। तभी सही मायनों में लेखक की आत्मकथा होगी।
नेगलूर के मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित करने के बाद से आत्मकथा लिखने की इच्छा हुई। एक दो मित्रों ने कहा, ‘‘लिख क्यों नहीं डालते ? तब एकदम मरने की इच्छा नहीं है’’ कहकर मैंने मजाक भी उड़ाया था। कुछ वर्ष पूर्व मित्र राजरत्नम् ने ‘दस वर्ष’ नाम से अपनी आत्मकथा लिखकर जनता को प्रदान की। ‘दस वर्ष’ में तो एक ‘निकली जुबली’ भी नहीं होती। भला मैं उतना छोटा हूँ क्यों लिखूँ ? यह सोचकर मैं पच्चीस वर्ष पूरे होने की प्रतीक्षा करता रहा। ये पच्चीस वर्ष मेरे पूरे जीवन के पच्चीस वर्ष जबसे मैं ‘मैं’ बना और अपने को समझने लगा तब के पच्चीस वर्ष हैं।
बिना दूसरे की सहायता के समाज के प्रवाह में मैंने जो पच्चीस वर्ष काटे उनकी प्रतीक्षा करता रहा। इस लेखन का पहला संस्करण समाप्त होने के पन्द्रह वर्ष बाद दूसरा संस्करण निकला। अब तक तीसरा है।
नेगलूर के मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित करने के बाद से आत्मकथा लिखने की इच्छा हुई। एक दो मित्रों ने कहा, ‘‘लिख क्यों नहीं डालते ? तब एकदम मरने की इच्छा नहीं है’’ कहकर मैंने मजाक भी उड़ाया था। कुछ वर्ष पूर्व मित्र राजरत्नम् ने ‘दस वर्ष’ नाम से अपनी आत्मकथा लिखकर जनता को प्रदान की। ‘दस वर्ष’ में तो एक ‘निकली जुबली’ भी नहीं होती। भला मैं उतना छोटा हूँ क्यों लिखूँ ? यह सोचकर मैं पच्चीस वर्ष पूरे होने की प्रतीक्षा करता रहा। ये पच्चीस वर्ष मेरे पूरे जीवन के पच्चीस वर्ष जबसे मैं ‘मैं’ बना और अपने को समझने लगा तब के पच्चीस वर्ष हैं।
बिना दूसरे की सहायता के समाज के प्रवाह में मैंने जो पच्चीस वर्ष काटे उनकी प्रतीक्षा करता रहा। इस लेखन का पहला संस्करण समाप्त होने के पन्द्रह वर्ष बाद दूसरा संस्करण निकला। अब तक तीसरा है।
इतना जीना काफी नहीं ?
सन् 1921 में कॉलेज से मुक्त हुआ। तब मैंने
केवल ब्रिटिश
सरकार से ही सम्बन्ध नहीं छोड़ा, कहना चाहिए कि अपरोक्ष रूप में मुझसे
कहने और पूछनेवाले सभी से सम्बन्ध तोड़ लिये। मेरा ऐसा ‘बे
लगाम’ जीवन रहा है। पर उस पर जो बाहरी नियन्त्रण था वह
‘बे’ नहीं था। अब वह जमाना पूरी तरह बीत गया है। 1983
चल रहा
है। इस बारे में मेरे मन में एक और ही बात उठ रही है-भारतीयों को यदि
जीवन-चरित्र लिखना हो तो उसे मेरी आयु से पहले ही लिख डालना चाहिए।
भारतीयों की औसत आयु करीब 23 वर्ष है तो उनके पास उस पर लिखने को ही भला
है क्या ? अब मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं उससे तिगुना जी चुका हूँ और
चौगुने तक जी सकता हूँ कौन जाने ! मेरे माता पिता, दादी सभी जिद करके इतने
समय तक जीये थे। मुझे क्यों नहीं इतना जीना चाहिए ?
आत्मकथाओं का अभाव
कन्नड़ में जीवनियों का अत्यन्त अभाव है।
श्री. डी. वी.
गुण्डप्पा ने गोखले की जीवनी लिखकर एक मार्गदर्शन किया। उन्होंने श्री
गोखले के राजनीतिक जीवन का गहरा अध्ययन किया था। वैसे उच्चकोटि के गुण और
संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कन्नड़ में जीवनियों का सर्वथा अभाव है।
तब आत्मकथा की बात कहाँ से उठी ? विदेशी साहित्य में ऐसी सैकड़ों पुस्तकें
हैं। जिन्होंने ऊँचा जीवन बिताया हो यदि वे स्वयं ही लिखें तो उनकी
आत्मकथा सशक्त होगी। विदेशों में अनेक वैज्ञानिकों, राजनयिकों, और विविध
क्षेत्रों में साहस दिखानेवालों ने रोचक आत्मकथाएँ लिखी है। हमारे यहाँ भी
गाँधी की आत्मकथा, जवाहार लाल की आत्मकथा मिलती है। उनका व्यक्तित्व महान
होने से उन पुस्तकों को अन्तरराष्टीय ख्याति भी मिली है। उन्हें पढ़कर
मैंने भी आनन्द का अनुभव किया है, और कुछ सीखा भी है। विदेशियों की
आत्मकथाएँ मैंने अधिक नहीं पढ़ी हैं। लेकिन जिन दो चार को पढ़ा है उनसे
मुझे बहुत सन्तोष मिला है। इनमें एच. जी. वेल्स की आत्मकथा, एडमिरल बर्डन
की आत्मकथा ने मुझे विशेष रूप से प्राभावित किया है। ऐसी रचनाएँ पढ़कर यह
महसूस होने पर भी कि मुझ जैसे व्यक्ति को ऐसे काम में हाथ नहीं डालना
चाहिए, मन में यह आशा अवश्य हुई कि एक बृहद् आत्मकथा के बदले एक छोटी-सी
आत्मकथा क्यों न लिखी जाए।। मैंने अपने उपन्यासों में बीसियों अमान
व्यक्तियों के जीवन को चित्रित किया है। फिर भला अपनी कलम का शिकार मैं
स्वयं क्यों न बनूँ। यह शरारत, साहस विनोद इस रचना में प्रतिबिम्बित होना
चाहिए। इस भूमिका को पहले लिखकर वास्तव में कहना चाहिए कि लिखवाया अर्थात्
मुँह से बोलकर लिखवाया है। ऐसा यह मेरा पहला प्रयास है। अब आगे इसके कुछ
और भी अध्याय लिखने हैं।
हम स्वयं नहीं देख सकते
इसका नाम मैंने ‘पगले मन के दस
चेहरे’ रखा है।
अपने मन के पागलपन का बोध हर समय नहीं होता है। दूसरे का पागलपन जितनी
सरलता से दिखाई देता है क्या उतनी ही सरलता से हमें अपने पागलपन दीखता है
? उसे देखने की इच्छा तो मुझे है। जिस प्रकार मैं अपने समाज से दूर खड़े
होकर उसे देखकर, समझने का प्रयत्न करता हूँ उसी प्रकार मैं अपने जीवन को
देखकर समझना चाहता हूँ। यदि वह आशा पूरी हो तो यह एक अपूर्व सन्तोष की बात
है। यदि इसे साध्य करना है तो मुझे अपने भीतर का अहंकार छोड़ना होगा।
दूसरों के सामने झूठी सज्जनता दिखाने का दुराशा छोड़नी होगी। इसके
अतिरिक्त अपने आपको धोखा देने का भी हमारा एक स्वभाव होता है। जब मनुष्य
अपने आपको सफलतापूर्वक धोखा देना सीख लेता है तभी उसमें दुनियाँ को धोखा
देने की शक्ति आती है। यह भी एक बात है। हम अपनी गहराई को नाप नहीं सकते।
अपना छिछलापन हमें दिखाई नहीं देता । अपने थोड़े गुण अथवा चाहे वे न भी
हों, वे ही हमें बहुत नजर आते हैं।
प्यारा-सा पागलपन
मैं अपने मन को पागल क्यों कहता हूँ ? इसका
कारण यह नहीं
है कि यह पागलपन नहीं चाहता बल्कि उसे मैं पसन्द करता हूँ। ऐसे पागलपन के
कारण अनेक ऐसे साहस करके जिन्हें करना नहीं चाहिए, मुझे अपनी और दुनिया का
पागलपन समझ में आया है। इसके आलावा इसका एक और भी विशेष कारण है। मैं अपना
सारा बचपन अपने दिशाहीन विद्यार्थी जीवन में ही खो बैठा । जब मैंने अपना
सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया तब देशाभिमान ने अपनी ओर आकर्षित किया। मैं
असहयोग आन्दोलन में कूद पड़ा। विष्णु के यदि दस अवतार हैं तो मेरे ध्येय
ने सोलह अवतार लिये। देशप्रेम, स्वदेशी प्रचार, व्यापार, पत्रकारिता
अध्यात्म साधना, कला के विभिन्न रूप फोटोग्राफी, नाटक, नृत्य, चित्रकला,
वास्तुकला, संगीत सिनेमा-इतना ही नहीं समाज- सुधार, ग्रामोद्धार, शिक्षा
के नये नये प्रयोग, उद्योग यह सब मेरे कार्य क्षेत्र रहे। और भी नये-नये
प्रयोग चल ही रहे हैं। कभी मैं एक प्रेस का मालिक भी रहा हूँ। पुस्तक-लेखन
से लेकर संन्यास के जीवन से गुजरकर गृहस्थ भी बना हूँ। केवल अपनी खिड़की
से बाहर झाँकनेवालों को भले ही इन सब परिवर्तनों में कोई परस्पर- सम्बन्ध
न दीखे पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। इस यात्रा में कोई और व्यक्ति यदि मेरे
साथ होता तो उसे पता चलता कि यह सब यात्रा के अलग-अलग पड़ाव हैं। वैसे भला
मेरे साथ मित्र ही कितने थे ? उनमें से मुझे केवल एक व्यक्ति की याद आती
है ? उस व्यक्ति का चित्रण मैंने अपने चिक्क-दोड्डवरू (बड़े भाई) में किया
है।
परन्तु मेरी प्रवृति उनमें एक दम भिन्न है। अतः वे मुझे आसानी से समझ नहीं सकते। वे इतने तेज भी नहीं हैं। केवल अभिमग्न और स्नेह से हमारी मित्रता चली आ रही है। तो यह निश्चित हुआ कि अपनी आत्मकथा लिखने को मैं अकेला ही उपयुक्त हूँ।
परन्तु मेरी प्रवृति उनमें एक दम भिन्न है। अतः वे मुझे आसानी से समझ नहीं सकते। वे इतने तेज भी नहीं हैं। केवल अभिमग्न और स्नेह से हमारी मित्रता चली आ रही है। तो यह निश्चित हुआ कि अपनी आत्मकथा लिखने को मैं अकेला ही उपयुक्त हूँ।
नवीनता में आसक्ति
यहाँ आत्मकथा के केवल कुछ ही रूप आप देख सकते
हैं। मैंने
भी कुछ ही देखे हैं। इस आठ दशक की अवधि में मेरा जीवन और मन इतनी सारी
दिशाओं में बहा है। और इससे आगे की यात्रा कैसी होगी इउसकी कल्पना में
कैसे कह सकता हूँ ? यदि मेरा उदेश्य इतना निश्चित होता तो मेरे इस तरह
जीने की आवश्यकता ही नहीं होती। तब क्या जीवन का उदेश्य पूरा हो जाता ?
विश्व का ‘कल’ जितना विचित्र प्रश्न है, हम सब लोगों
के
‘कल’ का रहस्य भी उतना ही गूढ़ और विचित्र है। ऐसे कल
के लिए
नवीनता है। उत्साह है। यह मेरी इच्छा है कि मेरे चारों ओर की दुनिया चिर
नवीनता के लिए अवकाश देती रहे। मन को सदा ताजा होना चाहिए, तेज होना
चाहिए, साँप की जीभ के समान आगे का रास्ता खोजते रहना चाहिए। परिचित
रास्ते पर अन्धे के समान चलने से क्या लाभ ? तात्पर्य यह है कि तब से लेकर
अब तक मेरे भीतर जितने परिवर्तन आये हैं। उतने ही परिवर्तन आज से कल में
भी आ सकते हैं। परन्तु कईयों के लिए वह अनिश्चित जीवन भयंकर दीख सकता है।
यश की गाथा नहीं
यह आत्मा मेरे जीवन के विविध साहसों के यश की कहानी दीखने की जगह हार की
कहानी के रूप में दीख सकती है। परन्तु मनुष्य को जीवन में अनुभव प्राप्त
करने के लिए सफलताएँ जितनी आवश्यक होती हैं असफलताएँ भी उतनी ही आवश्यक
हैं या उससे भी ज्यादा। क्योंकि तराजू के एक पलड़े में अपना भार और दूसरे
में परिस्थितियों का भार होने पर उसमें वह अपनेवाले भार को हल्का पाता है।
यशार्थी अपने समाज संघर्ष करनेवाले दूसरे प्राणियों के सामने अपना बड़प्पन दिखा सकते हैं। उस बड़प्पन से गर्व पैदा हो सकता है। पर वह व्यक्ति का सही वजन बता नहीं सकता। समाज के प्रवाह के अनुकूल बह जाने, हवा के रुख के मुताबिक छतरी पकड़ने वाले को यश जितना आसानी से मिल सकता है। उतना दूसरों को नहीं। दुनियाँ में चाहे जो भी यश क्यों न हो वह केवल हम पर ही निर्भर नहीं होता है, यह मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। विधि कहिए, भाग्य कहिए, अनुकूल परिस्थिति कहिए या और कुछ, कभी-कभी हमारे प्रयत्न से भी अधिक हमें यश मिल जाता है। कभी-कभी हम जब अत्यन्त परिश्रम करते हैं तो भी वही यश हमें ठोकर मार मजाक करके चला जाता है। पर एक बात सत्य है, पराजित को बार-बार कार्य करने का अवसर मिलता है। विजेता के लिए वह कार्य समाप्त होने के बराबर ही है। जब तक हम कार्य में अशक्ति रखते हैं, उसकी आवश्यकता समझते हैं, उसके सौन्दर्य का अनुभव करते है, तब तक कार्य ही आनन्द होता है। हार से दुनिया का अनुभव करते हैं, उसमें भी एक प्रकार एक प्रकार का आनन्द होता है।व्यक्ति यदि सचेत है तो हार से मिलनेवाला अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। भावी जीवन में वह सहायक होता है। यह सब हारे हुए व्यक्ति के कहने के दर्शन हैं-चाहे ऐसे ही समझा जाय, खैर मेरा दृष्टि कोण तो यही है।
यशार्थी अपने समाज संघर्ष करनेवाले दूसरे प्राणियों के सामने अपना बड़प्पन दिखा सकते हैं। उस बड़प्पन से गर्व पैदा हो सकता है। पर वह व्यक्ति का सही वजन बता नहीं सकता। समाज के प्रवाह के अनुकूल बह जाने, हवा के रुख के मुताबिक छतरी पकड़ने वाले को यश जितना आसानी से मिल सकता है। उतना दूसरों को नहीं। दुनियाँ में चाहे जो भी यश क्यों न हो वह केवल हम पर ही निर्भर नहीं होता है, यह मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। विधि कहिए, भाग्य कहिए, अनुकूल परिस्थिति कहिए या और कुछ, कभी-कभी हमारे प्रयत्न से भी अधिक हमें यश मिल जाता है। कभी-कभी हम जब अत्यन्त परिश्रम करते हैं तो भी वही यश हमें ठोकर मार मजाक करके चला जाता है। पर एक बात सत्य है, पराजित को बार-बार कार्य करने का अवसर मिलता है। विजेता के लिए वह कार्य समाप्त होने के बराबर ही है। जब तक हम कार्य में अशक्ति रखते हैं, उसकी आवश्यकता समझते हैं, उसके सौन्दर्य का अनुभव करते है, तब तक कार्य ही आनन्द होता है। हार से दुनिया का अनुभव करते हैं, उसमें भी एक प्रकार एक प्रकार का आनन्द होता है।व्यक्ति यदि सचेत है तो हार से मिलनेवाला अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। भावी जीवन में वह सहायक होता है। यह सब हारे हुए व्यक्ति के कहने के दर्शन हैं-चाहे ऐसे ही समझा जाय, खैर मेरा दृष्टि कोण तो यही है।
बहुमुखी होना
इस आत्मकथा में विविधा का मुख्य कारण मेरे मन
का बहुमुखी
होना है। मेरी इच्छा यह रही है कि मैं अपने शील को, स्वभाव के, इन्द्रियजन
लालसाओं को, सभी प्रकार की चेतनाओं को विकास के लिए अवकाश दूँ। अपने जीवन
को एक ही ओर मोड़कर एक ही ध्येय की साधना के लिए स्वयं को अर्पित करके
उसके लिए निरन्तर परिश्रम करना कुछ लोगों का स्वभाव है। ऐसा परिश्रम करते
समय, व्यक्ति कि कुछ शक्तियाँ ज्यादा विकसित होती हैं, पर साथ ही अनेक
शक्तियाँ मन्द पड़ जाती हैं। सदा लकड़ी काटनेवाले की बाँह, छाती और पीठ की
माँसपेशियाँ अधिक पुष्टि हो जाती हैं, पर पाँव की माँसपेशियाँ क्षीण रह
जाती हैं। यह मैं पसन्द नहीं करता। विकासवादियों का कहना है कि मनुष्य का
विकास बन्दर से हुआ। मैं अपने मन के स्वभाव से परिचित हूँ। उसकी बहुमुखी
चेष्टाओं को देखकर इस वाद को स्वीकार करने के सिवा मेरे लिए और कोई चारा
है ?
लम्बी प्रस्तावना लिखने के बदले, आत्मकथा को ही आगे बढ़ाते हुए, अपनी पूर्व स्मृतियों को पिराने का प्रयत्न करता हूँ। इसके सारे अंश सबको भले ही पसन्द न आएँ, पर कुछ अंश तो कुछ लोगों को अवश्य पसन्द आ सकते हैं। एक बात और है, चाहे किसी को पसन्द आएँ न आएँ, पर मुझे पसन्द हैं, अतः उनके लिखने में मुझे क्यों डरना चाहिए ?
लम्बी प्रस्तावना लिखने के बदले, आत्मकथा को ही आगे बढ़ाते हुए, अपनी पूर्व स्मृतियों को पिराने का प्रयत्न करता हूँ। इसके सारे अंश सबको भले ही पसन्द न आएँ, पर कुछ अंश तो कुछ लोगों को अवश्य पसन्द आ सकते हैं। एक बात और है, चाहे किसी को पसन्द आएँ न आएँ, पर मुझे पसन्द हैं, अतः उनके लिखने में मुझे क्यों डरना चाहिए ?
अण्डे के भीतर
कूपमण्डूक
हमारा गाँव समुद्र के किनारे बसा है। दक्षिण
कन्नड़ के
उत्तर में ‘कोट’ नाम का एक ग्राम समुदाय है। हमारे
बुजुर्गों
ने तो उस ‘कोट’ को कभी एक गाँव नहीं समझा। आज भी
बूढ़े लोग
उसे ‘कोट जगत्त’ ही कहते हैं। भला कितना बड़ा रहा
होगा मेरे
उन लोगों का वह जगत ! ‘कोट’ कोट नहीं, वह एक
‘कूट’ है, चौदह गाँवों का एक समुदाय। वहाँ का एक
मुख्य समुदाय
ब्राह्मणों का है जिसे ‘कूट’ ब्राह्मण कहते हैं।
हमारा इतिहास
बहुत छोटा है। प्रसिद्ध पुराण सह्याद्रिखण्ड में उसका वर्णन भी है। हमारे
लोग समुद्र के तट पर या गाँव के किसी तालाब में खड़े होकर
‘संकल्प’ करते समय, ‘गोदावरी-तीरे कहा करते
हैं।
साथ-साथ परशुराम क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रान्त के लोगों के उद्धार के
लिए ही वनवासियों के राजा मयूर वर्मा ने अहिच्छत्र से कुछ ब्राह्मण
परिवारों को लाकर यह प्रान्त बसाया था। उन्हीं से हम उच्च ब्राह्मणों का
विकास हुआ। पहले आए हमारे पूर्वजों ने यहाँ के ब्राह्मणों से मिलकर अपने
परिवारों की वृद्धि की फिर भी उनका दृण विश्वास है कि कोट ब्राह्मणों के
समान शुद्ध ब्राह्मण और नहीं है। मैं अपने मामा के साथ सन् 1922 में काशी
गया था। उन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों को देख अपना निर्णय देते हुए कहा,
ब्राह्मणत्व यदि कहीं बचा है तो वह हमारे कोट में ही है।’ उनके
इस
निर्णय को हाईकोर्ट भी नहीं बदल सकता। मुझे भी अपने बचपन में ऐसा ही लगता
था। मैंने अपने ‘मरळि मण्णिगे’ (माटी की ओर) उपन्यास
में अपने
लोगों की गरीबी, चाल-चलन और आचार-विचार का काफी विस्तार से चित्रण किया
है। उनके स्वभाव में घमण्ड, द्वेष, ओछापन मैंने अपने हल्लिय हत्तु
समस्तरल्लि’ में चित्रित किया है। मेरे समाज के स्थूल परिचय के
लिए
इतना पर्याप्त है।
सौन्दर्य के आगार में
मेरा गाँव बड़ा सुन्दर है। दक्षिण कन्नड़
जिले में एक
दुर्लभ मैदानी इलाका है। उस समतल भूमि में खेती-बाड़ी होती है। बीच-बीच
में नारियल के झुरमुट में घर हैं। वहाँ दो छोटी खारियाँ (Backwaters) बहती
हैं।
पश्चिम में हँगार-कट्टे की ‘कोडी’ से कुन्दापुर की ‘कोडी’ तक बारह मील के क्षेत्र में फैला समुद्र का सुन्दर विस्तार है। एक चट्टान तक नहीं है वहाँ। बचपन से अब तक हमारे घर से दो मील दूर के उस तट पर जब तक मैं घूमता नहीं, उस खारे पानी में कुलाटे नहीं मार लेता और सूखी मछली की गन्ध (अनिवार्य रूप से) सूँघ नहीं लेता, मुझे तृप्ति नहीं मिलती। ऐसा शान्त तट और कहाँ है ! अपने कई दोस्तों को भी वहाँ साथ लेकर गया हूँ। ‘राशि’ ने लिखा है कि मरने से पहले वहाँ जरूर आऊँगा। वी, सीतारामय्या वहाँ पता नहीं कितनी बार खड़े होकर लम्बी-लम्बी साँसे लेकर बेहद खुश हुए थे। वे वहाँ की रेत चुराकर अपने साथ ले भी गये हों तो कोई आश्चर्य नहीं। वहाँ पर सृष्टि के सौन्दर्य का कोई अन्त ही नहीं है। वहाँ के समुद्र की प्रशान्तता और विस्तार मन पर जो प्रभाव डालते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। समीप से देखने पर तो वह चकाचौंध कर डालता है। वह कभी जड़ नहीं। समीप से देखने पर तो वह चकाचौंध कर डालता है। वह कभी जड़ नहीं, निस्तब्ध नहीं है। जरा दूर पर ऊँचाई पर खड़े होकर उसका विशाल दृश्य देखने पर परम सन्तोष मिलता है।
पश्चिम में हँगार-कट्टे की ‘कोडी’ से कुन्दापुर की ‘कोडी’ तक बारह मील के क्षेत्र में फैला समुद्र का सुन्दर विस्तार है। एक चट्टान तक नहीं है वहाँ। बचपन से अब तक हमारे घर से दो मील दूर के उस तट पर जब तक मैं घूमता नहीं, उस खारे पानी में कुलाटे नहीं मार लेता और सूखी मछली की गन्ध (अनिवार्य रूप से) सूँघ नहीं लेता, मुझे तृप्ति नहीं मिलती। ऐसा शान्त तट और कहाँ है ! अपने कई दोस्तों को भी वहाँ साथ लेकर गया हूँ। ‘राशि’ ने लिखा है कि मरने से पहले वहाँ जरूर आऊँगा। वी, सीतारामय्या वहाँ पता नहीं कितनी बार खड़े होकर लम्बी-लम्बी साँसे लेकर बेहद खुश हुए थे। वे वहाँ की रेत चुराकर अपने साथ ले भी गये हों तो कोई आश्चर्य नहीं। वहाँ पर सृष्टि के सौन्दर्य का कोई अन्त ही नहीं है। वहाँ के समुद्र की प्रशान्तता और विस्तार मन पर जो प्रभाव डालते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। समीप से देखने पर तो वह चकाचौंध कर डालता है। वह कभी जड़ नहीं। समीप से देखने पर तो वह चकाचौंध कर डालता है। वह कभी जड़ नहीं, निस्तब्ध नहीं है। जरा दूर पर ऊँचाई पर खड़े होकर उसका विशाल दृश्य देखने पर परम सन्तोष मिलता है।
कमल के साथ कीचड़
हमारे गाँव में स्नान के लिए, छोटे बड़े
तालाब हैं। रेतीली
धरती को गहरा खोदकर चारों ओर पत्थर बाँधकर पुराने लोगों ने तालाब बनाये
थे। अब सीढ़ियाँ ढीली पड़ चली हैं। पत्थर टेढे-मेढ़े हो जाने से उनके नीचे
साँपों और मेंढकों के लिए बिल बन गये हैं। मेरी एक बुआ ऐसे ही एक तालाब के
किनारे साँप के काटने से मर गयी थी। अब भी वह चित्र मेरे मन पर से मिटा
नहीं। तब मैं कोई चार-पाँच का रहा हूँगा। फिर भी हम लोगों का नित्य स्नान
वहीं होता था। हमारे घर के बहुत समीपवाले तालाब का नाम ‘वरूण
तीर्थ’ है। उस पवित्रोदक में असंख्य भैंसें और भैंसे आनन्द लेते
हैं। मैंने भी गले तक गर्मी में डूबकर गर्मी का शमन करने का प्रयास किया
है। वहाँ के कमलों और कुमुदनियों को देख-देखकर मन ही मन आह्लदित हुआ हूँ।
उस तालाब के हर एक किनारे पर अलग-अलग जाति के लोग स्नान किया करते थे। अब
समतावाद आ गया, जाति-भेद चला गया है। सभी जहाँ जी चाहे स्नान करतें हैं।
तालाब को स्वच्छ रखने को भले न सही, उसे गन्दा करने का सभी ने समान अधिकार
पा लिया है।
हमारे तालाब के पानी का रंग सभी की पसन्द का है। सदा हरे रंग की काई से भरा रहता है। जब भी उस तालाब को देखता हूँ, अपने लोगों की उदासीनता देखकर दुखी होता हूँ।
हमारे तालाब के पानी का रंग सभी की पसन्द का है। सदा हरे रंग की काई से भरा रहता है। जब भी उस तालाब को देखता हूँ, अपने लोगों की उदासीनता देखकर दुखी होता हूँ।
बिना मठ के लोग
हमारे गाँव की मुख्य जाति ब्राह्मण ही है। हम
स्मार्त
ब्राह्मण हैं। यहाँ के लोगों के भाग्य में केवल कौपीन ही बदा है। उनकी
गरीबी का कोई ठिकाना नहीं। आज कल तो गाँव के लोग उडपि के कृष्ण की कृपा से
दूसरे गाँवों में जाकर होटल के व्यापार से खूब पैसा कमाकर गाँव भेज रहे
हैं। तब से अब उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो गया है। पैसे का
घमण्ड भी आ गया है। सट्टेबाजी में भी उत्साह लेने लगे हैं। हमारा ब्राह्मण
वर्ग एक दृष्टि से बड़ा ही विचित्र है। हमारा कोई मठ नहीं है। हमारे लिए
संन्यासियों की झंझट ही नहीं। एक जमाने में हमारे
‘कूट’ में
ही हमारे आचार-विचारों का निर्णय हो जाता था। लोग उडपि की भोजनशाला में
घुसने पर भी वहाँ के संन्यासियों को नमस्कार नहीं करते थे। पहले एक बार
श्रृंगेरी मठ के स्वामीजी आये थे तब उनके पाँव छूने से बचने को गाँव के
पासवाली नदी में नावों में खड़े होकर ही उनका स्वागत किया था। शायद बाद
में स्वामी जी हमारे गाँव आये ही नहीं होंगे। हमारे गाँव में
‘माता’ का एक मन्दिर है। विष्णु की भी मूर्ती है। एक
बड़ा-सा
शिवालय भी है। हम लोग समान रूप से उन सबकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे कुल
देवता लक्ष्मी-नरसिंह है। लक्षमी की कृपा भले ही हमारे गाँववालों पर अधिक
नहीं रही, पर नरसिंह से क्रोध तो पर्याप्त मिला है। मुझमें जो क्रोध है,
उसका कारण शायद वही नरसिंह रहा होगा जिसे मैं गाँव में ही छोड़ आया हूँ।
मेरे पूर्वज
सुना है कि हमारे पूर्वजों ने भी पहले गरीबी
देखी थी। मेरे
जन्म के समय परिस्थिति में थोड़ा सुधार हो चुका था। एक बड़े से घर में
मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता शेष कारन्त आठ आने मासिक वेतन पर अध्यापन
कार्य किया करते थे। उन्हें अपने पिता से केवल तीन रुपये लगान की भूमि
विरासत में मिली थी। मेरे पैदा होने से पहले मेरे दादा चल बसे थे। उनकी
स्थिति जरा अच्छी थी, परन्तु नागार्जुन के समान, उनमें रसायन विद्या का
बड़ा पागलपन था। सारे लोहे को गलाकर सोना बनाने के चक्कर में सारी
सम्पत्ति गँवा बैठे थे। मेरे पिता ने कुछ धनी मित्रों से कपड़े का व्यापार
आरम्भ किया, आगे-उसी से फूले फले।
हमारा घर मुख्य रास्ते पर था। वहीं मेरा जन्म हुआ। मुझसे पहले चार भाईयों का जन्म हो चुका था। उनमें से एक का बचपन में ही निधन हो चुका था। मेरे बाद में चार भाई और तीन बहनें पैदा हुए। घर में सबसे बड़ी दादी ही थीं। उनका नाम ही था महालक्ष्मी। उनके बाद पिताजी और माँ महालक्ष्मी देवी थे। माँ और दादी बड़े कष्ट में पली थीं। उनका जीवन अपार श्रद्धा और भक्ति से भरा था। तालाब पर स्नान को जाते समय हम कभी शरारत से मेढकों को पत्थर मारते तो वो कहतीं ‘मेंढक ब्राह्मण होता है उसे मारना नहीं चाहिए।’ यदि किसी भी प्राणी को हम सताते है तो हमें उसका दण्ड मिलता था और फिर दादी, माँ दोनों हमारी शरारत, हिंसा और पाप कृत्यों के लिए अपना-अपना जप आधा घण्टा और बढ़ा देती थीं। हमारे लिए भगवान से क्षमा भी माँगती थीं।
हमारा घर मुख्य रास्ते पर था। वहीं मेरा जन्म हुआ। मुझसे पहले चार भाईयों का जन्म हो चुका था। उनमें से एक का बचपन में ही निधन हो चुका था। मेरे बाद में चार भाई और तीन बहनें पैदा हुए। घर में सबसे बड़ी दादी ही थीं। उनका नाम ही था महालक्ष्मी। उनके बाद पिताजी और माँ महालक्ष्मी देवी थे। माँ और दादी बड़े कष्ट में पली थीं। उनका जीवन अपार श्रद्धा और भक्ति से भरा था। तालाब पर स्नान को जाते समय हम कभी शरारत से मेढकों को पत्थर मारते तो वो कहतीं ‘मेंढक ब्राह्मण होता है उसे मारना नहीं चाहिए।’ यदि किसी भी प्राणी को हम सताते है तो हमें उसका दण्ड मिलता था और फिर दादी, माँ दोनों हमारी शरारत, हिंसा और पाप कृत्यों के लिए अपना-अपना जप आधा घण्टा और बढ़ा देती थीं। हमारे लिए भगवान से क्षमा भी माँगती थीं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i