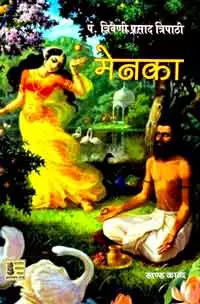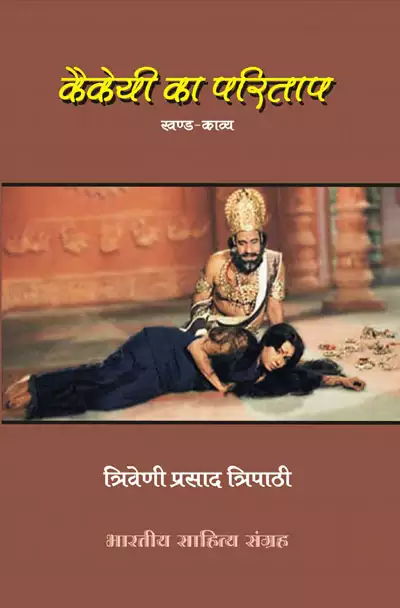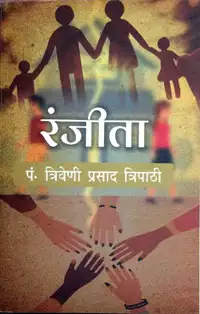|
कविता संग्रह >> अंतिम रात्रि अंतिम रात्रित्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी
|
|
||||||
मराठी कहानी आखरी रात्र का हिन्दी काव्यानुवाद
आमुख
सुधी वृन्द,
सन् 1980 की बात है, उन दिनों 'धर्मयुग' हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, अपने समय की साहित्यिक पत्रिकाओं में अग्रणी हुआ करती थी, और मैं, उस पत्रिका का नियमित पाठक था। 1980 के अगस्त 31 के अंक में, मुझे एक कहानी पढ़ने को मिली, जो 'अंतिम रात्रि' शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। यह कहानी मराठी के प्रसिद्ध कथाकार स्वर्गीय डॉ० विद्याधर पुण्डलीक की मराठी कहानी 'आखरी रात्र' का अनुवाद थी। जिसे मुंबई विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डॉ० चन्द्रकांत महादेव वांदिवडेकर जी ने उपर्युक्त शीर्षक से अनुवाद किया था और धर्मयुग के 31 अगस्त 1980 और 7 सितम्बर 1980 के अंक में प्रकाशित हुई थी। कहानी पढ़कर मेरे भीतर पता नहीं कैसी सुगबुगाहट सी होने लगी कि, मैं इस कहानी को इसी विषय वस्तु के साथ दूसरे किस सांचे में ढाल सकता हूं। चूंकि मुझे छुटपुट कविताएं लिखने का शौक है, मेरे भीतर से किसी ने कहा 'क्यों नहीं इसे पद्य-रूपांतर करके साहित्य-प्रेमियों के समक्ष लाते हो।' सचमुच ही इस प्रेरणा से मुझे खुशी तो हुई पर, यह डर भी घर कर गया कि, इतने महान लेखक की महान कहानी, जो दूसरे एक महान साहित्यकार द्वारा अनूदित की गई है, उसका पद्यानुवाद मैं यानी एक ऐसा व्यक्ति, जिसके पास न तो विद्या है और न ही शब्दों का भंडार कैसे कर सकूँगा ? कितने ही दिन इसी ऊहापोह की अवस्था में रहा, पर न जाने कौन मुझे आगे ठेल रहा था कि मैं यह कार्य शुरू करूं। अंतत: मैंने इस कथा का पद्यानुवाद शुरू किया और मुझमें जितनी क्षमता थी उसका भरपूर उपयोग करके इस कहानी को काव्य रूप में परिणत किया। अवश्य इस कार्य में कुछ पद मुझे अपनी तरफ से जोड़ने पड़े, क्योंकि जब एक पान का संवाद शुरू होता है तो उसके पहले की पृष्ठभूमि तैयार करनी पडती है, जिसे मैंने, इच्छा न होते हुए भी किया क्योंकि काव्य को सरल भाव से समझाने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो गया था। मेरी समय मुताबिक काव्य तो मैंने लिख डाला, लेकिन पुलिस विभाग की दौड़धूप भरी जिंदगी की वजह से इसे बक्से में ही रख देना पड़ा।
20 जन 2004 में विभाग से अवकाश के बाद फिर से अपने जीवन के बिखरे हुए तत्वों को समेटने की इच्छा हुई और उसी क्रम में उडीसा के कटक शहर में केंद्र हिंदी निदेशालय द्वारा आयोजित एक अहिंदी भाषी नवलेखक शिविर में मेरी मुलाकात मुंबई से आए हुए सज्जन श्री चंद्रशेखर पाटिल से हुई और बातचीत के दौरान यह पता चला कि श्री पाटिल डॉ० बांदिवडेकर जी के विश्वविद्यालय में हिंदी के शिष्य रह चुके हैं। अतः मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे यदि मेरी पाण्डुलिपि डॉ० वांदिवडेकर जी के पास तक पहुंचा देंगे तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। श्री पाटिल ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर पाण्डुलिपि डॉ० बांदिवडेकर जी तक मेरे एक अनुरोध पत्र के साथ पहुंचाया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉ० बांदिवडेकर जी ने पाण्डुलिपि पाकर उसमें कुछ सुधार करके और काव्य की भूमिका लिख कर पाण्डुलिपि मुझे वापस कर दी है। पाण्डुलिपि पाकर मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार उसे पुनः लिपिबद्ध किया। काव्य की कहानी कुछ इस तरह से उभर कर सामने आती है
कल अर्जुन और कर्ण का युद्ध। दोनों ही खेमे रात बीतने की प्रतीक्षा में उत्तेजित। कल का दिन जीवित वीरों के जीवन का, महाकुंभ का दिन होगा, जो कर्ण-अर्जुन के युद्ध-संगम में, दर्शन-डुबकी लगा कर अपने जन्म को सफल करेंगे। होना भी चाहिए। ऐसे महावीर पृथ्वी पर बार-बार थोड़े ही जन्म लेते हैं ? यह तो वसुंधरा का सौभाग्य है कि, दोनों वीर श्रेष्ठों ने एक ही समय में जन्म लिया और एक ही भूमि पर अपना रण-कौशल लेकर, आमने सामने खड़े होंगे और विश्व के वीरों को कृतार्थ करेंगे। अवश्य इस युद्ध में उन दो वीरों का व्यक्तिगत कृतित्व नहीं है। उसमें मिला हुआ है सत्य का, असत्य का, धर्म का, अधर्म का, द्वेष और घृणा का, उत्साह-निरुत्साह का अपार भंडार, जिसको लाद कर ही दोनों वीर, कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे हैं। उसके पहले जिस वीर के पल्ले जितना आशीर्वाद, अभिशाप पड़ा है, सभी कुछ सहेज कर दोनों आमने सामने हुए हैं।
होश संभालने के बाद से ही कर्ण अपने जन्म के खोज में लगा रहा, पर उसने जहां भी हाथ से टटोला, शून्य ही मिला और अंत में दुर्योधन जैसा मित्र,
उसकी प्रेरणा और जीवन के प्रति मोह का उत्स लेकर आया, अन्यथा वह अपमान का कड़वा चूंट पी पी कर, असमय ही इस संसार से लुप्त हो गया होता। फिर आज का यह दुर्लभ दिन, शायद विश्व के महारथियों को देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और माता ? वह तो सब कुछ जान कर भी अनजान बनी रही, और अपनी इस शाखा को तने से ही काट कर अलग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा गाई गयी माता की महिमा मानव-जगत की अमूल्य धरोहर है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। पर, पता नहीं क्यों, यह तर्क कर्ण के जीवन के प्रति उदासीन हो गया और कर्ण सुपुत्र ही बना रहा। माता उसके लिए कुमाता हो गयी।
कहते हैं अंधकार में देखकर किसी को पहचान लेना, तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है। शायद जीवन-अंधकार से जूझते जूझते कर्ण में भी वही तीक्ष्ण बुद्धि आ गई थी, इसीलिए तो युद्ध से पहले, अर्जुन का जीवन-दान मांगने आई मां को कर्ण ने सहजता से पहचान लिया, और उसके हृदय ने उसे बता दिया कि यही तुम्हारी मां है, तुम अपना प्राण इसके लिए सहर्ष दान कर दो। शायद इस तरह का दान सृष्टि में पहला और अंतिम था। इसीलिए चिरशत्रु का पक्ष लेती हुई माता को कर्ण ने दुर्व्यवहार नहीं दिखाया और अंत तक उसके पैरों के पास बैठ कर उसे आह्लादित करता रहा। मातृभक्ति का ऐसा उदाहरण शायद ही विश्व में कहीं मिले।
माता अपने एक पुत्र की जय कामना के साथ, दूसरे पुत्र के पास से वापस आ गई है। कल के बाद इस दूसरे पुत्र से माता की मुलाकात नहीं होगी। परन्तु यह कालजयीपुत्र, रणजयी भले न हो सके, पर कीर्तिजयी होने से, उसे कौन रोक सकता है? शायद इस सृष्टि के रहने तक।
मैं गुरुतुल्य डॉ. चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर जी की प्रशंसा के उपयुक्त शब्द नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जिस सहृदयता के साथ इस काव्य की प्रस्तावना लिखी है और काव्य के मर्म को जिस विस्तार से वर्णन किया है उसके कारण इस काव्य की गरिमा बढ़ सी गयी है। निश्चय ही उनके इस कृत्य से उनके बड़ेपन का परिचय मिलता है अन्यथा कटक से सुदूर पुणे नगरी में व्यस्त रहने वाले साहित्यकार के पास मुझ जैसे अकिंचन के लिए समय कहां? इसलिए उनकी इस उदारता के लिए मैं हृदय से आभारी हूं और इस कथा के मूल सर्जक स्व० डॉ० विद्याधर पुण्डलीक जी के विषय में मेरा कुछ कहना अतिशयोक्ति ही होगा, कारण उन्होंने ही इस सांस्कृतिक घटना को मौलिकता के अलंकार से सज्जित कर साहित्य को समृद्ध किया, नहीं तो मां सरस्वती के सृष्टि का कोई एक अंश शायद इस सौंदर्य से वंचित रह जाता। अतः उनके प्रति अपनी अटूट भक्तिपूत भावनाओं का अर्घ्य चढ़ाते हुए, उनकी वंदना करता हूँ।
अंत में मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि इस काव्य का जो भी सौंदर्य है, इसके मूल कथाकारों को अर्पित है और विद्वज्जनों को जो त्रुटियां परिलक्षित होंगी, उन्हें मैं अंगीकार करता हूं।
गोविन्द ! गोविन्द ! गोविन्द !
- त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी
|
|||||
- प्राक्कथन


 i
i