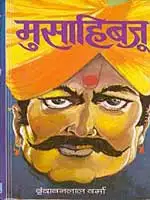|
ऐतिहासिक >> मुसाहिबजू, रामगढ़ की कहानी मुसाहिबजू, रामगढ़ की कहानीवृंदावनलाल वर्मा
|
10 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है मुसाहिबजू के जीवन पर आधारित उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
समर्पण, सेवा और अनुशासन का भाव सैनिक का गुण है। सच्चा सैनिक अपने देश और शासक के लिए अपना सिर दे भी सकता है और किसी का सिर ले भी सकता है। पर यदि शासक के कारण सैनिक के सिर पर ही आ बने तो। इतिहास गवाह हैं, ऐसे समय में
शासकों ने अपने सिर कटा दिए अपने सेवक के मान की खातिर। ऐतिहासिक घटना पर
आधारित वर्माजी का यह प्रसिद्ध उपन्यास ऐसे ही सैनिक और शासक की कहानी है।
परिचय
छोटू नाई दतिया का रहनावाला था। वह जब मुझे मिला, लगभग अस्सी वर्ष का था।
उसने जीवन-भर सिपाहीगिरी की थी। दतिया में बँकाजू कोतवाल के सिपाहियों में
नैकर रहा था। दतिया में अनेक पुरातन प्रथाओं के विध्वंस के साथ इसकी
सिपाहीगिरी खत्म हो गई। इस उपन्यास की घटना उसी की बतलाई हुई है। इस
उपन्यास के दो नाम मुसाहिब दलीपसिंह और रामसिंह धंधेरा सच्चे हैं, शेष
कल्पित हैं। उपन्यास की सब प्रमुख घटनाएं वास्तविक हैं। कोतवाल ने जिस
प्रकार मुसाहिबजू से बंदूक ले ली थी, वह घटना भी सही है। हमारा वर्तमान
समय सवा सौ वर्ष पहले की अवस्था का प्राकृतिक सिलसिला है। उस समय सामंत
युग की समाप्ति प्रारंभ हो गई थी; अब उस समाप्ति का अवशिष्ट मात्र है। उस
समय उसमें कुछ सौष्ठव था- अब ?
वृंदावनलाल शर्मा
मुसाहिबजू
1
चिड़िया चुप थीं। झींगुर झंकार रहे थे। तड़का नहीं हुआ था। साँय-साँय चलने
के बादल हवा मंद पड़ गई थी और उसमें कुछ ठंडक भी आ गई थी। मनुष्यों का एक
झुंड सुलगते हुए बोड़ोंवाली बंदूकें लिये टीलेदार बीहड़ वन में चुपचाप चला
जा रहा था। कभी-कभी ये लोग यकायक ठहरकर आहट ले लेते और फिर सपाटे के साथ
चल देते थे। गिनती के बीस-पच्चीस आदमी होंगे।
सघन वृक्षों से ढँकी हुई एक छोटी-सी पहाड़ी पर चढ़ने के उपरांत ये लोग अलग-अलग ऊँची-नीची टोरों पर छिपककर जा बैठे। एक टोर पर दो मनुष्य एक साथ थे। एक के पास बंदूक थी और दूसरे के पास म्यान में बंद तलवार।
धीरे-धीरे भोर हुआ। पूर्व दिशा के प्रतिक्षण बदलने वाले रंगों की ओर इन लोगों का ध्यान न था। इनकी गड़ी आँखें वृक्षों के एक झुरमुट के तले प्रभाप्रच्छन्न अँधकार में कुछ टटोल रही थीं। यह स्थान उस टोर के नीचे निकट ही था, जहाँ ये दो मनुष्य जा बैठे थे। आधी घड़ी पश्चात् दो आकार उस अँधकार की ओर रेंगते हुए दिखाई पड़े। उन दो मनुष्यों में से एक ने बिलकुल दबे हुए स्वर में कहा- ‘काकाजू, तेंदुआ की जोड़ी है।’
दूसरे ने भी देख लिया था। संकेत में उत्तर दिया। तेंदुओं को संदेह हो गया। वे वहीं दबकर बारीकी के साथ टोह लेने लगे। रह-रहकर सिमटे। इन दोनों मनुष्यों ने साँस साधी।
इतने में और प्रकाश हुआ। झुरमुट के तले का अँधेरा और खंडित हुआ।
तेंदुओं के आकार स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगे। उनकी चुल भी दिखलाई पड़ी। एक अदृश्य हो गया।
जिस मनुष्य को कुछ देर पहले ‘ककाजू’ शब्द से संबोधन किया गया था, उसने रंजक को तोड़ से छुला दिया। रंजक फुर्र-फुर्र हुई और फिर जोर का धड़ाका हुआ। उस धड़ाके के साथ ही एक चीत्कारमय गर्जन सुनाई पड़ा; परन्तु उस क्षण बारूद के कारण कुछ स्पष्ट न दिखलाई पड़ सका। उसी समय बंदूक चलानेवाले अपने साथी से दूसरे ने जरा जोर से प्रफुल्ल स्वर में कहा- ‘काकाजू’ तेंदुआ अवश्य मारा गया।’ वाक्य समाप्त ही हो पाया था कि लोहूलुहान तेंदुआ छलांग भरकर काकाजू-संबोधित व्यक्ति की छाती पर आ चढ़ा। छिपाव के स्थानों पर इधर-इधर जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से कुछ के मुँह से ‘अरे’ निकला और कोई-कोई अपनी ही घबराहट के कारण हथियार समेत नीचे की ओर लुढ़क गए।
तेंदुए के पिछले पंजे चट्टान पर थे। एक पंजा बंदूक चलानेवाले व्यक्ति के कंधे पर पहुँच गया था और दूसरा हवा में तुला-हुआ-सा था। पंजे के बड़े-बड़े नाखून निकले हुए थे। सिर पर बँधे हुए साँफे में वे नाखून धँस गए। साफा हिला, खिसका। तेंदुआ अपने प्रबल आक्रमण के धक्के को न सँभाल सका। उसी चट्टान पर जरा फिसलकर तिरछा हुआ, सँभला और दूसरे आक्रमण के लिए दुगने वेग के साथ तैयार हुआ।
तुरंत दूसरे व्यक्ति ने फुर्ती से तलवार निकालकर जोर का हाथ तेंदुए की गरदन और छाती के बीच में कर दिया। वार कसा हुआ था; परन्तु तुरन्त घात का काम न दे सका। तेंदुए का पिछला धड़ चट्टान के नीचे की ओर फिसलकर रुक गया और सिर तलवार चलानेवाले शिकारी की जाँघ पर जा अटका। साथ की पैने दाँत जाँघ में जा घुसे।
‘वाह पूरन ! वाह !’- बंदूक चलानेवाले ने कहा- ‘कैसा बढ़िया हाथ किया है !’
पूरन ने इस प्रशंसा की ओर ध्यान न देकर आहत तेंदुए को अपनी जाँघ पर से धकेलकर नीचे गिरा देने का प्रयत्न किया। मांस में दाँत धँसे हुए थे। अलग न कर पाया। पीड़ा हुई। तेंदुए के मुँह का लोहू पूरन की जाँघ के रक्त के साथ मिश्रित होकर बहने लगा। पूरन जरा घबराया, कराहा। पूरन का साथी उसकी पीड़ा का ठीक-ठीक कारण न समझ पाया और बगल में पड़ी हुई बंदूक को फिर से भरने के लिए जल्दी से उठाया कि पूरन कष्टपूर्ण स्वर में बोला- ‘काकाजू, इसने मरते-मरते मेरी जाँघ चबा डाली है।’
बंदूक अलग रखकर वह व्यक्ति तेंदुए के दाँतों को पूरन की जाँघ से छुड़ाने का उपाय करने लगा। बलिष्ठ होते हुए भी वह व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न कर सका ! चिल्लाकर बोला- ‘क्या सब मर गए ? चलो, इधर।’
सबसे पहले एक बुड्ढा आया। हिम-सदृश श्वेत-दाड़ी थी। उसके दोनों सिरे कानों पर लिपटे हुए थे। लंबी छरहरी देह। बंदूक हाथ में और तलवार बगल में। यह पूरन दादा था।
‘राजा, आप ठहरो,’ बुड्ढा बोला- ‘मांस में दाँत धँस गए हैं, मैं निकालता हूँ।’
बुड्ढे ने दोनों पैर पूरन की जाँघ में अड़ाकर हाथों के पूरे बल से तेंदुए के दाँत जाँघ से छुड़ा लिये। जाँघ का बहुत-सा भाग बँधी हुई दाढ़ों में बिंधा चला आया।
‘रमू कक्का, आज मेरे प्राण पूरन ने बचाए हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या देकर इसके प्राण बचाऊँ।’
‘चिंता न की जावे, राजा,’ बुड्ढे रमू ने काँपते हुए स्वर में कहा- ‘अपने साथ मरहम-पट्टी का सामान है।’
थोड़े क्षण उपरान्त और शिकारी भी आ गए। कुछ लोग तेंदुए के मारे जाने पर बधाई देने लगे, कुछ जरा दूरी से पूरन के घाव और मृत तेंदुए के सिर को देखने लगे। उन लोगों के इस भाव में उदासीनता का आभास पाकर पूरन के बंदूक चलानेवाले उस साथी ने आँख तरेरी और करारे स्वर में कहा- ‘तुरंत मरहम-पट्टी करो।’
रमू बोला- ‘आप कोई न छुओ। मुझको मरहम और पट्टी दे दो। मैं अभी बाँध देता हूँ।’
‘ठहरो ! मैं इस काम को अच्छा जानता हूँ।’ काकाजू ने कहा।
सघन वृक्षों से ढँकी हुई एक छोटी-सी पहाड़ी पर चढ़ने के उपरांत ये लोग अलग-अलग ऊँची-नीची टोरों पर छिपककर जा बैठे। एक टोर पर दो मनुष्य एक साथ थे। एक के पास बंदूक थी और दूसरे के पास म्यान में बंद तलवार।
धीरे-धीरे भोर हुआ। पूर्व दिशा के प्रतिक्षण बदलने वाले रंगों की ओर इन लोगों का ध्यान न था। इनकी गड़ी आँखें वृक्षों के एक झुरमुट के तले प्रभाप्रच्छन्न अँधकार में कुछ टटोल रही थीं। यह स्थान उस टोर के नीचे निकट ही था, जहाँ ये दो मनुष्य जा बैठे थे। आधी घड़ी पश्चात् दो आकार उस अँधकार की ओर रेंगते हुए दिखाई पड़े। उन दो मनुष्यों में से एक ने बिलकुल दबे हुए स्वर में कहा- ‘काकाजू, तेंदुआ की जोड़ी है।’
दूसरे ने भी देख लिया था। संकेत में उत्तर दिया। तेंदुओं को संदेह हो गया। वे वहीं दबकर बारीकी के साथ टोह लेने लगे। रह-रहकर सिमटे। इन दोनों मनुष्यों ने साँस साधी।
इतने में और प्रकाश हुआ। झुरमुट के तले का अँधेरा और खंडित हुआ।
तेंदुओं के आकार स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगे। उनकी चुल भी दिखलाई पड़ी। एक अदृश्य हो गया।
जिस मनुष्य को कुछ देर पहले ‘ककाजू’ शब्द से संबोधन किया गया था, उसने रंजक को तोड़ से छुला दिया। रंजक फुर्र-फुर्र हुई और फिर जोर का धड़ाका हुआ। उस धड़ाके के साथ ही एक चीत्कारमय गर्जन सुनाई पड़ा; परन्तु उस क्षण बारूद के कारण कुछ स्पष्ट न दिखलाई पड़ सका। उसी समय बंदूक चलानेवाले अपने साथी से दूसरे ने जरा जोर से प्रफुल्ल स्वर में कहा- ‘काकाजू’ तेंदुआ अवश्य मारा गया।’ वाक्य समाप्त ही हो पाया था कि लोहूलुहान तेंदुआ छलांग भरकर काकाजू-संबोधित व्यक्ति की छाती पर आ चढ़ा। छिपाव के स्थानों पर इधर-इधर जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से कुछ के मुँह से ‘अरे’ निकला और कोई-कोई अपनी ही घबराहट के कारण हथियार समेत नीचे की ओर लुढ़क गए।
तेंदुए के पिछले पंजे चट्टान पर थे। एक पंजा बंदूक चलानेवाले व्यक्ति के कंधे पर पहुँच गया था और दूसरा हवा में तुला-हुआ-सा था। पंजे के बड़े-बड़े नाखून निकले हुए थे। सिर पर बँधे हुए साँफे में वे नाखून धँस गए। साफा हिला, खिसका। तेंदुआ अपने प्रबल आक्रमण के धक्के को न सँभाल सका। उसी चट्टान पर जरा फिसलकर तिरछा हुआ, सँभला और दूसरे आक्रमण के लिए दुगने वेग के साथ तैयार हुआ।
तुरंत दूसरे व्यक्ति ने फुर्ती से तलवार निकालकर जोर का हाथ तेंदुए की गरदन और छाती के बीच में कर दिया। वार कसा हुआ था; परन्तु तुरन्त घात का काम न दे सका। तेंदुए का पिछला धड़ चट्टान के नीचे की ओर फिसलकर रुक गया और सिर तलवार चलानेवाले शिकारी की जाँघ पर जा अटका। साथ की पैने दाँत जाँघ में जा घुसे।
‘वाह पूरन ! वाह !’- बंदूक चलानेवाले ने कहा- ‘कैसा बढ़िया हाथ किया है !’
पूरन ने इस प्रशंसा की ओर ध्यान न देकर आहत तेंदुए को अपनी जाँघ पर से धकेलकर नीचे गिरा देने का प्रयत्न किया। मांस में दाँत धँसे हुए थे। अलग न कर पाया। पीड़ा हुई। तेंदुए के मुँह का लोहू पूरन की जाँघ के रक्त के साथ मिश्रित होकर बहने लगा। पूरन जरा घबराया, कराहा। पूरन का साथी उसकी पीड़ा का ठीक-ठीक कारण न समझ पाया और बगल में पड़ी हुई बंदूक को फिर से भरने के लिए जल्दी से उठाया कि पूरन कष्टपूर्ण स्वर में बोला- ‘काकाजू, इसने मरते-मरते मेरी जाँघ चबा डाली है।’
बंदूक अलग रखकर वह व्यक्ति तेंदुए के दाँतों को पूरन की जाँघ से छुड़ाने का उपाय करने लगा। बलिष्ठ होते हुए भी वह व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न कर सका ! चिल्लाकर बोला- ‘क्या सब मर गए ? चलो, इधर।’
सबसे पहले एक बुड्ढा आया। हिम-सदृश श्वेत-दाड़ी थी। उसके दोनों सिरे कानों पर लिपटे हुए थे। लंबी छरहरी देह। बंदूक हाथ में और तलवार बगल में। यह पूरन दादा था।
‘राजा, आप ठहरो,’ बुड्ढा बोला- ‘मांस में दाँत धँस गए हैं, मैं निकालता हूँ।’
बुड्ढे ने दोनों पैर पूरन की जाँघ में अड़ाकर हाथों के पूरे बल से तेंदुए के दाँत जाँघ से छुड़ा लिये। जाँघ का बहुत-सा भाग बँधी हुई दाढ़ों में बिंधा चला आया।
‘रमू कक्का, आज मेरे प्राण पूरन ने बचाए हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या देकर इसके प्राण बचाऊँ।’
‘चिंता न की जावे, राजा,’ बुड्ढे रमू ने काँपते हुए स्वर में कहा- ‘अपने साथ मरहम-पट्टी का सामान है।’
थोड़े क्षण उपरान्त और शिकारी भी आ गए। कुछ लोग तेंदुए के मारे जाने पर बधाई देने लगे, कुछ जरा दूरी से पूरन के घाव और मृत तेंदुए के सिर को देखने लगे। उन लोगों के इस भाव में उदासीनता का आभास पाकर पूरन के बंदूक चलानेवाले उस साथी ने आँख तरेरी और करारे स्वर में कहा- ‘तुरंत मरहम-पट्टी करो।’
रमू बोला- ‘आप कोई न छुओ। मुझको मरहम और पट्टी दे दो। मैं अभी बाँध देता हूँ।’
‘ठहरो ! मैं इस काम को अच्छा जानता हूँ।’ काकाजू ने कहा।
2
तेंदुए पर बंदूक चलानेवाले और मरहम-पट्टी का दृढ़ प्रस्ताव करने वाले
दतिया राज्यांतर्गत केरुआ जागीरदार, जो ग्वालियर राज्य में है, मुसाहिब
दलीपसिंह थे और रमू तथा पूरन जाति के मेहतर और मुसाहिब के सैनिक थे।
अठारहवीं शताब्दी का अंत हो गया। भारत में दूरवर्ती पश्चिम से आई हुई एक नई जाति द्वारा नई राजनीतिक संस्था द्वारा स्थापित होती चली जा रही थी। बुंदेलखंड के रजवाड़ों के ऊपर संधियों के बंधन पड़ चुके थे। नई संस्था की नई प्रणाली बुंदेलखण्ड, अन्य प्रांतों की तरह सम्मोहित और संप्रभावित हो चुका था; परन्तु उसकी जकड़ में इतनी कठोरता नहीं आई थी कि परंपराएँ और स्थानिक रीतियाँ स्मारकों के उत्सव-मात्र रह जाएँ और जीने-मरने की स्वाधीनता का उच्छ्वास निरोध के दबोचनेवाले संयम में कस जाए।
दतिया की परंपरागत अनियमित सेना में उस समय कई सहस्त्र सैनिक थे। केरुआ के मुसाहिब दलीपसिंह को बारह सौ योद्धा रखने का आदेश था। इसी प्रयोजन में उनको बारह सहस्र रुपया वार्षिक आय की जागीर में सेंहुड़े के पास चिरूली इत्यादि आठ गाँव मिले हुए थे। इन बारह सौ सैनिकों में से लगभग आधे मुसाहिब के पास आते-जाते बने रहते थे, बाकी छ: सौ के विषय में विश्वास था कि अटक पड़ने पर कहीं से बुला लिये जाएँगे। पूरे बारह सौ दशहरे के दरबार के दिन भी हाजिरी देने न आते थे; परंतु भीड़भाड़ को देखकर बारह सौ का अनुमान कल्पनाशक्ति द्वारा कर लिया जाता था। किले में रखी हुई तोपें, जिनको श्रीवास्तव ने ढाला था और जिन पर उसका नाम खुदा या ढला हुआ था, कल्पना के प्रत्येक टुकड़ी की चीज समझी जाती थीं। थोड़े वर्षों पहले इन्हीं तोपों का प्रयोग दिल्ली के मुगलों की हरावल में दक्षिण और उत्तर में किया था। परंतु अब वे किसी संभव-घटना-संपात के केवल संभावनीय प्रयोग की साधन रह गई थीं और अब इन तोपों का गर्व इन टुकड़ियों को अंग्रेजी तोपों के सामने उतना नहीं रहा था। युद्ध की शैली परंपरा में परिणत हो चुकी थी। नई सूझबूझ के लिए कोई स्थान न रहा था।
और यह परंपरा भी पारस्परिक बखेड़ों के समय जात-पाँत का अभिमान प्रकट करने के लिए ही अधिक उपयोग में आने लगी थी, युद्ध और योद्धा के नाम की लकीर पीटी जाने लगी थी। किसी सैनिक को थोड़ी-सी भूमि और किसी को एक-एक दो-दो रुपए मासिक वेतन मिलता था, वह भी महीनों बकाया में पड़ा रहता था और कभी-कभी बकाया बिना दिए-लिये ही साफ भी हो जाया करता था।
परंतु मुसाहिब दलीपसिंह का नियम था कि जब कभी जितने सैनिक उनके घर आ जाते, वे उनको भोजन कराते। भोजन के लिए दो-चार घंटे का विलंब भले ही हो जाए, परन्तु कराया अवश्य जाता था।
अठारहवीं शताब्दी का अंत हो गया। भारत में दूरवर्ती पश्चिम से आई हुई एक नई जाति द्वारा नई राजनीतिक संस्था द्वारा स्थापित होती चली जा रही थी। बुंदेलखंड के रजवाड़ों के ऊपर संधियों के बंधन पड़ चुके थे। नई संस्था की नई प्रणाली बुंदेलखण्ड, अन्य प्रांतों की तरह सम्मोहित और संप्रभावित हो चुका था; परन्तु उसकी जकड़ में इतनी कठोरता नहीं आई थी कि परंपराएँ और स्थानिक रीतियाँ स्मारकों के उत्सव-मात्र रह जाएँ और जीने-मरने की स्वाधीनता का उच्छ्वास निरोध के दबोचनेवाले संयम में कस जाए।
दतिया की परंपरागत अनियमित सेना में उस समय कई सहस्त्र सैनिक थे। केरुआ के मुसाहिब दलीपसिंह को बारह सौ योद्धा रखने का आदेश था। इसी प्रयोजन में उनको बारह सहस्र रुपया वार्षिक आय की जागीर में सेंहुड़े के पास चिरूली इत्यादि आठ गाँव मिले हुए थे। इन बारह सौ सैनिकों में से लगभग आधे मुसाहिब के पास आते-जाते बने रहते थे, बाकी छ: सौ के विषय में विश्वास था कि अटक पड़ने पर कहीं से बुला लिये जाएँगे। पूरे बारह सौ दशहरे के दरबार के दिन भी हाजिरी देने न आते थे; परंतु भीड़भाड़ को देखकर बारह सौ का अनुमान कल्पनाशक्ति द्वारा कर लिया जाता था। किले में रखी हुई तोपें, जिनको श्रीवास्तव ने ढाला था और जिन पर उसका नाम खुदा या ढला हुआ था, कल्पना के प्रत्येक टुकड़ी की चीज समझी जाती थीं। थोड़े वर्षों पहले इन्हीं तोपों का प्रयोग दिल्ली के मुगलों की हरावल में दक्षिण और उत्तर में किया था। परंतु अब वे किसी संभव-घटना-संपात के केवल संभावनीय प्रयोग की साधन रह गई थीं और अब इन तोपों का गर्व इन टुकड़ियों को अंग्रेजी तोपों के सामने उतना नहीं रहा था। युद्ध की शैली परंपरा में परिणत हो चुकी थी। नई सूझबूझ के लिए कोई स्थान न रहा था।
और यह परंपरा भी पारस्परिक बखेड़ों के समय जात-पाँत का अभिमान प्रकट करने के लिए ही अधिक उपयोग में आने लगी थी, युद्ध और योद्धा के नाम की लकीर पीटी जाने लगी थी। किसी सैनिक को थोड़ी-सी भूमि और किसी को एक-एक दो-दो रुपए मासिक वेतन मिलता था, वह भी महीनों बकाया में पड़ा रहता था और कभी-कभी बकाया बिना दिए-लिये ही साफ भी हो जाया करता था।
परंतु मुसाहिब दलीपसिंह का नियम था कि जब कभी जितने सैनिक उनके घर आ जाते, वे उनको भोजन कराते। भोजन के लिए दो-चार घंटे का विलंब भले ही हो जाए, परन्तु कराया अवश्य जाता था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i