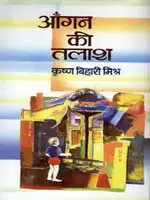|
लेख-निबंध >> आँगन की तलाश आँगन की तलाशकृष्णबिहारी मिश्र
|
300 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है ललित निबन्ध...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृति छात्र और आग्रणी पंक्ति के निबन्धकार
कृष्ण बिहारी मिश्र के निबन्धों की विशिष्टता को रेखांकित करते अज्ञेयजी
ने लिखा है- ’ललित निबन्ध के लालित्य का एक पहलू वह भी हो सकता
है, जिनके केन्द्र में स्वयं भाषा होती है। ऐसे ललित निबंधों को अच्छे और
सही अर्थ में वाग्विलास भी कहा जा सकता है। श्री कृष्ण बिहारी मिश्र का
भाषा के साथ वैसा संबंध नहीं है, वे रचनात्मक ऊर्जा क्रीड़ा के रूप में
नहीं प्रकट करते। उनकी भाषा हमेशा कुछ कहने में लगी रहती है क्यों की
उसमें कहने को बहुत कुछ है-ऐसा बहुत कुछ, जो स्वयं रागरंजिस है और इसलिए
रंजित भाषा की अपेक्षा नहीं रखता।‘ शीर्शक निबंधकार पं. विद्यानिवास मिश्र कृष्ण बिहारी मिश्र को अपना संवेदना गोत्र मानते हैं तो इसका आधार महज इतना नहीं है कि दोनों का भोज पुरी धरती से अंतरंग संबंध है बल्कि यह है दोनों की गँवाई संवेदना, जो मूल्य संवर्धन-संरक्षण के लिए व्याकुल और सर्जनशील है।
सभ्यता-संघात से आँगन छोटा हो रहा है आँगन की वास्तविक पहचान मिट रही है-यह सांस्कृतिक दर्द मिश्र जी के निबंधों में मुखर है। अपने आँगन में अजनबी बन जाना असह्य त्रासदी है। यह त्रासदी की स्थिति आज के मनुष्य की नियति बन गई है-बोलते हैं लोग ज्यों मुँह फेरकर। अपना ही आँगन पराया लगता है और अपनी ही बोली का अर्थ समझ में नहीं आता । शब्द और अर्थ का फासला इतना बढ़ गया है कि शब्द से आस्था उठ रही है। यह अनास्था सांस्कृतिक संकट की डरावनी घंटी जान पड़ती है, जो चिन्तनशील जगत के लिए विकट चुनौती बन गई है। इसी चुनौती से जुड़ी है इस पुस्तक में संकलित निबंधों की वेदना, जो एक नए और सर्जनशील आयाम की ओर इशारा करती है और जो वर्तमान अंधड़ का विधायक विकल्प हो सकता है।
सभ्यता-संघात से आँगन छोटा हो रहा है आँगन की वास्तविक पहचान मिट रही है-यह सांस्कृतिक दर्द मिश्र जी के निबंधों में मुखर है। अपने आँगन में अजनबी बन जाना असह्य त्रासदी है। यह त्रासदी की स्थिति आज के मनुष्य की नियति बन गई है-बोलते हैं लोग ज्यों मुँह फेरकर। अपना ही आँगन पराया लगता है और अपनी ही बोली का अर्थ समझ में नहीं आता । शब्द और अर्थ का फासला इतना बढ़ गया है कि शब्द से आस्था उठ रही है। यह अनास्था सांस्कृतिक संकट की डरावनी घंटी जान पड़ती है, जो चिन्तनशील जगत के लिए विकट चुनौती बन गई है। इसी चुनौती से जुड़ी है इस पुस्तक में संकलित निबंधों की वेदना, जो एक नए और सर्जनशील आयाम की ओर इशारा करती है और जो वर्तमान अंधड़ का विधायक विकल्प हो सकता है।
काम्य
अपने आँगन में अजनबी बन जाना असह्य त्रासदी
है। यह त्रासद स्थिति आज के मनुष्य की नियति बन गई है-‘बोलते हैं लोग ज्यों
मुँह फेरकर’। और आँगन छोटा हो रहा है। अपना ही आँगन पराया लगता है और
अपनी ही बोली का अर्थ समझ में नहीं आता। शब्द और अर्थ का फासला इतना बढ़
गया है कि शब्द से आस्था उठ रही है। यह अनास्था सांस्कृतिक संकट की डरावनी
घंटी जान पड़ती है, जो चिंतनशील जगत् के लिए विकट चुनौती बन गई है।
मनुष्य के सामने सांस्कृतिक संकट पहली बार नहीं खड़ा हुआ है। यह जरूरी है कि आज का असमंजस अपेक्षाकृत अधिक गहरा है। मूल्यों के पहरुओं पर से ही भरोसा उठने लगा है। संकट का ज्वलंत बिंदु यही है। असमंजस का हेतु भी यही है।
अपने आँगन में साँस लेता संवेदनशील आदमी निर्वासन—दंश की आँच को गहराई से महसूस करते आँगन की संवेदना की सुरक्षा के लिए व्याकुल है। और भूमंडलीकरण के शोर में आँगन की आवाज दब रही है। समय की रफ्तार इतनी तेज है कि क्षण भर की प्रतीक्षा भारी लगती है। नादान शिशु के खेलवाड़ की तरह सयाने भी बीज-वपन के दूसरे ही क्षण पल्लवित-फलित गाछ देखने को व्याकुल हो उठे हैं। बालखिल्य के सौंदर्य में दिलचस्पी क्षीण हो रही है। बच्चों की पकठाई बोली-बानी हमें सुहाती है। माँ-बाप को आज यही काम्य है कि बच्चे अकाल वयस्क हो जाएँ, इसलिए नैसर्गिक कौतुक को नृशंस अनुशासन से कुंठित करने का संवेदनहीन आचरण सामान्य स्वभाव बनता जा रहा है। एक सनकी स्पर्द्धा हर घर में क्रियाशील हो गई है। और आँगन के सहज उल्लास को विजातीय दबाव धीरे-धीरे लील रहा है।
पर अनास्था-अभिशप्त आज के तमस के प्रतिरोध की आवाज कोने-अँतरे से उठने लगी है। आँगन की सुरक्षा की बात, जड़ से जुड़ने की बात और छीजती संवेदना को नई ऊर्जा-ऊष्मा से पुनर्नवा कर जागरुक पहरेदारी द्वारा पोसने की चिंता जाग रही है। विचार की नई उठान अंधे समय में रोशनी की राह रचने लगी है कि आदमी को और उसके भरोसे को मरने से बचाया जा सकता है। भारत की संस्कृति की बूढ़ी साँसे उपभोक्तावाद को स्वधर्म के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और सचेत प्रज्ञा आर्ष वाणी का अर्थ समझने-समझाने लगी है कि ‘जो नवीन है वह स्थायी नहीं हो सकता। जो सत्य है वही सनातन है।’ यह सनातन राग बाबा आम्टे, सुंदर लाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर जैसे सत्याग्रही चरित्र के कंठ और क्रिया-कलाप में गूँजने लगा है।
उपभोक्ता-औद्धात्य और कदाचार के बावजूद प्रकृति ने अभी मनुष्य से प्रतिशोध लेना नहीं शुरू किया है। वह मुद्दई का रुख अपना ले तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाए। इतने विजातीय बोझ को ढोते हुए भी मनुष्य हँसना-रोना भूला नहीं है। शेफाली की वदान्यता मरुआई नहीं है। कोयल का व्याकुल राग प्रमाण है कि उसे वसंत का नेवता मिला है। अशोक ठहाका लगाकर हँस रहा है, सरेह की चैती सुरभी क्षीण नहीं हुई है और न तो उस मादक आस्वाद से पगलाए लोगों की संख्या ही कम हुई है। रामबचन बइठा बेटे के साथ ही बूढ़ी माँ और अपने नींबू-शरीफा के गाछ की हिफाजत के लिए चिंतित है। आश्वासन की रोशनी जागती है कि आदमी की पहचान मरते-मरते भी मरेगी नहीं। रस से उसका सरोकार कमजोर नहीं होगा। जो कहता है, रस मर गया, वह सरासर झूठ बोलता है। रस पर लाठी चलाने वालों में भी रस की व्याकुल भूख है। रस-लीला की साझीदारी के लिए ही वह दरवाजे-दरवाजे दस्तक देता फिरता है। ‘मन के मानुष’ के संधान में हर आदमी लालन फकीर की तरह व्याकुल है। यही व्याकुल भाव मुझे शोभन में, कुंतला के रोष में, नादान बालिका की निष्पाप मु्द्रा में, रामबचन बइठा की संवेदना में, टोरमल में और युगल किशोर घोष की जीवनचर्या में दिखाई पड़ता है तो मेरी संवेदना आलोकित हो उठती है। और गहरी आश्वस्ति महसूस करता हूँ जब अपने आँगन से भागे, सुरक्षा की तसल्ली खोजते अयूब खाँ की बात सुनता हूँ कि ‘हिंदू से नहीं, दंगा से डर लगता है!’ निपट निरक्षर अयूब खाँ का वक्तव्य प्रमाण है कि मानुष सत्य अभी मरा नहीं है। राजनीतिक छल आम आदमी को बरगलाने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। अयूब खाँ भाईचारा की ऊष्मा का अर्थ और कूटभाषा का अर्थ मर्म समझता है। इसलिए हिंसा की लपट से बचने के लिए हिंदू पड़ोसियों के साथ हिंदू बस्ती के शरणार्थी शिविर में भाग आया है सपरिवार। और अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त है। यह आश्वासन बेहतर अहिंसक आबोहवा की संभावना का संकेत है। और यह संभावना संर्जनशीलता को चुनौती भरा आमंत्रण देती है। यह आमंत्रण समय-संवेदना पर केंद्रित है। समय-संवेदना के प्रति जागरुकता सर्जक का सबसे बड़ा दायित्व है, और कदाचित् सबसे बड़ी चुनौती भी। इस चुनौती से तथाकथित विप्लवी लोगों की तरह मुठभेड़ करने का दावा मैं नहीं करता पर चुनौती को पीठ न दिखाने का तोष है मन में। सहृदय पाठकों के पत्र से प्राप्त आशंसा से प्रेरक संकेत मिलता रहा है कि मेरा लेखन अपने समय के सवालों के प्रति जागरुक है। सांस्कृतिक सुस्ती इस दौर में सहृदय जन के पत्र जब सचेत करते हैं कि साहित्य से मनुष्य का सोरकार अभी पूरी तरह शेष नहीं हुआ है तो सृजनशील विकल्प की संभावना जागती है मन में। मेरे रम्य निबंध उसी संभावना की ओर इशारा करते हैं। मेरे संकेत लक्ष्य को स्पर्श कर सकें तो लेखन-कर्म की सार्थकता मेरे लिए प्रेरक संबल का काम करेगी।
उन्मुक्त रम्य शैली में रचित कुछ ललितेतर गद्य-लेखन इस संग्रह में संकलित कर दिया गया है। सोच की दिशा को सर्जनशील समृद्धि देनेवाले प्रातिभ पुरुषों का अंतरंग परिचय अपने अभिप्राय को अधिक बल के साथ रेखांकित करने की प्रचेष्टा है। आशा है, यह लेखकीय व्यवस्था सहृदय के आस्वाद को समृद्धतर करेगी। यही काम्य है।
मनुष्य के सामने सांस्कृतिक संकट पहली बार नहीं खड़ा हुआ है। यह जरूरी है कि आज का असमंजस अपेक्षाकृत अधिक गहरा है। मूल्यों के पहरुओं पर से ही भरोसा उठने लगा है। संकट का ज्वलंत बिंदु यही है। असमंजस का हेतु भी यही है।
अपने आँगन में साँस लेता संवेदनशील आदमी निर्वासन—दंश की आँच को गहराई से महसूस करते आँगन की संवेदना की सुरक्षा के लिए व्याकुल है। और भूमंडलीकरण के शोर में आँगन की आवाज दब रही है। समय की रफ्तार इतनी तेज है कि क्षण भर की प्रतीक्षा भारी लगती है। नादान शिशु के खेलवाड़ की तरह सयाने भी बीज-वपन के दूसरे ही क्षण पल्लवित-फलित गाछ देखने को व्याकुल हो उठे हैं। बालखिल्य के सौंदर्य में दिलचस्पी क्षीण हो रही है। बच्चों की पकठाई बोली-बानी हमें सुहाती है। माँ-बाप को आज यही काम्य है कि बच्चे अकाल वयस्क हो जाएँ, इसलिए नैसर्गिक कौतुक को नृशंस अनुशासन से कुंठित करने का संवेदनहीन आचरण सामान्य स्वभाव बनता जा रहा है। एक सनकी स्पर्द्धा हर घर में क्रियाशील हो गई है। और आँगन के सहज उल्लास को विजातीय दबाव धीरे-धीरे लील रहा है।
पर अनास्था-अभिशप्त आज के तमस के प्रतिरोध की आवाज कोने-अँतरे से उठने लगी है। आँगन की सुरक्षा की बात, जड़ से जुड़ने की बात और छीजती संवेदना को नई ऊर्जा-ऊष्मा से पुनर्नवा कर जागरुक पहरेदारी द्वारा पोसने की चिंता जाग रही है। विचार की नई उठान अंधे समय में रोशनी की राह रचने लगी है कि आदमी को और उसके भरोसे को मरने से बचाया जा सकता है। भारत की संस्कृति की बूढ़ी साँसे उपभोक्तावाद को स्वधर्म के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और सचेत प्रज्ञा आर्ष वाणी का अर्थ समझने-समझाने लगी है कि ‘जो नवीन है वह स्थायी नहीं हो सकता। जो सत्य है वही सनातन है।’ यह सनातन राग बाबा आम्टे, सुंदर लाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर जैसे सत्याग्रही चरित्र के कंठ और क्रिया-कलाप में गूँजने लगा है।
उपभोक्ता-औद्धात्य और कदाचार के बावजूद प्रकृति ने अभी मनुष्य से प्रतिशोध लेना नहीं शुरू किया है। वह मुद्दई का रुख अपना ले तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाए। इतने विजातीय बोझ को ढोते हुए भी मनुष्य हँसना-रोना भूला नहीं है। शेफाली की वदान्यता मरुआई नहीं है। कोयल का व्याकुल राग प्रमाण है कि उसे वसंत का नेवता मिला है। अशोक ठहाका लगाकर हँस रहा है, सरेह की चैती सुरभी क्षीण नहीं हुई है और न तो उस मादक आस्वाद से पगलाए लोगों की संख्या ही कम हुई है। रामबचन बइठा बेटे के साथ ही बूढ़ी माँ और अपने नींबू-शरीफा के गाछ की हिफाजत के लिए चिंतित है। आश्वासन की रोशनी जागती है कि आदमी की पहचान मरते-मरते भी मरेगी नहीं। रस से उसका सरोकार कमजोर नहीं होगा। जो कहता है, रस मर गया, वह सरासर झूठ बोलता है। रस पर लाठी चलाने वालों में भी रस की व्याकुल भूख है। रस-लीला की साझीदारी के लिए ही वह दरवाजे-दरवाजे दस्तक देता फिरता है। ‘मन के मानुष’ के संधान में हर आदमी लालन फकीर की तरह व्याकुल है। यही व्याकुल भाव मुझे शोभन में, कुंतला के रोष में, नादान बालिका की निष्पाप मु्द्रा में, रामबचन बइठा की संवेदना में, टोरमल में और युगल किशोर घोष की जीवनचर्या में दिखाई पड़ता है तो मेरी संवेदना आलोकित हो उठती है। और गहरी आश्वस्ति महसूस करता हूँ जब अपने आँगन से भागे, सुरक्षा की तसल्ली खोजते अयूब खाँ की बात सुनता हूँ कि ‘हिंदू से नहीं, दंगा से डर लगता है!’ निपट निरक्षर अयूब खाँ का वक्तव्य प्रमाण है कि मानुष सत्य अभी मरा नहीं है। राजनीतिक छल आम आदमी को बरगलाने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। अयूब खाँ भाईचारा की ऊष्मा का अर्थ और कूटभाषा का अर्थ मर्म समझता है। इसलिए हिंसा की लपट से बचने के लिए हिंदू पड़ोसियों के साथ हिंदू बस्ती के शरणार्थी शिविर में भाग आया है सपरिवार। और अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त है। यह आश्वासन बेहतर अहिंसक आबोहवा की संभावना का संकेत है। और यह संभावना संर्जनशीलता को चुनौती भरा आमंत्रण देती है। यह आमंत्रण समय-संवेदना पर केंद्रित है। समय-संवेदना के प्रति जागरुकता सर्जक का सबसे बड़ा दायित्व है, और कदाचित् सबसे बड़ी चुनौती भी। इस चुनौती से तथाकथित विप्लवी लोगों की तरह मुठभेड़ करने का दावा मैं नहीं करता पर चुनौती को पीठ न दिखाने का तोष है मन में। सहृदय पाठकों के पत्र से प्राप्त आशंसा से प्रेरक संकेत मिलता रहा है कि मेरा लेखन अपने समय के सवालों के प्रति जागरुक है। सांस्कृतिक सुस्ती इस दौर में सहृदय जन के पत्र जब सचेत करते हैं कि साहित्य से मनुष्य का सोरकार अभी पूरी तरह शेष नहीं हुआ है तो सृजनशील विकल्प की संभावना जागती है मन में। मेरे रम्य निबंध उसी संभावना की ओर इशारा करते हैं। मेरे संकेत लक्ष्य को स्पर्श कर सकें तो लेखन-कर्म की सार्थकता मेरे लिए प्रेरक संबल का काम करेगी।
उन्मुक्त रम्य शैली में रचित कुछ ललितेतर गद्य-लेखन इस संग्रह में संकलित कर दिया गया है। सोच की दिशा को सर्जनशील समृद्धि देनेवाले प्रातिभ पुरुषों का अंतरंग परिचय अपने अभिप्राय को अधिक बल के साथ रेखांकित करने की प्रचेष्टा है। आशा है, यह लेखकीय व्यवस्था सहृदय के आस्वाद को समृद्धतर करेगी। यही काम्य है।
आँगन की तलाश
शोभन की बाल ऊर्जा मेरे संकीर्ण भूगोल में अँट नहीं रही
है। उछलती उल्लास-ऊर्जा से टकराकर प्रायः इस बालक के शरीर को क्षत कर देती
है। अपनी लीला के लिए उसे बड़े आँगन की तलाश है। जिस संकीर्ण भूगोल में
कैद है, उसकी नियति उसे अतिक्रांत कर जाने को अकसर व्याकुल हो उठती है।
मगर सयाने उसे भरपूर आजादी देने को तैयार नहीं हैं। कहाँ रुचती है बच्चों
को सयानों की पहरेदारी !
घर की सामान्य चर्या के प्रतिकूल चलता है शोभन का उल्लास-आवेग और उसका क्रीड़ा-उत्पात घरवालों की असुविधा का कारण बन जाता है। इसलिए उसे दबाने की विधि सोती जाती है, जो शोभन के स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ती। दोपहर के पहले भरपूर खेल-खाकर कुछ देर गहरी नींद में सोना चाहता है। अकसर सो जाता है। नींद पूरी कर दोपहर के भोजन के समय तक जाग जाता है। और एक बार जब जग जाता है, पूरे वातारण को जगाए रखना चाहता है। दिवा-शयन के अभ्यस्त लोगों के विलास में बाधा पड़ती है। मुझे भी थोड़ी असुविधा होती है। दिन में सोने का वैसा व्यसन तो मुझमें नहीं है, पर दोपहर के भोजन के बाद कुछ समय नीरवता की गोद में पड़ा रहना चाहता हूँ। कभी नींद भी आ जाती है और कभी यों ही शिथिल पड़ा रहना चाहता हूँ। मगर दोस्तों ने ढोल पीटकर जगत् को खबर कर दी है कि मेरा सबसे प्रिय व्यसन है दिवा-शयन। किसी की धारणा का विरोध कर बदनामी से बच पाना संभव होता तो मैं भी अपने पक्ष को स्पष्ट करने की कोशिश करता। मगर यह सोचकर कि मेरी कोशिश का कोई फल नहीं निकलेगा, लोगों के दिलचस्प व्यसन में बाधक नहीं बनना चाहता। दोष-दर्शन मनुष्य का नैसर्गिक व्यसन है। आज कुछ अधिक लोकप्रिय है। पढ़वइए और सफेदपोशों की बात छोड़िए, जिन्हें दुनिया जाहिल-गँवार समझती है उनकी अंतरंग जिंदगी में घुसिए तो पता चल जाएगा कि अपनी सारी कल्पना-शक्ति वे छिद्रान्वेषण में खर्च कर रहे हैं। होती बड़ी रंगीन है दोष की कल्पना। और निंदा रस के आस्वाद में अच्छे-अच्छे लोग फँस जाते हैं। सो मित्रों के मनोरंजन की बात सोचकर उनके सरस कटाक्ष का सुख भोगता रहता हूँ। शोभन के कोलाहल का भी मैं भरपूर आस्वाद लेता हूँ। जिन्हें अपने व्यसन की ही चिंता रहती है उन्हें शोभन की मुखर क्रीड़ा कष्ट देती है। सुबह नहाते ही शोभन ऊँघने लगता है, घरवालों ने उसकी कमजोरी लक्ष्य कर ली है। इसलिए इस जलक्रीड़ाप्रिय बालक को तपती दोपहरी में स्नान का सुख मिल पाता है। सयानों के भोजन के समय ताकि शयन-सुख शोभन के उत्पात से खंडित न हो।
सीढ़ी के बीच के संकीर्ण भूगोल में शोभन की लहर बार-बार क्षत होती है और मेरे मन की आबोहवा बिगड़ जाती है। अपनी उल्लास-उर्मि की अबाधित अभिव्यक्ति के लिए शोभन को बड़े आँगन की तलाश है। शायद सबको फैलाव की खोज है। या कि कोई भी फैलाव में जीना नहीं चाहता। अपनी दुनिया को हर तरह से बंद कर सुख भोगने की एकांत साध से लोग व्याकुल हैं। मेरा देहाती मन मैदान-जंगल और बड़े आँगन से जुड़ी उन्मुक्तता के लिए पागल बना रहता है। महानगर की बंद जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने में सहज संकोच होता है। नगर सभ्यता के आतंक से बिना पूर्व सूचना दिए किसी के यहाँ जाता नहीं। शाम को किसी के यहाँ जाने में और भी डर लगता है। किसी का रस-भंग नहीं करना चाहता। अनुभव से बात समझ में आ गई है कि दूरदर्शन कार्यक्रम और वारुणी-लीला में बाहरी आदमी का हस्तक्षेप किसी को रुचता नहीं, शिष्टाचार के दबाव में भले ही कुछ देर कोई झेल ले अपने अतिथि को। इसलिए अर्गलाविहीन देहाती मन नए शऊर में जीने को मजबूर है। यह लाचारी मेरे मूल भाव को घायल करती रहती है जैसे मेरे शोभन का उल्लास संकीर्ण भूगोल से आहत होता रहता है।
मगर आज जब मैं अपने गाँव के सिवान में प्रवेश करता हूँ, अनायास जाँ निसार अख्तर के शेर की पंक्ति याद आती है-‘गाँव में आकर शहर बसे, गाँव बेचारे जाएँ कहाँ’ कहाँ गया गाँव का खुलापन ? वह उन्मुक्त परिसर, जिसका चप्पा-चप्पा अपना लगता था, गाँव से किसने छीन लिया ? अड़ोस-पड़ोस के दुआर-आँगन में अधिकारपूर्वक प्रवेश करने वाले गँवई मन को किसने मार दिया ? कहाँ गायब हो गई मेरी माटी की सजातीय पहचान ? नए लोगों को पुराने परिदृश्य-प्रसंग सरासर झूठ लगते हैं। और उनकी व्यंग्य-मुसकान के दंश को झेलना हमारी नियति है। गाँव का नैसर्गिक खुलापन अब केवल कहने-सुनने की बात है; उस रहनि में जीना तो दूर, कोई संवेदना पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आजादी के बाद कितनी गहरी गुलामी में हम फँस गए। सबसे बड़ी क्षति हुई कि हमारा लीला-परिसर बहुत छोटा हो गया। इतना छोटा कि मन को जब-तब खरोंच लग जाती है जैसे मेरे शोभन के उल्लास को मेरी सँकरी जगह प्रायः कुंठित करती रहती है। और उन्मुक्त परिसर की भूख मेरे भीतर गाँव की याद जगा देती है। मेरे बाल्यकाल के लीलाधाम की याद। उस गाँव की याद, जिसने हमारे उल्लास-नर्तन के लिए उन्मुक्त भूगोल दिया था, बड़े परिदृश्य का आस्वाद दिया था, धरती के छोह और चुनौती का मर्म समझाया था। वही अपना गाँव आज पराया लगता है। पराई क्यों लगने लगी अपनी माटी माँ ? वह माँ, जिसकी स्वाभिमान-रक्षा के लिए व्याकुलताविद्ध युवक ने गवना की ‘पीअरी’ पहने अपने को होम दिया था। उस बलिदान का चौरा पूजनेवाले और अवदान बाबा को सर्वोच्च देव-प्रहरी मानकर संकटमोचन के लिए सुमिरते, उनकी जय-जयकार से हर अनुष्ठान शुरू करने वाले गाँव के नवहीं ‘रामगढ़ ढाला’ पर बैठे कूटबुद्धि पैनी करने में मशगूल दिखाई पड़ते हैं। वे अवदान बाबा के मर्म को नहीं समझते। नहीं समझते उस अवदान के मूल्य को कि गाँव की अन्नपूर्णा के आँचल की रक्षा करते उस युवा सत्याग्रही ने अपने आँगन में सद्य : उदित शोभा को राख में मिला दिया था, और परवर्ती पीढ़ी के उल्लास की सुरक्षा के लिए उदग्र होकर धरती माता को अपने रक्त से सींच दिया था ताकि माटी माँ का आँगन सिकुड़ न जाए, गाँव का माथा न झुक जाए, नई पौध की उल्लास-तरंगें संकीर्ण परिसर में कैद होकर ऊँचाई को स्पर्श करने के पहले ही मुरझा न जाएँ। अवदान बाबा के रक्त ने गाँव को बड़ा भूखण्ड उपलब्ध कराया, अन्यथा समृद्धि-दर्प का आधार गाँव के हाथ से निकल गया होता। बाबा का स्मरण करते गर्व होता है, और अपनी अपात्रता पर ग्लानि भी कि अपने शोभन की ऊर्जा-क्रीड़ा के लिए उपयुक्त आँगन नहीं सुलभ करा पा रहा हूँ। और पीड़क है कि उसकी उपद्रव-लीला का सहचर बनने को कोई तैयार नहीं है।
अपने विलास-मुख के लिए सयाने शोभन की प्रकृति बदलने की कोशिश में लगे हैं। उसकी सहज तरंग को मारने की सयानी कोशिश मेरी भावना को घायल कर देती है। उसके नहाने-खाने, खेलने और स्वच्छंद लीला को शहराती चर्या-छंद से अनुशासित करनेवाले बड़े लोग कितने नादान हैं कि चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक बड़ी संभावना को अपनी महत्त्वकांक्षा के अंधे आवेग में तहस-नहस किए जा रहे हैं। बच्चे को ‘आदमी’ बनाने की सनकी स्पर्द्धा हर माँ-बाप को पागल बनाए रहती है।
शहर तो शहर, अपने गाँव के लोगों से बोलते-बतियाते मैंने लक्ष्य किया, बेटों के आचरण से लगभग हर बाप विक्षिप्त है। आतंकित रहता है कि बेटे का औद्धत्य कहीं घायल न कर दे। युवा पीढ़ी की ढीठ मुद्रा से बूढ़ी पीढ़ी भीत रहने लगी है। यह आश्वासन की बेटा जवान होगा तो विपदा दूर होगी, कमजोर हो गया है। कभी-कभी सोचता हूँ कि जन्म के साथ ही जिसे भोग का व्याकरण समझाया गया, उसकी नजर में माँ-बाप का मूल्यहीन हो जाना अचरज की बात नहीं है। पशु-पक्षी और वनस्पति-लोक के अमर्यादित भोग का अंधा आवेग पगलाए आदमी की मनोवृत्ति का संकेत देता है कि पयपान से तुष्ट न होने वाला आदमी माँ का मांस-भक्षण करने को व्याकुल हो उठा है। तथाकथित सयानों ने यह जीवन-कला सिखाई है। दुःख उन्हींका गहराया है। माता की अवमानना आज का पीड़क यथार्थ है।
जिस धरती माँ की रक्षा करते अवदान बाबा ने अपनी नवपरिणिता के सौभाग्य को क्षार कर दिया था, वह माँ बेटों की अमर्यादित भोग की मार से श्रीहीन होती जा रही है। लोगों का विलास कुछ भी सुनने-समझने को तैयार नहीं है। दायरा सिकुड़ रहा है और मैला हो रहा है। दूसरे का भूगोल हड़पने और शोभाहीन बनानेवाली पाप-बुद्धि को पौरुष–प्रताप माना जाने लगा है। जिस पर हमें गर्व था वह लम्बा-चौड़ा, हँसमुख परिसर मेरा क्रीड़ाक्षेत्र और मेरा आँगन छोटा और उदास हो रहा है। पर अपना आत्मीय परिसर पराया लगता है। मूल पहचान दब गई है। कुछ घट गया है। ऐसा कुछ जो बाँधे रहता था, अपनी संतान को हाँक लगाता रहता था। लगता है, यात्रा को विराम देने के लिए अपरिचित पड़ाव पर हम ठहरे हैं और अत्यधिक सतर्क हैं कि कहीं कोई चूक न हो जाए। अपने आँगन में जीने का यह ढंग नहीं है। मेरे शोभन की शैली ठीक है। खुल के उछलता है। घायल होकर भी अपने परिसर को अपना मानता है। अपने कौतुक से अपने संकीर्ण भूगोल को हँसमुख बनाए रहता है। घर के सयानों को असुविधा होती है तो होती रहे। अपना संकीर्ण भूगोल मुझे छोटा लगता है। शोभन को बड़ी जगह उपलब्ध कराने के लिए व्याकुल रहता हूँ। पर शोभन की सीढ़ी की सँकरी जगह हमेशा मुसकराती और बड़ी लगती है। अपनी क्रीड़ा के लिए वह दूसरे का भूगोल हड़पना नहीं चाहता। शोभन की चाल मेरे गाँव की चाल से कुछ अलग है।
गाँव गया था। मेरी पट्टीदारी की काकी अपना दुर्भाग्य निवेदित करते कहने लगी-‘चकबंदी में मेरा खेत खो गया। वही जीने का सहारा था।’ उनकी पीड़ा मुझे अपने गिरफ्त में ले लेती है। बउड़म ससुर और निठल्ले भँगेड़ी पति के चलते भूमि-सम्पन्न परिवार की बहू निःस्व हो गई। ससुर-पति की सनक में स्वाहा होने से बची महज ढाई बीघे जमीन को चकबंदी की चाल खा गई। गाँव के समर्थ लोगों से काकी के दुर्भाग्यमोचन का संकेत करता हूँ, यह समझते हुए कि किसी को किसी की भूगोल-सुरक्षा की चिंता नहीं है। दूसरे के उल्लास को हड़पने की ताक में सारी दुनिया पगला गई है। भावना के आग्रह से तथापि अनुरोध करता हूँ। अपनी संवेदना के करीब गाँव के बेटे कैफी आजमी को पाता हूँ-‘वो मेरा गाँव है और वो मेरे गाँव के चूल्हे, जहाँ आग तो आग धुआँ नहीं मिलता।’ थोड़ी तसल्ली मिलती है कि मैं अकेला घायल नहीं हूँ। मेरे गाँव का चपल युवक कटाक्ष करता है, ‘बहुत दिनों बाद गाँव की याद आई, भइया !’ मैं कुछ जवाब नहीं देता। सोचता हूँ, जो गाँव को खा-चबा रहे हैं, उनकी प्रकृति परिसर का भरपूर सुख उपलब्ध है पर वह संवेदना, जो गँवई माटी से मन को जोड़ती है, गाँव की सही पहचान जगाती है, कहाँ है उनके हृदय में ? कहाँ ध्यान है किसी को कि निःसर्ग के आँगन पर सबका आधिकार होता है ! अवदान बाबा को ध्यान था। समष्टि-सुख की चिंता और धरती माता की अस्मिता की रक्षा प्रेरणा ने ही ने उन्हें बलिदान का बल दिया। और वे देवता बन गए। पर उन्हें पूजनेवालों का नाता उनकी ग्रामीण संवेदना से, उनकी बलिदान कथा की रोशनी से क्षीण हो गया है।
एक रस्म पूरी करने के लिए जब-तब उनके नाम पर जय-जयकार कर लेते हैं। मन में पीड़ा कौंधती है, गाँव की माटी शहर के तंग भूगोल में जीने को अभिशप्त है। अपने शोभन के सहज क्रीड़ा-कौतुक के लिए अपेक्षित पोषण सुलभ कराना मेरे लिए असंभव है, और सीढ़ी की सँकरी जगह में नाचते उसका उल्लास-आवेग बार-बार मार खाता है। पर उसकी मूल पीड़ा किसी को स्पर्श नहीं करती। संवेदना का गला घोंटकर आदमी बनाने की नई तकनीकि किसिम-किसिम के केंद्रों में क्रियाशील हो गई है। प्रधान केंद्र आँगन है। दूसरे नंबर पर विद्यालय हैं। और न जाने कितने-कितने सबल माध्यम खड़े हो गए हैं। शायद कायदे का आदमी बनने लग गया है, जो किसी के दुःख-दर्द से संवेदित नहीं होता ! न तो कोई मेरे गाँव की अभागिन काकी का साथ देने को तैयार है और न तो मेरे शोभन का लीला-सहचर बनने को।
निपट अकेला हरिचरन बइठा। अपनी पत्नी के नाम मुझसे चिट्ठी लिखवाता-‘देवंती को मालूम हुआ कि बबुआ बरमेस्सर को मामा किंहा से जल्दी बुलवा लेना। ननिअउरे में लरिका बिगड़ जाते हैं, सो जानना। अउर खियाल रखना कि हमार महतारी को जाड़े में कवनो तरह का तकलीफ न होने पावे। रुपए का दरकार होने से जनाना। फगुआ के पहिले रामबचन कोइरी के हाथे रुपया भेजेंगे। टोल-पड़ोस का समाचार ठीक से लिखवाना। नींबू और शरीफा के गाछ पर नजर रखना।’ और मेरा मन आलोकित हो जाता है कि महानगर में रोजी कमा रहा हरिचरन गाँव की संवेदना में जी रहा है। खोलाबाड़ी के एक अँतरे में जैसे-तैसे गुजारा करने वाले हरिचरन के मन का परिसर बहुत बड़ा है। भूमिहीन होकर भी वह सर्वहारा नहीं है। सर्वहारा वे हैं, जिन्होंने केवल भोग का व्याकरण पढ़ा है, और जो बड़े भूखंड-भवन के स्वामी होकर भी छोटे मनवाले हैं। अड़ोस-पड़ोस के लिए जिनके आँगन में आमंत्रण नहीं है। जड़ वस्तुओं के प्राचुर्य के बावजूद जो अभाव-बोध से दहकते रहते हैं, और जिनके भूगोल को माँ-बाप का बोझा भी असह्य जान पड़ता है। हरिचरन को अपने नींबू-शरीफा की हिफाजत की ही नहीं, अड़ोस-पड़ोस की भी चिंता है। बेटे के भविष्य के लिए ही नहीं, महतारी के सुख के लिए भी वह व्याकुल है। उसका आँगन बड़ा है। मेरे शोभन को भी अपनी नियति से कोई शिकायत नहीं है। मगर मुझे अपने शोभन के लिए उन्मुक्त लीलाक्षेत्र की तलाश है।
घर की सामान्य चर्या के प्रतिकूल चलता है शोभन का उल्लास-आवेग और उसका क्रीड़ा-उत्पात घरवालों की असुविधा का कारण बन जाता है। इसलिए उसे दबाने की विधि सोती जाती है, जो शोभन के स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ती। दोपहर के पहले भरपूर खेल-खाकर कुछ देर गहरी नींद में सोना चाहता है। अकसर सो जाता है। नींद पूरी कर दोपहर के भोजन के समय तक जाग जाता है। और एक बार जब जग जाता है, पूरे वातारण को जगाए रखना चाहता है। दिवा-शयन के अभ्यस्त लोगों के विलास में बाधा पड़ती है। मुझे भी थोड़ी असुविधा होती है। दिन में सोने का वैसा व्यसन तो मुझमें नहीं है, पर दोपहर के भोजन के बाद कुछ समय नीरवता की गोद में पड़ा रहना चाहता हूँ। कभी नींद भी आ जाती है और कभी यों ही शिथिल पड़ा रहना चाहता हूँ। मगर दोस्तों ने ढोल पीटकर जगत् को खबर कर दी है कि मेरा सबसे प्रिय व्यसन है दिवा-शयन। किसी की धारणा का विरोध कर बदनामी से बच पाना संभव होता तो मैं भी अपने पक्ष को स्पष्ट करने की कोशिश करता। मगर यह सोचकर कि मेरी कोशिश का कोई फल नहीं निकलेगा, लोगों के दिलचस्प व्यसन में बाधक नहीं बनना चाहता। दोष-दर्शन मनुष्य का नैसर्गिक व्यसन है। आज कुछ अधिक लोकप्रिय है। पढ़वइए और सफेदपोशों की बात छोड़िए, जिन्हें दुनिया जाहिल-गँवार समझती है उनकी अंतरंग जिंदगी में घुसिए तो पता चल जाएगा कि अपनी सारी कल्पना-शक्ति वे छिद्रान्वेषण में खर्च कर रहे हैं। होती बड़ी रंगीन है दोष की कल्पना। और निंदा रस के आस्वाद में अच्छे-अच्छे लोग फँस जाते हैं। सो मित्रों के मनोरंजन की बात सोचकर उनके सरस कटाक्ष का सुख भोगता रहता हूँ। शोभन के कोलाहल का भी मैं भरपूर आस्वाद लेता हूँ। जिन्हें अपने व्यसन की ही चिंता रहती है उन्हें शोभन की मुखर क्रीड़ा कष्ट देती है। सुबह नहाते ही शोभन ऊँघने लगता है, घरवालों ने उसकी कमजोरी लक्ष्य कर ली है। इसलिए इस जलक्रीड़ाप्रिय बालक को तपती दोपहरी में स्नान का सुख मिल पाता है। सयानों के भोजन के समय ताकि शयन-सुख शोभन के उत्पात से खंडित न हो।
सीढ़ी के बीच के संकीर्ण भूगोल में शोभन की लहर बार-बार क्षत होती है और मेरे मन की आबोहवा बिगड़ जाती है। अपनी उल्लास-उर्मि की अबाधित अभिव्यक्ति के लिए शोभन को बड़े आँगन की तलाश है। शायद सबको फैलाव की खोज है। या कि कोई भी फैलाव में जीना नहीं चाहता। अपनी दुनिया को हर तरह से बंद कर सुख भोगने की एकांत साध से लोग व्याकुल हैं। मेरा देहाती मन मैदान-जंगल और बड़े आँगन से जुड़ी उन्मुक्तता के लिए पागल बना रहता है। महानगर की बंद जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने में सहज संकोच होता है। नगर सभ्यता के आतंक से बिना पूर्व सूचना दिए किसी के यहाँ जाता नहीं। शाम को किसी के यहाँ जाने में और भी डर लगता है। किसी का रस-भंग नहीं करना चाहता। अनुभव से बात समझ में आ गई है कि दूरदर्शन कार्यक्रम और वारुणी-लीला में बाहरी आदमी का हस्तक्षेप किसी को रुचता नहीं, शिष्टाचार के दबाव में भले ही कुछ देर कोई झेल ले अपने अतिथि को। इसलिए अर्गलाविहीन देहाती मन नए शऊर में जीने को मजबूर है। यह लाचारी मेरे मूल भाव को घायल करती रहती है जैसे मेरे शोभन का उल्लास संकीर्ण भूगोल से आहत होता रहता है।
मगर आज जब मैं अपने गाँव के सिवान में प्रवेश करता हूँ, अनायास जाँ निसार अख्तर के शेर की पंक्ति याद आती है-‘गाँव में आकर शहर बसे, गाँव बेचारे जाएँ कहाँ’ कहाँ गया गाँव का खुलापन ? वह उन्मुक्त परिसर, जिसका चप्पा-चप्पा अपना लगता था, गाँव से किसने छीन लिया ? अड़ोस-पड़ोस के दुआर-आँगन में अधिकारपूर्वक प्रवेश करने वाले गँवई मन को किसने मार दिया ? कहाँ गायब हो गई मेरी माटी की सजातीय पहचान ? नए लोगों को पुराने परिदृश्य-प्रसंग सरासर झूठ लगते हैं। और उनकी व्यंग्य-मुसकान के दंश को झेलना हमारी नियति है। गाँव का नैसर्गिक खुलापन अब केवल कहने-सुनने की बात है; उस रहनि में जीना तो दूर, कोई संवेदना पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आजादी के बाद कितनी गहरी गुलामी में हम फँस गए। सबसे बड़ी क्षति हुई कि हमारा लीला-परिसर बहुत छोटा हो गया। इतना छोटा कि मन को जब-तब खरोंच लग जाती है जैसे मेरे शोभन के उल्लास को मेरी सँकरी जगह प्रायः कुंठित करती रहती है। और उन्मुक्त परिसर की भूख मेरे भीतर गाँव की याद जगा देती है। मेरे बाल्यकाल के लीलाधाम की याद। उस गाँव की याद, जिसने हमारे उल्लास-नर्तन के लिए उन्मुक्त भूगोल दिया था, बड़े परिदृश्य का आस्वाद दिया था, धरती के छोह और चुनौती का मर्म समझाया था। वही अपना गाँव आज पराया लगता है। पराई क्यों लगने लगी अपनी माटी माँ ? वह माँ, जिसकी स्वाभिमान-रक्षा के लिए व्याकुलताविद्ध युवक ने गवना की ‘पीअरी’ पहने अपने को होम दिया था। उस बलिदान का चौरा पूजनेवाले और अवदान बाबा को सर्वोच्च देव-प्रहरी मानकर संकटमोचन के लिए सुमिरते, उनकी जय-जयकार से हर अनुष्ठान शुरू करने वाले गाँव के नवहीं ‘रामगढ़ ढाला’ पर बैठे कूटबुद्धि पैनी करने में मशगूल दिखाई पड़ते हैं। वे अवदान बाबा के मर्म को नहीं समझते। नहीं समझते उस अवदान के मूल्य को कि गाँव की अन्नपूर्णा के आँचल की रक्षा करते उस युवा सत्याग्रही ने अपने आँगन में सद्य : उदित शोभा को राख में मिला दिया था, और परवर्ती पीढ़ी के उल्लास की सुरक्षा के लिए उदग्र होकर धरती माता को अपने रक्त से सींच दिया था ताकि माटी माँ का आँगन सिकुड़ न जाए, गाँव का माथा न झुक जाए, नई पौध की उल्लास-तरंगें संकीर्ण परिसर में कैद होकर ऊँचाई को स्पर्श करने के पहले ही मुरझा न जाएँ। अवदान बाबा के रक्त ने गाँव को बड़ा भूखण्ड उपलब्ध कराया, अन्यथा समृद्धि-दर्प का आधार गाँव के हाथ से निकल गया होता। बाबा का स्मरण करते गर्व होता है, और अपनी अपात्रता पर ग्लानि भी कि अपने शोभन की ऊर्जा-क्रीड़ा के लिए उपयुक्त आँगन नहीं सुलभ करा पा रहा हूँ। और पीड़क है कि उसकी उपद्रव-लीला का सहचर बनने को कोई तैयार नहीं है।
अपने विलास-मुख के लिए सयाने शोभन की प्रकृति बदलने की कोशिश में लगे हैं। उसकी सहज तरंग को मारने की सयानी कोशिश मेरी भावना को घायल कर देती है। उसके नहाने-खाने, खेलने और स्वच्छंद लीला को शहराती चर्या-छंद से अनुशासित करनेवाले बड़े लोग कितने नादान हैं कि चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक बड़ी संभावना को अपनी महत्त्वकांक्षा के अंधे आवेग में तहस-नहस किए जा रहे हैं। बच्चे को ‘आदमी’ बनाने की सनकी स्पर्द्धा हर माँ-बाप को पागल बनाए रहती है।
शहर तो शहर, अपने गाँव के लोगों से बोलते-बतियाते मैंने लक्ष्य किया, बेटों के आचरण से लगभग हर बाप विक्षिप्त है। आतंकित रहता है कि बेटे का औद्धत्य कहीं घायल न कर दे। युवा पीढ़ी की ढीठ मुद्रा से बूढ़ी पीढ़ी भीत रहने लगी है। यह आश्वासन की बेटा जवान होगा तो विपदा दूर होगी, कमजोर हो गया है। कभी-कभी सोचता हूँ कि जन्म के साथ ही जिसे भोग का व्याकरण समझाया गया, उसकी नजर में माँ-बाप का मूल्यहीन हो जाना अचरज की बात नहीं है। पशु-पक्षी और वनस्पति-लोक के अमर्यादित भोग का अंधा आवेग पगलाए आदमी की मनोवृत्ति का संकेत देता है कि पयपान से तुष्ट न होने वाला आदमी माँ का मांस-भक्षण करने को व्याकुल हो उठा है। तथाकथित सयानों ने यह जीवन-कला सिखाई है। दुःख उन्हींका गहराया है। माता की अवमानना आज का पीड़क यथार्थ है।
जिस धरती माँ की रक्षा करते अवदान बाबा ने अपनी नवपरिणिता के सौभाग्य को क्षार कर दिया था, वह माँ बेटों की अमर्यादित भोग की मार से श्रीहीन होती जा रही है। लोगों का विलास कुछ भी सुनने-समझने को तैयार नहीं है। दायरा सिकुड़ रहा है और मैला हो रहा है। दूसरे का भूगोल हड़पने और शोभाहीन बनानेवाली पाप-बुद्धि को पौरुष–प्रताप माना जाने लगा है। जिस पर हमें गर्व था वह लम्बा-चौड़ा, हँसमुख परिसर मेरा क्रीड़ाक्षेत्र और मेरा आँगन छोटा और उदास हो रहा है। पर अपना आत्मीय परिसर पराया लगता है। मूल पहचान दब गई है। कुछ घट गया है। ऐसा कुछ जो बाँधे रहता था, अपनी संतान को हाँक लगाता रहता था। लगता है, यात्रा को विराम देने के लिए अपरिचित पड़ाव पर हम ठहरे हैं और अत्यधिक सतर्क हैं कि कहीं कोई चूक न हो जाए। अपने आँगन में जीने का यह ढंग नहीं है। मेरे शोभन की शैली ठीक है। खुल के उछलता है। घायल होकर भी अपने परिसर को अपना मानता है। अपने कौतुक से अपने संकीर्ण भूगोल को हँसमुख बनाए रहता है। घर के सयानों को असुविधा होती है तो होती रहे। अपना संकीर्ण भूगोल मुझे छोटा लगता है। शोभन को बड़ी जगह उपलब्ध कराने के लिए व्याकुल रहता हूँ। पर शोभन की सीढ़ी की सँकरी जगह हमेशा मुसकराती और बड़ी लगती है। अपनी क्रीड़ा के लिए वह दूसरे का भूगोल हड़पना नहीं चाहता। शोभन की चाल मेरे गाँव की चाल से कुछ अलग है।
गाँव गया था। मेरी पट्टीदारी की काकी अपना दुर्भाग्य निवेदित करते कहने लगी-‘चकबंदी में मेरा खेत खो गया। वही जीने का सहारा था।’ उनकी पीड़ा मुझे अपने गिरफ्त में ले लेती है। बउड़म ससुर और निठल्ले भँगेड़ी पति के चलते भूमि-सम्पन्न परिवार की बहू निःस्व हो गई। ससुर-पति की सनक में स्वाहा होने से बची महज ढाई बीघे जमीन को चकबंदी की चाल खा गई। गाँव के समर्थ लोगों से काकी के दुर्भाग्यमोचन का संकेत करता हूँ, यह समझते हुए कि किसी को किसी की भूगोल-सुरक्षा की चिंता नहीं है। दूसरे के उल्लास को हड़पने की ताक में सारी दुनिया पगला गई है। भावना के आग्रह से तथापि अनुरोध करता हूँ। अपनी संवेदना के करीब गाँव के बेटे कैफी आजमी को पाता हूँ-‘वो मेरा गाँव है और वो मेरे गाँव के चूल्हे, जहाँ आग तो आग धुआँ नहीं मिलता।’ थोड़ी तसल्ली मिलती है कि मैं अकेला घायल नहीं हूँ। मेरे गाँव का चपल युवक कटाक्ष करता है, ‘बहुत दिनों बाद गाँव की याद आई, भइया !’ मैं कुछ जवाब नहीं देता। सोचता हूँ, जो गाँव को खा-चबा रहे हैं, उनकी प्रकृति परिसर का भरपूर सुख उपलब्ध है पर वह संवेदना, जो गँवई माटी से मन को जोड़ती है, गाँव की सही पहचान जगाती है, कहाँ है उनके हृदय में ? कहाँ ध्यान है किसी को कि निःसर्ग के आँगन पर सबका आधिकार होता है ! अवदान बाबा को ध्यान था। समष्टि-सुख की चिंता और धरती माता की अस्मिता की रक्षा प्रेरणा ने ही ने उन्हें बलिदान का बल दिया। और वे देवता बन गए। पर उन्हें पूजनेवालों का नाता उनकी ग्रामीण संवेदना से, उनकी बलिदान कथा की रोशनी से क्षीण हो गया है।
एक रस्म पूरी करने के लिए जब-तब उनके नाम पर जय-जयकार कर लेते हैं। मन में पीड़ा कौंधती है, गाँव की माटी शहर के तंग भूगोल में जीने को अभिशप्त है। अपने शोभन के सहज क्रीड़ा-कौतुक के लिए अपेक्षित पोषण सुलभ कराना मेरे लिए असंभव है, और सीढ़ी की सँकरी जगह में नाचते उसका उल्लास-आवेग बार-बार मार खाता है। पर उसकी मूल पीड़ा किसी को स्पर्श नहीं करती। संवेदना का गला घोंटकर आदमी बनाने की नई तकनीकि किसिम-किसिम के केंद्रों में क्रियाशील हो गई है। प्रधान केंद्र आँगन है। दूसरे नंबर पर विद्यालय हैं। और न जाने कितने-कितने सबल माध्यम खड़े हो गए हैं। शायद कायदे का आदमी बनने लग गया है, जो किसी के दुःख-दर्द से संवेदित नहीं होता ! न तो कोई मेरे गाँव की अभागिन काकी का साथ देने को तैयार है और न तो मेरे शोभन का लीला-सहचर बनने को।
निपट अकेला हरिचरन बइठा। अपनी पत्नी के नाम मुझसे चिट्ठी लिखवाता-‘देवंती को मालूम हुआ कि बबुआ बरमेस्सर को मामा किंहा से जल्दी बुलवा लेना। ननिअउरे में लरिका बिगड़ जाते हैं, सो जानना। अउर खियाल रखना कि हमार महतारी को जाड़े में कवनो तरह का तकलीफ न होने पावे। रुपए का दरकार होने से जनाना। फगुआ के पहिले रामबचन कोइरी के हाथे रुपया भेजेंगे। टोल-पड़ोस का समाचार ठीक से लिखवाना। नींबू और शरीफा के गाछ पर नजर रखना।’ और मेरा मन आलोकित हो जाता है कि महानगर में रोजी कमा रहा हरिचरन गाँव की संवेदना में जी रहा है। खोलाबाड़ी के एक अँतरे में जैसे-तैसे गुजारा करने वाले हरिचरन के मन का परिसर बहुत बड़ा है। भूमिहीन होकर भी वह सर्वहारा नहीं है। सर्वहारा वे हैं, जिन्होंने केवल भोग का व्याकरण पढ़ा है, और जो बड़े भूखंड-भवन के स्वामी होकर भी छोटे मनवाले हैं। अड़ोस-पड़ोस के लिए जिनके आँगन में आमंत्रण नहीं है। जड़ वस्तुओं के प्राचुर्य के बावजूद जो अभाव-बोध से दहकते रहते हैं, और जिनके भूगोल को माँ-बाप का बोझा भी असह्य जान पड़ता है। हरिचरन को अपने नींबू-शरीफा की हिफाजत की ही नहीं, अड़ोस-पड़ोस की भी चिंता है। बेटे के भविष्य के लिए ही नहीं, महतारी के सुख के लिए भी वह व्याकुल है। उसका आँगन बड़ा है। मेरे शोभन को भी अपनी नियति से कोई शिकायत नहीं है। मगर मुझे अपने शोभन के लिए उन्मुक्त लीलाक्षेत्र की तलाश है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i