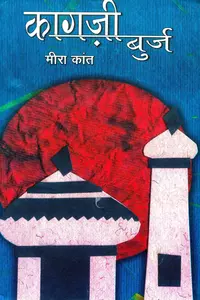|
पारिवारिक >> ततः किम् ततः किम्मीरा कांत
|
253 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है श्रेष्ठ उपन्यास....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
याद-भर आसमान
सम्बन्धों की भी एक सन्धि-वेला होती है ऋचा...शुरू में भी, अन्त में भी।
‘‘आसमान क्या होता है बब्बा ?’’
‘‘...’’
‘‘बब्बा...आसमान क्या होता है ?’’
‘‘जहाँ नजर टिक जाए वही आसमान है बेटा ।’’
एक धूमिल-सी मुस्कान कानन के चेहरे का स्पर्श कर गई। चेहरा कुछ ऊपर की ओर उठ गया। पलकें कुछ और फैल गईं। उनमें एक हल्की याद-भर जितना आसमान समा गया। और होंठ...बस जरा-सा फैले, कुछ क्षण ठहरे और लौट आए।
‘‘क्या सोच रही हो ?’’
‘‘हैं...!’’ कानन ने धीमे से आँखें ढाँप लीं, पलकों से। आसमान नीचे उतर गया, बहुत गहरे। पलकों ने फिर राह बनाई एक नई, धुली-सी दृष्टि के लिए। हल्की नीली दृष्टि, ‘‘सन्धि-वेला इंसान को बहुत तंग करती है जीवन में।’’
‘‘ऐसा क्यों लगा तुम्हें ?’’
‘‘..बचपन और बुढ़ापा जीवन की सन्धि वेला ही है..और सम्बन्धों की भी एक सन्धि-वेला होती है ऋचा...शुरू में भी, अन्त में भी।’’
ऋचा ने हरी नम घास पर खुद को छोड़ दिया। उसके दोनों हाथों की उँगलियाँ आपस में जकड़ गईं और एक नर्म सिरहाना तैयार हुआ। उस पर अपने खुले घने बालों को टिकाते हुए उसने कहा, ‘‘क्या क्या सोचती रहती हो तुम भी बस !’’
‘‘ऋचा आज..आज यहाँ इतना खुला और नीला...आसमान जैसा ही आसमान देखा तो बचपन के कुछ लम्हे लौट आए..फिर लगा कि..आसमान..आसमान कहाँ महसूस किया है मैंने !’’
‘‘तो जहाँ कभी ठहरी थीं वो ?’’
‘‘नहीं ऋचा...अब इधर लगता है कि आसमान वो नहीं था।’’
‘‘...’’
‘‘नजर टिक ही कहाँ पाई !’’
उम्र की एक खास खिड़की से बाहर देखने पर क्यों दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह तब थी जब हम भी बाहर थे खिड़की से। खिड़की से बाहर एक लम्बी सुनसान सड़क। चारों ओर पेड़ लगे हैं। हरे-भरे। पर नजर जाकर टिकती है वो दूर उस एक अकेले पेड़ पर। सूखे पत्तोंवाला पेड़। पतझड़ से सजा पेड़। ऐसा ही कुछ सोचा कानन ने।
हर जिन्दगी का एक पतझड़ होता है। यही कोई 45 के आस-पास या न भी होता हो। सिर्फ कानन को लगा हो यह पेड़ देखकर। वह भी अपना 39वाँ पूरा करने को ही थी। जिन्दगी का पतझड़...कितना भिन्न होता है...उतना ही शायद जितना पेड़ जिन्दगी से या जिन्दगी पेड़ से। इस पतझड़ में एक जीवन मिलता है-भीतर के डर को...सलेटी अकेलेपन को। अब तक जो डर खुशनुमा लम्हों या सुखों पर पुता होता था वह अब दुखों के लिए गर्म ऊनी जुराब बुनने लगता है जो हर साल कुछ और बड़े करने पड़ते हैं। यही नहीं सम्बन्धों का भी एक पतझड़ होता है। सूखे पत्तो की तरह ही खड़खड़ाकर गिरते हैं वे भी। शोर मचाते हुए...और कभी-कभी उस एक पत्ते की तरह हौले से...बेआवाज..चुपचाप...। पर ये बेआवाज झरनेवाले सम्बन्ध ही भीतर आवाजों के टीले उगा देते हैं।...इतने साथ-साथ कि उन टीलों की मिट्टी भी अलग से न पहचानी जा सके।
‘‘आसमान क्या होता है बब्बा ?’’
‘‘...’’
‘‘बब्बा...आसमान क्या होता है ?’’
‘‘जहाँ नजर टिक जाए वही आसमान है बेटा ।’’
एक धूमिल-सी मुस्कान कानन के चेहरे का स्पर्श कर गई। चेहरा कुछ ऊपर की ओर उठ गया। पलकें कुछ और फैल गईं। उनमें एक हल्की याद-भर जितना आसमान समा गया। और होंठ...बस जरा-सा फैले, कुछ क्षण ठहरे और लौट आए।
‘‘क्या सोच रही हो ?’’
‘‘हैं...!’’ कानन ने धीमे से आँखें ढाँप लीं, पलकों से। आसमान नीचे उतर गया, बहुत गहरे। पलकों ने फिर राह बनाई एक नई, धुली-सी दृष्टि के लिए। हल्की नीली दृष्टि, ‘‘सन्धि-वेला इंसान को बहुत तंग करती है जीवन में।’’
‘‘ऐसा क्यों लगा तुम्हें ?’’
‘‘..बचपन और बुढ़ापा जीवन की सन्धि वेला ही है..और सम्बन्धों की भी एक सन्धि-वेला होती है ऋचा...शुरू में भी, अन्त में भी।’’
ऋचा ने हरी नम घास पर खुद को छोड़ दिया। उसके दोनों हाथों की उँगलियाँ आपस में जकड़ गईं और एक नर्म सिरहाना तैयार हुआ। उस पर अपने खुले घने बालों को टिकाते हुए उसने कहा, ‘‘क्या क्या सोचती रहती हो तुम भी बस !’’
‘‘ऋचा आज..आज यहाँ इतना खुला और नीला...आसमान जैसा ही आसमान देखा तो बचपन के कुछ लम्हे लौट आए..फिर लगा कि..आसमान..आसमान कहाँ महसूस किया है मैंने !’’
‘‘तो जहाँ कभी ठहरी थीं वो ?’’
‘‘नहीं ऋचा...अब इधर लगता है कि आसमान वो नहीं था।’’
‘‘...’’
‘‘नजर टिक ही कहाँ पाई !’’
उम्र की एक खास खिड़की से बाहर देखने पर क्यों दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह तब थी जब हम भी बाहर थे खिड़की से। खिड़की से बाहर एक लम्बी सुनसान सड़क। चारों ओर पेड़ लगे हैं। हरे-भरे। पर नजर जाकर टिकती है वो दूर उस एक अकेले पेड़ पर। सूखे पत्तोंवाला पेड़। पतझड़ से सजा पेड़। ऐसा ही कुछ सोचा कानन ने।
हर जिन्दगी का एक पतझड़ होता है। यही कोई 45 के आस-पास या न भी होता हो। सिर्फ कानन को लगा हो यह पेड़ देखकर। वह भी अपना 39वाँ पूरा करने को ही थी। जिन्दगी का पतझड़...कितना भिन्न होता है...उतना ही शायद जितना पेड़ जिन्दगी से या जिन्दगी पेड़ से। इस पतझड़ में एक जीवन मिलता है-भीतर के डर को...सलेटी अकेलेपन को। अब तक जो डर खुशनुमा लम्हों या सुखों पर पुता होता था वह अब दुखों के लिए गर्म ऊनी जुराब बुनने लगता है जो हर साल कुछ और बड़े करने पड़ते हैं। यही नहीं सम्बन्धों का भी एक पतझड़ होता है। सूखे पत्तो की तरह ही खड़खड़ाकर गिरते हैं वे भी। शोर मचाते हुए...और कभी-कभी उस एक पत्ते की तरह हौले से...बेआवाज..चुपचाप...। पर ये बेआवाज झरनेवाले सम्बन्ध ही भीतर आवाजों के टीले उगा देते हैं।...इतने साथ-साथ कि उन टीलों की मिट्टी भी अलग से न पहचानी जा सके।
सिल्वर फिश
अपने यहाँ पत्नी माँ, बहन, बेटी, गणिका-सब कुछ हो सकती है पर श्मशान-बन्धु
नहीं हो सकती।
पहले खुद पढ़ते हुए और फिर लड़कियों को पढ़ाते-पढ़ाते जिन्दगी भी कानन के लिए एक ‘सब्जेक्ट’-सी बन गई थी। फिलासफी...दर्शन..फलसफा। हर सफा एक अलग फलसफा।
पहली खुशबू जो याद आती है वह माँ की है। धुले हल्की छींटवाले कपड़ों में साँस लेती धीमी गतिवाली धड़कनों की। बिना किसी आस के लपक-झपक करती उस चमक की जो आँखों में खिलती है जाड़ों की उस हल्की धूप की तरह जिसे हर सुबह मुँडेरो पर सुबह को सुबह बनाने के लिए अक्सर आना ही होता है। या एक ठंडी खुशबू..गर्मियों में खस जैसी।
इससे तेज़ एक और खुशबू थी आस-पास। बब्बा की। एक ऐसी खुशबू जो खींचती थी सर्दियों में रजाई न होने पर सुबह गली में चक्कर लगाते धुनिया के टुनटुने की झंकार की तरह। और बब्बा का साथ ? बाजारों में बड़ी दुकानों के बाहर एक कोने में बैठा पुराने या बिना चाबी के तालों की चाबियाँ बनानेवाला। जिन्दगी के हर सवाल की अपनी तरह की एक अलग ‘मास्टर की’ रखनेवाला साथ। ‘‘बब्बा-बब्बा’’ में ऐसी पिरोई रहती थी कानन कि पहली बार छठी कक्षा के लिए बड़े स्कूल में दाखिले का फॉर्म भरते हुए उसे महसूस हुआ था कि वे उसके पिता नहीं उसकी माँ के भाई हैं क्योंकि फॉर्म में जो नाम भरा गया वह बब्बा का नहीं था। तभी समझ गई थी कानन कि कोई चाहे या न चाहे एक नाम जीवन भर उसके साथ रहेगा। चाहे सिर्फ प्रमाण-पत्रों या फॉर्मों में ही। उसके पिता का नाम-बद्री प्रसाद कौशिक।
चेतना के धराऊ बक्सों में रखी स्मृतियों पर समय की सिल्वर फिश अपने निशान जरूर छोड़ती है पर स्मृतियाँ...वो तो बनी ही रहती हैं वहाँ, उन कुछ निशानों की तब्दीलियों के साथ। बचपन में...बहुत छुटपन में...वह अक्सर चुपके से आकर बब्बा की टाँगों के साथ खड़ी हो जाती थी और धीरे से उनकी तर्जनी पकड़ लेती थी। और खड़ी रहती थी यों ही उनके साथ उन्हें देखती हुई कि कैसे वे सुबह बागीचे के हर पौधे, हर फूल, कली और हर पत्ते को निहारते थे। उनकी बस एक उँगली..सिर्फ एक तर्जनी ही चाहिए होती थी कानन को सहारे के लिए। अगर कभी कुछ और उँगलियाँ पकड़ में आ जातीं तो उन्हें कुछ घुमाकर पीछे कर देती थी वह। पूरे हाथ का सहारा जो नहीं चाहिए होता था। बब्बा खीझ जाते थे इस तरह बाकी उँगलियाँ घुमाने पर, ‘‘ये क्या किया करे है तू कुक्कू ?’’ और वह मुस्कुराकर अपने हाथ में थामी उस तर्जनी को देखने लगती थी। छोटे कद के बब्बा का छोटा और हड्डियों के एहसासवाला दायाँ हाथ। अनामिका में ठहर-सी गई पुखराज जड़ी एक सोने की अँगूठी जो अक्सर उसका ध्यान खींचती थी। जो ‘एक ज़माने से’ वहीं थी। शायद बचपन में पहनी अँगूठी हाथ के साथ साथ अपना आकार बड़ा करती चलती हो !
कानन बस ढाई वर्ष की थी जब 262 बी.एम. अहाता, साहिबाबाद में यही हाथ उसकी ओर बढ़ा था और पहली बार उसकी निगाह उस अँगूठी की ओर गई थी। उस हाथ की तर्जनी पकड़कर लगभग खिंचते हुए कानन ने माँ और बहन के साथ दिल्ली की एक सरकारी कॉलोनी के एक प्लैट में प्रवेश किया था। फिर ता-जिन्दगी उसने जब-जब निगाह उठाई तो यही हाथ सामने पाया। मगर उसकी अपनी बारी आने पर वह सिर्फ उस हाथ की तर्जनी ही पकड़ती रही थी। बस।
बी.एम. अहाता उसकी जिन्दगी से मिट गया था। अब कभी-कभार वह बब्बा के प्यार भरे गुस्से या खीझ से भरे एकालाप में सिर उठाता भी था तो अपने असली भौंदू मल के अहाते के रूप में ही। अपनी कुक्कू को छेड़ते हुए वे कभी कभी कहते थे, ‘‘आहता तो वहीं छूट गया और हमारा भौंदूमल यहाँ आ गया।’’
माँ को देखा था पापा के नाम-भर का कत्थई देवत्व थामे जिन्दगी की चढ़ाई चढ़ते। हल्के कदमों से, फुर्सत के साथ। किसी बदलाव के इन्तजार के बिना। एक ऐसी सपाट जिन्दगी जीते जो जानती है कि ‘घटना’ शब्द उसके लिए नहीं बना है। जिसे गुजरते-गुजरते ही गुजरना है।
एक बेटा और दो बेटियाँ उनकी जमा पूँजी थी विवाहित जीवन के कुल सात सालों की जिसका अन्ततः बँटवारा हुआ था। उनके हिस्से में आई कानन और बड़ी बेटी केसर।
माँ की तबीयत में एक वैसा ही ठहराव था जैसा उनकी आँखों में उतर आया था बाद के दिनों में। एक सहनशील, परम्परागत, सिरझुकाऊपन में गुँथी हींग और देसी घी से महकते हाथोंवाली खुशबू जो पापा को नहीं चाहिए थी। न दिन के उजाले में, न रात के बियाबान में। और वे तीनों प्राणी आ गए थे बब्बा के पास हमेशा के लिए।
बब्बा यानी श्री मुकुट बिहारी त्रिवेदी, सुपुत्र मास्टर कृष्ण बिहारी त्रिवेदी को नामकरण का जो मुकुट धारण कराया गया था, कोई नहीं जानता था कि इस तीन वर्ष के बालक को आजीवन इसकी जिम्मेदारियों को ढोना होगा। लक्कड़ का बोझा उठाए पहाड़ी मजदूर की भाँति ऊँचाइयों पर चढ़ते-उतरते। पहलौठी की सन्तान और चार बहनों के एकमात्र भाई बिहारी ने जाने क्यों और कैसे चारों छोटी बहनों के लिए भैया से ‘बब्बा’ हो गए थे। बहुत पीछे चलें तो इसका कारण शायद उनकी तीसरी बहन स्नेहलता हो। बचपन में एक तो स्नेह को मुकुट बिहारी के लिए ‘भाई साहब’ और ‘भैया’ जैसे सम्बोधन कभी रास नहीं आए। ये तो सभी कहते हैं अपने भाई को ! फिर वह भी क्यों कहे ? मुकुट बिहारी कोई औरों जैसे तो हैं नहीं। जानता है किसी का भाई इतनी अंग्रेजी, इतनी हिन्दी और साथ ही इतना उर्दू-फारसी ! अपनी छोटी बहन को अपनी सारी पढ़ाई पढ़ा देने का मन होता है किसी का ? बहन का सहेलियों के साथ पिकनिक जाने का मन हो तो बाऊजी को तरह-तरह से मनाता है कोई भाई। बहन की किताब से अचानक पानी की धार की तरह कोई सूखी पंखुड़ी बह निकले तो काँपती हुई उँगलियों से चुपचाप उन्हीं वर्कों में दोबारा रखता है कोई भाई ! तो उन्हें भाई साहब या भैया क्यों कहा जाए फिर !
मुकुट बिहारी भी कौन उन्नीस थे। जब-तब बहनों पर ऊपरी रौब जमाकर याद दिलाते रहते थे कि वे सबसे बड़े हैं। इसलिए ‘बब्बा’ सम्बोधन उन पर किशोर वय से फबा भी खूब।
मुकुट बिहारी के पिता मास्टर कृष्ण बिहारी त्रिवेदी अपने हाथों से अपनी दो बड़ी बेटियों का विवाह कर गए थे। पहली आशालता गंगानगर में ब्याही थी। पहले ही प्रसव में जीवन से थक कर नवजात के साथ ही चल दी। चन्द ही महीनों में आशालता के ससुरालवालों ने पीछे छूट गए उसके पति के लिए दूसरी बहन सुमनलता का हाथ माँग लिया। थोड़ा बहुत सोच-विचार कर कृष्ण बिहारीजी इस नतीजे पर पहुँचने ही वाले थे कि ‘इसमें हर्ज भी क्या है’ कि तीसरी बहन स्नेहलता ने हौले से उनसे एक सवाल कर लिया।
वे रसोई में बैठ भोजन करते हुए अपनी पत्नी के सामने तीन लड़कियों को ब्याहने की जिम्मेदारी निबाहने का राग छेड़ बैठे थे। यह शायद उनके लिए अपना फैसला सुनाने की भूमिका रही होगी। तभी उनकी थाली में रोटी परोसती हुई स्नेह ने काँपती आवाज में पूछा, ‘‘बाऊजी अगर सुमन जीजी को भी कुछ हो गया तो अगले साल मुझे भी ब्याह दोगे गंगानगर ?’’ बाऊजी ने दूसरी रोटी का एक कौर तोड़ा था और बड़े चाव से हाथ आलू की झोलवाली सब्जी की ओर बढ़ाया ही था कि रसोई में धुएँ की तरह एक चीख भर आई। अँगीठी पर फुलका सेंकती उनकी पत्नी ने गलती से फुलके के स्थान पर जलता हुआ कोयला पकड़ लिया था। कृष्ण बिहारीजी को भी थाल छोड़कर उठना पड़ा। स्नेह चिल्लाती हुई बाहर भागी। शायद सुमन और मुकुट को बुलाने। इधर मास्टरजी आलू के झोल से सने अपने दाएँ हाथ के नीचे बाएँ हाथ की हथेली लगाए अजब मुद्रा में खड़े थे। क्या करें, क्या न करें ! अब तक उनकी पत्नी समझ चुकी थी कि अपने जले का उपचार स्वयं ही करना होता है। सो पास रखी आटे की परत से उसने आधी लोई जितना सना हुआ आटा लिया और अपनी तर्जनी और अँगूठे पर लपेट लिया। बात आई गई हो गई मगर बाऊजी अपना फैसला सुनाने की अब हिम्मत न जुटा पाए। गंगानगरवालों का ‘न’ कह दी गई।
गंगानगरवालों को कही गई यह ‘न’ त्रिवेदी परिवार को बहुत भारी पड़ी। उतने प्रयास गंगानगरवालों ने अपने बेटे के दूसरे विवाह के लिए भी नहीं किए होंगे जितने कि हर जगह से सुमनलता का ब्याह रुकवाने के हुए। दामाद का विवाह साल-भर बाद हो गया। बारात में कृष्ण बिहारीजी भी गेंदे के फूलों की माला धारण कर समधी की जिम्मेदारियों में हाथ बँटाते देखे गए। स्वर्गीया आशालता की माँ भी समय-समय पर हर नेग-टेहले में जाकर खड़ी हुईं। मगर गंगानगरवालों के दिलों में चुभी फाँस भला इतने से ही निकल जाती ! पूरे तीन सालों में उन्होंने सुमनलता के सात रिश्ते तुड़वाए।
अब तक मास्टरजी समझ चुके थे कि गंगानगरवालों को ‘न’ कहना जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल रही है। दुनिया उन्हें अँधियारी दिखाई देने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि सुमन तो सुमन भविष्य में स्नेहलता और गीता दोनों अनब्याही रह जाएँगी। वे भीतर तक सहम गए थे। अबकी बार उन्होंने घर में किसी से ज्यादा सलाह-मशविरा करना भी ठीक नहीं समझा। वे समझ गए थे कि बिनब्याहे लड़के की फिराक में ज्यादा दिन नहीं रहा जा सकता। इटावा से जैसे ही शिव मोहन बाबू का रिश्ता आया उन्होंने सगाई ठहरा दी। यहाँ तक कि बाद में पूछा गया कि पहली पत्नी से उन्हें कितने बच्चे हैं सगाई के बाद उनके तीनों बच्चे जब सुमनलता से मिलने दिल्ली आए तभी लोगों को उनके बारे में ठीक-ठीक जानकारी मिल पाई।
सुमनलता के भी दो बच्चे हुए। सो इटावा में घर गृहस्थी के चक्कर में वह ऐसी लगी कि मायके की याद भी कभी-कभार सुख-दुख के समय ही आती थी। पर जब आती थी तो बरसात में अचानक उभर आए मोच के दर्द की तरह कसकती थी। ऐसी कसक में बस जी वहाँ से हटा लिया जाता है, उपचार क्या करना !
पीछे रह गई स्नेहलता और गीता। गीता न तो शक्ल से तीनों लताओं की बहन लगती थी, न नाम से। गीता के होने पर तीनों लताएँ एक हो गईं और बाऊँजी को इस बात के लिए राजी कर ही लिया कि गोल-मटोल रूहअफ़्ज़ा वाले दूध जैसी छुटकी कोई लता नहीं बनेगी। बाऊजी को राजी तो होना पड़ा मगर उनकी भी एक शर्त थी। नाम वही रखा जाएगा जो सद्गुण सम्पन्न और फिल्मों से कतई दूर होगा। सो बहुत खोजबीन के बाद ‘गीता’ नाम पर पूरा परिवार एकमत हो पाया था।
वह बुद्ध पूर्णिमा की भोर थी जब कृष्ण बिहारीजी स्नान कर, आँगन में सू्र्य देवता को अर्घ्य दे, तुलसीजी की देहरी पर मस्तक नवा कर ही चुके थे कि दालान में चलते हुए एक झटके के साथ ठहर गए। उनके सीने में टीस-सा दर्द उभरा जो बादलों की तरह अन्दर घुमड़ता रहा। बस उन्हीं बादलों में उन्होंने जीवन की अन्तिम साँस ली। पास ही रखी आरामकुर्सी पर उन्होंने खुद को छोड़ दिया।
मुकुट बिहारी को अपने सम्बोधन ‘बब्बा’ का अर्थ अब समझ आने लगा था। सारा घर हर अच्छी-बुरी घड़ी में उन्हीं की ओर तकता था। माँ की इच्छानुसार साल-भर बाद उनका विवाह अपनी मामी की छोटी बहन विद्यावती से सम्पन्न हुआ। माँ मानो उसी का इन्तजार कर रही थी। विद्यावती को घर-गृहस्थी क्या सौंपी, दुनिया सौंप चली। विद्यावती भी जीवन-पर्यन्त भाभी कहलाने के बावजूद सही मायने में ‘बब्बा’ की अर्द्धांगिनी बनी रहीं।
गीता तब बी.ए. में थी कि एक दिन सुबह स्नेह ने उसे देखा तो अपनी हिचकियाँ न रोक पाई। उसके होंठों से एक नीली धार बहकर गले से होती हुई तकिए के गिलाफ को भिगो रही थी। कारण कोई न जान पाया। बिन माँ-बाप की बेटी के दुखी होकर आत्महत्या करने की तोहमत भाई-भाभी पर ही लगी। वे सहम गए थे। अभी उन्हें स्नेहलता का घर बसाना था।
मुकुट बिहारी ने अंग्रेजी में एम.ए. किया था मगर जान उनकी उर्दू और कुछ-कुछ फारसी में बसती थी। ‘दीवान-ए-ग़ालिब’ रात को टार्च की जगह सिरहाने रखा मिलता था। एम.ए. के बाद चाहा तो बहुत कि कालेज लेक्चरर हो जाएँ, मगर उससे पहले ही वे कृ्षि मन्त्रालय की एक लिखित परीक्षा पास कर उसमें उत्तीर्ण होने की गलती कर बैठे। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही तरक्की भी मिल गई। वहाँ अंडर सेक्रेटरी हो गए। समय और नौकरी के दबदबे ने पढ़ाने की वो चाह धुँधला दी। इस बीच शादी हो चुकी थी, माँ-बाप दोनों जाते रहे, गीता भी नहीं रही और स्नेहलता को भी कब तक नए-नए उपन्यासों या पत्रिकाओं के बहाने व्यस्त रखा जा सकता था। नौकरी के बाद जितना समय बचता था पंडितों और बिचौलियों के चक्कर काटने में गुजर जाता था। विद्यावती पीहर से ही ढेर-सा कलेजा लेकर आई थीं। फिर बचपन में अपनी जिज्जी का रिश्ता ठहरने के समय से ही दूल्हे के घर से आए मेहमानों में से जिस लड़के का झिझका, झेंपा शर्मीला सा चेहरा उनकी आँखों से मन तक उतरकर वहाँ बस गया था वह मुकुट ही तो थे। यह बात बस दुनिया में जिज्जी ही भाँप पाई थी। यहाँ तक कि मुकुट को भी उसने यह शादी के छह-सात महीने बाद बताया था। ये तो जिज्जी का प्रताप ही था कि कृष्ण बिहारीजी के न रहने पर जीजाजी अपनी बहन पर भारी पड़े और अपनी एकमात्र साली के भाँवरे मुकुट बिहारी से डलवा दिए।
मन्त्रालय के बड़े बाबू द्विवेदीजी अपने प्रतिभावन युवा अफसर का खास खयाल रखते थे। उनके माथे की सलवटें द्विवेदीजी को चिन्ता की लहरों में डुबाती उतराती रहती थीं। फिर साहब के घर जवान बहन बैठी हो और साहब उसके रिश्ते के लिए परेशान हों तो बड़े बाबू भला पीछे रह सकते थे ! वैसे भी जात-बिरादरी का ही मामला ठहरा। उन्होंने झट अपने रिश्ते के भाई पंडित राम प्रसाद कौशिक के छोटे बेटे बद्री प्रसाद का रिश्ता सुझाया। मुकुट बिहारी कुछ जवाब दें इससे पहले ही साहिबाबाद से अपने बेटे का
टेवा लेकर आए पंडित राम प्रसादजी ने स्वयं दर्शन दिए। ग्रह-नक्षत्रों की दुनिया में मुकुट बिहारीजी की न गति थी और न मन। सो यह कारज भी पंडितजी के सुपुर्द हुआ। स्नेहलता की जन्मपत्री उन्हें सौंपी गई। यह जानकर सभी के हर्ष का ठिकाना न रहा कि बद्री प्रसाद और स्नेहलता के टेवों में 34 गुण मिलते थे। अति उत्तम ! श्राद्धों के बाद जैसे ही डूबे तारों ने करवट ली और विवाह का पहला शुभ साया मिला, उसी में सबकी सलाह से बब्बा ने अपनी स्नेह को कौशिक परिवार के सुपुर्द किया। बब्बा के साथ-साथ विद्यावती भी कुछ-कुछ अकेली सी हो गई।
मुकुट बिहारी की दबदबेवाली नौकरी ने उन्हें अफसरोंवाला जो फ्लैट दिलवाया था वह भी सारा-सारा दिन अकेली विद्यावती के साथ भाँय-भाँय करता था। भरे पूरे परिवार के आदी मुकुट बिहारी के लिए अपनी जिन्दगी जीना सीखना अभी बाकी था।
लम्बे कद और इकहरे बदनवाले पंडित राम प्रसाद कौशिक साहिबाबाद के बिजली बोर्ड में एकाउंटेंट थे। वे आँखों से ज्यादा ताड़ते थे और जुबान से शब्द कम जाया करते थे। अपनी ज्योतिष विद्या की वजह से राम प्रसादजी ‘पंडितजी’ के नाम से ही जाने जाते थे। उनकी गम्भीर निगाहों और माथे की गहरी रेखाओं से हर पल उनका तजुर्बा झाँकता रहता था। दफ्तर के एकाउंट रजिस्टर उनकी ओढ़ना-बिछौना थे। दो और दो चार पर उनकी सुबह होती थी तो निन्यानवे के फेर पर शाम। वैसे साइकिल के कैरियर पर बँधे बही खातों के पुलिन्दों की तहों में कितने पंचांग और कितनी जन्मपत्रियाँ होंगी कहना मुश्किल रहता था। बही खातों से निगाह उठती तो सामने कोई जन्मपत्री होती या किसी की फैली हथेली। घर का नीरस बोझ उठाने को पत्नी सावित्री देवी मौजूद थीं। ही। विशेषता यह कि पंडितजी की खामोश तबीयत ने परिवार पर पूरा नियन्त्रण जमा रखा था। बेटे महेश प्रसाद व बद्री प्रसाद बचपन से ही पिता की आँख के इशारे समझते थे और निबाहते भी थे।
महेश प्रसाद एक चार्टर्ड एकाउंटेंसी की प्राइवेट कम्पनी में काम करते थे। स्वभाव से बहुत मेहनती थे। जिस काम को उनके साथी एक घंटे में निपटाते उसी काम को ढाई-तीन घंटों में करते थे। काम को निपटाना उनके बस के बाहर था। उन्हें तो काम करना ही होता था। इसलिए देर रात तक दफ्तर में उलझे रहते थे। फिर घर आकर भी पीछे छूट गया कोई काम या उसकी चिन्ता सिर से कन्धे पर तो कन्धे से गोद में कूदती-फाँदती मिलती थी। महेश प्रसाद का सम्बन्ध मुज़फ़्फ़रनगर की रतनबाला से तय होना था कि माँ सावित्री देवी को बुखार ने जकड़ लिया। बुखार फिर उनकी देह के साथ ही हो गया। घर में स्त्री न होने से आब नहीं रही। ऐसे में साल-भर के मातम तक कौन रुकता ! दो महीने बाद ही रतनबाला के फेरे हुए और उसने आकर सारी गृहस्थी सँभाली।
छोटे, बद्री प्रसाद इस परिवार में पूरी तरह से फिट नहीं बैठते थे। डील डौल में पिता जैसे ही थे और कह सुनकर अपने ऊँचे जजमानों की मदद से पंडितजी ने उन्हें पी.डब्ल्यू.डी. में ओवरसियर लगवा दिया था। उनका मन वहाँ रमता न था। होठों पर हमेशा रचा पान अगर उनकी खुशमिजाजी का सबूत था तो कलफदार कपड़े और खुशबू का फाहा जीवन में उनकी आसक्ति का संकेत। पर थे वे भी पिता की तरह ही एक बन्द किताब। मन की बात जानने के लिए सिर्फ पृष्ठ पलटकर सरसरी तौर पर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।
बद्री प्रसाद को दफ्तर की ओर से पहली बार इमारत के निर्माण के सिलसिले में जिस साइट पर भेजा गया, वहाँ चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए एक मकान की छाया का सहारा लेना जरूरी हो गया था। कौन जानता था कि वह मकान उनकी जिन्दगी को ही अपनी छाया में समेट लेगा। बाहर ही खटिया डाले बैठनेवाली अम्मा उन्हें अक्सर पानी को पूछ लेती थी। और पानी का लोटा लेकर आती थी उनकी बेटी प्रभा। कुछ ही दिनों में बद्री को प्रभा के हाथ की चाय भी मिलने लगी थी। कभी-कभार वे अन्दर कमरे में जाकर भी बैठ लेते थे। प्रभा ब्याहता थी पर पति की असामयिक मौत की वजह से मायके में ही रहती थी। ससुरालवालों ने भी उसके मायके जाते ही बोझ से मुक्ति की साँस ली। कौन जिन्दगी भर बैठा कर खिलाता ! प्रभा की सादगी ने बद्री का मन बस में कर लिया था। पहले जिस हमदर्दी की लाठी टेकते वे प्रभा तक पहुँचे थे अब वह किसी ने छिपा दी थी। उसकी जगह एक ऐसा कलम-दल खिल आया था जो शीतल छाया चाहता है बद्री ने जीवन में पहली बार अपने पिता की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करना चाहा था। जल्द ही प्रभा से विवाह का फैसला घर-भर में गुँजा दिया गया था।
इधर पंडितजी के सम्मुख जैसे ही कृषि मन्त्रालय में सेवारत उनके रिश्ते के भाई और जजमान द्विवेदीजी ने अपने अफसर मुकुट बिहारी की परेशानी का विलम्बित छेड़ा और उनकी बहन स्नेहलता के लिए कोई योग्य वर सुझाने का अनुरोध किया तो पंडितजी की आँखें कोई भावी नक्शा खींचकर चमक उठीं। घर में जिस बगावत का सिर अधिक ऊँचा उठने की आशंका थी उसे समय रहते कलम कर देना ही बुद्धिमानी थी। फिर बिन माँ-बाप के बेटी के रिश्ते में कौन बारीक छानता ! सो पंडितजी ने द्विवेदीजी को उपकृत करते हुए अपने बेटे बद्री प्रसाद का रिश्ता ही आगे सरका दिया। मुकुट बिहारी अभी अनुभवों की आँच में इतना कहाँ पके थे कि पंडितजी का मन सूँघ पाते। जन्मपत्रियाँ भी पंडितजी ने ही मिला ली थीं। सो स्नेहलता ने अपना पहला कदम उस परिवार की चौखट पर रखा तो जेठानी रतनबाला ने देहरी को तेल से भिगोते हुए दूल्हा-दुल्हन की आरती उतारी। बद्री प्रसाद पूरे समय मुहर्रम की पैदाइशवाला चेहरा बनाए रहे। विद्रोह का बिगुल बजा देना एक बात होती है और अन्त तक उस पर डटे रहकर उसे निबाह पाना दूसरी।
पहले खुद पढ़ते हुए और फिर लड़कियों को पढ़ाते-पढ़ाते जिन्दगी भी कानन के लिए एक ‘सब्जेक्ट’-सी बन गई थी। फिलासफी...दर्शन..फलसफा। हर सफा एक अलग फलसफा।
पहली खुशबू जो याद आती है वह माँ की है। धुले हल्की छींटवाले कपड़ों में साँस लेती धीमी गतिवाली धड़कनों की। बिना किसी आस के लपक-झपक करती उस चमक की जो आँखों में खिलती है जाड़ों की उस हल्की धूप की तरह जिसे हर सुबह मुँडेरो पर सुबह को सुबह बनाने के लिए अक्सर आना ही होता है। या एक ठंडी खुशबू..गर्मियों में खस जैसी।
इससे तेज़ एक और खुशबू थी आस-पास। बब्बा की। एक ऐसी खुशबू जो खींचती थी सर्दियों में रजाई न होने पर सुबह गली में चक्कर लगाते धुनिया के टुनटुने की झंकार की तरह। और बब्बा का साथ ? बाजारों में बड़ी दुकानों के बाहर एक कोने में बैठा पुराने या बिना चाबी के तालों की चाबियाँ बनानेवाला। जिन्दगी के हर सवाल की अपनी तरह की एक अलग ‘मास्टर की’ रखनेवाला साथ। ‘‘बब्बा-बब्बा’’ में ऐसी पिरोई रहती थी कानन कि पहली बार छठी कक्षा के लिए बड़े स्कूल में दाखिले का फॉर्म भरते हुए उसे महसूस हुआ था कि वे उसके पिता नहीं उसकी माँ के भाई हैं क्योंकि फॉर्म में जो नाम भरा गया वह बब्बा का नहीं था। तभी समझ गई थी कानन कि कोई चाहे या न चाहे एक नाम जीवन भर उसके साथ रहेगा। चाहे सिर्फ प्रमाण-पत्रों या फॉर्मों में ही। उसके पिता का नाम-बद्री प्रसाद कौशिक।
चेतना के धराऊ बक्सों में रखी स्मृतियों पर समय की सिल्वर फिश अपने निशान जरूर छोड़ती है पर स्मृतियाँ...वो तो बनी ही रहती हैं वहाँ, उन कुछ निशानों की तब्दीलियों के साथ। बचपन में...बहुत छुटपन में...वह अक्सर चुपके से आकर बब्बा की टाँगों के साथ खड़ी हो जाती थी और धीरे से उनकी तर्जनी पकड़ लेती थी। और खड़ी रहती थी यों ही उनके साथ उन्हें देखती हुई कि कैसे वे सुबह बागीचे के हर पौधे, हर फूल, कली और हर पत्ते को निहारते थे। उनकी बस एक उँगली..सिर्फ एक तर्जनी ही चाहिए होती थी कानन को सहारे के लिए। अगर कभी कुछ और उँगलियाँ पकड़ में आ जातीं तो उन्हें कुछ घुमाकर पीछे कर देती थी वह। पूरे हाथ का सहारा जो नहीं चाहिए होता था। बब्बा खीझ जाते थे इस तरह बाकी उँगलियाँ घुमाने पर, ‘‘ये क्या किया करे है तू कुक्कू ?’’ और वह मुस्कुराकर अपने हाथ में थामी उस तर्जनी को देखने लगती थी। छोटे कद के बब्बा का छोटा और हड्डियों के एहसासवाला दायाँ हाथ। अनामिका में ठहर-सी गई पुखराज जड़ी एक सोने की अँगूठी जो अक्सर उसका ध्यान खींचती थी। जो ‘एक ज़माने से’ वहीं थी। शायद बचपन में पहनी अँगूठी हाथ के साथ साथ अपना आकार बड़ा करती चलती हो !
कानन बस ढाई वर्ष की थी जब 262 बी.एम. अहाता, साहिबाबाद में यही हाथ उसकी ओर बढ़ा था और पहली बार उसकी निगाह उस अँगूठी की ओर गई थी। उस हाथ की तर्जनी पकड़कर लगभग खिंचते हुए कानन ने माँ और बहन के साथ दिल्ली की एक सरकारी कॉलोनी के एक प्लैट में प्रवेश किया था। फिर ता-जिन्दगी उसने जब-जब निगाह उठाई तो यही हाथ सामने पाया। मगर उसकी अपनी बारी आने पर वह सिर्फ उस हाथ की तर्जनी ही पकड़ती रही थी। बस।
बी.एम. अहाता उसकी जिन्दगी से मिट गया था। अब कभी-कभार वह बब्बा के प्यार भरे गुस्से या खीझ से भरे एकालाप में सिर उठाता भी था तो अपने असली भौंदू मल के अहाते के रूप में ही। अपनी कुक्कू को छेड़ते हुए वे कभी कभी कहते थे, ‘‘आहता तो वहीं छूट गया और हमारा भौंदूमल यहाँ आ गया।’’
माँ को देखा था पापा के नाम-भर का कत्थई देवत्व थामे जिन्दगी की चढ़ाई चढ़ते। हल्के कदमों से, फुर्सत के साथ। किसी बदलाव के इन्तजार के बिना। एक ऐसी सपाट जिन्दगी जीते जो जानती है कि ‘घटना’ शब्द उसके लिए नहीं बना है। जिसे गुजरते-गुजरते ही गुजरना है।
एक बेटा और दो बेटियाँ उनकी जमा पूँजी थी विवाहित जीवन के कुल सात सालों की जिसका अन्ततः बँटवारा हुआ था। उनके हिस्से में आई कानन और बड़ी बेटी केसर।
माँ की तबीयत में एक वैसा ही ठहराव था जैसा उनकी आँखों में उतर आया था बाद के दिनों में। एक सहनशील, परम्परागत, सिरझुकाऊपन में गुँथी हींग और देसी घी से महकते हाथोंवाली खुशबू जो पापा को नहीं चाहिए थी। न दिन के उजाले में, न रात के बियाबान में। और वे तीनों प्राणी आ गए थे बब्बा के पास हमेशा के लिए।
बब्बा यानी श्री मुकुट बिहारी त्रिवेदी, सुपुत्र मास्टर कृष्ण बिहारी त्रिवेदी को नामकरण का जो मुकुट धारण कराया गया था, कोई नहीं जानता था कि इस तीन वर्ष के बालक को आजीवन इसकी जिम्मेदारियों को ढोना होगा। लक्कड़ का बोझा उठाए पहाड़ी मजदूर की भाँति ऊँचाइयों पर चढ़ते-उतरते। पहलौठी की सन्तान और चार बहनों के एकमात्र भाई बिहारी ने जाने क्यों और कैसे चारों छोटी बहनों के लिए भैया से ‘बब्बा’ हो गए थे। बहुत पीछे चलें तो इसका कारण शायद उनकी तीसरी बहन स्नेहलता हो। बचपन में एक तो स्नेह को मुकुट बिहारी के लिए ‘भाई साहब’ और ‘भैया’ जैसे सम्बोधन कभी रास नहीं आए। ये तो सभी कहते हैं अपने भाई को ! फिर वह भी क्यों कहे ? मुकुट बिहारी कोई औरों जैसे तो हैं नहीं। जानता है किसी का भाई इतनी अंग्रेजी, इतनी हिन्दी और साथ ही इतना उर्दू-फारसी ! अपनी छोटी बहन को अपनी सारी पढ़ाई पढ़ा देने का मन होता है किसी का ? बहन का सहेलियों के साथ पिकनिक जाने का मन हो तो बाऊजी को तरह-तरह से मनाता है कोई भाई। बहन की किताब से अचानक पानी की धार की तरह कोई सूखी पंखुड़ी बह निकले तो काँपती हुई उँगलियों से चुपचाप उन्हीं वर्कों में दोबारा रखता है कोई भाई ! तो उन्हें भाई साहब या भैया क्यों कहा जाए फिर !
मुकुट बिहारी भी कौन उन्नीस थे। जब-तब बहनों पर ऊपरी रौब जमाकर याद दिलाते रहते थे कि वे सबसे बड़े हैं। इसलिए ‘बब्बा’ सम्बोधन उन पर किशोर वय से फबा भी खूब।
मुकुट बिहारी के पिता मास्टर कृष्ण बिहारी त्रिवेदी अपने हाथों से अपनी दो बड़ी बेटियों का विवाह कर गए थे। पहली आशालता गंगानगर में ब्याही थी। पहले ही प्रसव में जीवन से थक कर नवजात के साथ ही चल दी। चन्द ही महीनों में आशालता के ससुरालवालों ने पीछे छूट गए उसके पति के लिए दूसरी बहन सुमनलता का हाथ माँग लिया। थोड़ा बहुत सोच-विचार कर कृष्ण बिहारीजी इस नतीजे पर पहुँचने ही वाले थे कि ‘इसमें हर्ज भी क्या है’ कि तीसरी बहन स्नेहलता ने हौले से उनसे एक सवाल कर लिया।
वे रसोई में बैठ भोजन करते हुए अपनी पत्नी के सामने तीन लड़कियों को ब्याहने की जिम्मेदारी निबाहने का राग छेड़ बैठे थे। यह शायद उनके लिए अपना फैसला सुनाने की भूमिका रही होगी। तभी उनकी थाली में रोटी परोसती हुई स्नेह ने काँपती आवाज में पूछा, ‘‘बाऊजी अगर सुमन जीजी को भी कुछ हो गया तो अगले साल मुझे भी ब्याह दोगे गंगानगर ?’’ बाऊजी ने दूसरी रोटी का एक कौर तोड़ा था और बड़े चाव से हाथ आलू की झोलवाली सब्जी की ओर बढ़ाया ही था कि रसोई में धुएँ की तरह एक चीख भर आई। अँगीठी पर फुलका सेंकती उनकी पत्नी ने गलती से फुलके के स्थान पर जलता हुआ कोयला पकड़ लिया था। कृष्ण बिहारीजी को भी थाल छोड़कर उठना पड़ा। स्नेह चिल्लाती हुई बाहर भागी। शायद सुमन और मुकुट को बुलाने। इधर मास्टरजी आलू के झोल से सने अपने दाएँ हाथ के नीचे बाएँ हाथ की हथेली लगाए अजब मुद्रा में खड़े थे। क्या करें, क्या न करें ! अब तक उनकी पत्नी समझ चुकी थी कि अपने जले का उपचार स्वयं ही करना होता है। सो पास रखी आटे की परत से उसने आधी लोई जितना सना हुआ आटा लिया और अपनी तर्जनी और अँगूठे पर लपेट लिया। बात आई गई हो गई मगर बाऊजी अपना फैसला सुनाने की अब हिम्मत न जुटा पाए। गंगानगरवालों का ‘न’ कह दी गई।
गंगानगरवालों को कही गई यह ‘न’ त्रिवेदी परिवार को बहुत भारी पड़ी। उतने प्रयास गंगानगरवालों ने अपने बेटे के दूसरे विवाह के लिए भी नहीं किए होंगे जितने कि हर जगह से सुमनलता का ब्याह रुकवाने के हुए। दामाद का विवाह साल-भर बाद हो गया। बारात में कृष्ण बिहारीजी भी गेंदे के फूलों की माला धारण कर समधी की जिम्मेदारियों में हाथ बँटाते देखे गए। स्वर्गीया आशालता की माँ भी समय-समय पर हर नेग-टेहले में जाकर खड़ी हुईं। मगर गंगानगरवालों के दिलों में चुभी फाँस भला इतने से ही निकल जाती ! पूरे तीन सालों में उन्होंने सुमनलता के सात रिश्ते तुड़वाए।
अब तक मास्टरजी समझ चुके थे कि गंगानगरवालों को ‘न’ कहना जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल रही है। दुनिया उन्हें अँधियारी दिखाई देने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि सुमन तो सुमन भविष्य में स्नेहलता और गीता दोनों अनब्याही रह जाएँगी। वे भीतर तक सहम गए थे। अबकी बार उन्होंने घर में किसी से ज्यादा सलाह-मशविरा करना भी ठीक नहीं समझा। वे समझ गए थे कि बिनब्याहे लड़के की फिराक में ज्यादा दिन नहीं रहा जा सकता। इटावा से जैसे ही शिव मोहन बाबू का रिश्ता आया उन्होंने सगाई ठहरा दी। यहाँ तक कि बाद में पूछा गया कि पहली पत्नी से उन्हें कितने बच्चे हैं सगाई के बाद उनके तीनों बच्चे जब सुमनलता से मिलने दिल्ली आए तभी लोगों को उनके बारे में ठीक-ठीक जानकारी मिल पाई।
सुमनलता के भी दो बच्चे हुए। सो इटावा में घर गृहस्थी के चक्कर में वह ऐसी लगी कि मायके की याद भी कभी-कभार सुख-दुख के समय ही आती थी। पर जब आती थी तो बरसात में अचानक उभर आए मोच के दर्द की तरह कसकती थी। ऐसी कसक में बस जी वहाँ से हटा लिया जाता है, उपचार क्या करना !
पीछे रह गई स्नेहलता और गीता। गीता न तो शक्ल से तीनों लताओं की बहन लगती थी, न नाम से। गीता के होने पर तीनों लताएँ एक हो गईं और बाऊँजी को इस बात के लिए राजी कर ही लिया कि गोल-मटोल रूहअफ़्ज़ा वाले दूध जैसी छुटकी कोई लता नहीं बनेगी। बाऊजी को राजी तो होना पड़ा मगर उनकी भी एक शर्त थी। नाम वही रखा जाएगा जो सद्गुण सम्पन्न और फिल्मों से कतई दूर होगा। सो बहुत खोजबीन के बाद ‘गीता’ नाम पर पूरा परिवार एकमत हो पाया था।
वह बुद्ध पूर्णिमा की भोर थी जब कृष्ण बिहारीजी स्नान कर, आँगन में सू्र्य देवता को अर्घ्य दे, तुलसीजी की देहरी पर मस्तक नवा कर ही चुके थे कि दालान में चलते हुए एक झटके के साथ ठहर गए। उनके सीने में टीस-सा दर्द उभरा जो बादलों की तरह अन्दर घुमड़ता रहा। बस उन्हीं बादलों में उन्होंने जीवन की अन्तिम साँस ली। पास ही रखी आरामकुर्सी पर उन्होंने खुद को छोड़ दिया।
मुकुट बिहारी को अपने सम्बोधन ‘बब्बा’ का अर्थ अब समझ आने लगा था। सारा घर हर अच्छी-बुरी घड़ी में उन्हीं की ओर तकता था। माँ की इच्छानुसार साल-भर बाद उनका विवाह अपनी मामी की छोटी बहन विद्यावती से सम्पन्न हुआ। माँ मानो उसी का इन्तजार कर रही थी। विद्यावती को घर-गृहस्थी क्या सौंपी, दुनिया सौंप चली। विद्यावती भी जीवन-पर्यन्त भाभी कहलाने के बावजूद सही मायने में ‘बब्बा’ की अर्द्धांगिनी बनी रहीं।
गीता तब बी.ए. में थी कि एक दिन सुबह स्नेह ने उसे देखा तो अपनी हिचकियाँ न रोक पाई। उसके होंठों से एक नीली धार बहकर गले से होती हुई तकिए के गिलाफ को भिगो रही थी। कारण कोई न जान पाया। बिन माँ-बाप की बेटी के दुखी होकर आत्महत्या करने की तोहमत भाई-भाभी पर ही लगी। वे सहम गए थे। अभी उन्हें स्नेहलता का घर बसाना था।
मुकुट बिहारी ने अंग्रेजी में एम.ए. किया था मगर जान उनकी उर्दू और कुछ-कुछ फारसी में बसती थी। ‘दीवान-ए-ग़ालिब’ रात को टार्च की जगह सिरहाने रखा मिलता था। एम.ए. के बाद चाहा तो बहुत कि कालेज लेक्चरर हो जाएँ, मगर उससे पहले ही वे कृ्षि मन्त्रालय की एक लिखित परीक्षा पास कर उसमें उत्तीर्ण होने की गलती कर बैठे। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही तरक्की भी मिल गई। वहाँ अंडर सेक्रेटरी हो गए। समय और नौकरी के दबदबे ने पढ़ाने की वो चाह धुँधला दी। इस बीच शादी हो चुकी थी, माँ-बाप दोनों जाते रहे, गीता भी नहीं रही और स्नेहलता को भी कब तक नए-नए उपन्यासों या पत्रिकाओं के बहाने व्यस्त रखा जा सकता था। नौकरी के बाद जितना समय बचता था पंडितों और बिचौलियों के चक्कर काटने में गुजर जाता था। विद्यावती पीहर से ही ढेर-सा कलेजा लेकर आई थीं। फिर बचपन में अपनी जिज्जी का रिश्ता ठहरने के समय से ही दूल्हे के घर से आए मेहमानों में से जिस लड़के का झिझका, झेंपा शर्मीला सा चेहरा उनकी आँखों से मन तक उतरकर वहाँ बस गया था वह मुकुट ही तो थे। यह बात बस दुनिया में जिज्जी ही भाँप पाई थी। यहाँ तक कि मुकुट को भी उसने यह शादी के छह-सात महीने बाद बताया था। ये तो जिज्जी का प्रताप ही था कि कृष्ण बिहारीजी के न रहने पर जीजाजी अपनी बहन पर भारी पड़े और अपनी एकमात्र साली के भाँवरे मुकुट बिहारी से डलवा दिए।
मन्त्रालय के बड़े बाबू द्विवेदीजी अपने प्रतिभावन युवा अफसर का खास खयाल रखते थे। उनके माथे की सलवटें द्विवेदीजी को चिन्ता की लहरों में डुबाती उतराती रहती थीं। फिर साहब के घर जवान बहन बैठी हो और साहब उसके रिश्ते के लिए परेशान हों तो बड़े बाबू भला पीछे रह सकते थे ! वैसे भी जात-बिरादरी का ही मामला ठहरा। उन्होंने झट अपने रिश्ते के भाई पंडित राम प्रसाद कौशिक के छोटे बेटे बद्री प्रसाद का रिश्ता सुझाया। मुकुट बिहारी कुछ जवाब दें इससे पहले ही साहिबाबाद से अपने बेटे का
टेवा लेकर आए पंडित राम प्रसादजी ने स्वयं दर्शन दिए। ग्रह-नक्षत्रों की दुनिया में मुकुट बिहारीजी की न गति थी और न मन। सो यह कारज भी पंडितजी के सुपुर्द हुआ। स्नेहलता की जन्मपत्री उन्हें सौंपी गई। यह जानकर सभी के हर्ष का ठिकाना न रहा कि बद्री प्रसाद और स्नेहलता के टेवों में 34 गुण मिलते थे। अति उत्तम ! श्राद्धों के बाद जैसे ही डूबे तारों ने करवट ली और विवाह का पहला शुभ साया मिला, उसी में सबकी सलाह से बब्बा ने अपनी स्नेह को कौशिक परिवार के सुपुर्द किया। बब्बा के साथ-साथ विद्यावती भी कुछ-कुछ अकेली सी हो गई।
मुकुट बिहारी की दबदबेवाली नौकरी ने उन्हें अफसरोंवाला जो फ्लैट दिलवाया था वह भी सारा-सारा दिन अकेली विद्यावती के साथ भाँय-भाँय करता था। भरे पूरे परिवार के आदी मुकुट बिहारी के लिए अपनी जिन्दगी जीना सीखना अभी बाकी था।
लम्बे कद और इकहरे बदनवाले पंडित राम प्रसाद कौशिक साहिबाबाद के बिजली बोर्ड में एकाउंटेंट थे। वे आँखों से ज्यादा ताड़ते थे और जुबान से शब्द कम जाया करते थे। अपनी ज्योतिष विद्या की वजह से राम प्रसादजी ‘पंडितजी’ के नाम से ही जाने जाते थे। उनकी गम्भीर निगाहों और माथे की गहरी रेखाओं से हर पल उनका तजुर्बा झाँकता रहता था। दफ्तर के एकाउंट रजिस्टर उनकी ओढ़ना-बिछौना थे। दो और दो चार पर उनकी सुबह होती थी तो निन्यानवे के फेर पर शाम। वैसे साइकिल के कैरियर पर बँधे बही खातों के पुलिन्दों की तहों में कितने पंचांग और कितनी जन्मपत्रियाँ होंगी कहना मुश्किल रहता था। बही खातों से निगाह उठती तो सामने कोई जन्मपत्री होती या किसी की फैली हथेली। घर का नीरस बोझ उठाने को पत्नी सावित्री देवी मौजूद थीं। ही। विशेषता यह कि पंडितजी की खामोश तबीयत ने परिवार पर पूरा नियन्त्रण जमा रखा था। बेटे महेश प्रसाद व बद्री प्रसाद बचपन से ही पिता की आँख के इशारे समझते थे और निबाहते भी थे।
महेश प्रसाद एक चार्टर्ड एकाउंटेंसी की प्राइवेट कम्पनी में काम करते थे। स्वभाव से बहुत मेहनती थे। जिस काम को उनके साथी एक घंटे में निपटाते उसी काम को ढाई-तीन घंटों में करते थे। काम को निपटाना उनके बस के बाहर था। उन्हें तो काम करना ही होता था। इसलिए देर रात तक दफ्तर में उलझे रहते थे। फिर घर आकर भी पीछे छूट गया कोई काम या उसकी चिन्ता सिर से कन्धे पर तो कन्धे से गोद में कूदती-फाँदती मिलती थी। महेश प्रसाद का सम्बन्ध मुज़फ़्फ़रनगर की रतनबाला से तय होना था कि माँ सावित्री देवी को बुखार ने जकड़ लिया। बुखार फिर उनकी देह के साथ ही हो गया। घर में स्त्री न होने से आब नहीं रही। ऐसे में साल-भर के मातम तक कौन रुकता ! दो महीने बाद ही रतनबाला के फेरे हुए और उसने आकर सारी गृहस्थी सँभाली।
छोटे, बद्री प्रसाद इस परिवार में पूरी तरह से फिट नहीं बैठते थे। डील डौल में पिता जैसे ही थे और कह सुनकर अपने ऊँचे जजमानों की मदद से पंडितजी ने उन्हें पी.डब्ल्यू.डी. में ओवरसियर लगवा दिया था। उनका मन वहाँ रमता न था। होठों पर हमेशा रचा पान अगर उनकी खुशमिजाजी का सबूत था तो कलफदार कपड़े और खुशबू का फाहा जीवन में उनकी आसक्ति का संकेत। पर थे वे भी पिता की तरह ही एक बन्द किताब। मन की बात जानने के लिए सिर्फ पृष्ठ पलटकर सरसरी तौर पर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।
बद्री प्रसाद को दफ्तर की ओर से पहली बार इमारत के निर्माण के सिलसिले में जिस साइट पर भेजा गया, वहाँ चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए एक मकान की छाया का सहारा लेना जरूरी हो गया था। कौन जानता था कि वह मकान उनकी जिन्दगी को ही अपनी छाया में समेट लेगा। बाहर ही खटिया डाले बैठनेवाली अम्मा उन्हें अक्सर पानी को पूछ लेती थी। और पानी का लोटा लेकर आती थी उनकी बेटी प्रभा। कुछ ही दिनों में बद्री को प्रभा के हाथ की चाय भी मिलने लगी थी। कभी-कभार वे अन्दर कमरे में जाकर भी बैठ लेते थे। प्रभा ब्याहता थी पर पति की असामयिक मौत की वजह से मायके में ही रहती थी। ससुरालवालों ने भी उसके मायके जाते ही बोझ से मुक्ति की साँस ली। कौन जिन्दगी भर बैठा कर खिलाता ! प्रभा की सादगी ने बद्री का मन बस में कर लिया था। पहले जिस हमदर्दी की लाठी टेकते वे प्रभा तक पहुँचे थे अब वह किसी ने छिपा दी थी। उसकी जगह एक ऐसा कलम-दल खिल आया था जो शीतल छाया चाहता है बद्री ने जीवन में पहली बार अपने पिता की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करना चाहा था। जल्द ही प्रभा से विवाह का फैसला घर-भर में गुँजा दिया गया था।
इधर पंडितजी के सम्मुख जैसे ही कृषि मन्त्रालय में सेवारत उनके रिश्ते के भाई और जजमान द्विवेदीजी ने अपने अफसर मुकुट बिहारी की परेशानी का विलम्बित छेड़ा और उनकी बहन स्नेहलता के लिए कोई योग्य वर सुझाने का अनुरोध किया तो पंडितजी की आँखें कोई भावी नक्शा खींचकर चमक उठीं। घर में जिस बगावत का सिर अधिक ऊँचा उठने की आशंका थी उसे समय रहते कलम कर देना ही बुद्धिमानी थी। फिर बिन माँ-बाप के बेटी के रिश्ते में कौन बारीक छानता ! सो पंडितजी ने द्विवेदीजी को उपकृत करते हुए अपने बेटे बद्री प्रसाद का रिश्ता ही आगे सरका दिया। मुकुट बिहारी अभी अनुभवों की आँच में इतना कहाँ पके थे कि पंडितजी का मन सूँघ पाते। जन्मपत्रियाँ भी पंडितजी ने ही मिला ली थीं। सो स्नेहलता ने अपना पहला कदम उस परिवार की चौखट पर रखा तो जेठानी रतनबाला ने देहरी को तेल से भिगोते हुए दूल्हा-दुल्हन की आरती उतारी। बद्री प्रसाद पूरे समय मुहर्रम की पैदाइशवाला चेहरा बनाए रहे। विद्रोह का बिगुल बजा देना एक बात होती है और अन्त तक उस पर डटे रहकर उसे निबाह पाना दूसरी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i