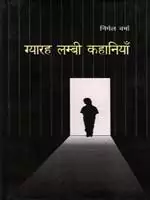|
लेख-निबंध >> आदि, अन्त और आरम्भ आदि, अन्त और आरम्भनिर्मल वर्मा
|
436 पाठक हैं |
|||||||
आत्म-उन्मूलन के अन्धकार पर आधारित निबन्ध...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्राक्कथन
अक्सर कहा जाता है कि बीसवीं शती में जितनी बड़ी संख्या में लोगों को अपना
देश, अपना घर-बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने जाना पड़ा, शायद किसी
और शती में नहीं। राजनीति दमन, तानाशाही, आतंक, आर्थिक विपन्नता-कारण कुछ
भी रहा हो-पिछले सौ वर्षों के दौरान अधिकांश लोगों को पराये आकाश के नीचे
एक दूसरी जिन्दगी को चुनने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह एक ऐसी ऐतिहासिक
दुर्घटना थी, जिसने लाखों की ज़िन्दगी को तहस-नहस कर दिया।
किन्तु इससे बड़ी त्रासदी शायद यह है कि जब मनुष्य अपना घर छोड़े बिना निर्वासित हो जाता है, अपने ही घर में एक शरणार्थी की तरह रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। फ्रांस की सबसे मौलिक अन्तर्दृष्टिसंपन्न चिन्तक सिमोन वेल कहा करती थीं कि आधुनिक जीवन की सबसे भयानक, असहनीय और अक्षम्य देन ‘आत्मा-उन्मूलन’ का बोध है। यह एक ऐसा वेस्टलैंड, आन्तरिक मरुस्थल है, जहाँ मनुष्य के समस्त संरक्षण स्थल-ईश्वर, परंपरा अतीत, प्रकृति-जो एक समय उसके आत्म को गठित और रूपायित करते थे, उससे छूटते जाते हैं। वह स्वयं अपने आत्म से निर्वासित हो जाता है, जो आत्म-उन्मूलन की चरमावस्था है।
अजीब बात है कि यह चरमावस्था, जो अपने में काफी ‘एबनॉर्मल’ है आज हम भारतवासियों की सामान्य अवस्था बन गयी है। आत्म-उन्मूलन का त्रास अब ‘त्रास’ भी नहीं रहा, वह हमारे दैनिक जीवन का अभ्यास बन चुका है। अक्सर वही चीज़ जो सर्वव्यापी है, हमें आँखों से दिखायी नहीं देती। ऊपर की बीमारियाँ दिखायी देती हैं, किन्तु जो कीड़ा हमारे अस्तित्व की जड़ से चिपका है, जिससे समस्त व्याधियों का जन्म होता है-आत्मशून्यता का अन्धकार उसे शब्द देने के लिए जिस आत्मबोध की जरूरत है, हम आज उससे भी वंचित हो गए हैं। इस पुस्तक के अधिकांश निबन्ध-उसके विषय कुछ भी क्यों न हों-विभिन्न कोणों से इस ‘अन्धकार’ को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं। यह वह केन्द्रीय़ ‘थीम’ है जो इन निबन्धों को एक सूत्र में बाँधे है। धर्मनिरपेक्षता, भूमंडलीकरण, ‘आधुनिकता’ बुद्धिजीवी की आध्यात्मिक कुंठाएँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी इस अवरुद्ध मानसिकता की देन हैं जो हर कदम पर हमें अपनी अस्मिता के प्रति सशंकित करते हैं, अपने होने में ‘न होने’ का अहसास कराते हैं। ‘उत्तर-औपनिवेशिकता’ के दौर में वे हमें अपने अन्तर्निहित औपनिवेशिक अवशेषों से अवगत कराते हैं।
पुस्तक के दूसरे खंड में मैंने भारती की कहानियों और बेगड़जी की नर्मदा यात्रा पर अपनी आत्मीय प्रतिक्रियाएँ प्रगट की हैं। यद्यपि इन्हें दोनों लेखकों की पुस्तकों की प्रस्तावनाओं के रूप में लिखा गया था, किन्तु उनके बहाने मैं उन लेखकों के प्रति अपना कृतज्ञता-ज्ञापन कर सका हूँ, जिनके लेखन ने इतने अलग ढंग से मुझे अपने देश और समय के प्रति सम्वेदनशील बनाने में योगदान है।
पुस्तक का अन्तिम खंड बीते हुए इतिहास की दो मर्मान्तक घटनाओं को-1968 में चेकोस्लोवाकिया पर सोवियत सेनाओं का आक्रमण और 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा-दो अलग काल-बिन्दुओं से देखने का प्रयास है; एक जो उनका जीवन्त, स्पन्दित वर्तमान था, दूसरे अब, जब वे सिर्फ अतीत की स्मृति मात्र बनकर रह गये हैं। इतिहास का अपराध-बोध कितना हास्यास्पद हो सकता है, यह इससे विदित होता है, कि वे लोग जो एक समय में ‘इतिहास की दुहाई’ देते फिरते थे, वे आज उससे मुँह चुराने लगे हैं, मानो वह कोई प्रेत हो जिससे वह जल्द से जल्द अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते हों मार्क्स ने कभी कम्यूनिज़्म को यूरोप का प्रेत कहा था; तब कौन सोचता था कि एक दिन स्वयं कम्यूनिज़्म के लिए इतिहास एक प्रेत बन जाएगा ?
16 जनवरी, 2001
किन्तु इससे बड़ी त्रासदी शायद यह है कि जब मनुष्य अपना घर छोड़े बिना निर्वासित हो जाता है, अपने ही घर में एक शरणार्थी की तरह रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। फ्रांस की सबसे मौलिक अन्तर्दृष्टिसंपन्न चिन्तक सिमोन वेल कहा करती थीं कि आधुनिक जीवन की सबसे भयानक, असहनीय और अक्षम्य देन ‘आत्मा-उन्मूलन’ का बोध है। यह एक ऐसा वेस्टलैंड, आन्तरिक मरुस्थल है, जहाँ मनुष्य के समस्त संरक्षण स्थल-ईश्वर, परंपरा अतीत, प्रकृति-जो एक समय उसके आत्म को गठित और रूपायित करते थे, उससे छूटते जाते हैं। वह स्वयं अपने आत्म से निर्वासित हो जाता है, जो आत्म-उन्मूलन की चरमावस्था है।
अजीब बात है कि यह चरमावस्था, जो अपने में काफी ‘एबनॉर्मल’ है आज हम भारतवासियों की सामान्य अवस्था बन गयी है। आत्म-उन्मूलन का त्रास अब ‘त्रास’ भी नहीं रहा, वह हमारे दैनिक जीवन का अभ्यास बन चुका है। अक्सर वही चीज़ जो सर्वव्यापी है, हमें आँखों से दिखायी नहीं देती। ऊपर की बीमारियाँ दिखायी देती हैं, किन्तु जो कीड़ा हमारे अस्तित्व की जड़ से चिपका है, जिससे समस्त व्याधियों का जन्म होता है-आत्मशून्यता का अन्धकार उसे शब्द देने के लिए जिस आत्मबोध की जरूरत है, हम आज उससे भी वंचित हो गए हैं। इस पुस्तक के अधिकांश निबन्ध-उसके विषय कुछ भी क्यों न हों-विभिन्न कोणों से इस ‘अन्धकार’ को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं। यह वह केन्द्रीय़ ‘थीम’ है जो इन निबन्धों को एक सूत्र में बाँधे है। धर्मनिरपेक्षता, भूमंडलीकरण, ‘आधुनिकता’ बुद्धिजीवी की आध्यात्मिक कुंठाएँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी इस अवरुद्ध मानसिकता की देन हैं जो हर कदम पर हमें अपनी अस्मिता के प्रति सशंकित करते हैं, अपने होने में ‘न होने’ का अहसास कराते हैं। ‘उत्तर-औपनिवेशिकता’ के दौर में वे हमें अपने अन्तर्निहित औपनिवेशिक अवशेषों से अवगत कराते हैं।
पुस्तक के दूसरे खंड में मैंने भारती की कहानियों और बेगड़जी की नर्मदा यात्रा पर अपनी आत्मीय प्रतिक्रियाएँ प्रगट की हैं। यद्यपि इन्हें दोनों लेखकों की पुस्तकों की प्रस्तावनाओं के रूप में लिखा गया था, किन्तु उनके बहाने मैं उन लेखकों के प्रति अपना कृतज्ञता-ज्ञापन कर सका हूँ, जिनके लेखन ने इतने अलग ढंग से मुझे अपने देश और समय के प्रति सम्वेदनशील बनाने में योगदान है।
पुस्तक का अन्तिम खंड बीते हुए इतिहास की दो मर्मान्तक घटनाओं को-1968 में चेकोस्लोवाकिया पर सोवियत सेनाओं का आक्रमण और 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा-दो अलग काल-बिन्दुओं से देखने का प्रयास है; एक जो उनका जीवन्त, स्पन्दित वर्तमान था, दूसरे अब, जब वे सिर्फ अतीत की स्मृति मात्र बनकर रह गये हैं। इतिहास का अपराध-बोध कितना हास्यास्पद हो सकता है, यह इससे विदित होता है, कि वे लोग जो एक समय में ‘इतिहास की दुहाई’ देते फिरते थे, वे आज उससे मुँह चुराने लगे हैं, मानो वह कोई प्रेत हो जिससे वह जल्द से जल्द अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते हों मार्क्स ने कभी कम्यूनिज़्म को यूरोप का प्रेत कहा था; तब कौन सोचता था कि एक दिन स्वयं कम्यूनिज़्म के लिए इतिहास एक प्रेत बन जाएगा ?
16 जनवरी, 2001
-निर्मल वर्मा
मेरे लिए भारतीय होने का अर्थ
(स्वतन्त्रता के पचास वर्ष बाद)
स्वतन्त्रता मिले पचास वर्ष गुजर गए। मैं सोचता हूँ ?
लोग
पूछते हैं, परिचर्चाएँ होती हैं, जश्न मनाए जाते हैं-लेकिन फिर भी लगता
है, जैसे हाथ से कुछ छूट गया है, कोई भरा-पूरा प्रतीक, जिसको हम उस जमीन,
जमीन के टुकड़े के साथ सम्पृक्त कर सकें, जिसे देश की संज्ञा दी जाती है;
क्या मैं उसे प्यार करता हूँ ? क्या जमीन के एक टुकड़े से प्यार किया जा
सकता है, जिसका अपना आकाश है, अतीत है; जहाँ जीते हुए लोग ही नहीं,
मृतात्माएँ भी बसती हैं ? देशभक्ति, देशप्रेम....क्या .ये सिर्फ थोथे शब्द
हैं, जिन्हें हमारे आधुनिक बुद्धिजीवी मुँह पर लाते हुए झिझकते हैं, जैसे
वे कोई अपशब्द हों, सिर्फ एक सतही, मस्ती भावुकता, और कुछ नहीं
?
कौन स्वतन्त्र हुआ ? वे हिकारत से पूछते हैं....गरीब, अमीर, छोटे बड़े,
कौन ? और यदि कोई उत्तर में कहें....मैं और तुम नहीं, बल्कि...वह, जो
हमारे बीच में है, हमें बाँधता हुआ, शताब्दियों से हमें
‘हम’
बनाता हुआ, खुद अदृश्य होते हुए भी हमें एक परिदृश्य में अंकित करता
हुआ,......क्या है यह ? क्या अनाम भावना को कोई नाम दिया जा
सकता है
?
भवनाएँ भी घटनाएँ होती हैं, आत्मा की घटनाएँ.. जैसा नादीन गॉडीमर ने कहा है। मेरे लिए ‘देशप्रेम’ एक ऐसी ही घटना है। मेरे जीवन में यह घटना कब घटी कहना असम्भव है, किन्तु एक बार जन्म लेने के पश्चात वह बेल की तरह फैलती गई। यह एक विचित्र भावना है जो किसी घटना की प्रतिक्रिया में नहीं जगती, बल्कि स्वयं अपने भीतर उच्छ्वासित होती है। हम उस पर अँगुली नहीं रख सकते, जैसे हम देश को छूकर उसकी समग्रता में नहीं पा सकते, सिवा एटलस के नक्शे पर, किन्तु तब बोर्खेस की कहानी की तरह नक्शा उतना बड़ा ही होना चाहिए, जितना बड़ा देश है, उसकी जमीन, पड़ाहों, नदी-नालों के इंच-इंच को अपने में समोता हुआ !
नहीं, देश के प्रति यह लगाव न तो इतिहास में अंकित है, न भूगोल की छड़ी से नापा जा सकता है, क्योंकि अन्ततः वह...एक स्मृति है, व्यक्तिगत जीवन से कहीं अधिक विराट और समय की सीमाओं से कहीं अधिक विस्तीर्ण....हमारे समस्त पूर्वजन्मों का पवित्र-स्थल, जहाँ कभी हमारे पूर्वज और पुरखे रहते आए थे। यदि हर भावना एक घटना है, तो ‘देशप्रेम’ एक चिरन्तन घटना है, हर पीढ़ी की आत्मा में नए सिरे से घटती हुई।
किन्तु वह कोई अमूर्त भावना नहीं; एक कविता की तरह वह किसी ठोस घटना अथवा अनुभव के धुँधले, टीसते, टिमटिमाते बिन्दु से उत्पन्न हो सकती है। अपनी बात कहूँ तो मुझे बचपन का वह क्षण याद आता है,, जब मैं माँ के साथ ट्रेन में बैठकर जा रहा था। कहाँ जा रहा था। कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैं सो रहा था, अचानक मुझे धड़धड़ाती-सी आवाज सुनाई दी; हमारी ट्रेन पुल पर से गुजर रही थी। माँ ने जल्दी से मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे और मुझसे कहा कि मैं उन्हें नीचे फेंक दूँ। नीचे नदी में। नदी ? कहाँ थी वह ? मैंने पुल के नीचे झाँका, शाम के डूबते आलोक में एक पीली, डबडबायी-सी रेखा चमक रही थी। पता नहीं, वह कौन-सी नदी थी, गंगा, कावेरी या नर्वदा ? मेरी माँ के लिए सब नदियाँ पवित्र थीं।
यह मेरे लिए अपने देश ‘ भारत’ की पहली छवि थी, जो मेरी समृति में टँगी रह गई है....वह शाम, वह पुल के परे रेत के ढूह और डूबता सूरज और एक अनाम नदी...कहीं से कहीं की ओर जाती हुई ! मुझे लगता है, अपने देश के साथ मेरा प्रेम प्रसंग यहीं से शुरू हुआ था...उत्पीड़ित, उन्मादपूर्ण, कभी-कभी बेहद निराशापूर्ण; किंतु आज मुझे लगता है कि अन्य प्रेम-प्रसंगों की तुलना में वह कितनी छोटी-सी घटना से शुरू हुआ था, माँ का मुझे सोते में हिलाना, दिल की धड़कन, नदी में फेंका हुआ पैसा ....बस इतना ही
बाद के वर्षों में मेरे भीतर यह विश्वास जमता गया, कि देशप्रेम यदि ‘आत्मा की घटना’ है, तो सिर्फ एक ऐसी संस्कृति में पल्लवित होती है, जहाँ ‘स्पेस’ और ‘स्मृति’ अन्तर्गुम्फित हो सकें। मनुष्य और पशु के सम्बन्ध की बात तो अलग रही, उन चीजों का परस्पर सम्बन्ध भी बहुत गहरा हो, जो ऊपर से अजीवन्त दिखाई देते हैं.....पत्थर, नदी, पहाड़, पेड़....आपस में किंतु अपने अन्तर्सम्बधों में वे एक जीवन्त पवित्रता का गौरव, एक तरह की धार्मिक संवेदना ग्रहण कर लेते हैं। यह क्या महज संयोग था कि हमारे यहाँ प्रकृति के इन आत्मीय उपकरणों के प्रति लगाव ने ‘देशभक्ति’ की भावना को जन्म दिया जो राष्ट्र की सेक्युलर, और संकीर्ण अवधारणा से बहुत भिन्न था ? क्या भारत का कोई ऐसा कोना, जहाँ रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के प्रतीक मनुष्य को अपने जीवन की अर्थवत्ता पाने में सहायक नहीं होते ? यदि एक भूखंड में जीता हुआ व्यक्ति एक ‘रूपक’ में अपने होने का प्रत्यक्षीकरण करता है, तो यह वहीं सम्भव हो सकता है, जहाँ भूगोल की देह पर संस्कृति के स्मृति-स्थल अंकित रहते हैं। पत्थर को छूते हुए कोई देवता, नदी का स्पर्श करते ही कोई स्मृति,पहाड़ पर चढ़ते हुए किसी पौराणिक यात्रा की अन्तर्कथा ऐसे पदचिन्ह हैं, जिन पर कदम रखते हुए हम अपनी जीवन-यात्रा को तीर्थ-यात्रा में परिणत कर लेते हैं।
अतीत में देश के प्रति यह भावना अन्य देशों में भी देखी जा सकती थी, जहाँ देश-प्रेम का गहरा सम्बन्ध संस्कृति और परम्परा की स्मृति से जुड़ा था। मुझे तारकोवस्की की फिल्म ‘मिरर’ की याद आती है, जिसमें एक पत्र पुश्किन का पत्र अपने मित्र को पढ़कर सुनाता है, और उस पत्र में पुश्किन रूस के बारे में जो कुछ अपने उदगार प्रकट करते हैं, वे एक अजीब तरह का आध्यात्मिक उन्मेष के लिए हुए हैं, वे लिखते हैं, ‘‘एक लेखक होने के नाते मुझे कभी-कभी अपने देश के प्रति गहरी झुँझलाहट और कटुता महसूस होती है लेकिन मैं सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर अपना देश किसी और देश से नहीं बदलना चाहूँगा। न ही अपने देश के इतिहास को किसी दूसरे इतिहास में परिणत करना चाहूँगा, जो ईश्वर ने मेरे पूर्वजों के हाथों में दिया था।’’
शब्द पुश्किन के हैं, देश ‘मदर रशिया’ के बारे में, लेकिन उनमें देशभक्ति का एक ऐसा धार्मिक आयाम दिखाई देता है, जिससे हमें विवेकानन्द, श्री अरविन्द और गाँधी की भावनाएँ प्रतिध्वनित होती सुनाई देती हैं, जो उन्होंने समय-समय पर गहरे भावोन्मेष के साथ भारत-भूमि के प्रति प्रकट की थीं। आज के आधुनिक भारतीय धर्मनिरपेक्षीय बुद्धिजीवियों को भारत के सन्दर्भ में ईश्वर और पूर्वजों की स्मृति का उल्लेख करना कितना अजीब जान पड़ता होगा,. इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। वे लोग तो वन्दे मातरम्’ जैसे गीत में भी साम्प्रदायिकता सूँघ लेते हैं। सच बात तो यह है कि देशप्रेम की भावना को देश से जुड़ी स्मृतियों और उसके इतिहास की धूल में सनी पीड़ाओं को अलग करते ही इस भावना की गरिमा और पवित्रता नष्ट हो जाती है। वह या तो राष्ट्रवाद के संकीर्ण और कुत्सित पूर्वाग्रह में बदल जाती है। अथवा आत्म घृणा में....दोनों ही एक तस्वीर के दो पहलू हैं।
कोई राष्ट्र जब अपनी सांस्कृतिक जड़ों से उन्मूलित होने लगता है, तो भले ही ऊपर से बहुत सशक्त और स्वस्थ दिखाई दे....भीतर से मुरझाने लगता है। स्वतन्त्रता के बाद भारत के सामने यह सबसे दुर्गम चुनौती थी.....पाँच हजार वर्ष पुरानी परम्परा से क्या ऐसे ‘राष्ट्र’ का जन्म हो सकता है, जो अपने में ‘एक’ होता हुआ भी उन ‘अनेक’ स्रोतों से अपनी संजीवनी शक्ति खींच सके, जिसने भारतीय सभ्यता का रूप-गठन किया था। यह एक ऐसी अद्भुत ‘सिम्फनी’ रचने की परिकल्पना थी, जिसके संगीत में हर छोटे-से-छोटे वाद्य का सुर संयोजित होकर गूँजता था। जिस तरह गाँधी की आंखों से कभी ‘आखिरी आदमी’ ओझल होता था, वैसे ही इस सभ्यता के अदृश्य कंडक्टर का बेटन ऑरकेस्ट्रा की अन्तिम पंक्ति में बैठे वादक को नहीं भूलता था। कोई परम्परा इतनी छोटी इतनी नगण्य नहीं थीं, जिसकी ‘आवाज’ भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में से जुड़कर अपनी विशिष्ट लय में अनुगंजित न होती हो। बहुत वर्ष पहले जब मैंने मध्य प्रदेश के हतस्थल में नर्वदा को सहस्त्र धाराओं में फूटते देखा था, तो मुझे वह भारतीय, संस्कृति का सबसे उजला प्रतीक जान पड़ता था। क्या यह प्रतीक आज कुछ मैला-सा नहीं पड़ गया ?
पिछले पचास वर्षों में यदि कोई दुखदायी घटना हुई है तो यह कि हमने भारतीय संस्कृति की इस प्रवाहमान धारा को धीरे-धीरे सूख जाने दिया। हम भूल गए कि भारत केवल एक राज्य-सत्ता, नेशन स्टेट ही नहीं है- जैसा पश्चिमी की अनेक राष्ट्रीय सत्ताएँ हैं..,जो अपनी सीमाओं में आबद्ध होकर ही अपनी अस्मित परिभाषा कर पाते हैं। इसके विपरीत शताब्दियों से हमारे देश की सीमाएँ वे स्वागत द्वार रहे हैं, जिनके भीतर आते ही उत्पीड़ित और त्रस्त जातियाँ अपने को सुरक्षित पाती रही हैं। सातवीं-आठवीं शती में इरान पर इस्लामी आक्रमण के बाद पारसियों ने अपना शरण-स्थल भारत में ही ढूँढा था। कौन सोच सकता था कि यूरोप से भागे हुए यहूदियों को सुरक्षा देने वाले कोचीन के एक हिन्दू राजा होंगे...जो केवल उन्हें सहायता ही न देंगे, बल्कि अपने राज्य में उन्हें अपना प्रार्थना-गृह, सिनागौग बनाने में मदद करेंगे। हजारों तिब्बती निवासियों और भिक्षुओं का दलाई लाभा के साथ भारत में शरण लेने आना तो कोई पुराई घटना भी नहीं है, जिसे भुलाया जा सके। एक प्राचीन वट-वृक्ष की तरह भारतीय संस्कृति ने अपनी छाया तले सैकड़ों जातियों, जनजातियों, धार्मिक समुदायों को वह पवित्र स्पेस प्रदान की थी, जहाँ वे मुक्त हवा में साँस ले सकें। यह केवल सहिष्णुता की बात नहीं थी, जहाँ ‘अन्य’ को अपने से अलग मानकर उसे सहन किया जाता था, बल्कि इसके पीछे कहीं यह मान्यता काम करती थी कि विभिन्न विश्वासों के बीच सत्य समान रूप से क्रियाशील रहती है....अपने में अखंडित और अपरिवर्तन ! भारतीय सभ्यता को अपनी यह अनमोल अन्तर्दृष्टि स्वयं अपनी आध्यात्मिक परम्परा से प्राप्त हुई थी, जहाँ ‘आत्म’ और ‘अन्य’ के बीच का भेद अविद्या का लक्षण था, सत्य का नहीं।
भारतीय सभ्यता के इस आध्यात्मिक सिद्धान्त को अनदेखा करने का ही यह दुष्परिणाम था कि पश्चिमी इतिहासकारों...और उनके भारतीय ‘सबाल्टर्न’ अनुयायियों की आँखों में भारत की अपनी कोई सांस्कृतिक इयत्ता नहीं, वह तो सिर्फ कबीली जातियों सम्प्रदायों का महज एक पुंज मात्र है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि ऐसा होता, तो भारत की सत्ता और उसके अन्तर्गत रहनेवाले सांस्कृतिक समूहों की अस्मिता कब की नष्ट हो गई होती, उसी तरह जैसे अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के साथ हुआ, जिनकी संस्कृति के आज सिर्फ अवशेष दिखाई देते हैं।
यदि भारत भी ‘सभ्यता बोध’ और सांस्कृतिक परम्पराएँ आज भी मौजूद हैं, तो उसका मुख्य कारण वह केन्द्रीय आध्यात्मिक तत्त्व है, जिसमें इतनी क्षमता और ऊर्जा थी कि इतिहास के निर्मम थपेड़ों के बावजूद वह समस्त प्रभावों को अपने भीतर समाहित कर सका। अंग्रेजी मार्क्सवाद इतिहासकार ई.पी. टॉप्सन के शब्दों में ‘‘भारत सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं दुनिया का सबसे महत्तवपूर्ण देश है, जिस पर सारी दुनिया का भविष्य निर्भर करता है। भारतीय समाज में दुनिया के विभिन्न दिशाओं से आते प्रभाव एक-दूसरे से मिलते हैं ।’’ टॉप्सन के इन शब्दों को पढ़ते हुए मैं सोचने लगा कि भारत में कितने मार्क्सवाद हैं, जिनमें अपने देश के प्रति के उदगार प्रकट करने की ईमानदारी और विनम्रता हो।
देखा जाए तो यह ‘विचार तत्त्व’ ही है जो हमारे राष्ट्रीय जीवन की विपन्नता और ऐतिहासिक दुर्घटनाओं के बावजूद इस देश को बचाए रखने में सफल हुआ है। देश-विभाजन से बड़ी भीषण दुर्घटना और क्या हो सकती थी ? यदि गाँधीजी के लिए यह उनके जीवन का सबसे मर्मान्तक घाव था, तो इसलिए कि आज के अनेक राजनेताओं की तरह उनके लिए देश की भौगोलिक अखंडता सिर्फ एक संविधानिक बात नहीं थी, जहाँ सिर्फ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना महत्त्वपूर्ण हो।
इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी इन सीमाओं के भीतर शताब्दियों से हमारे पुरखों-पूर्वजों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों, स्मृतियों, स्वप्नों का साँझा किया था-एक जीवित संग्रहालय-जिसमें कला, साहित्य और दर्शन की असाधारण रचनाएँ सृजित हुई थीं। कश्मीर केवल भौगोलिक दृष्टि से भारत का ही नहीं रहा, बल्कि अल-बरूनी के शब्दों में हिन्दू दर्शन और आध्यात्मिक शोध का यदि काशी के बाद कोई अध्ययन-केन्द्र था, तो वह कश्मीर था। शैव-बौद्ध दर्शन और राजरंगिणी जैसी इतिहास-रचनाओं को क्या हम अपनी पारम्परिक सम्पदा से अलग कर देख सकते हैं ? धर्मपरिवर्तन से ही किसी देश का अतीत परिवर्तन नहीं हो जाता। एक देश की पहचान सिर्फ उन लोगों से नहीं बनती, जो आज उनमें जीते हैं, बल्कि उनसे भी बनती है, जो एक समय में जीवित थे और आज उनकी मिट्टी के नीचे दबे हैं। समय के बीतने के साथ भूमि की भौगोलिक सीमाएँ धीरे-धीरे संस्कृति के नक्शे में बदल जाती हैं। एक के खंडित होते ही दूसरे की गरिमा को भी चोट पहुँचती है।
भवनाएँ भी घटनाएँ होती हैं, आत्मा की घटनाएँ.. जैसा नादीन गॉडीमर ने कहा है। मेरे लिए ‘देशप्रेम’ एक ऐसी ही घटना है। मेरे जीवन में यह घटना कब घटी कहना असम्भव है, किन्तु एक बार जन्म लेने के पश्चात वह बेल की तरह फैलती गई। यह एक विचित्र भावना है जो किसी घटना की प्रतिक्रिया में नहीं जगती, बल्कि स्वयं अपने भीतर उच्छ्वासित होती है। हम उस पर अँगुली नहीं रख सकते, जैसे हम देश को छूकर उसकी समग्रता में नहीं पा सकते, सिवा एटलस के नक्शे पर, किन्तु तब बोर्खेस की कहानी की तरह नक्शा उतना बड़ा ही होना चाहिए, जितना बड़ा देश है, उसकी जमीन, पड़ाहों, नदी-नालों के इंच-इंच को अपने में समोता हुआ !
नहीं, देश के प्रति यह लगाव न तो इतिहास में अंकित है, न भूगोल की छड़ी से नापा जा सकता है, क्योंकि अन्ततः वह...एक स्मृति है, व्यक्तिगत जीवन से कहीं अधिक विराट और समय की सीमाओं से कहीं अधिक विस्तीर्ण....हमारे समस्त पूर्वजन्मों का पवित्र-स्थल, जहाँ कभी हमारे पूर्वज और पुरखे रहते आए थे। यदि हर भावना एक घटना है, तो ‘देशप्रेम’ एक चिरन्तन घटना है, हर पीढ़ी की आत्मा में नए सिरे से घटती हुई।
किन्तु वह कोई अमूर्त भावना नहीं; एक कविता की तरह वह किसी ठोस घटना अथवा अनुभव के धुँधले, टीसते, टिमटिमाते बिन्दु से उत्पन्न हो सकती है। अपनी बात कहूँ तो मुझे बचपन का वह क्षण याद आता है,, जब मैं माँ के साथ ट्रेन में बैठकर जा रहा था। कहाँ जा रहा था। कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैं सो रहा था, अचानक मुझे धड़धड़ाती-सी आवाज सुनाई दी; हमारी ट्रेन पुल पर से गुजर रही थी। माँ ने जल्दी से मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे और मुझसे कहा कि मैं उन्हें नीचे फेंक दूँ। नीचे नदी में। नदी ? कहाँ थी वह ? मैंने पुल के नीचे झाँका, शाम के डूबते आलोक में एक पीली, डबडबायी-सी रेखा चमक रही थी। पता नहीं, वह कौन-सी नदी थी, गंगा, कावेरी या नर्वदा ? मेरी माँ के लिए सब नदियाँ पवित्र थीं।
यह मेरे लिए अपने देश ‘ भारत’ की पहली छवि थी, जो मेरी समृति में टँगी रह गई है....वह शाम, वह पुल के परे रेत के ढूह और डूबता सूरज और एक अनाम नदी...कहीं से कहीं की ओर जाती हुई ! मुझे लगता है, अपने देश के साथ मेरा प्रेम प्रसंग यहीं से शुरू हुआ था...उत्पीड़ित, उन्मादपूर्ण, कभी-कभी बेहद निराशापूर्ण; किंतु आज मुझे लगता है कि अन्य प्रेम-प्रसंगों की तुलना में वह कितनी छोटी-सी घटना से शुरू हुआ था, माँ का मुझे सोते में हिलाना, दिल की धड़कन, नदी में फेंका हुआ पैसा ....बस इतना ही
बाद के वर्षों में मेरे भीतर यह विश्वास जमता गया, कि देशप्रेम यदि ‘आत्मा की घटना’ है, तो सिर्फ एक ऐसी संस्कृति में पल्लवित होती है, जहाँ ‘स्पेस’ और ‘स्मृति’ अन्तर्गुम्फित हो सकें। मनुष्य और पशु के सम्बन्ध की बात तो अलग रही, उन चीजों का परस्पर सम्बन्ध भी बहुत गहरा हो, जो ऊपर से अजीवन्त दिखाई देते हैं.....पत्थर, नदी, पहाड़, पेड़....आपस में किंतु अपने अन्तर्सम्बधों में वे एक जीवन्त पवित्रता का गौरव, एक तरह की धार्मिक संवेदना ग्रहण कर लेते हैं। यह क्या महज संयोग था कि हमारे यहाँ प्रकृति के इन आत्मीय उपकरणों के प्रति लगाव ने ‘देशभक्ति’ की भावना को जन्म दिया जो राष्ट्र की सेक्युलर, और संकीर्ण अवधारणा से बहुत भिन्न था ? क्या भारत का कोई ऐसा कोना, जहाँ रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के प्रतीक मनुष्य को अपने जीवन की अर्थवत्ता पाने में सहायक नहीं होते ? यदि एक भूखंड में जीता हुआ व्यक्ति एक ‘रूपक’ में अपने होने का प्रत्यक्षीकरण करता है, तो यह वहीं सम्भव हो सकता है, जहाँ भूगोल की देह पर संस्कृति के स्मृति-स्थल अंकित रहते हैं। पत्थर को छूते हुए कोई देवता, नदी का स्पर्श करते ही कोई स्मृति,पहाड़ पर चढ़ते हुए किसी पौराणिक यात्रा की अन्तर्कथा ऐसे पदचिन्ह हैं, जिन पर कदम रखते हुए हम अपनी जीवन-यात्रा को तीर्थ-यात्रा में परिणत कर लेते हैं।
अतीत में देश के प्रति यह भावना अन्य देशों में भी देखी जा सकती थी, जहाँ देश-प्रेम का गहरा सम्बन्ध संस्कृति और परम्परा की स्मृति से जुड़ा था। मुझे तारकोवस्की की फिल्म ‘मिरर’ की याद आती है, जिसमें एक पत्र पुश्किन का पत्र अपने मित्र को पढ़कर सुनाता है, और उस पत्र में पुश्किन रूस के बारे में जो कुछ अपने उदगार प्रकट करते हैं, वे एक अजीब तरह का आध्यात्मिक उन्मेष के लिए हुए हैं, वे लिखते हैं, ‘‘एक लेखक होने के नाते मुझे कभी-कभी अपने देश के प्रति गहरी झुँझलाहट और कटुता महसूस होती है लेकिन मैं सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर अपना देश किसी और देश से नहीं बदलना चाहूँगा। न ही अपने देश के इतिहास को किसी दूसरे इतिहास में परिणत करना चाहूँगा, जो ईश्वर ने मेरे पूर्वजों के हाथों में दिया था।’’
शब्द पुश्किन के हैं, देश ‘मदर रशिया’ के बारे में, लेकिन उनमें देशभक्ति का एक ऐसा धार्मिक आयाम दिखाई देता है, जिससे हमें विवेकानन्द, श्री अरविन्द और गाँधी की भावनाएँ प्रतिध्वनित होती सुनाई देती हैं, जो उन्होंने समय-समय पर गहरे भावोन्मेष के साथ भारत-भूमि के प्रति प्रकट की थीं। आज के आधुनिक भारतीय धर्मनिरपेक्षीय बुद्धिजीवियों को भारत के सन्दर्भ में ईश्वर और पूर्वजों की स्मृति का उल्लेख करना कितना अजीब जान पड़ता होगा,. इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। वे लोग तो वन्दे मातरम्’ जैसे गीत में भी साम्प्रदायिकता सूँघ लेते हैं। सच बात तो यह है कि देशप्रेम की भावना को देश से जुड़ी स्मृतियों और उसके इतिहास की धूल में सनी पीड़ाओं को अलग करते ही इस भावना की गरिमा और पवित्रता नष्ट हो जाती है। वह या तो राष्ट्रवाद के संकीर्ण और कुत्सित पूर्वाग्रह में बदल जाती है। अथवा आत्म घृणा में....दोनों ही एक तस्वीर के दो पहलू हैं।
कोई राष्ट्र जब अपनी सांस्कृतिक जड़ों से उन्मूलित होने लगता है, तो भले ही ऊपर से बहुत सशक्त और स्वस्थ दिखाई दे....भीतर से मुरझाने लगता है। स्वतन्त्रता के बाद भारत के सामने यह सबसे दुर्गम चुनौती थी.....पाँच हजार वर्ष पुरानी परम्परा से क्या ऐसे ‘राष्ट्र’ का जन्म हो सकता है, जो अपने में ‘एक’ होता हुआ भी उन ‘अनेक’ स्रोतों से अपनी संजीवनी शक्ति खींच सके, जिसने भारतीय सभ्यता का रूप-गठन किया था। यह एक ऐसी अद्भुत ‘सिम्फनी’ रचने की परिकल्पना थी, जिसके संगीत में हर छोटे-से-छोटे वाद्य का सुर संयोजित होकर गूँजता था। जिस तरह गाँधी की आंखों से कभी ‘आखिरी आदमी’ ओझल होता था, वैसे ही इस सभ्यता के अदृश्य कंडक्टर का बेटन ऑरकेस्ट्रा की अन्तिम पंक्ति में बैठे वादक को नहीं भूलता था। कोई परम्परा इतनी छोटी इतनी नगण्य नहीं थीं, जिसकी ‘आवाज’ भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में से जुड़कर अपनी विशिष्ट लय में अनुगंजित न होती हो। बहुत वर्ष पहले जब मैंने मध्य प्रदेश के हतस्थल में नर्वदा को सहस्त्र धाराओं में फूटते देखा था, तो मुझे वह भारतीय, संस्कृति का सबसे उजला प्रतीक जान पड़ता था। क्या यह प्रतीक आज कुछ मैला-सा नहीं पड़ गया ?
पिछले पचास वर्षों में यदि कोई दुखदायी घटना हुई है तो यह कि हमने भारतीय संस्कृति की इस प्रवाहमान धारा को धीरे-धीरे सूख जाने दिया। हम भूल गए कि भारत केवल एक राज्य-सत्ता, नेशन स्टेट ही नहीं है- जैसा पश्चिमी की अनेक राष्ट्रीय सत्ताएँ हैं..,जो अपनी सीमाओं में आबद्ध होकर ही अपनी अस्मित परिभाषा कर पाते हैं। इसके विपरीत शताब्दियों से हमारे देश की सीमाएँ वे स्वागत द्वार रहे हैं, जिनके भीतर आते ही उत्पीड़ित और त्रस्त जातियाँ अपने को सुरक्षित पाती रही हैं। सातवीं-आठवीं शती में इरान पर इस्लामी आक्रमण के बाद पारसियों ने अपना शरण-स्थल भारत में ही ढूँढा था। कौन सोच सकता था कि यूरोप से भागे हुए यहूदियों को सुरक्षा देने वाले कोचीन के एक हिन्दू राजा होंगे...जो केवल उन्हें सहायता ही न देंगे, बल्कि अपने राज्य में उन्हें अपना प्रार्थना-गृह, सिनागौग बनाने में मदद करेंगे। हजारों तिब्बती निवासियों और भिक्षुओं का दलाई लाभा के साथ भारत में शरण लेने आना तो कोई पुराई घटना भी नहीं है, जिसे भुलाया जा सके। एक प्राचीन वट-वृक्ष की तरह भारतीय संस्कृति ने अपनी छाया तले सैकड़ों जातियों, जनजातियों, धार्मिक समुदायों को वह पवित्र स्पेस प्रदान की थी, जहाँ वे मुक्त हवा में साँस ले सकें। यह केवल सहिष्णुता की बात नहीं थी, जहाँ ‘अन्य’ को अपने से अलग मानकर उसे सहन किया जाता था, बल्कि इसके पीछे कहीं यह मान्यता काम करती थी कि विभिन्न विश्वासों के बीच सत्य समान रूप से क्रियाशील रहती है....अपने में अखंडित और अपरिवर्तन ! भारतीय सभ्यता को अपनी यह अनमोल अन्तर्दृष्टि स्वयं अपनी आध्यात्मिक परम्परा से प्राप्त हुई थी, जहाँ ‘आत्म’ और ‘अन्य’ के बीच का भेद अविद्या का लक्षण था, सत्य का नहीं।
भारतीय सभ्यता के इस आध्यात्मिक सिद्धान्त को अनदेखा करने का ही यह दुष्परिणाम था कि पश्चिमी इतिहासकारों...और उनके भारतीय ‘सबाल्टर्न’ अनुयायियों की आँखों में भारत की अपनी कोई सांस्कृतिक इयत्ता नहीं, वह तो सिर्फ कबीली जातियों सम्प्रदायों का महज एक पुंज मात्र है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि ऐसा होता, तो भारत की सत्ता और उसके अन्तर्गत रहनेवाले सांस्कृतिक समूहों की अस्मिता कब की नष्ट हो गई होती, उसी तरह जैसे अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के साथ हुआ, जिनकी संस्कृति के आज सिर्फ अवशेष दिखाई देते हैं।
यदि भारत भी ‘सभ्यता बोध’ और सांस्कृतिक परम्पराएँ आज भी मौजूद हैं, तो उसका मुख्य कारण वह केन्द्रीय आध्यात्मिक तत्त्व है, जिसमें इतनी क्षमता और ऊर्जा थी कि इतिहास के निर्मम थपेड़ों के बावजूद वह समस्त प्रभावों को अपने भीतर समाहित कर सका। अंग्रेजी मार्क्सवाद इतिहासकार ई.पी. टॉप्सन के शब्दों में ‘‘भारत सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं दुनिया का सबसे महत्तवपूर्ण देश है, जिस पर सारी दुनिया का भविष्य निर्भर करता है। भारतीय समाज में दुनिया के विभिन्न दिशाओं से आते प्रभाव एक-दूसरे से मिलते हैं ।’’ टॉप्सन के इन शब्दों को पढ़ते हुए मैं सोचने लगा कि भारत में कितने मार्क्सवाद हैं, जिनमें अपने देश के प्रति के उदगार प्रकट करने की ईमानदारी और विनम्रता हो।
देखा जाए तो यह ‘विचार तत्त्व’ ही है जो हमारे राष्ट्रीय जीवन की विपन्नता और ऐतिहासिक दुर्घटनाओं के बावजूद इस देश को बचाए रखने में सफल हुआ है। देश-विभाजन से बड़ी भीषण दुर्घटना और क्या हो सकती थी ? यदि गाँधीजी के लिए यह उनके जीवन का सबसे मर्मान्तक घाव था, तो इसलिए कि आज के अनेक राजनेताओं की तरह उनके लिए देश की भौगोलिक अखंडता सिर्फ एक संविधानिक बात नहीं थी, जहाँ सिर्फ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना महत्त्वपूर्ण हो।
इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी इन सीमाओं के भीतर शताब्दियों से हमारे पुरखों-पूर्वजों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों, स्मृतियों, स्वप्नों का साँझा किया था-एक जीवित संग्रहालय-जिसमें कला, साहित्य और दर्शन की असाधारण रचनाएँ सृजित हुई थीं। कश्मीर केवल भौगोलिक दृष्टि से भारत का ही नहीं रहा, बल्कि अल-बरूनी के शब्दों में हिन्दू दर्शन और आध्यात्मिक शोध का यदि काशी के बाद कोई अध्ययन-केन्द्र था, तो वह कश्मीर था। शैव-बौद्ध दर्शन और राजरंगिणी जैसी इतिहास-रचनाओं को क्या हम अपनी पारम्परिक सम्पदा से अलग कर देख सकते हैं ? धर्मपरिवर्तन से ही किसी देश का अतीत परिवर्तन नहीं हो जाता। एक देश की पहचान सिर्फ उन लोगों से नहीं बनती, जो आज उनमें जीते हैं, बल्कि उनसे भी बनती है, जो एक समय में जीवित थे और आज उनकी मिट्टी के नीचे दबे हैं। समय के बीतने के साथ भूमि की भौगोलिक सीमाएँ धीरे-धीरे संस्कृति के नक्शे में बदल जाती हैं। एक के खंडित होते ही दूसरे की गरिमा को भी चोट पहुँचती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i