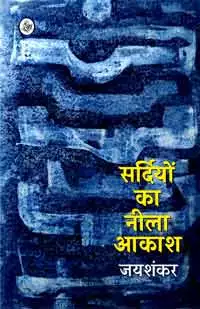|
कहानी संग्रह >> बारिश, ईश्वर और मृत्यु बारिश, ईश्वर और मृत्युजयशंकर
|
39 पाठक हैं |
|||||||
इसमें मनुष्य के द्वारा सहन करने वाले कष्टों का वर्णन किया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
स्कूल के टेरेस पर अपनी उन चिठ्ठियों को फाड़ते हुए मैं उस व्यक्ति को याद
करता रहा था जिससे मैंने कितना कुछ पाया था और किसके साथ मैंने कुछ पुरानी
और पवित्र चीजों को पहचाना था। प्रेम और उसकी पीड़ा को मैं कभी पहचान ही
नहीं पाता अगर मैंने उस प्रस्ताव के कुछ दिन उसके साथ न बिताये होते।
(सुबह)
कहीं कोई आदमी लड़की की लिखी गई चिठ्ठियों को जलाता है और कहीं कोई औरत
अपने घर की छत पर खड़े होकर जलती चिठ्ठियों से उड़ती आग और धुएँ को देखती
रहती है। इस तरह पुराने प्रेम की पीड़ा परछाईं और पछतावे बीच-बीच में
लोगों को छेड़ते रहते हैं, घेरते रहते हैं।
(एक नीरस कविता)
सदियाँ बीत जाती हैं। समय कितने निराले, लापरवाह और चुपचाप ढंग से बढ़ता
चला जाता है। जिस पर बीतती है, वही जनता है और दूसरे के लिए कभी भी उसका
कोई महत्व नहीं रहता। समय हर आदमी के जीवन में अपने ढंग से बनता, उतरता और
गुजरता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि हर आदमी का अपना समय होता है।
केवल उसका समय ही अकेला समय।
(दूसरा प्रेम)
और उसके जाने के बाद मैं सोचती रही कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं आता तब
मेरे साथ क्या-क्या नहीं होता, मैं किन अभावों के बीच जीती कितनी-कितनी
बातों को महसूस न कर पाती। इस तरह सोचते चले जाने का सिलसिला लम्बा भी था
और दिलचस्प भी। जो लोग हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं, उनके न जुड़ने के
बारे में सोचना अपने आपको खाली होते देखना है, अपने आपको आधा-अधूरा पाना
है।
(मुरमुंडा)
घरघोर बारिश के उन दिनों में न जाने क्यों ऐसा लगता था कि मृत्यु बारिश की
वजह से ही कहीं खड़ी हो जाएगी और मीरा तक आने में अपने संकल्प को भूल
जाएगी। तब तक मृत्यु के संकल्प का मुझे पता ही क्या था ? मीरा का जीवन
समाप्त हुआ और तब ही मेरा जीवन भी शुरु हुआ। उसके नहीं रहने पर, मैंने
उसके होने को जीना शुरू किया।
(बारिश, ईश्वर और मृत्यु)
सुबह
उस रोज मैं उनकी दहलीज से ही लौट आया था। वह मार्च की सुबह थी लेकिन बारिश
हो जाने के बाद का मटियाला उजाला हवा में टँगा था। उनके बहुत पुराने मकान
में वैसे ही बहुत कम रोशनी आती थी इसलिए वे अपनी बड़ी-सी खिड़की खुली ही
रखा करती थीं। मैंने उन्हें खिड़की से ही देख लिया था। वे बेंत की कुर्सी
पर बैठे हुए न जाने किस चीज को लगातार देख रही थीं। उनकी आँखों में शून्य
उतर आया था। उनके बाहर भी शून्य रहा होगा जिसकी तरफ उनकी आँखें खींची हुई
थीं। उस वक्त उनका चेहरा मुझे किसी मृतक चेहरे सा जान पड़ा। कहीं बहुत दूर
गया हुआ। अपनी देह और आत्मा से छूटा हुआ। मैं उनकी बेल बजाने का साहस न
बटोर सका और मैं न चाहते हुए भी उनकी देहरी से लौट आया।
उनके घर से लौटते वक्त वह शहर कुछ ज्यादा ही पराया महसूस होने लगा। उस शहर का वह तालाब भी मन में नहीं उतरा जहाँ उनसे पहचान के पहले की शामों को मैं बिताया करता था। तालाब की सीढ़ियों से तालाब ही नहीं, पड़ोस का पुराना मन्दिर, वहाँ पर आ रहे लोग, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पुजारी, खेलते हुए बच्चे, लौटते हुए परिन्दे और ऐसी कितनी ही चीजों को मैं उन दिनों में देखा करता था। पर उस सुबह वहाँ की पहचान-सी परिचित चीजें भी परायी जान पड़ रही थीं। उनके घर से इस तरह लौटना अपनी तरफ भी लौटना रहा। अपने उन कुछ महीनों में जो मैंने उनके साथ बिताये थे। मुझे सुबह लगा था कि अब उनके साथ जितना कुछ बीताना मेरे भाग्य में लिखा था वह सब बीत चुका है। समय बीतता जाता है। बहता जाता है। इसे मैंने पहली बार तीस बरस की उम्र में, उस पुराने और पराये शहर में महसूस किया था।
एकदम शुरुआत के दिनों में, छोटे शहर की बारिश में समय बीतता ही नहीं था। हमारा स्कूल दुपहर में लगता। मुझे तीन-चार पीरियड पढ़ाना पड़ता। मैं इस प्रसिद्ध स्कूल में आया-आया ही था और प्रिंसिपल मुझ पर बहुत भरोसा नहीं रखते थे। मैं सुबह खाली ही रहता और दुपहर में चार बजे के आसपास खाली हो जाता। तालाब के किनारे मन नहीं लगता तो कुम्हारों के इलाके में चला जाता और वहाँ के मन्दिर की सीढ़ियों, पर बैठा हुआ, बूढ़े हो चले कुम्हारों की बातें सुनता रहता। कुम्हारों के बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। तब तक पुस्तकों में मन लगना शुरू नहीं हुआ था। घर की याद आती रहती और नौकरी से नफरत होती रहती और जिन्दगी से शिकायतें।
बड़ी बहनों की चिट्ठियाँ आती रहतीं और वे दोनों ही मुझे आगे की पढ़ाई की याद दिलाती रहतीं। उन दोनों ने ही पिता के अध्यापक होने की जीवन को करीब से देखा था और वे घर में एक और अध्यापक होने नहीं देना चाहती थीं। मैं बीच-बीच में पढ़ाई के लिए अपना मन बनाता लेकिन उस मन को भरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बारिश के वे दिन, पराये शहर की वे शामें मन को मरा हुआ महसूस करने, मन को मरता हुआ देखने की शामें थीं। मरे हुए मन के मनहूस दिन। जब न मन मौसम से जुड़ता था और न ही मन्दिर के उस परिवेश से जहाँ हमेशा चहल-पहल बनी रहती थी। अब बरसों बाद जब मैं अपने मन को थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ तब मेरे उन दिनों के मन के लिए मुझमें ममत्व जाग पड़ता है। एक तरह की ममतामयी मार्मिकता उस मन के लिए जन्मती है जो मन्दिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मुरझाता रहता था, मरता रहता था।
स्कूल में मैं सबसे कम उम्र का था और ज्यादातर अध्यापक मुझे अनाड़ी समझते थे। कोई-कोई तो मुझे बालों को सँवारने के लिए, कपड़ों को ठीक तरह से प्रेम करने के लिए कहने में भी नहीं हिचकता था। ये वे लोग थे जिन्हें माँ मेरी देखभाल करने के लिए पत्र लिखा करती थी। बहुत पहले ये अध्यापक पिता के साथ किसी शहर में पढ़ाते थे। वे मुझे तालाब के किनारे शाम न गुजारने की सलाहें देते। वे मुझे कुम्हारों की गरीब और गलीज बस्ती में जाने के लिए रोकते। वे मुझे छात्रों से ज्यादा बातें करने के लिए मना करते और इस तरह वे मेरी हर उस बात से असहमत जान पड़ते थे जो मैं अपने मन को मनाने के लिए किया करता था। मैं उनके साथ अपनी शामें गुजार नहीं सकता था और वे यही चाहते थे कि मैं हमेशा उनकी निगरानी में रहूँ या कम से कम उन्हें इन अहसासों में रखूँ कि वे मेरे लोकल गार्जियन हैं। मैं तालाब के किनारे ही अपनी खाली और अकेली शामें गुजारा करता था और मैं कुम्हारों की बस्ती में भी जाया करता था लेकिन मैं अपने स्कूल के अध्यापकों की बातें इत्मीनान और ध्यान से सुना करता था।
बारिश बीत रही थी। बारिश में ही चन्द्रमा पर पहली बार आदमी उतरा था। फिर चन्द्रमा से आये पत्थरों को उस शहर में भी लाया गया जहाँ मैं उन दिनों विज्ञान पढ़ा रहा था। मुझे छात्रों के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की उस लाल इमारत में जाना पड़ा जहाँ पर उन चन्द्रमा के पत्थरों को लोगों के देखने के लिए रखा गया था। उस इमारत के ही हाल में नील आर्मस्ट्रांग की बड़ी-सी तस्वीर के करीब मैं उनसे पहली बार मिला था। वे अपने स्कूल की छात्राओं के साथ वहाँ आयी थीं। मैं बरसों बाद भी इंस्टीट्यूट की दीवार के करीब खड़ी उस युवा लड़की की एक-एक चीज को याद कर सकता हूँ। सर्दियों की उस दुपहर में मैंने नहीं जाना था कि उस युवा लड़की के साथ-साथ में मेरे छोटे शहर में बीते कुछ दिन मेरे अपने जीवन के इतने निर्णायक और अविस्मरणीय दिन रहेंगे कि तीस बरसों के बाद भी उस स्त्री के बारे में बीच बीच में सोचता रहूँगा जिसके सान्निध्य में मैंने अपनी उम्र के तीसवें बरस के कुछ दिन बिताये थे।
अक्टूबर की एक शाम मैं पहली बार उनके घर गया था। उनके घर जाते वक्त बस एक पुल को पार करती थी जिसके नीचे शहर का रेलवे स्टेशन खड़ा रहता। बस की खिड़की से पटरियाँ, प्लेटफॉर्म रेलगाड़ियाँ, यात्री और वे इमारतें नजर आतीं जो स्टेशनों पर रहती हैं। वह स्टेशन भी अंग्रेजों के जमाने में बसा था और उसकी इमारतों में कभी अंग्रेजों के उस शहर में होने के संकेत मिलते थे। उनका घर विक्टोरियन शैली में बना हुआ। वे उस पीले मकान में अपनी छः बरस की बिटिया और अपनी नौकरानी के साथ रहती थीं। उनकी बिटिया जन्म से ही बीमार रहती आयी थी और उसकी देह और दिमाग का विकास धीरे-धीरे हो रहा था। मेरे पहली बार उनके घर जाने पर वे नहीं मिली थीं। वे पुल के पार कहीं संगीत सीखने के लिए जाया करती थीं। उनकी नौकरानी ने मुझे बिठाया था। चाय पिलायी थी। मैं उनके लिए छोटा-सा नोट रखकर लौट आया था।
दीवाली की छुट्टी में मैं अपने घर चला गया। लौटने पर स्टाफरूम में मेरे लिए जो चिट्ठियाँ थीं उनमें एक ग्रीटिंग कार्ड उनका भी था। ग्रीटिंग कार्ड के एक हिस्से में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता को काली स्याही के फाउण्टेन पेन से लिखा गया था। कविता के पड़ोस में कुछ आत्मीय पंक्तियाँ थीं। कम शब्दों में बहुत ज्यादा व्यक्त करती हुई पंक्तियाँ। बाद में मैंने यह भी जाना था कि वे उन लोगों में आती हैं जो अपने आपको अच्छी तरह व्यक्त करना चाहते हैं। जिनके साथ भाषा की सीमाओं का ध्यान बना रहता है। जो बोलने और चुप रहने के बीच सन्तुलन बनाये रखते हैं। साल के आखिरी दिनों तक आते-आते मैं अपनी खाली शामों को उनके घर पर बिताने लगा। मैं शाम की प्रतीक्षा करता। मैं बस की प्रतीक्षा करता। मैं उनके घर के आ जाने की प्रतीक्षा करता। पहली बार ही मेरे अपने जीवन में प्रतीक्षा ने ऐसी जगह पायी थी और मैं प्रतीक्षा को, प्रतीक्षा, की पीड़ा को पहचान रहा था। एकदम शुरुआत के दिनों में उनके साथ अपने संवादों के वक्त मेरे मन में एक तरह का संकोच, एक तरह का सन्ताप रहा करता था।
ऐसा शायद यह जानकार भी होता रहा होगा कि उनके तलाकशुदा होने के बारे में मैंने स्कूल के अध्यापकों से सुन रखा था। वे उम्र में मुझसे चार-पाँच बरस बड़ी थीं और उन्होंने बहुत कुछ देखा था और जिया था। उनके जीवन के शुरुआत के सत्ताइस बरस गाँधी जी के भक्तों के बीच बीते थे और उन भक्तों में उनके माता-पिता शामिल थे। जब उनके पिता ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर अपनी किताब तैयार कर रहे थे तब अपने पिता के साथ गाँव दर गाँव घूमती रहती थीं। बहुत कम उम्र में उन्होंने गाँव की गरीबी को बहुत करीब से देखा था।
हम दोनों उनकी बैठक में देर-देर तक न जाने कैसे कैसे विषयों पर कितनी-कितनी बातें करते रहते। उन शामों में ही मैंने संवाद को काम की तरह जाना था। उनकी बातों में समझ में आता रहता कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, समझा और सोचा है। वे धीरे-धीरे और धीमी आवाज में बोलती थीं और बोलने से ज्यादा सुना करती थीं। मैं आज सोचता हूँ कि मैं उन दिनों में उन सब विषयों पर क्या-क्या बोलता रहा होऊँगा जिन पर आज भी, अपनी पचपन बरस की उम्र में थोड़ी सी गम्भीरता के साथ नहीं बोल सकता हूँ। पर मुझे याद नहीं आता है कि कभी भी उन्होंने मुझे मेरे कम जानने, गलत जानने का थोड़ा-सा भी आभास अपनी तरफ से दिया था।
उनसे पहचान के बाद मेरा वक्त सहजता से बीतने लगा। मेरे लिए उस छोटे शहर के दिन सहनीय होने लगे। किसी गहरी पहचान से जन्म लेने वाली एक निजी दुनिया मेरे भीतर पलने और बढ़ने लगी। उस उम्र में यह सब सुख का आना था और सन्ताप का जाना। वे कभी-कभी अपने खाली वक्त में मेरे स्कूल में चली आतीं और मेरा पीरियड न होने पर मैं उनके साथ पड़ोस के रेस्तरां में चला जाता। यह वह समय था जब उस शहर में गर्मियों की शुरुआत की धूल उड़ने लगी थी, हवाएँ चलने लगी थीं और पेड़ों से पत्ते झरने लगे थे। अब मैं शहर की सड़कों, पहाड़ियों पेड़ों, इमारतों और गलियों से जुड़ने लगा। उनका मकान गली के अन्तिम सिरे पर था और उसके सामने गुलमोहर का पेड़।
गर्मियाँ आयीं और हम दोनों के ही स्कूल सुबह लगने लगे। परीक्षाएँ करीब खड़ी थीं और स्कूल में ज्यादा देर नहीं रहना पड़ता था। मैं स्कूल का अपना पूरा काम करता और दुपहर में वहाँ से निकल जाता। यह कुछ अध्यापकों को अखरने लगा। उनमें वे ही अध्यापक थे जिन्हें माँ ने मेरी देखभाल के लिए कहा था। उनकी शिकायतों का सिलसिला कुछ इतना बड़ा कि उनमें से दो-तीन लोग एक दिन मेरे घर पर ही आ गये। मुझे उनका घर पर आना नहीं, उस लड़की के बारे में अनाप-शनाप बातें करना अच्छा नहीं लगा। वे तीनों बूढ़े हो रहे थे लेकिन उनकी समझ और संवेदना का स्तर उनकी उम्र को शोभा नहीं देता था। मैं उन लोगों की बातों को सुनता रहा। मैं आज सोचता हूँ कि मुझे उन लोगों की घटिया और घिनौनी बातों से अपनी असहमति को तभी व्यक्त करना था। तब मैं ऐसा कर लेता तो बाद के दिनों में मेरे साथ वह सब घटता ही नहीं।
मार्च के एक रविवार की दुपहर में, होली, के करीब खड़े एक दिन को, हम लोग उनके इलाके के एक पब्लिक पार्क में गये थे, मैंने पार्क के गेट से उनको उनकी बिटिया और नौकरानी को रिक्शे से उतरते हुए देखा था। उनकी गोद में बिटिया थी और नौकरानी के हाथों में एक बड़ा-सा थैला और चटाई। बरसों पुराने बरगद की छाया में हम लोगों ने अपना डेरा डाला। हमने अपना दुपहर का भोजन वहीं किया था। और बाद में नौकरानी और बिटिया आपस में खेलने लगे थे और हम दोनों ने अपने लिए शतरंज की बाजी बिछायी थी। गर्मियों की शुरुआत की दुपहरों में, किसी बरसों पुराने पेड़ के नीचे, एक लड़की के साथ शतरंज खेलते रहना। वह गहरी तसल्ली का वक्त था। मेरी तकदीर से बाहर निकलती तसल्ली। मैं अपनी इस तकदीर से, अपनी उस तसल्ली से कभी भी अलग न होने के स्वप्न को साथ लिए हुए अपनी अनाड़ी चालों को चल रहा था। तब मैं कहाँ जानता था कि तकदीर की अपनी चालें होती हैं, अपना चक्र। भाग्य का भँवर। जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
हमारे आस पास बरगद के सूखे पत्ते झरते रहे। हमारे आस-पास कितना कुछ झर रहा था कितना कुछ घट रहा था। उन्होंने मार्च के आकाश की तरफ देखा और किसी पक्षी को देखकर कहा था-
‘‘हम छुट्टियों में नागझिरा चलेंगे...वहाँ छोटी सी सैक्टयूरी है...उसके करीब ही तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती भी है...।’’
‘‘रिजल्ट के बाद मैं घर जाऊँगा।’’
‘‘मैं तो भूल ही गयी...।’’
‘‘आप कुछ कह रही थीं।’’
‘‘क्या आप मेरी बात सुनेंगे।’’
‘‘आप पहले कहिये तो सही...।’’
‘‘आप अपनी छुट्टियाँ यहीं क्यों नहीं बिताते....माँ को यहीं बुलाया जा सकता है....मेरे घर में दो कमरे खाली रहते हैं.....आपकी माँ मेरे यहाँ भी रह सकती हैं...’’
‘‘इससे आपको तकलीफ नहीं होगी।’’
‘‘आपके लिए यह सब करना अच्छा लगेगा...।’’
तब मैंने उनकी आँखों में उस चीज की चमक को देखा था जो जीवन में चमत्कार की तरह उतरती है। सृष्टि का अपना स्वप्न जो उसके बच्चों की आँखों में उतरता है और किसी के लिए गर्मियों की एक साधारण-सी दुपहर, अपने आखिरी दिन तक के लिए अविस्मरणीय हो जाती है। क्या मैं उस दुपहर के एक भी डिटेल को कभी भी भूल सकूँगा ? हमारे सामने शतरंज के मोहरे खड़े थे। आकाश साफ था और बीच-बीच में कोई अकेला परिन्दा या परिन्दों का ग्रुप हमारे ऊपर से निकल जाता था। हम शाम की शुरुआत होने तक उस बरगद की छाया में बैठे रहे थे। बतियाते रहे थे। होली के पड़ोस की उस दुपहर में, बूढ़े बरगद की घनी और शान्त छाया में, हमारे बीच वह चीज चमकी थी जिसे हम दोनों ही बना रहे थे। उस चीज का बनना, उस चीज का गाढ़ा हो जाना तो मेरे लिए एकदम अप्रत्याशित अनुभव नहीं होता रहा था। अपनी तीस बरस की उम्र में मैंने पहली बार किसी के लिए अपने भीतर ऐसा कुछ, इतना कुछ बनते हुए, पलते हुए देखा था।
उस वक्त मैं इस बात को पहचान रहा था कि प्रेम किस तरह हमारे भीतर अपनी जगह बनाता है। हमारे भीतर बहने लगता है और हमें बहाने लगता है। उन दिनों में ही पहली और आखिरी बार मैंने ढाई अक्षर की महिमा और मर्म को महसूस किया था।
दूसरे दिन मैं स्कूल न जा सका। मैंने स्कूल में अपने अस्वस्थ होने के समाचार को फोन पर बताया और मुझे लगा कि प्रिंसिपल मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मुझे उनके भरोसा न करने से बुरा लगा। मैंने पहली बार इस तरह अचानक छुट्टी ली थी और वह भी पहले से सूचना देते हुए, उसके लिए खेद व्यक्त करते हुए। पर मैं स्कूल के बारे में, नहीं, अपने बसने वाले संसार के बारे में सोचना चाहता था। मैं सोचना नहीं, जीना चाहता था। उस सुबह के पहले की दुपहर जैसा जीवन जिसमें मैंने मटर पुलाव के बाद गाजर का हलवा खाया था। मैंने सरसराती घास को छुआ था। आसमान की तरफ मुँह करके लेटा था और उन आँखों को देखा था जिसमें जीवन अपनी जीवन्तता और जादू के साथ पल रहा था। मैं उस जीवन, उस जीवन के स्रोत और सौन्दर्य के पास एक और बार लौटना चाह रहा था और बस में बैठकर मैं सुबह-सुबह ही उनके घर की तरफ निकला था।
मैंने बेल बजायी। दरवाजा खुलने में थोड़ी देर लगी। दरवाजे के खुलने पर पता चला कि वे नहा रही थीं। सुबह-सुबह और पहले से बताये बिना आने का संकोच मेरे साथ था। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा मेरे हाथ में अखबार दिया और भीतर चली गयीं। उनके कैलेण्डर में साइबेरिया के सारस उड़ रहे थे। मुझे याद आया कि कल ही उन्होंने करीब की सैंक्टयूरी का जिक्र किया था। वहीं बैठे-बैठे मैंने सोचा कि किसी दिन मैं उनके साथ भरतपुर जाऊँगा लेकिन तब तक मुझे क्या पता था कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा कि मैं उनके साथ फिर कभी भी और कहीं भी बाहर नहीं निकल सकूँगा।
वे चाय की ट्रे के साथ लौटीं। किसी ट्रेन के शहर से निकलने की आवाज आने लगी। ट्रेन की आवाज से ही शायद दूसरे कमरे में सोती उनकी बच्ची जागी होगी। वे वहाँ गयीं और उसे दुबारा सुलाकर लौट आयीं। वे बेंत की कुर्सी पर बैठे हुए अपने बालों को सुखाने लगीं। मैं उनके घने और काले बालों पर चलती उनकी अँगुलियों को देखता रहा।
‘‘कल आपको बुरा तो नहीं लगा,’’ उन्होंने पूछा।
‘‘क्यों...ऐसी क्या बात हुई,’’ मैं चौंका था।
‘‘मुझे आपसे यहीं रहने का कहना नहीं चाहिए था...आप क्या सोचेंगे....आपकी माँ को कैसा लगेगा....।’’
‘‘मुझे आपका कहना अच्छा लगा...माँ का मुझ पर हमेशा विश्वास रहा है...वे मुझे जानती हैं...हम दोनों ने एक-दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाया है...’’
‘‘मैं भी आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहती...’’
‘‘लेकिन आपने छिपाया है...’’
‘‘मैंने कहा कि मैं छिपाना नहीं चाहती...ऐसी बातें हो सकती हैं जिन पर आपसे बातचीत नहीं हुई होगी लेकिन ऐसा कुछ छिपाने का इरादा मैं नहीं रखती हूँ....’’
‘‘खैर छोड़िए....मैंने ऐसे ही कह दिया...शायद आपको अच्छा नहीं लगा होगा।’’
‘‘अब बात निकल गयी है तो उसे पूरी करनी चाहिए....मैंने आपसे क्या छिपाया है...’’
उनके पूछने में कुछ था कि मुझे रुक जाना चाहिए था। मैं उस पीड़ा को उनके सामने, सुबह के उजाले में ले आने के लिए तैयार होने लगा। मैं अपने मन को साफ कर लेना चाहता था। मुझे उन अध्यापकों की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था लेकिन उनकी बातें आँख की किरकिरी की तरह मुझे कभी-कभी तकलीफ जरूर देती रही थीं। उनके चेहरे से लगा कि वे वहाँ नहीं हैं, वे कहीं जा रही हैं या कहीं से लौट रही हैं। तभी ऊपर से प्लेन के गुजरने की आवाज आयी और वे उसे देखने बाहर निकल गयीं। लौटने पर वे खुश थीं और मैं थोड़ा-सा बेचैन। उन्होंने हँसते हुए कहा-
‘‘क्या आप डर रहे हैं...मैं आपको बहुत मानती हूँ...मुझे आप पर भरोसा है...आपके मन में कुछ है तो आपको कहना चाहिए...’’
‘‘क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ।’’
‘‘ऑफकोर्स....पर यह सवाल तो आपको खुद से करना चाहिए।’’
‘‘मैंने सुना है कि शादी के बाद आपका किसी से अफेसर था...वही आपके तलाक का कारण बना...आपके पति आप पर शक करते थे।’’
‘‘यह सच है....मेरे पति मुझ पर शक करने लगे थे...पर मेरे अफेयर की बात सच नहीं है....’’
‘‘तब वे लोग ऐसी अफवाहें क्यों उड़ाते हैं !’’
‘‘यह तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए।’’
‘‘उन लोगों ने ही मुझे बहुत कुछ बताया है...बार-बार बताया है..।’’
‘‘यह सब आपने कब सुना था ?’’
‘‘बहुत पहले...आप उस दिन मेरे स्कूल आयी थीं...आपके जाने के बाद वे लोग आपकी बदनामी करते रहे थे...।’’
‘‘आपको मुझे यह सब पहले ही बताना चाहिए था...।’’
‘‘इससे क्या फर्क पड़ता है ?’’
‘‘मुझे पड़ता है....मैं आप पर विश्वास करती थी...।’’
‘‘तो अब ऐसा क्या हो गया है ?’’
‘‘आप भी वैसे ही निकले...पर आपने यह अच्छा किया कि अपने मन की बात कह डाली...इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी....’’
‘‘आप मुझे गलत समझ रही हैं।’’
‘‘मैं आपको गलत समझ रही थी...’’
उसके बाद मैं उन सब बातों को दुहराने लगा जिन्हें मैंने अपने स्कूल के अध्यापकों से सुना था। मैं भटकने लगा। मैं भूलने लगा। मैं बहता गया। वे चुपचाप सुनती रहीं। वे शायद अपने आपको बचाना ही नहीं चाह रही थीं। मेरी चढ़ती-उतरती आवाजों से बच्ची जागी होगी। उनकी बिटिया रो रही थी। वे उसके पास गयीं। मैंने उठते हुए कहा-
‘‘मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ।’’
‘‘अभी मत आइएगा...मुझे बाहर जाना है...।’’
‘‘मुझे आपसे कुछ कहना है...वह मेरे लिए बहुत जरूरी है।’’
‘‘अभी आपका मन अशान्त है...फिर मैं इन बातों को सुनती रही हूँ....मैं आपको सन्देह को दूर भी नहीं कर सकूँगी...’’
‘‘लेकिन मैं आप पर शक कहाँ कर रहा हूँ।’’
‘‘आप विश्वास भी कहाँ कर रहे हैं !’’
‘‘मैं सिर्फ जानना चाहता था कि सच क्या है...’’
‘‘ऐसा था तो आप मुझसे सीधे ही पूछ लेते....मैं आपको सब कुछ बताती...खैर...’’
‘‘अब क्या हो गया है...जो सच है उसे अब भी बताया जा सकता है।’’
‘‘अब आपको बताने का मन नहीं हो रहा है...शायद फिर कभी बता पाऊँगी...लेकिन अब इन बातों का अर्थ ही क्या रहेगा....’’
‘‘मैं अभी सुनना चाहता हूँ, मेरे लिए वह सब जरूरी है...’’
‘‘इस वक्त मुझे माफ करना...बिटिया उठने ही वाली है...मुझे जाना भी है...’’
उनके घर से लौटते वक्त वह शहर कुछ ज्यादा ही पराया महसूस होने लगा। उस शहर का वह तालाब भी मन में नहीं उतरा जहाँ उनसे पहचान के पहले की शामों को मैं बिताया करता था। तालाब की सीढ़ियों से तालाब ही नहीं, पड़ोस का पुराना मन्दिर, वहाँ पर आ रहे लोग, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पुजारी, खेलते हुए बच्चे, लौटते हुए परिन्दे और ऐसी कितनी ही चीजों को मैं उन दिनों में देखा करता था। पर उस सुबह वहाँ की पहचान-सी परिचित चीजें भी परायी जान पड़ रही थीं। उनके घर से इस तरह लौटना अपनी तरफ भी लौटना रहा। अपने उन कुछ महीनों में जो मैंने उनके साथ बिताये थे। मुझे सुबह लगा था कि अब उनके साथ जितना कुछ बीताना मेरे भाग्य में लिखा था वह सब बीत चुका है। समय बीतता जाता है। बहता जाता है। इसे मैंने पहली बार तीस बरस की उम्र में, उस पुराने और पराये शहर में महसूस किया था।
एकदम शुरुआत के दिनों में, छोटे शहर की बारिश में समय बीतता ही नहीं था। हमारा स्कूल दुपहर में लगता। मुझे तीन-चार पीरियड पढ़ाना पड़ता। मैं इस प्रसिद्ध स्कूल में आया-आया ही था और प्रिंसिपल मुझ पर बहुत भरोसा नहीं रखते थे। मैं सुबह खाली ही रहता और दुपहर में चार बजे के आसपास खाली हो जाता। तालाब के किनारे मन नहीं लगता तो कुम्हारों के इलाके में चला जाता और वहाँ के मन्दिर की सीढ़ियों, पर बैठा हुआ, बूढ़े हो चले कुम्हारों की बातें सुनता रहता। कुम्हारों के बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। तब तक पुस्तकों में मन लगना शुरू नहीं हुआ था। घर की याद आती रहती और नौकरी से नफरत होती रहती और जिन्दगी से शिकायतें।
बड़ी बहनों की चिट्ठियाँ आती रहतीं और वे दोनों ही मुझे आगे की पढ़ाई की याद दिलाती रहतीं। उन दोनों ने ही पिता के अध्यापक होने की जीवन को करीब से देखा था और वे घर में एक और अध्यापक होने नहीं देना चाहती थीं। मैं बीच-बीच में पढ़ाई के लिए अपना मन बनाता लेकिन उस मन को भरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बारिश के वे दिन, पराये शहर की वे शामें मन को मरा हुआ महसूस करने, मन को मरता हुआ देखने की शामें थीं। मरे हुए मन के मनहूस दिन। जब न मन मौसम से जुड़ता था और न ही मन्दिर के उस परिवेश से जहाँ हमेशा चहल-पहल बनी रहती थी। अब बरसों बाद जब मैं अपने मन को थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ तब मेरे उन दिनों के मन के लिए मुझमें ममत्व जाग पड़ता है। एक तरह की ममतामयी मार्मिकता उस मन के लिए जन्मती है जो मन्दिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मुरझाता रहता था, मरता रहता था।
स्कूल में मैं सबसे कम उम्र का था और ज्यादातर अध्यापक मुझे अनाड़ी समझते थे। कोई-कोई तो मुझे बालों को सँवारने के लिए, कपड़ों को ठीक तरह से प्रेम करने के लिए कहने में भी नहीं हिचकता था। ये वे लोग थे जिन्हें माँ मेरी देखभाल करने के लिए पत्र लिखा करती थी। बहुत पहले ये अध्यापक पिता के साथ किसी शहर में पढ़ाते थे। वे मुझे तालाब के किनारे शाम न गुजारने की सलाहें देते। वे मुझे कुम्हारों की गरीब और गलीज बस्ती में जाने के लिए रोकते। वे मुझे छात्रों से ज्यादा बातें करने के लिए मना करते और इस तरह वे मेरी हर उस बात से असहमत जान पड़ते थे जो मैं अपने मन को मनाने के लिए किया करता था। मैं उनके साथ अपनी शामें गुजार नहीं सकता था और वे यही चाहते थे कि मैं हमेशा उनकी निगरानी में रहूँ या कम से कम उन्हें इन अहसासों में रखूँ कि वे मेरे लोकल गार्जियन हैं। मैं तालाब के किनारे ही अपनी खाली और अकेली शामें गुजारा करता था और मैं कुम्हारों की बस्ती में भी जाया करता था लेकिन मैं अपने स्कूल के अध्यापकों की बातें इत्मीनान और ध्यान से सुना करता था।
बारिश बीत रही थी। बारिश में ही चन्द्रमा पर पहली बार आदमी उतरा था। फिर चन्द्रमा से आये पत्थरों को उस शहर में भी लाया गया जहाँ मैं उन दिनों विज्ञान पढ़ा रहा था। मुझे छात्रों के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की उस लाल इमारत में जाना पड़ा जहाँ पर उन चन्द्रमा के पत्थरों को लोगों के देखने के लिए रखा गया था। उस इमारत के ही हाल में नील आर्मस्ट्रांग की बड़ी-सी तस्वीर के करीब मैं उनसे पहली बार मिला था। वे अपने स्कूल की छात्राओं के साथ वहाँ आयी थीं। मैं बरसों बाद भी इंस्टीट्यूट की दीवार के करीब खड़ी उस युवा लड़की की एक-एक चीज को याद कर सकता हूँ। सर्दियों की उस दुपहर में मैंने नहीं जाना था कि उस युवा लड़की के साथ-साथ में मेरे छोटे शहर में बीते कुछ दिन मेरे अपने जीवन के इतने निर्णायक और अविस्मरणीय दिन रहेंगे कि तीस बरसों के बाद भी उस स्त्री के बारे में बीच बीच में सोचता रहूँगा जिसके सान्निध्य में मैंने अपनी उम्र के तीसवें बरस के कुछ दिन बिताये थे।
अक्टूबर की एक शाम मैं पहली बार उनके घर गया था। उनके घर जाते वक्त बस एक पुल को पार करती थी जिसके नीचे शहर का रेलवे स्टेशन खड़ा रहता। बस की खिड़की से पटरियाँ, प्लेटफॉर्म रेलगाड़ियाँ, यात्री और वे इमारतें नजर आतीं जो स्टेशनों पर रहती हैं। वह स्टेशन भी अंग्रेजों के जमाने में बसा था और उसकी इमारतों में कभी अंग्रेजों के उस शहर में होने के संकेत मिलते थे। उनका घर विक्टोरियन शैली में बना हुआ। वे उस पीले मकान में अपनी छः बरस की बिटिया और अपनी नौकरानी के साथ रहती थीं। उनकी बिटिया जन्म से ही बीमार रहती आयी थी और उसकी देह और दिमाग का विकास धीरे-धीरे हो रहा था। मेरे पहली बार उनके घर जाने पर वे नहीं मिली थीं। वे पुल के पार कहीं संगीत सीखने के लिए जाया करती थीं। उनकी नौकरानी ने मुझे बिठाया था। चाय पिलायी थी। मैं उनके लिए छोटा-सा नोट रखकर लौट आया था।
दीवाली की छुट्टी में मैं अपने घर चला गया। लौटने पर स्टाफरूम में मेरे लिए जो चिट्ठियाँ थीं उनमें एक ग्रीटिंग कार्ड उनका भी था। ग्रीटिंग कार्ड के एक हिस्से में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता को काली स्याही के फाउण्टेन पेन से लिखा गया था। कविता के पड़ोस में कुछ आत्मीय पंक्तियाँ थीं। कम शब्दों में बहुत ज्यादा व्यक्त करती हुई पंक्तियाँ। बाद में मैंने यह भी जाना था कि वे उन लोगों में आती हैं जो अपने आपको अच्छी तरह व्यक्त करना चाहते हैं। जिनके साथ भाषा की सीमाओं का ध्यान बना रहता है। जो बोलने और चुप रहने के बीच सन्तुलन बनाये रखते हैं। साल के आखिरी दिनों तक आते-आते मैं अपनी खाली शामों को उनके घर पर बिताने लगा। मैं शाम की प्रतीक्षा करता। मैं बस की प्रतीक्षा करता। मैं उनके घर के आ जाने की प्रतीक्षा करता। पहली बार ही मेरे अपने जीवन में प्रतीक्षा ने ऐसी जगह पायी थी और मैं प्रतीक्षा को, प्रतीक्षा, की पीड़ा को पहचान रहा था। एकदम शुरुआत के दिनों में उनके साथ अपने संवादों के वक्त मेरे मन में एक तरह का संकोच, एक तरह का सन्ताप रहा करता था।
ऐसा शायद यह जानकार भी होता रहा होगा कि उनके तलाकशुदा होने के बारे में मैंने स्कूल के अध्यापकों से सुन रखा था। वे उम्र में मुझसे चार-पाँच बरस बड़ी थीं और उन्होंने बहुत कुछ देखा था और जिया था। उनके जीवन के शुरुआत के सत्ताइस बरस गाँधी जी के भक्तों के बीच बीते थे और उन भक्तों में उनके माता-पिता शामिल थे। जब उनके पिता ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर अपनी किताब तैयार कर रहे थे तब अपने पिता के साथ गाँव दर गाँव घूमती रहती थीं। बहुत कम उम्र में उन्होंने गाँव की गरीबी को बहुत करीब से देखा था।
हम दोनों उनकी बैठक में देर-देर तक न जाने कैसे कैसे विषयों पर कितनी-कितनी बातें करते रहते। उन शामों में ही मैंने संवाद को काम की तरह जाना था। उनकी बातों में समझ में आता रहता कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, समझा और सोचा है। वे धीरे-धीरे और धीमी आवाज में बोलती थीं और बोलने से ज्यादा सुना करती थीं। मैं आज सोचता हूँ कि मैं उन दिनों में उन सब विषयों पर क्या-क्या बोलता रहा होऊँगा जिन पर आज भी, अपनी पचपन बरस की उम्र में थोड़ी सी गम्भीरता के साथ नहीं बोल सकता हूँ। पर मुझे याद नहीं आता है कि कभी भी उन्होंने मुझे मेरे कम जानने, गलत जानने का थोड़ा-सा भी आभास अपनी तरफ से दिया था।
उनसे पहचान के बाद मेरा वक्त सहजता से बीतने लगा। मेरे लिए उस छोटे शहर के दिन सहनीय होने लगे। किसी गहरी पहचान से जन्म लेने वाली एक निजी दुनिया मेरे भीतर पलने और बढ़ने लगी। उस उम्र में यह सब सुख का आना था और सन्ताप का जाना। वे कभी-कभी अपने खाली वक्त में मेरे स्कूल में चली आतीं और मेरा पीरियड न होने पर मैं उनके साथ पड़ोस के रेस्तरां में चला जाता। यह वह समय था जब उस शहर में गर्मियों की शुरुआत की धूल उड़ने लगी थी, हवाएँ चलने लगी थीं और पेड़ों से पत्ते झरने लगे थे। अब मैं शहर की सड़कों, पहाड़ियों पेड़ों, इमारतों और गलियों से जुड़ने लगा। उनका मकान गली के अन्तिम सिरे पर था और उसके सामने गुलमोहर का पेड़।
गर्मियाँ आयीं और हम दोनों के ही स्कूल सुबह लगने लगे। परीक्षाएँ करीब खड़ी थीं और स्कूल में ज्यादा देर नहीं रहना पड़ता था। मैं स्कूल का अपना पूरा काम करता और दुपहर में वहाँ से निकल जाता। यह कुछ अध्यापकों को अखरने लगा। उनमें वे ही अध्यापक थे जिन्हें माँ ने मेरी देखभाल के लिए कहा था। उनकी शिकायतों का सिलसिला कुछ इतना बड़ा कि उनमें से दो-तीन लोग एक दिन मेरे घर पर ही आ गये। मुझे उनका घर पर आना नहीं, उस लड़की के बारे में अनाप-शनाप बातें करना अच्छा नहीं लगा। वे तीनों बूढ़े हो रहे थे लेकिन उनकी समझ और संवेदना का स्तर उनकी उम्र को शोभा नहीं देता था। मैं उन लोगों की बातों को सुनता रहा। मैं आज सोचता हूँ कि मुझे उन लोगों की घटिया और घिनौनी बातों से अपनी असहमति को तभी व्यक्त करना था। तब मैं ऐसा कर लेता तो बाद के दिनों में मेरे साथ वह सब घटता ही नहीं।
मार्च के एक रविवार की दुपहर में, होली, के करीब खड़े एक दिन को, हम लोग उनके इलाके के एक पब्लिक पार्क में गये थे, मैंने पार्क के गेट से उनको उनकी बिटिया और नौकरानी को रिक्शे से उतरते हुए देखा था। उनकी गोद में बिटिया थी और नौकरानी के हाथों में एक बड़ा-सा थैला और चटाई। बरसों पुराने बरगद की छाया में हम लोगों ने अपना डेरा डाला। हमने अपना दुपहर का भोजन वहीं किया था। और बाद में नौकरानी और बिटिया आपस में खेलने लगे थे और हम दोनों ने अपने लिए शतरंज की बाजी बिछायी थी। गर्मियों की शुरुआत की दुपहरों में, किसी बरसों पुराने पेड़ के नीचे, एक लड़की के साथ शतरंज खेलते रहना। वह गहरी तसल्ली का वक्त था। मेरी तकदीर से बाहर निकलती तसल्ली। मैं अपनी इस तकदीर से, अपनी उस तसल्ली से कभी भी अलग न होने के स्वप्न को साथ लिए हुए अपनी अनाड़ी चालों को चल रहा था। तब मैं कहाँ जानता था कि तकदीर की अपनी चालें होती हैं, अपना चक्र। भाग्य का भँवर। जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
हमारे आस पास बरगद के सूखे पत्ते झरते रहे। हमारे आस-पास कितना कुछ झर रहा था कितना कुछ घट रहा था। उन्होंने मार्च के आकाश की तरफ देखा और किसी पक्षी को देखकर कहा था-
‘‘हम छुट्टियों में नागझिरा चलेंगे...वहाँ छोटी सी सैक्टयूरी है...उसके करीब ही तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती भी है...।’’
‘‘रिजल्ट के बाद मैं घर जाऊँगा।’’
‘‘मैं तो भूल ही गयी...।’’
‘‘आप कुछ कह रही थीं।’’
‘‘क्या आप मेरी बात सुनेंगे।’’
‘‘आप पहले कहिये तो सही...।’’
‘‘आप अपनी छुट्टियाँ यहीं क्यों नहीं बिताते....माँ को यहीं बुलाया जा सकता है....मेरे घर में दो कमरे खाली रहते हैं.....आपकी माँ मेरे यहाँ भी रह सकती हैं...’’
‘‘इससे आपको तकलीफ नहीं होगी।’’
‘‘आपके लिए यह सब करना अच्छा लगेगा...।’’
तब मैंने उनकी आँखों में उस चीज की चमक को देखा था जो जीवन में चमत्कार की तरह उतरती है। सृष्टि का अपना स्वप्न जो उसके बच्चों की आँखों में उतरता है और किसी के लिए गर्मियों की एक साधारण-सी दुपहर, अपने आखिरी दिन तक के लिए अविस्मरणीय हो जाती है। क्या मैं उस दुपहर के एक भी डिटेल को कभी भी भूल सकूँगा ? हमारे सामने शतरंज के मोहरे खड़े थे। आकाश साफ था और बीच-बीच में कोई अकेला परिन्दा या परिन्दों का ग्रुप हमारे ऊपर से निकल जाता था। हम शाम की शुरुआत होने तक उस बरगद की छाया में बैठे रहे थे। बतियाते रहे थे। होली के पड़ोस की उस दुपहर में, बूढ़े बरगद की घनी और शान्त छाया में, हमारे बीच वह चीज चमकी थी जिसे हम दोनों ही बना रहे थे। उस चीज का बनना, उस चीज का गाढ़ा हो जाना तो मेरे लिए एकदम अप्रत्याशित अनुभव नहीं होता रहा था। अपनी तीस बरस की उम्र में मैंने पहली बार किसी के लिए अपने भीतर ऐसा कुछ, इतना कुछ बनते हुए, पलते हुए देखा था।
उस वक्त मैं इस बात को पहचान रहा था कि प्रेम किस तरह हमारे भीतर अपनी जगह बनाता है। हमारे भीतर बहने लगता है और हमें बहाने लगता है। उन दिनों में ही पहली और आखिरी बार मैंने ढाई अक्षर की महिमा और मर्म को महसूस किया था।
दूसरे दिन मैं स्कूल न जा सका। मैंने स्कूल में अपने अस्वस्थ होने के समाचार को फोन पर बताया और मुझे लगा कि प्रिंसिपल मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मुझे उनके भरोसा न करने से बुरा लगा। मैंने पहली बार इस तरह अचानक छुट्टी ली थी और वह भी पहले से सूचना देते हुए, उसके लिए खेद व्यक्त करते हुए। पर मैं स्कूल के बारे में, नहीं, अपने बसने वाले संसार के बारे में सोचना चाहता था। मैं सोचना नहीं, जीना चाहता था। उस सुबह के पहले की दुपहर जैसा जीवन जिसमें मैंने मटर पुलाव के बाद गाजर का हलवा खाया था। मैंने सरसराती घास को छुआ था। आसमान की तरफ मुँह करके लेटा था और उन आँखों को देखा था जिसमें जीवन अपनी जीवन्तता और जादू के साथ पल रहा था। मैं उस जीवन, उस जीवन के स्रोत और सौन्दर्य के पास एक और बार लौटना चाह रहा था और बस में बैठकर मैं सुबह-सुबह ही उनके घर की तरफ निकला था।
मैंने बेल बजायी। दरवाजा खुलने में थोड़ी देर लगी। दरवाजे के खुलने पर पता चला कि वे नहा रही थीं। सुबह-सुबह और पहले से बताये बिना आने का संकोच मेरे साथ था। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा मेरे हाथ में अखबार दिया और भीतर चली गयीं। उनके कैलेण्डर में साइबेरिया के सारस उड़ रहे थे। मुझे याद आया कि कल ही उन्होंने करीब की सैंक्टयूरी का जिक्र किया था। वहीं बैठे-बैठे मैंने सोचा कि किसी दिन मैं उनके साथ भरतपुर जाऊँगा लेकिन तब तक मुझे क्या पता था कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा कि मैं उनके साथ फिर कभी भी और कहीं भी बाहर नहीं निकल सकूँगा।
वे चाय की ट्रे के साथ लौटीं। किसी ट्रेन के शहर से निकलने की आवाज आने लगी। ट्रेन की आवाज से ही शायद दूसरे कमरे में सोती उनकी बच्ची जागी होगी। वे वहाँ गयीं और उसे दुबारा सुलाकर लौट आयीं। वे बेंत की कुर्सी पर बैठे हुए अपने बालों को सुखाने लगीं। मैं उनके घने और काले बालों पर चलती उनकी अँगुलियों को देखता रहा।
‘‘कल आपको बुरा तो नहीं लगा,’’ उन्होंने पूछा।
‘‘क्यों...ऐसी क्या बात हुई,’’ मैं चौंका था।
‘‘मुझे आपसे यहीं रहने का कहना नहीं चाहिए था...आप क्या सोचेंगे....आपकी माँ को कैसा लगेगा....।’’
‘‘मुझे आपका कहना अच्छा लगा...माँ का मुझ पर हमेशा विश्वास रहा है...वे मुझे जानती हैं...हम दोनों ने एक-दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाया है...’’
‘‘मैं भी आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहती...’’
‘‘लेकिन आपने छिपाया है...’’
‘‘मैंने कहा कि मैं छिपाना नहीं चाहती...ऐसी बातें हो सकती हैं जिन पर आपसे बातचीत नहीं हुई होगी लेकिन ऐसा कुछ छिपाने का इरादा मैं नहीं रखती हूँ....’’
‘‘खैर छोड़िए....मैंने ऐसे ही कह दिया...शायद आपको अच्छा नहीं लगा होगा।’’
‘‘अब बात निकल गयी है तो उसे पूरी करनी चाहिए....मैंने आपसे क्या छिपाया है...’’
उनके पूछने में कुछ था कि मुझे रुक जाना चाहिए था। मैं उस पीड़ा को उनके सामने, सुबह के उजाले में ले आने के लिए तैयार होने लगा। मैं अपने मन को साफ कर लेना चाहता था। मुझे उन अध्यापकों की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था लेकिन उनकी बातें आँख की किरकिरी की तरह मुझे कभी-कभी तकलीफ जरूर देती रही थीं। उनके चेहरे से लगा कि वे वहाँ नहीं हैं, वे कहीं जा रही हैं या कहीं से लौट रही हैं। तभी ऊपर से प्लेन के गुजरने की आवाज आयी और वे उसे देखने बाहर निकल गयीं। लौटने पर वे खुश थीं और मैं थोड़ा-सा बेचैन। उन्होंने हँसते हुए कहा-
‘‘क्या आप डर रहे हैं...मैं आपको बहुत मानती हूँ...मुझे आप पर भरोसा है...आपके मन में कुछ है तो आपको कहना चाहिए...’’
‘‘क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ।’’
‘‘ऑफकोर्स....पर यह सवाल तो आपको खुद से करना चाहिए।’’
‘‘मैंने सुना है कि शादी के बाद आपका किसी से अफेसर था...वही आपके तलाक का कारण बना...आपके पति आप पर शक करते थे।’’
‘‘यह सच है....मेरे पति मुझ पर शक करने लगे थे...पर मेरे अफेयर की बात सच नहीं है....’’
‘‘तब वे लोग ऐसी अफवाहें क्यों उड़ाते हैं !’’
‘‘यह तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए।’’
‘‘उन लोगों ने ही मुझे बहुत कुछ बताया है...बार-बार बताया है..।’’
‘‘यह सब आपने कब सुना था ?’’
‘‘बहुत पहले...आप उस दिन मेरे स्कूल आयी थीं...आपके जाने के बाद वे लोग आपकी बदनामी करते रहे थे...।’’
‘‘आपको मुझे यह सब पहले ही बताना चाहिए था...।’’
‘‘इससे क्या फर्क पड़ता है ?’’
‘‘मुझे पड़ता है....मैं आप पर विश्वास करती थी...।’’
‘‘तो अब ऐसा क्या हो गया है ?’’
‘‘आप भी वैसे ही निकले...पर आपने यह अच्छा किया कि अपने मन की बात कह डाली...इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी....’’
‘‘आप मुझे गलत समझ रही हैं।’’
‘‘मैं आपको गलत समझ रही थी...’’
उसके बाद मैं उन सब बातों को दुहराने लगा जिन्हें मैंने अपने स्कूल के अध्यापकों से सुना था। मैं भटकने लगा। मैं भूलने लगा। मैं बहता गया। वे चुपचाप सुनती रहीं। वे शायद अपने आपको बचाना ही नहीं चाह रही थीं। मेरी चढ़ती-उतरती आवाजों से बच्ची जागी होगी। उनकी बिटिया रो रही थी। वे उसके पास गयीं। मैंने उठते हुए कहा-
‘‘मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ।’’
‘‘अभी मत आइएगा...मुझे बाहर जाना है...।’’
‘‘मुझे आपसे कुछ कहना है...वह मेरे लिए बहुत जरूरी है।’’
‘‘अभी आपका मन अशान्त है...फिर मैं इन बातों को सुनती रही हूँ....मैं आपको सन्देह को दूर भी नहीं कर सकूँगी...’’
‘‘लेकिन मैं आप पर शक कहाँ कर रहा हूँ।’’
‘‘आप विश्वास भी कहाँ कर रहे हैं !’’
‘‘मैं सिर्फ जानना चाहता था कि सच क्या है...’’
‘‘ऐसा था तो आप मुझसे सीधे ही पूछ लेते....मैं आपको सब कुछ बताती...खैर...’’
‘‘अब क्या हो गया है...जो सच है उसे अब भी बताया जा सकता है।’’
‘‘अब आपको बताने का मन नहीं हो रहा है...शायद फिर कभी बता पाऊँगी...लेकिन अब इन बातों का अर्थ ही क्या रहेगा....’’
‘‘मैं अभी सुनना चाहता हूँ, मेरे लिए वह सब जरूरी है...’’
‘‘इस वक्त मुझे माफ करना...बिटिया उठने ही वाली है...मुझे जाना भी है...’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i