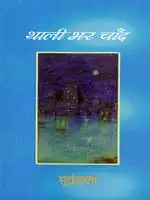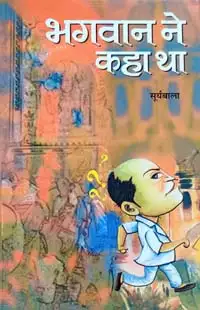|
कहानी संग्रह >> थाली भर चाँद थाली भर चाँदसूर्यबाला
|
295 पाठक हैं |
|||||||
अत्यन्त सरस, मार्मिक एवं जीवंत कहानियाँ जो पाठक को स्पंदित कर देती हैं....
Thali Bhar Chand
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कैसे जीते हैं लोग यहाँ ? उफ, कब उद्धार होगा सभ्यता से कटे, ऊँघते कस्बे के इन लोगों का ? सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद नहीं मालूम कि वे कितने गए-गुजरे, अहमक किस्म के लोग हैं और दुनिया कितनी-कितनी आगे बढ़ गई है। यहाँ औरतें मर्तबानों को धूप-छाँह में सरकाती, पापड़ों को उलटती-पलटती और बेटियों की कसी-कसी चोटियाँ गूँथती इतनी-इतनी दुर्लभ जिंदगी काट जाती हैं। उफ, अपना तो सोचकर भी दम घुटता है। इतनी-इतनी नेमत से मिली जिंदगी सिर्फ कुछ अदद मर्तबानों में भरकर सील कर दी जाए, तेल चुपड़ी चोटियों के साथ गूँथ दी जाए ! अपनी बिट्टा रानी भी बचपन में एक-दो बार ठुनकी तो थी लहरियादार लंबी चोटियों के लिए। तब समझाया बेटे ! तेरी मम्मी सिर्फ एक चूल्हे-चौकेवाली औरत तो है नहीं न; उसे कितनी गोष्ठियों, सेमिनारों, संस्थाओं की धुरी सँभालनी पड़ती है। वह सिर्फ तेरी चोटियाँ गूँथते तो जिंदगी नहीं बिता सकती। बिट्टा मान गई बाल कटने के बाद लच्छे-लच्छे देख हिलक के रोई जरूर तो क्या, एक ‘फाइव-स्टार’ थमा दिया, फुसल गई।
अत्यंत सरस, मार्मिक एवं जीवंत कहानियाँ, जो पाठकों को स्पंदित करेंगी और उनकी संवेदना को छू जाएँगी।
अत्यंत सरस, मार्मिक एवं जीवंत कहानियाँ, जो पाठकों को स्पंदित करेंगी और उनकी संवेदना को छू जाएँगी।
न किन्नी, न
एक शाम अचानक कैसे वे लोग याद आ गए, पता नहीं।
बीस-पच्चीस साल पहले हमारे मकान के एक हिस्से में रहनेवाले किराएदार, टूटी कमानीवाले चश्मे को काले धागे से बाँधे, एकदम चिपके गालोंवाली सड़क-चौराहे डाँव-डाँव डोलती बूढ़ी माँ, हमेशा झूठे ठाट बनाने का महत्त्वाकांक्षी थुलथुल-सा बेटा, औसत पत्नी और एक के बाद एक पैदा होते बच्चे।
उस परिवार में जलजला-सा आता, जब मौसीजी आतीं। बूढ़ी से कुछ ही वर्षों छोटी दूसरी बहन-स्वस्थ, संपन्न, ठसी चकरी-सी अपनी आयु से दस वर्ष कम दिखतीं-वैसी ही खुशमिजाज और फुरतीली, अपने हिसाब से स्मार्ट भी।
उस छोटी वय में पहली बार महसूस किया था कि पैसा आत्मविश्वास का किताब बड़ा स्रोत होता है।
बहरहाल, मौसीजी चली जातीं। उनकी छोड़ी हुई सौगातें रह जातीं। सबसे विद्रूप भरा दृश्य होता, जब बूढ़ी बहन छोटी बहन की छोड़ी गई ऊँची हीलवाली चप्पलें पहनकर खटर-पटर करती अपने लिए पान-तंबाकू लाने जाती होती।
तब बिलकुल नहीं जाना था कि यह चित्र मेरे अंदर फ्रीज होता चला जा रहा है और आज से बरसों-बरसों बाद किसी किन्नी-कथा की मूल संवेदना के रूप में पिघल उठेगा।
किन्नी कौन ? कहाँ की ? अब सबकुछ ही थोड़ी बता दूँगी !
मौसी आतीं तो घर रोशनी और रौनक से भर जाता। हम छज्जे-छज्जे चहकते फिरते। सबसे कहते-हमारी मौसी आ रही हैं, बिजनौरवाली मौसी। हमारे मौसाजी शक्कर की मिल में मैनेजर हैं। उनके पास मिल की जीप है, उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं; दो कुत्ते हैं और एक खरगोश भी। उनके दो बच्चे हैं-गगन और रोजी। गगन के पास बंदूक है चिड़िया मारने की। रोजी के पास बुलबुल तरंग-मास्टर आते हैं उसे सिखाने को।
मौसी खूब चिट्टी हैं, माँ जैसी धूमिल-धूमिल-सी नहीं और खूब हँसती-खिलखिलाती चुस्त-दुरुस्त सी रहती हैं, माँ जैसी सुस्त-सुस्त-सी नहीं।
रोजी को लेकर स्कूल जाती हूँ तो मेरा रुतबा बढ़ जाता है। सारी सहेलियाँ लट्टू हो जाती हैं उसकी स्कर्टों, सैंडिलों और नई-नई डिजाईन की क्लिपों पर। कैसी तो थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश मिलाकर चटर-पटर-सी बोलती है और आँखें गोल-गोल-सी घुमाती बेफिक्र, बिंदास चहकती रहती है।
जब तक मौसी रहती हैं, गगन और रोजी सारा घर सिरपे उठाए रहते हैं। अब इतने बड़े हो जाने पर भी गगन रोजी के बाल खींचकर या चुटकी काटकर भागता रहता है। रोजी चीखती हुई उसे दौड़ाती रहती है और मौसी अंदर-अंदर मगन होती हुई ऊपर-ऊपर खीझकर लाड़ से डाँटती हैं-
‘अरे, शरम करो शैतानों ! इन बच्चों को देखकर भी तुम्हें अकल नहीं आती। कैसे सीधे, बिना मुँह के-से हैं। जरा देखो किन्नी को, अभी कॉलेज से आए दस मिनट भी नहीं हुए और देखते-देखते फटाफट तुम लोगों की बिखेरी चीजें सँभाल दी, कपड़े तहा लिये और इधर चाय भी चढ़ा दी। ला तो बेटा, एक प्याला, जरा सुस्ती दूर हो।’ फिर चाय का घूँट भरती हुई अम्मा से कहतीं, दीदी ! इस बार मैं सचमुच रोजिया को यहीं छोड़ जाऊँगी तुम्हारे पास और किरण को अपने साथ ले जाऊँगी बिजनौर।’
और खुद ही अपने मजाक पर खुलकर हँस पड़तीं। यों अपने आप में सचमुच इससे बड़ा मजाक दूसरा नहीं हो सकता था और मौसी की तो वैसे भी आदत थी खूट चटपटी बातें करना और अपनी बात खत्म होने से पहले ही जोर से हँस पड़ना।
रंग तो करीब-करीब एक सा ही था दोनों बहनों का, लेकिन अम्मा दुबली फीकी-फीकी-सी लगतीं, जैसे ऊपर एक झाँईं-सी पड़ी हो-अभी नहीं, बाबूजी थे तब भी दूसरी तरफ मौसी एकदम ठसी चकरी सी ऊपर, से नीचे तक जैसे रंग रोगन पॉलिश से दमकती हुईं और चेहरे पर तो खासकर हमेशा एक पूर्ण परितृप्त भी लुनाई फैली रहती थी। अम्मा से पूरे पांच साल छोटी, पर देखने में तो एकदम बेटी ही लगतीं।
आज भी मैं मेज पर तार देखते ही किलक उठी-‘मौसी आ रही हैं !...कब आया तार ? रोजी, गगन भी आ रहे हैं या नहीं ?’
‘‘दोनों सफेद धारीवाली नीली चादरें धोकर फैला दूँ।’
‘बाँसवाले किताबों के रैक पर अँटी धूल साफ कर दूँ।’
‘कोनेवाली मेज की आधी प्लाई उखड़ गई है। ठहरो, इस फटीवाली हैंडलूम की चादर काटकर इस पर मेजपोश सिले देती हूँ।’
‘रसोई की अलमारियों पर अखबार बिछा दूँ।’
‘गुसलखाने की मोरी रगड़कर धो दूँ।’
और साड़ी का फेंटा कसकर तुरत-फुरत मोरचे पर जुट गई, क्योंकि भाभी तो अपने तीनों बच्चों की फ्रॉकों और पैंटों की उधड़ी सिलाई ही दुरुस्त करने भर को होतीं और अम्मा रसोई के डिब्बों में हाथ डाल-डालकर आधा किलो डालडा, एक किलो चीनी सूजी मैदा और चाय मसालों की सूची बनाने में।
दो-तीन दिनों में घर धो-रगड़कर साफ हो जाता, गुसलखाने में फिनाइल की बोतल रख दी जाती और भैया आधे दिन की छुट्टी लेकर स्टेशन पहुँच जाते।
आधे-पौने घंटे के अंदर ही चमकते सूटकेसों और रंग-बिरंगे बैगों, टोकरियों से लदी-फँसी मौसी आ जातीं। सारा घर आवाजों से चहचहा उठता। मौसी हम सबको बारी-बारी से बाँहों में भरतीं। भाभी के तीनों बच्चों को चिपटा-चिपटाकर प्यार करतीं और भाभी को पाँव छूने के लिए झुकने के साथ उठाकर बलाएँ लेने लगतीं।
भाभी हुलसती हुई जल्दी से रंगदार चाय, मठरी, सेव सजा देतीं और हमारी तंग-अँधेरी कोठरियों से हँसी के झरने फूट पड़ते।
अब इसके बाद हम सबों के चिर-प्रतीक्षित क्षण आता। मौसी सामानों से ही नहीं, सौगातों से भी लदी-फँदी आतीं। सबको अंदर-ही-अंदर इस बात की कितनी खलबली रहती है, यह मौसी भी खूब अच्छी तरह समझती थीं। इसलिए झटपट सूटकेस खोलकर सोत्साह जादुई-सी एक के बाद एक चीजें निकालने लगतीं-‘किन्नी, इधर आ, ये देख, ये रोजी ने तेरे लिए टाप्स और मैचिंग लॉकेट भेजे हैं और ये चार रूमालें। बहू, यह तुम्हारे पर्स है और ये मिंटू-चिंटू के लिए हेयर बैंड और क्लिपें...गुड्डू के लिए ये रंगीन पेंसिलों का सेट गगन ने भेजा है।’
लेकिन यह सब तो औपचारिक सौगातें होतीं। असली सौगातें तो इसके बाद निकलतीं मौसीके होल्डॉल से तीन-तीन, चार-चार जोड़ी पुरानी चप्पलें सैंड़िले-‘ये वाली मुझे पंजों पे कसे सी हैं; ये रोजी ने खरीदी तो बड़े चाव से, लेकिन अब मन भिटक गया उसका-जानती तो हो मूडी नंबर एक। इस वाली पे बस तू दो कीलें ठुकवा लेना। और इस वाली पे इसी रंग की सिलाई करवा लेना किसी अच्छे मोची से। किन्नी, मेरी इस नई-सी साड़ी पे रोजी रानी खोंच लगा आई ठीक सामने नीचे की तरफ, तू उलटी करके पहनेगी न तो बिलकुल पता नहीं चलेगा। और ये, इन दोनों की बस प्रिंट जरा हलकी हो आई है...इस मेरे बैग का हैंडल निकल गया है बस...अमर ! जरा ये बुश्शर्ट देख तो, मिल की वर्कशॉप का राऊंड लेते समय यह छींटा पड़ गया गंदे तेल का-मैंने कहा लिये चलती हूँ अमर जरा फिट करवा के पहन डालेगा। तेरा तो रंग भी गोरा है, फबेगी तुझ पर।’
इसी तरह-‘ये रोजी की नाइटी, ये स्वेटरों के बचे-खुचे ऊन मैंने सोचा, बहू गुणी है, काट छाँटकर चिंटू-नीटू की फ्रॉक बना देगी और थोड़ा और ऊन मिलाकर रंग बिरंगा प्यारा सा स्वेटर बन जाएगा, खूब खिलेगा इन पर। और हाँ, ये स्टील की दो छोटी प्लेटें और कटोरियाँ भी....दीवाली पर आई थीं न मिल में बँटने के लिए, मैंने चुपके से चार रख लीं। इन्हें कहाँ होश-हवास कि कितने आए, कितने गए, सारे दिन मिल भर के ही होते हैं।’
हाँ, मौसाजी को तो पूरे होशोहवास में बस दो बार देखा था-शायद बाबूजी की मौत पर-शायद भैया की शादी में, इससे कम जरूरी मौकों पर वे कभी पहुँच ही न पाए। दोनों बार एक प्लेन से आए और दूसरे प्लेन से वापस। जितनी देर रहे भी न सामने जाने की हिम्मत न बात करने का धड़का-सिर्फ सिर झुकाए।
‘मौसाजी, नाश्ता लग गया।’
या फिर-‘मौसाजी, बाथरूम खाली है।’
मौसाजी बहुत कम बोलते, जितना बोलते उसके भी शब्द-शब्द बड़प्पन और मातबरी के फ्रेम में जड़े-से होते। कभी हलके से मुसकराकर पढ़ाई-लिखाई के बारे में एकाध शब्द पूछ लेते तो हम सिर से पांव तक निहाल हो जाते।
लेकिन असली चौकड़ी तो हमारी मौसी के साथ ही जमती। हर आधे घंटे पर चाय की तलब और भाप छोड़ते प्यालों के साथ मौसी सारे समय कहाँ कहाँ के हँसी-लतीफे छोड़ती जातीं। मौसीजी के गुमाश्तों, कारकुनों से लेकर अपने शहर के एस.पी., डी.एम. की नकनकाती बीवियों तक के किस्सों की फुलझड़ियाँ।
नए-से-नए फैशन तक की बातें बड़े चाव से सुनती-सुनातीं और रस लेतीं। असल में रुतवा मौसाजी का बड़ा था, लेकिन शहर हमारा। और मिलें-फैक्टरियाँ तो वैसे भी शहरी आबादी से मीलों दूर, स्कूल-कॉलेज भी उतने अच्छे नहीं जितने हमारे शहर के तो फैशन की नई-से-नई जानकारी मुझसे ही लेतीं। यहाँ तक कि हाथों में प्लास्टिक के सादे इकरंगे कंगन या कानों में सिर्फ एक नन्हा कल्पर का मोती देखते ही।
‘अरे किन्नी, देखूँ तो जरा तेरे कंगन, लाख के होंगे ?’
‘नहीं, सादे प्लास्टिक के।’
‘और जरा कानों के टॉप्स तो दिखा।’
‘यहीं के चौक से खरीदे हैं।’
‘असल में तेरी पसंद बहुत बढ़िया है। जानती है, क्या तुझे सूट करेगा। चल, जरा आज बाजार ले चल, दो-चार पेयर रोजी के लिए खरीदवा दे।’
मैं मौसी के ना-ना कहने पर भी फौरन कानों के बुदे निकाल रोजी के लिए पैक कर देती। फिर बाजार ले जाकर मौसी और जो-जो चाहतीं, खरीदवा देती। मौसी हर चीज से पहले मेरी सलाह लेतीं कि फलाँ चीज उनपर, रोजी पर खिलेगी। या नहीं ? मेरी पसंद पर पूरा भरोसा था। मेरी पसंद की हमेशा दाद देतीं। मुझसे पसंद करवाकर ढेर सारे टॉप्स, पेंडैंट, अँगूठियाँ ले जातीं और उनमें से बहुत सी डिजाइनें सुनारो को दिखाकर सच्चे मोती, सोने में गढ़वा लेतीं। अगली बार जब आतीं तो मुझे दिखाकर पूछतीं, ‘देख किन्नी, कैसे लगे ये ? इमीटेशन में तो काली पड़ जाएँगी न ?’
मेरे मुँह से बेसाख्ता ‘वाह’ निकल जाता मौसी की पारखी दृष्टि पर।
उतनी उमर होने पर भी मौसी में हमेशा नई उमरवालियों-सी उमंग, उत्साह छलकता रहता।
आजकल जरूर मौसी को एक फिक्र सी हो गई है रोजी के मोटापे की। जब-जब टोकती रहती हैं उसे-‘ठूसे चली जा रही है गपागप भाभी के बनाए पकौड़े-मालपूए। शीशे में नजर डाली है खुद पर ! कैसी खुद भी फूलकर पकौड़े, मालपूए-सी हुई जा रही है। किन्नी, तू ही समझा न जरा इसे।’
लेकिन रोजी उसी बेफिक्री से एक और पूआ चुभलाती हुई खिलखिला देती, ‘‘साफ-साफ कहो न मम्मी, तुम्हें मेरी शादी की फिक्र ही सताए जा रही है न ! अरे, तुम बेकार घबराती हो। देखना, सब दौड़ते हुए शादी करेंगे। असल में आजकल सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा और मेरे शक्तिशाली साए में कोई भी पति भयरहित और निर्द्वंद्व जीवन जी सकता है, समझीं। मजाल है जो कोई उसकी ओर आँख उठाकर भी देखे। अरे, वो क्या, उसका बॉस भी मुझे देखकर दुम हिलाएगा। लाओ भाभी, एक और मालपूआ इसी बात पर।’
अम्मा धीमे से हँसती हुई समझातीं, कहाँ मोटी है बेचारी। जरा दोहरा शरीर है बस। तू बेकार इसके पीछे पड़ी रहती है। लड़के-बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं-और नहीं तो क्या इस किन्नी-सी सींक-सलाई ! मैं तो इसे मुटवाने की कोशिश में हार मान चुकी हूँ।’
सचमुच मैं रोजी से तीन साल बड़ी थी और बेहद दुबली, इतनी कि रोजी के सलवार-कुरते सब तीन-तीन, चार–चार सिलाइयों के बाद ही मुझे फिट आते। अपने तईं मैं उन्हें पूरी तरह काट-छाँटकर नया-सा कर डालती। फिर भी कॉलेज में लड़कियाँ देखते ही ठिठोली करतीं-‘रोजी ब्रांड !’ और मैं शरमाकर हँस देती।
माँ को क्या कहूँ, खुद मेरी भी तो यही हालत है। बहुत जोर से हँस-खिलखिला सकती ही नहीं। अपनी बात पूरे वजन और आत्मविश्वास से सबके बीच में कह सकती ही नहीं। इसलिए सही बात भी सुननेवाले के साथ-साथ खुद अपने आपको भी कच्ची, अधूरी, अनिश्चित सी लगती है; जबकि रोजी और मौसी एकदम घिसी-पिटी कहावतों और जुमलों को भी इतनी ठसक के साथ पेश करती हैं कि सुननेवाला फौरन उनकी गिरफ्त में आ जाता है।
इसी तरह अपने शादी-ब्याह या गुण-शऊर की बात चलने पर भी लाख कोशिशों के बावजूद पलकें जैसे मारे घबराहट और संकोच के यहाँ-वहाँ छुपने की ठौर तलाशने लगती हैं; लेकिन वहीं रोजी अपने लिए ऐसी कोई बात सुनते ही गोल-गोल आँखें चमकाती ठठाकर हँस पड़ती है। और उसे आँखें तरेरकर बरजती हुई मौसी भी उसी ठहाके में शामिल हो जाती हैं।
मौसी के जाते ही वे ठहाके थम जाते हैं। घर वापस श्मशान-सी खामोशी में साँय-साँय कर उठता है। माँ फैली-बिखरी चीजें समेटने लगती हैं। भाभी दो-तीन या चार दिनों की थकान उतारने खाट पर पसर जाती हैं और भाई मौसी की लाई ढीली कमीजों-पतलूनों की फिटिंग कराने के लिए पैसे माँगते हुए माँ से हुज्जत करने लगते हैं। सबको मालूम है, उन पैसों में से काट-कपट कर रूमाल या तौलिए में लपेटी एक दो बोतलें आएँगी। उनके बूते पर बैठक में भाई जैसे ही भाई के खस्ताहाल दोस्तों का जमावड़ा जुटेगा, जश्न मनेगा और एक तीखी मिठास के तहत कई सुस्त से हाथ किसी तरह हवा में लहराकर गिरते हुए एक से एक हवाई योजनाएँ बनाएँगे, हलके सुरूर के पंखों पर उड़ते हुए, कभी किसी साबुन की एजेंसी, कभी स्कूटर मरम्मत का गैरेज, कभी दर्दनाशक गोलियाँ या दंत-मंजन बनाने के नुस्खे की तजवीज, या ऐसा ही कुछ और।
ऐसे मौकों पर किताबें उठाकर मैं सीधी कटरेवाली चाची के पास पहुँच जाती और चाची बिना सिर उठाए सब्जी का रसा अंदाजतीं या पराँठे उतारती-उतारती ही कह देतीं, ‘कौन किन्नी ? चली जा, खाली है बैठक।’
चाचा का तो टाइम ही आठ से आठ है। इसीलिए आज चाची से पूछा भी नहीं, सिर्फ इत्तिला दे दी। ‘चाची, जाती हूँ बैठक में पढ़ने।’
कि चाची जल्दी से अँगीठी छोड़ आईं, किन्नी, बैठक तो खाली नहीं।’ वे फुसफुसाई सी बोली।
‘अरे वाह ! चाचा आज छुट्टी मार बैठे ?’
‘नहीं, मेरा भतीजा आया हुआ है, रिश्ते का।’
मेरी आवाज दयनीय हो उठी, ‘फिर क्या करूँ चाची ? मेरा तो कल पॉलिटिक्स का परचा है।’
‘क्या करूँ ?’ चाची खुद असमंजस में थीं, ‘वह भी पढ़ने ही आया है। आज ही नहीं, कुछ महीनों तक के लिए। दंगों की वजह से लड़कों का पूरा हॉस्टल खाली करा लिया गया है। मटरगश्ती करनेवालों को तो माँगी मुराद मिली, लेकिन ये बेचारे पढ़नेवालों को....’
‘क्या हुआ, बुआ ?’ दंगों का मारा खुद ही आन खड़ा हुआ, ‘कोई परेशानी है ?’
चाची जल्दी से बोलीं, ‘परेशानी नहीं, यह किन्नी है।’ सुधारा-‘किरन-और किन्नी, यह आकाश है।’
उसने सुधारा, ‘कुशा ! पढ़ने आई हैं आप ?’
‘जी..लेकिन ?’
‘तो जाइए, पढ़िए न।’
‘और आप-आपको भी तो पढ़ना है !’
‘हाँ-हाँ, मैं भी पढ़ूँगा।’
‘जी !’ मैं चौंकी।
‘जी हाँ, उधर दुछती पर।’ और मेरी लमहे पहले की घबराहट का मजा लेता हुआ हँस दिया।
‘नहीं-नहीं आप पढ़िए।’
‘आप भी।’
अब के चाची खिलखिलाईं, ‘अब ‘आप’ और ‘आपके’ फेर में मेरे पराँठे जले जा रहे हैं।’
चाची के जाते ही दोनों अपनी-अपनी जगह पढ़ने चले गए।
और मैं ठीक समय पर पढ़ाई खत्म कर सीधी गरदन, सधी चाल घर आ गई, बगैर किसी तरफ ताके-झाँके। मुझे सचमुच खबर नहीं थी कि मैं अपने आँचल में कस्तूरी का एक छोटा-सा टुकड़ा बाँधे चली आई हूँ।
चौथे दिन कॉलेज से लौटते हुए यों ही चाची दिख गईं, ‘सुन किन्नी।’
‘हाँ, चाची।’
‘कौन सी क्लास में है तू ?’
‘चाची !’ मैंने चिढ़ाया, ‘अब इसके बाद मेरा नाम भी पूछोगी क्या ’
चाची झेंप गईं, ‘नहीं रे, यों ही। मेरा मतलब है, बी.ए. प्रीवियस या फाइनल ?’
‘क्यों ? कहीं नौकरी लगवा रही हो मेरी ?’
‘अरे भई, कल यों ही तेरी बात चलने पर कुशा ने पूछा था तो मुझे बड़ी कोफ्त आई कि मुझे इतना भी नहीं मालूम।’
‘अच्छा, तो वो नौकरी लगवा रहे हैं ?’
अरे नहीं, वो बेचारा तो खुद ही दूध का जला है।’
‘च-च्च...तो गलती तुम्हारी है, इतना खौलता दूध काहे को पिलाया ? मारे लाड़ के, ऐं ?’
यह क्या मेरे अंदर छुपी कस्तूरी ही परिहास के तमाम रंगों में छिटकी पड़ रही थी ?
लेकिन चाची का ध्यान मेरे परिहास में जरा भी नहीं था। उसी अवसाद और आक्रोश में एक साथ डूबी-सी बोलीं, ‘कुशा की सात सौ की स्कॉलरशिप का मामला विश्वविद्यालय की ब्राह्मण-ठाकुर गुटबंदी की खटाई में फँसा पड़ा है। बेचारा न इधर का हो पा रहा है, न उधर का। आज तो खीजकर कह रहा था-चल रहा हूँ विश्वविद्यालय के फाटक पर रिक्शा खींचने या जूते गाँठने।’
‘ओह !’ मैं अपनी ऊल-जलूल वाचालता पर सचमुच लज्जित थी, ‘रिसर्च में खर्च भी तो काफी आता है ?’
‘खाली रिसर्च भर नहीं न-समूची घर गहस्थी-माँ-बहनों की पूरी-पूरी जिम्मेदारी..दो ही साल पहले पिता नहीं रहे न इसके।’
उस शाम सूरज के साथ एक सिंदूरी अवसाद घुलते-घुलते डूब रहा था और डूबने के बाद की निस्तब्धता एक उदास सहेली-सी लगी थी।
उस कस्तूरी से एक कुतूहल की खुशबू उड़ी थी-क्या बातें होंगी मुझे लेकर ? कैसे चर्चा चली होगी मेरी ? क्या कहा होगा चाची ने और कैसे पूछा होगा और किसी ने ? मुझे ‘किन्नी’ कहा होगा या ‘किरन’ ?
अब चिलचिलाती धूप में कॉलेज से जल्दी-जल्दी घर की ओर बढ़ते कदम अनायास चाची के घर के सामने से गुजरते हुए ठहरने-से लगते। आहिस्ते, बहुत आहिस्ते-आहिस्ते, थकान का छल, खुद अपने आप से !
‘अरे किन्नी, कहाँ भागी जाती है ? बैठ, चाय पी मेरे साथ।’
‘लेकिन मुझे तो भूख भी लगी है, चाची।’
‘मुझे भी।’ आँचल से बँधी कस्तूरी की गाँठ जैसे खुलकर बिखर पड़ी। बरुनियों की आड़ में दुबकी-सी मैं मुसकराई।
‘भला दो अनखातों को एक साथ भूख तो लगी-सुबह के पराँठे रखे हैं, वही लाती हूँ। चलेगा कि बनाऊँ कुछ ?’
‘चलेगा।’ दो आवाजें एक साथ सिहरकर उलझ लीं। फिर जल्दी से सँभलकर अलग-अलग हो लीं।
‘बस, मैं तो चला।’
‘अरे, क्या हुआ ? तू अपने अंदर कोई अलार्म घड़ी फिट किए रहता है क्या, जो खाते पीते भी घन्न से बजकर चौकन्न कर देती है तुझे ?’
सुनिए, आपकी लाइब्रेरी में पॉलिटिक्स की एक दो किताबें मिल सकती हैं ?’
‘होनी तो चाहिए, क्योंकि आजकल बिना पॉलिटिक्स पढ़े कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता।’
‘छोड़िए, आप नहीं समझेंगे।’ मैं आहत-सी हुई।
‘नहीं, शायद आप...! वह फीकी हँसी हँसा।
‘असल में मेरे कॉलेज में सिर्फ दो किताबें हैं, जो दोनों लेक्चरर्स के लिए बारी-बारी रिजर्व रहती हैं।’
‘आप दोनों किताबों के नाम लिखकर दे दीजिएगा। मैं तो नहीं, मेरा दोस्त जाता है आर्ट्स सेक्शन की लाइब्रेरी में।’
बीस-पच्चीस साल पहले हमारे मकान के एक हिस्से में रहनेवाले किराएदार, टूटी कमानीवाले चश्मे को काले धागे से बाँधे, एकदम चिपके गालोंवाली सड़क-चौराहे डाँव-डाँव डोलती बूढ़ी माँ, हमेशा झूठे ठाट बनाने का महत्त्वाकांक्षी थुलथुल-सा बेटा, औसत पत्नी और एक के बाद एक पैदा होते बच्चे।
उस परिवार में जलजला-सा आता, जब मौसीजी आतीं। बूढ़ी से कुछ ही वर्षों छोटी दूसरी बहन-स्वस्थ, संपन्न, ठसी चकरी-सी अपनी आयु से दस वर्ष कम दिखतीं-वैसी ही खुशमिजाज और फुरतीली, अपने हिसाब से स्मार्ट भी।
उस छोटी वय में पहली बार महसूस किया था कि पैसा आत्मविश्वास का किताब बड़ा स्रोत होता है।
बहरहाल, मौसीजी चली जातीं। उनकी छोड़ी हुई सौगातें रह जातीं। सबसे विद्रूप भरा दृश्य होता, जब बूढ़ी बहन छोटी बहन की छोड़ी गई ऊँची हीलवाली चप्पलें पहनकर खटर-पटर करती अपने लिए पान-तंबाकू लाने जाती होती।
तब बिलकुल नहीं जाना था कि यह चित्र मेरे अंदर फ्रीज होता चला जा रहा है और आज से बरसों-बरसों बाद किसी किन्नी-कथा की मूल संवेदना के रूप में पिघल उठेगा।
किन्नी कौन ? कहाँ की ? अब सबकुछ ही थोड़ी बता दूँगी !
मौसी आतीं तो घर रोशनी और रौनक से भर जाता। हम छज्जे-छज्जे चहकते फिरते। सबसे कहते-हमारी मौसी आ रही हैं, बिजनौरवाली मौसी। हमारे मौसाजी शक्कर की मिल में मैनेजर हैं। उनके पास मिल की जीप है, उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं; दो कुत्ते हैं और एक खरगोश भी। उनके दो बच्चे हैं-गगन और रोजी। गगन के पास बंदूक है चिड़िया मारने की। रोजी के पास बुलबुल तरंग-मास्टर आते हैं उसे सिखाने को।
मौसी खूब चिट्टी हैं, माँ जैसी धूमिल-धूमिल-सी नहीं और खूब हँसती-खिलखिलाती चुस्त-दुरुस्त सी रहती हैं, माँ जैसी सुस्त-सुस्त-सी नहीं।
रोजी को लेकर स्कूल जाती हूँ तो मेरा रुतबा बढ़ जाता है। सारी सहेलियाँ लट्टू हो जाती हैं उसकी स्कर्टों, सैंडिलों और नई-नई डिजाईन की क्लिपों पर। कैसी तो थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश मिलाकर चटर-पटर-सी बोलती है और आँखें गोल-गोल-सी घुमाती बेफिक्र, बिंदास चहकती रहती है।
जब तक मौसी रहती हैं, गगन और रोजी सारा घर सिरपे उठाए रहते हैं। अब इतने बड़े हो जाने पर भी गगन रोजी के बाल खींचकर या चुटकी काटकर भागता रहता है। रोजी चीखती हुई उसे दौड़ाती रहती है और मौसी अंदर-अंदर मगन होती हुई ऊपर-ऊपर खीझकर लाड़ से डाँटती हैं-
‘अरे, शरम करो शैतानों ! इन बच्चों को देखकर भी तुम्हें अकल नहीं आती। कैसे सीधे, बिना मुँह के-से हैं। जरा देखो किन्नी को, अभी कॉलेज से आए दस मिनट भी नहीं हुए और देखते-देखते फटाफट तुम लोगों की बिखेरी चीजें सँभाल दी, कपड़े तहा लिये और इधर चाय भी चढ़ा दी। ला तो बेटा, एक प्याला, जरा सुस्ती दूर हो।’ फिर चाय का घूँट भरती हुई अम्मा से कहतीं, दीदी ! इस बार मैं सचमुच रोजिया को यहीं छोड़ जाऊँगी तुम्हारे पास और किरण को अपने साथ ले जाऊँगी बिजनौर।’
और खुद ही अपने मजाक पर खुलकर हँस पड़तीं। यों अपने आप में सचमुच इससे बड़ा मजाक दूसरा नहीं हो सकता था और मौसी की तो वैसे भी आदत थी खूट चटपटी बातें करना और अपनी बात खत्म होने से पहले ही जोर से हँस पड़ना।
रंग तो करीब-करीब एक सा ही था दोनों बहनों का, लेकिन अम्मा दुबली फीकी-फीकी-सी लगतीं, जैसे ऊपर एक झाँईं-सी पड़ी हो-अभी नहीं, बाबूजी थे तब भी दूसरी तरफ मौसी एकदम ठसी चकरी सी ऊपर, से नीचे तक जैसे रंग रोगन पॉलिश से दमकती हुईं और चेहरे पर तो खासकर हमेशा एक पूर्ण परितृप्त भी लुनाई फैली रहती थी। अम्मा से पूरे पांच साल छोटी, पर देखने में तो एकदम बेटी ही लगतीं।
आज भी मैं मेज पर तार देखते ही किलक उठी-‘मौसी आ रही हैं !...कब आया तार ? रोजी, गगन भी आ रहे हैं या नहीं ?’
‘‘दोनों सफेद धारीवाली नीली चादरें धोकर फैला दूँ।’
‘बाँसवाले किताबों के रैक पर अँटी धूल साफ कर दूँ।’
‘कोनेवाली मेज की आधी प्लाई उखड़ गई है। ठहरो, इस फटीवाली हैंडलूम की चादर काटकर इस पर मेजपोश सिले देती हूँ।’
‘रसोई की अलमारियों पर अखबार बिछा दूँ।’
‘गुसलखाने की मोरी रगड़कर धो दूँ।’
और साड़ी का फेंटा कसकर तुरत-फुरत मोरचे पर जुट गई, क्योंकि भाभी तो अपने तीनों बच्चों की फ्रॉकों और पैंटों की उधड़ी सिलाई ही दुरुस्त करने भर को होतीं और अम्मा रसोई के डिब्बों में हाथ डाल-डालकर आधा किलो डालडा, एक किलो चीनी सूजी मैदा और चाय मसालों की सूची बनाने में।
दो-तीन दिनों में घर धो-रगड़कर साफ हो जाता, गुसलखाने में फिनाइल की बोतल रख दी जाती और भैया आधे दिन की छुट्टी लेकर स्टेशन पहुँच जाते।
आधे-पौने घंटे के अंदर ही चमकते सूटकेसों और रंग-बिरंगे बैगों, टोकरियों से लदी-फँसी मौसी आ जातीं। सारा घर आवाजों से चहचहा उठता। मौसी हम सबको बारी-बारी से बाँहों में भरतीं। भाभी के तीनों बच्चों को चिपटा-चिपटाकर प्यार करतीं और भाभी को पाँव छूने के लिए झुकने के साथ उठाकर बलाएँ लेने लगतीं।
भाभी हुलसती हुई जल्दी से रंगदार चाय, मठरी, सेव सजा देतीं और हमारी तंग-अँधेरी कोठरियों से हँसी के झरने फूट पड़ते।
अब इसके बाद हम सबों के चिर-प्रतीक्षित क्षण आता। मौसी सामानों से ही नहीं, सौगातों से भी लदी-फँदी आतीं। सबको अंदर-ही-अंदर इस बात की कितनी खलबली रहती है, यह मौसी भी खूब अच्छी तरह समझती थीं। इसलिए झटपट सूटकेस खोलकर सोत्साह जादुई-सी एक के बाद एक चीजें निकालने लगतीं-‘किन्नी, इधर आ, ये देख, ये रोजी ने तेरे लिए टाप्स और मैचिंग लॉकेट भेजे हैं और ये चार रूमालें। बहू, यह तुम्हारे पर्स है और ये मिंटू-चिंटू के लिए हेयर बैंड और क्लिपें...गुड्डू के लिए ये रंगीन पेंसिलों का सेट गगन ने भेजा है।’
लेकिन यह सब तो औपचारिक सौगातें होतीं। असली सौगातें तो इसके बाद निकलतीं मौसीके होल्डॉल से तीन-तीन, चार-चार जोड़ी पुरानी चप्पलें सैंड़िले-‘ये वाली मुझे पंजों पे कसे सी हैं; ये रोजी ने खरीदी तो बड़े चाव से, लेकिन अब मन भिटक गया उसका-जानती तो हो मूडी नंबर एक। इस वाली पे बस तू दो कीलें ठुकवा लेना। और इस वाली पे इसी रंग की सिलाई करवा लेना किसी अच्छे मोची से। किन्नी, मेरी इस नई-सी साड़ी पे रोजी रानी खोंच लगा आई ठीक सामने नीचे की तरफ, तू उलटी करके पहनेगी न तो बिलकुल पता नहीं चलेगा। और ये, इन दोनों की बस प्रिंट जरा हलकी हो आई है...इस मेरे बैग का हैंडल निकल गया है बस...अमर ! जरा ये बुश्शर्ट देख तो, मिल की वर्कशॉप का राऊंड लेते समय यह छींटा पड़ गया गंदे तेल का-मैंने कहा लिये चलती हूँ अमर जरा फिट करवा के पहन डालेगा। तेरा तो रंग भी गोरा है, फबेगी तुझ पर।’
इसी तरह-‘ये रोजी की नाइटी, ये स्वेटरों के बचे-खुचे ऊन मैंने सोचा, बहू गुणी है, काट छाँटकर चिंटू-नीटू की फ्रॉक बना देगी और थोड़ा और ऊन मिलाकर रंग बिरंगा प्यारा सा स्वेटर बन जाएगा, खूब खिलेगा इन पर। और हाँ, ये स्टील की दो छोटी प्लेटें और कटोरियाँ भी....दीवाली पर आई थीं न मिल में बँटने के लिए, मैंने चुपके से चार रख लीं। इन्हें कहाँ होश-हवास कि कितने आए, कितने गए, सारे दिन मिल भर के ही होते हैं।’
हाँ, मौसाजी को तो पूरे होशोहवास में बस दो बार देखा था-शायद बाबूजी की मौत पर-शायद भैया की शादी में, इससे कम जरूरी मौकों पर वे कभी पहुँच ही न पाए। दोनों बार एक प्लेन से आए और दूसरे प्लेन से वापस। जितनी देर रहे भी न सामने जाने की हिम्मत न बात करने का धड़का-सिर्फ सिर झुकाए।
‘मौसाजी, नाश्ता लग गया।’
या फिर-‘मौसाजी, बाथरूम खाली है।’
मौसाजी बहुत कम बोलते, जितना बोलते उसके भी शब्द-शब्द बड़प्पन और मातबरी के फ्रेम में जड़े-से होते। कभी हलके से मुसकराकर पढ़ाई-लिखाई के बारे में एकाध शब्द पूछ लेते तो हम सिर से पांव तक निहाल हो जाते।
लेकिन असली चौकड़ी तो हमारी मौसी के साथ ही जमती। हर आधे घंटे पर चाय की तलब और भाप छोड़ते प्यालों के साथ मौसी सारे समय कहाँ कहाँ के हँसी-लतीफे छोड़ती जातीं। मौसीजी के गुमाश्तों, कारकुनों से लेकर अपने शहर के एस.पी., डी.एम. की नकनकाती बीवियों तक के किस्सों की फुलझड़ियाँ।
नए-से-नए फैशन तक की बातें बड़े चाव से सुनती-सुनातीं और रस लेतीं। असल में रुतवा मौसाजी का बड़ा था, लेकिन शहर हमारा। और मिलें-फैक्टरियाँ तो वैसे भी शहरी आबादी से मीलों दूर, स्कूल-कॉलेज भी उतने अच्छे नहीं जितने हमारे शहर के तो फैशन की नई-से-नई जानकारी मुझसे ही लेतीं। यहाँ तक कि हाथों में प्लास्टिक के सादे इकरंगे कंगन या कानों में सिर्फ एक नन्हा कल्पर का मोती देखते ही।
‘अरे किन्नी, देखूँ तो जरा तेरे कंगन, लाख के होंगे ?’
‘नहीं, सादे प्लास्टिक के।’
‘और जरा कानों के टॉप्स तो दिखा।’
‘यहीं के चौक से खरीदे हैं।’
‘असल में तेरी पसंद बहुत बढ़िया है। जानती है, क्या तुझे सूट करेगा। चल, जरा आज बाजार ले चल, दो-चार पेयर रोजी के लिए खरीदवा दे।’
मैं मौसी के ना-ना कहने पर भी फौरन कानों के बुदे निकाल रोजी के लिए पैक कर देती। फिर बाजार ले जाकर मौसी और जो-जो चाहतीं, खरीदवा देती। मौसी हर चीज से पहले मेरी सलाह लेतीं कि फलाँ चीज उनपर, रोजी पर खिलेगी। या नहीं ? मेरी पसंद पर पूरा भरोसा था। मेरी पसंद की हमेशा दाद देतीं। मुझसे पसंद करवाकर ढेर सारे टॉप्स, पेंडैंट, अँगूठियाँ ले जातीं और उनमें से बहुत सी डिजाइनें सुनारो को दिखाकर सच्चे मोती, सोने में गढ़वा लेतीं। अगली बार जब आतीं तो मुझे दिखाकर पूछतीं, ‘देख किन्नी, कैसे लगे ये ? इमीटेशन में तो काली पड़ जाएँगी न ?’
मेरे मुँह से बेसाख्ता ‘वाह’ निकल जाता मौसी की पारखी दृष्टि पर।
उतनी उमर होने पर भी मौसी में हमेशा नई उमरवालियों-सी उमंग, उत्साह छलकता रहता।
आजकल जरूर मौसी को एक फिक्र सी हो गई है रोजी के मोटापे की। जब-जब टोकती रहती हैं उसे-‘ठूसे चली जा रही है गपागप भाभी के बनाए पकौड़े-मालपूए। शीशे में नजर डाली है खुद पर ! कैसी खुद भी फूलकर पकौड़े, मालपूए-सी हुई जा रही है। किन्नी, तू ही समझा न जरा इसे।’
लेकिन रोजी उसी बेफिक्री से एक और पूआ चुभलाती हुई खिलखिला देती, ‘‘साफ-साफ कहो न मम्मी, तुम्हें मेरी शादी की फिक्र ही सताए जा रही है न ! अरे, तुम बेकार घबराती हो। देखना, सब दौड़ते हुए शादी करेंगे। असल में आजकल सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा और मेरे शक्तिशाली साए में कोई भी पति भयरहित और निर्द्वंद्व जीवन जी सकता है, समझीं। मजाल है जो कोई उसकी ओर आँख उठाकर भी देखे। अरे, वो क्या, उसका बॉस भी मुझे देखकर दुम हिलाएगा। लाओ भाभी, एक और मालपूआ इसी बात पर।’
अम्मा धीमे से हँसती हुई समझातीं, कहाँ मोटी है बेचारी। जरा दोहरा शरीर है बस। तू बेकार इसके पीछे पड़ी रहती है। लड़के-बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं-और नहीं तो क्या इस किन्नी-सी सींक-सलाई ! मैं तो इसे मुटवाने की कोशिश में हार मान चुकी हूँ।’
सचमुच मैं रोजी से तीन साल बड़ी थी और बेहद दुबली, इतनी कि रोजी के सलवार-कुरते सब तीन-तीन, चार–चार सिलाइयों के बाद ही मुझे फिट आते। अपने तईं मैं उन्हें पूरी तरह काट-छाँटकर नया-सा कर डालती। फिर भी कॉलेज में लड़कियाँ देखते ही ठिठोली करतीं-‘रोजी ब्रांड !’ और मैं शरमाकर हँस देती।
माँ को क्या कहूँ, खुद मेरी भी तो यही हालत है। बहुत जोर से हँस-खिलखिला सकती ही नहीं। अपनी बात पूरे वजन और आत्मविश्वास से सबके बीच में कह सकती ही नहीं। इसलिए सही बात भी सुननेवाले के साथ-साथ खुद अपने आपको भी कच्ची, अधूरी, अनिश्चित सी लगती है; जबकि रोजी और मौसी एकदम घिसी-पिटी कहावतों और जुमलों को भी इतनी ठसक के साथ पेश करती हैं कि सुननेवाला फौरन उनकी गिरफ्त में आ जाता है।
इसी तरह अपने शादी-ब्याह या गुण-शऊर की बात चलने पर भी लाख कोशिशों के बावजूद पलकें जैसे मारे घबराहट और संकोच के यहाँ-वहाँ छुपने की ठौर तलाशने लगती हैं; लेकिन वहीं रोजी अपने लिए ऐसी कोई बात सुनते ही गोल-गोल आँखें चमकाती ठठाकर हँस पड़ती है। और उसे आँखें तरेरकर बरजती हुई मौसी भी उसी ठहाके में शामिल हो जाती हैं।
मौसी के जाते ही वे ठहाके थम जाते हैं। घर वापस श्मशान-सी खामोशी में साँय-साँय कर उठता है। माँ फैली-बिखरी चीजें समेटने लगती हैं। भाभी दो-तीन या चार दिनों की थकान उतारने खाट पर पसर जाती हैं और भाई मौसी की लाई ढीली कमीजों-पतलूनों की फिटिंग कराने के लिए पैसे माँगते हुए माँ से हुज्जत करने लगते हैं। सबको मालूम है, उन पैसों में से काट-कपट कर रूमाल या तौलिए में लपेटी एक दो बोतलें आएँगी। उनके बूते पर बैठक में भाई जैसे ही भाई के खस्ताहाल दोस्तों का जमावड़ा जुटेगा, जश्न मनेगा और एक तीखी मिठास के तहत कई सुस्त से हाथ किसी तरह हवा में लहराकर गिरते हुए एक से एक हवाई योजनाएँ बनाएँगे, हलके सुरूर के पंखों पर उड़ते हुए, कभी किसी साबुन की एजेंसी, कभी स्कूटर मरम्मत का गैरेज, कभी दर्दनाशक गोलियाँ या दंत-मंजन बनाने के नुस्खे की तजवीज, या ऐसा ही कुछ और।
ऐसे मौकों पर किताबें उठाकर मैं सीधी कटरेवाली चाची के पास पहुँच जाती और चाची बिना सिर उठाए सब्जी का रसा अंदाजतीं या पराँठे उतारती-उतारती ही कह देतीं, ‘कौन किन्नी ? चली जा, खाली है बैठक।’
चाचा का तो टाइम ही आठ से आठ है। इसीलिए आज चाची से पूछा भी नहीं, सिर्फ इत्तिला दे दी। ‘चाची, जाती हूँ बैठक में पढ़ने।’
कि चाची जल्दी से अँगीठी छोड़ आईं, किन्नी, बैठक तो खाली नहीं।’ वे फुसफुसाई सी बोली।
‘अरे वाह ! चाचा आज छुट्टी मार बैठे ?’
‘नहीं, मेरा भतीजा आया हुआ है, रिश्ते का।’
मेरी आवाज दयनीय हो उठी, ‘फिर क्या करूँ चाची ? मेरा तो कल पॉलिटिक्स का परचा है।’
‘क्या करूँ ?’ चाची खुद असमंजस में थीं, ‘वह भी पढ़ने ही आया है। आज ही नहीं, कुछ महीनों तक के लिए। दंगों की वजह से लड़कों का पूरा हॉस्टल खाली करा लिया गया है। मटरगश्ती करनेवालों को तो माँगी मुराद मिली, लेकिन ये बेचारे पढ़नेवालों को....’
‘क्या हुआ, बुआ ?’ दंगों का मारा खुद ही आन खड़ा हुआ, ‘कोई परेशानी है ?’
चाची जल्दी से बोलीं, ‘परेशानी नहीं, यह किन्नी है।’ सुधारा-‘किरन-और किन्नी, यह आकाश है।’
उसने सुधारा, ‘कुशा ! पढ़ने आई हैं आप ?’
‘जी..लेकिन ?’
‘तो जाइए, पढ़िए न।’
‘और आप-आपको भी तो पढ़ना है !’
‘हाँ-हाँ, मैं भी पढ़ूँगा।’
‘जी !’ मैं चौंकी।
‘जी हाँ, उधर दुछती पर।’ और मेरी लमहे पहले की घबराहट का मजा लेता हुआ हँस दिया।
‘नहीं-नहीं आप पढ़िए।’
‘आप भी।’
अब के चाची खिलखिलाईं, ‘अब ‘आप’ और ‘आपके’ फेर में मेरे पराँठे जले जा रहे हैं।’
चाची के जाते ही दोनों अपनी-अपनी जगह पढ़ने चले गए।
और मैं ठीक समय पर पढ़ाई खत्म कर सीधी गरदन, सधी चाल घर आ गई, बगैर किसी तरफ ताके-झाँके। मुझे सचमुच खबर नहीं थी कि मैं अपने आँचल में कस्तूरी का एक छोटा-सा टुकड़ा बाँधे चली आई हूँ।
चौथे दिन कॉलेज से लौटते हुए यों ही चाची दिख गईं, ‘सुन किन्नी।’
‘हाँ, चाची।’
‘कौन सी क्लास में है तू ?’
‘चाची !’ मैंने चिढ़ाया, ‘अब इसके बाद मेरा नाम भी पूछोगी क्या ’
चाची झेंप गईं, ‘नहीं रे, यों ही। मेरा मतलब है, बी.ए. प्रीवियस या फाइनल ?’
‘क्यों ? कहीं नौकरी लगवा रही हो मेरी ?’
‘अरे भई, कल यों ही तेरी बात चलने पर कुशा ने पूछा था तो मुझे बड़ी कोफ्त आई कि मुझे इतना भी नहीं मालूम।’
‘अच्छा, तो वो नौकरी लगवा रहे हैं ?’
अरे नहीं, वो बेचारा तो खुद ही दूध का जला है।’
‘च-च्च...तो गलती तुम्हारी है, इतना खौलता दूध काहे को पिलाया ? मारे लाड़ के, ऐं ?’
यह क्या मेरे अंदर छुपी कस्तूरी ही परिहास के तमाम रंगों में छिटकी पड़ रही थी ?
लेकिन चाची का ध्यान मेरे परिहास में जरा भी नहीं था। उसी अवसाद और आक्रोश में एक साथ डूबी-सी बोलीं, ‘कुशा की सात सौ की स्कॉलरशिप का मामला विश्वविद्यालय की ब्राह्मण-ठाकुर गुटबंदी की खटाई में फँसा पड़ा है। बेचारा न इधर का हो पा रहा है, न उधर का। आज तो खीजकर कह रहा था-चल रहा हूँ विश्वविद्यालय के फाटक पर रिक्शा खींचने या जूते गाँठने।’
‘ओह !’ मैं अपनी ऊल-जलूल वाचालता पर सचमुच लज्जित थी, ‘रिसर्च में खर्च भी तो काफी आता है ?’
‘खाली रिसर्च भर नहीं न-समूची घर गहस्थी-माँ-बहनों की पूरी-पूरी जिम्मेदारी..दो ही साल पहले पिता नहीं रहे न इसके।’
उस शाम सूरज के साथ एक सिंदूरी अवसाद घुलते-घुलते डूब रहा था और डूबने के बाद की निस्तब्धता एक उदास सहेली-सी लगी थी।
उस कस्तूरी से एक कुतूहल की खुशबू उड़ी थी-क्या बातें होंगी मुझे लेकर ? कैसे चर्चा चली होगी मेरी ? क्या कहा होगा चाची ने और कैसे पूछा होगा और किसी ने ? मुझे ‘किन्नी’ कहा होगा या ‘किरन’ ?
अब चिलचिलाती धूप में कॉलेज से जल्दी-जल्दी घर की ओर बढ़ते कदम अनायास चाची के घर के सामने से गुजरते हुए ठहरने-से लगते। आहिस्ते, बहुत आहिस्ते-आहिस्ते, थकान का छल, खुद अपने आप से !
‘अरे किन्नी, कहाँ भागी जाती है ? बैठ, चाय पी मेरे साथ।’
‘लेकिन मुझे तो भूख भी लगी है, चाची।’
‘मुझे भी।’ आँचल से बँधी कस्तूरी की गाँठ जैसे खुलकर बिखर पड़ी। बरुनियों की आड़ में दुबकी-सी मैं मुसकराई।
‘भला दो अनखातों को एक साथ भूख तो लगी-सुबह के पराँठे रखे हैं, वही लाती हूँ। चलेगा कि बनाऊँ कुछ ?’
‘चलेगा।’ दो आवाजें एक साथ सिहरकर उलझ लीं। फिर जल्दी से सँभलकर अलग-अलग हो लीं।
‘बस, मैं तो चला।’
‘अरे, क्या हुआ ? तू अपने अंदर कोई अलार्म घड़ी फिट किए रहता है क्या, जो खाते पीते भी घन्न से बजकर चौकन्न कर देती है तुझे ?’
सुनिए, आपकी लाइब्रेरी में पॉलिटिक्स की एक दो किताबें मिल सकती हैं ?’
‘होनी तो चाहिए, क्योंकि आजकल बिना पॉलिटिक्स पढ़े कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता।’
‘छोड़िए, आप नहीं समझेंगे।’ मैं आहत-सी हुई।
‘नहीं, शायद आप...! वह फीकी हँसी हँसा।
‘असल में मेरे कॉलेज में सिर्फ दो किताबें हैं, जो दोनों लेक्चरर्स के लिए बारी-बारी रिजर्व रहती हैं।’
‘आप दोनों किताबों के नाम लिखकर दे दीजिएगा। मैं तो नहीं, मेरा दोस्त जाता है आर्ट्स सेक्शन की लाइब्रेरी में।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i