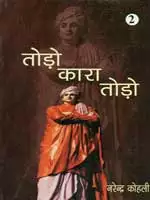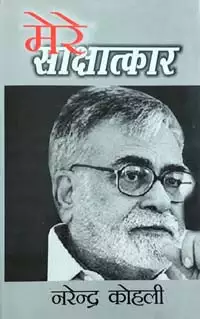|
बहुभागीय पुस्तकें >> तोड़ो, कारा तोड़ो - 2 तोड़ो, कारा तोड़ो - 2नरेन्द्र कोहली
|
334 पाठक हैं |
|||||||
दूसरा खंड ‘साधना’
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पिछले दस वर्षों में लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली रचना
तोड़ो, कारा तोड़ो नरेन्द्र कोहली की नवीनतम उपन्यास-श्रृंखला है। यह
शीर्षक रवीन्द्र ठाकुर के गीत की एक पंक्ति का अनुवाद है। किंतु उपन्यास
का संबंध स्वामी विवेकानन्द की जीवनकथा से है। स्वामी विवेकानन्द का जीवन
बंधनों तथा सीमाओं के अतिक्रमण के लिए सार्थक संघर्ष था : बंधन चाहे
प्रकृति के हों, समाज के हों, राजनीति के हों, धर्म के हों, अध्यात्म के
हों। नरेन्द्र कोहली के ही शब्दों में, ‘‘स्वामी विवेकानन्द
के व्यक्तित्व का आकर्षण...आकर्षण नहीं, जादू....जादू जो सिर चढ़कर बोलता
है। कोई संवेदनशील व्यक्ति उनके निकट जाकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रह
सकता।...और युवा मन तो उत्साह से पागल ही हो जाता है।
कौन-सा गुण था, जो स्वामी जी में नहीं था। मानव के चरम विकास की साक्षात् मूर्ति थे वे। भारत की आत्मा...और वे एकाकार हो गये थे। उन्हें किसी एक युग, प्रदेश, संप्रदाय अथवा संगठन के साथ बाँध देना अज्ञान भी है और अन्याय भी।’’ ऐसे स्वामी विवेकानन्द के साथ तादात्म्य किया है नरेन्द्र कोहली ने। उनका यह उपन्यास ऐसा ही तादात्म्य करा देता है, पाठक का उस विभूति से।
इस बृहत् उपन्यास का प्रथम खंड ‘निर्माण’ स्वामी जी के व्यक्तित्व के निर्माण के विभिन्न आयामों तथा चरणों की कथा कहता है। इसका क्षेत्र उनके जन्म से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस तथा जगन्माता भवतारिणी के सम्मुख निर्द्वंद्व आत्मसमर्पण तक की घटनाओं पर आधृत है।
दूसरा खंड ‘साधना’ में अपने गुरु के चरणों में बैठकर की गयी साधना और गुरु के शरीर-त्याग के पश्चात् उनके आदेशानुसार, अपने गुरुभाइयों को एक मठ में संगठित करने की कथा है। अगले दो खण्डों-‘परिव्राजक’ और ‘गंतव्य’ में उनके एक अज्ञात संन्यासी के रूप में भारत में भ्रमण तथा पश्चिम के देशों में जाकर भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के ध्वजारोहण की कथा है।
तोड़ो, कारा तोड़ो रचनाकर्म की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न तथा अभिनव उपन्यास है। पौराणिक गाथाओं पर आधारित उपन्यासों के लेखन में, पौराणिक कथाशैली और प्राचीनता के कारण, लेखक की कल्पना तथा सृजन के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। उसमें मौलिक उद्भावनाओं के रूप में प्राचीन कथा तथा पात्रों पर लेखक का अपना व्यक्तित्व और चिन्तन भी आरोपित हो सकता है।
स्वामी विवेकानन्द का जीवन निकट अतीत की घटना है। उनके जीवन की प्रायः घटनाएँ सप्रमाण इतिहासांकित हैं। यहाँ उपन्यासकार के लिए अपनी कल्पना अथवा अपने चिंतन को आरोपित करने की सुविधा नहीं है। उपन्यासकार को वही कहना होगा, जो स्वामी जी ने कहा था। अपने नायक के व्यक्तित्व और चिंतन से तादात्म्य ही उसके लिए एकमात्र मार्ग है।
अंग्रेज़ी तथा बाँग्ला में कुछ विस्तृत तथा प्रामाणिक जीवनियाँ उपलब्ध हैं। ये जीवनियाँ विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखी गयी हैं। फिर भी उनमें स्वामी जी के आध्यात्मिक साधक तथा समाज-सुधारक होने पर ही एकदेशीय एवं एकांगिक बल दिया गया है। जीवनीकार तथा उपन्यासकार के दृष्टिकोण में अंतर होता है। उपन्यासकार की रुचि कुछ व्यापक होती है। वह अपने नायक तथा उसके संपूर्ण युग को उनकी समग्रता में चित्रित करना चाहता है। अतः साधना को केंद्र में मानते हुए भी वह अन्य पक्षों की उपेक्षा नहीं कर सकता।
उपन्यास का शिल्प भी जीवनी के शिल्प से भिन्न है। उपन्यासकार, घटनाओं तथा चरित्रों को अलग-अलग खंडों में रख, उनका एक-दूसरे से सर्वथा असंपृक्त विकास नहीं दिखाता। वह अलग-अलग स्रोतस्विनियों के असंबद्ध प्रवाह का वर्णन कर ही संतुष्ट नहीं हो सकता, उसे उन स्रोतस्विनियों के साथ-साथ उन्हें संपृक्त करने वाली भूमि का भी चित्रण करना होगा।
नरेन्द्र कोहली ने अपने नायक को उनकी परंपरा तथा उनके परिवेश से पृथक् कर नहीं देखा। स्वामी विवेकानन्द ऐसे नायक हैं भी नहीं, जिन्हें अपने परिवेश से अलग-थलग किया जा सके। वे तो जैसे महासागर के असाधारण ज्वार के उद्दामतम चरम अंश थे। तोड़ो, कारा तोड़ो उस ज्वार को पूर्ण रूप से जीवंत करने का औपन्यासिक प्रयत्न है, जो स्वामी जी को उनके पूर्वापर के मध्य रखकर ही देखना चाहता है। अतः इस उपन्यास के लिए, न श्री रामकृष्ण पराए हैं, न स्वामी जी के सहयोगी, गुरुभाई, और न ही उनकी शिष्य परंपरा की प्रतीक भगिनी निवेदिता।
‘‘मेरे बच्चे ! मान लो एक कमरे में सोने का एक थैला रखा है और उसके पास ही दूसरे कमरे में एक चोर है, तो क्या तुम सोच सकते हो कि उस चोर को नींद आएगी ? नहीं, कदापि नहीं—उसके मन में लगातार यही उथल-पुथल मची रहेगी कि मैं उस कमरे में कैसे पहुँचूँ तथा उस सोने को कैसे पाऊँ। इसी प्रकार क्या तुम सोच सकते हो कि जिस मनुष्य की यह दृढ़ धारणा हो गई कि इस माया के प्रसार के पीछे एक अविनाशी, अखंड, आनंदमय परमेश्वर है, जिसके सामने इंद्रियों का सुख कुछ भी नहीं है, तो उस परमेश्वर को प्राप्त किए बिना वह मनुष्य चुपचाप बैठ सकता है ? क्या वह अपने प्रयत्न क्षण-भर के लिए भी स्थगित कर सकता है ? कदापि नहीं—असह्य छटपटाहट के कारण वह पागल हो जाएगा।
कौन-सा गुण था, जो स्वामी जी में नहीं था। मानव के चरम विकास की साक्षात् मूर्ति थे वे। भारत की आत्मा...और वे एकाकार हो गये थे। उन्हें किसी एक युग, प्रदेश, संप्रदाय अथवा संगठन के साथ बाँध देना अज्ञान भी है और अन्याय भी।’’ ऐसे स्वामी विवेकानन्द के साथ तादात्म्य किया है नरेन्द्र कोहली ने। उनका यह उपन्यास ऐसा ही तादात्म्य करा देता है, पाठक का उस विभूति से।
इस बृहत् उपन्यास का प्रथम खंड ‘निर्माण’ स्वामी जी के व्यक्तित्व के निर्माण के विभिन्न आयामों तथा चरणों की कथा कहता है। इसका क्षेत्र उनके जन्म से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस तथा जगन्माता भवतारिणी के सम्मुख निर्द्वंद्व आत्मसमर्पण तक की घटनाओं पर आधृत है।
दूसरा खंड ‘साधना’ में अपने गुरु के चरणों में बैठकर की गयी साधना और गुरु के शरीर-त्याग के पश्चात् उनके आदेशानुसार, अपने गुरुभाइयों को एक मठ में संगठित करने की कथा है। अगले दो खण्डों-‘परिव्राजक’ और ‘गंतव्य’ में उनके एक अज्ञात संन्यासी के रूप में भारत में भ्रमण तथा पश्चिम के देशों में जाकर भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के ध्वजारोहण की कथा है।
तोड़ो, कारा तोड़ो रचनाकर्म की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न तथा अभिनव उपन्यास है। पौराणिक गाथाओं पर आधारित उपन्यासों के लेखन में, पौराणिक कथाशैली और प्राचीनता के कारण, लेखक की कल्पना तथा सृजन के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। उसमें मौलिक उद्भावनाओं के रूप में प्राचीन कथा तथा पात्रों पर लेखक का अपना व्यक्तित्व और चिन्तन भी आरोपित हो सकता है।
स्वामी विवेकानन्द का जीवन निकट अतीत की घटना है। उनके जीवन की प्रायः घटनाएँ सप्रमाण इतिहासांकित हैं। यहाँ उपन्यासकार के लिए अपनी कल्पना अथवा अपने चिंतन को आरोपित करने की सुविधा नहीं है। उपन्यासकार को वही कहना होगा, जो स्वामी जी ने कहा था। अपने नायक के व्यक्तित्व और चिंतन से तादात्म्य ही उसके लिए एकमात्र मार्ग है।
अंग्रेज़ी तथा बाँग्ला में कुछ विस्तृत तथा प्रामाणिक जीवनियाँ उपलब्ध हैं। ये जीवनियाँ विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखी गयी हैं। फिर भी उनमें स्वामी जी के आध्यात्मिक साधक तथा समाज-सुधारक होने पर ही एकदेशीय एवं एकांगिक बल दिया गया है। जीवनीकार तथा उपन्यासकार के दृष्टिकोण में अंतर होता है। उपन्यासकार की रुचि कुछ व्यापक होती है। वह अपने नायक तथा उसके संपूर्ण युग को उनकी समग्रता में चित्रित करना चाहता है। अतः साधना को केंद्र में मानते हुए भी वह अन्य पक्षों की उपेक्षा नहीं कर सकता।
उपन्यास का शिल्प भी जीवनी के शिल्प से भिन्न है। उपन्यासकार, घटनाओं तथा चरित्रों को अलग-अलग खंडों में रख, उनका एक-दूसरे से सर्वथा असंपृक्त विकास नहीं दिखाता। वह अलग-अलग स्रोतस्विनियों के असंबद्ध प्रवाह का वर्णन कर ही संतुष्ट नहीं हो सकता, उसे उन स्रोतस्विनियों के साथ-साथ उन्हें संपृक्त करने वाली भूमि का भी चित्रण करना होगा।
नरेन्द्र कोहली ने अपने नायक को उनकी परंपरा तथा उनके परिवेश से पृथक् कर नहीं देखा। स्वामी विवेकानन्द ऐसे नायक हैं भी नहीं, जिन्हें अपने परिवेश से अलग-थलग किया जा सके। वे तो जैसे महासागर के असाधारण ज्वार के उद्दामतम चरम अंश थे। तोड़ो, कारा तोड़ो उस ज्वार को पूर्ण रूप से जीवंत करने का औपन्यासिक प्रयत्न है, जो स्वामी जी को उनके पूर्वापर के मध्य रखकर ही देखना चाहता है। अतः इस उपन्यास के लिए, न श्री रामकृष्ण पराए हैं, न स्वामी जी के सहयोगी, गुरुभाई, और न ही उनकी शिष्य परंपरा की प्रतीक भगिनी निवेदिता।
‘‘मेरे बच्चे ! मान लो एक कमरे में सोने का एक थैला रखा है और उसके पास ही दूसरे कमरे में एक चोर है, तो क्या तुम सोच सकते हो कि उस चोर को नींद आएगी ? नहीं, कदापि नहीं—उसके मन में लगातार यही उथल-पुथल मची रहेगी कि मैं उस कमरे में कैसे पहुँचूँ तथा उस सोने को कैसे पाऊँ। इसी प्रकार क्या तुम सोच सकते हो कि जिस मनुष्य की यह दृढ़ धारणा हो गई कि इस माया के प्रसार के पीछे एक अविनाशी, अखंड, आनंदमय परमेश्वर है, जिसके सामने इंद्रियों का सुख कुछ भी नहीं है, तो उस परमेश्वर को प्राप्त किए बिना वह मनुष्य चुपचाप बैठ सकता है ? क्या वह अपने प्रयत्न क्षण-भर के लिए भी स्थगित कर सकता है ? कदापि नहीं—असह्य छटपटाहट के कारण वह पागल हो जाएगा।
रामकृष्ण परमहंस
साधना
ठाकुर की समाधि भंग हो गई। उनकी आँखें खुलीं और उनमें चेतना लौटी। वे
प्रकृतिस्थ लग रहे थे और शिष्यों से चर्चा करने की मुद्रा में आ गए थे।
‘‘स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण।’’ वे बोले, ‘‘महाकारण में जाने पर चुप हैं। वहाँ बातचीत नहीं हो सकती।’’
नरेंद्र समझ गया, ठाकुर आध्यात्मिक अनुभव की बातें कर रहे हैं। अभी-अभी उनकी समाधि टूटी है। वे किसी उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव से होकर सामान्य भूमि पर लौटे हैं। महाकारण...संभवतः सृष्टि के महाकारण की बात कह रहे हैं। ठाकुर की तो चर्चा करने की पद्धति यही थी। वे विद्यालय के शिक्षक के समान यह मानकर नहीं चलते थे कि उनके सामने बैठा छात्र कुछ नहीं जानता, इसलिए उसे सब कुछ उसकी बुद्धि, ज्ञान और समझ के अनुसार समझाना है...कभी-कभी वैसा भी करते थे, किंतु जब समाधि के पश्चात् प्रकृतिस्थ होते थे तो उस भावक के समान होते थे, जिसने कुछ बहुत अद्भुत देखा हो, अनुभव किया हो और अब वह उसे अभिव्यक्ति देने के लिए तड़प रहा हो।...उस समय वे अध्यापक नहीं सर्जक कलाकार होते थे। अपने भीतर की सृष्टि को अभिव्यक्ति दे रहे होते थे।...भक्तों ने आत्मानुभव की चर्चा करते हुए कब चिंता की कि उनकी बात कोई समझ रहा है या नहीं, वे तो अपनी अनुभूति को बाँट रहे होते हैं।
‘‘ईश्वर-कोटि, महाकारण में पहुँचकर लौट आते हैं।’’ ठाकुर कह रहे थे, ‘‘वे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। वे ऊपर चढ़ भी सकते हैं और नीचे उतर भी सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर, फिर सीढ़ी से उतर कर, नीचे चल-फिर सकते हैं। अनुलोम और विलोम।...’’
नरेंद्र समझ रहा था कि ‘ईश्वर-कोटि’ के माध्यम से ठाकुर अपनी ही स्थिति समझा रहे थे। वे अपनी इच्छानुसार सृष्टि और स्रष्टा के मध्य कहीं भी स्वयं को स्थिर कर सकते थे, किंतु यह उन साधकों की स्थिति नहीं थी जो अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति से पतित हो जाते हैं, न उन साधकों की स्थिति थी जिनके लिए, एक बार आरोह करने के पश्चात् ‘अवरोह’ संभव नहीं रहता। ठाकुर तो उन ईश्वर-कोटि लोगों की बात कर रहे थे, जो भगवान् में रमे रहने के पश्चात् भी सामान्य व्यक्ति के धरातल पर उतर सकते हैं...
‘‘सात मंजिला मकान है। किसी की पहुँच बाहर के फाटक तक ही होती है, किसी की भीतरी फाटक तक। जो राजा का लड़का है, उसका तो वह अपना ही मकान है। वह सातों मंजिलों पर घूम-फिर सकता है।’’ निश्चय ही ठाकुर ईश्वर-कोटि जीवों की तुलना राजकुमार से कर रहे थे। और फिर उन्होंने एक नया उदाहरण दिया, ‘‘अनार कई प्रकार के होते हैं—दीपावली पर जलने वाले बारूद के अनार ! एक विशेष प्रकार का अनार होता है, जिसमें थोड़ी देर तक तो एक प्रकार की फुलझड़ियाँ छूटती हैं, फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे प्रकार के फूल निकलने लगते हैं, फिर किसी और प्रकार के...।’’ ठाकुर रुके, ‘‘एक प्रकार के अनार वे हैं...आग लगाने के थोड़ी ही देर बाद वे भुस्स से फूट जाते हैं। उसी प्रकार बहुत प्रयत्न करके कोई साधारण आदमी यदि ऊपर चला भी जाता है, तो वह लौटकर खबर नहीं देता। जीव-कोटि के जो साधक हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि तो हो सकती है, परंतु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उतरकर खबर ही दे सकते हैं।...’’ठाकुर बिना रुके ही कहते चले गए, ‘‘एक हैं नित्य-सिद्ध की तरह। वे जन्म से ही ईश्वर की आकांक्षा करते हैं। संसार की कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। वे होमा पक्षी होते हैं। अवतारों के संग आने वाले, नित्य-सिद्ध होते हैं, या फिर अन्तिम जन्म वाले प्राणी...।’’
नरेंद्र को लगा, ठाकुर आज बहुत कुछ कह देने को तत्पर थे। वे अपनी ध्यानावस्था की अनुभूतियाँ ही नहीं बाँट रहे थे, बहुत सारे संकेत भी दे रहे थे। उनसे स्पष्ट पूछे जाने पर कि क्या वे अवतार हैं, वे कभी प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देते थे। उलटे प्रश्न को पलटकर स्वयं ही पूछ बैठते थे, ‘‘वो जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं अवतार हूँ, उस विषय में तुम्हारा क्या विचार है ?’’...किंतु आज वे स्वयं अवतार ही नहीं, अपने साथ के लोगों को भी नित्य-सिद्ध अथवा अंतिम जन्म वाले लोग कह रहे थे। स्वयं नरेंद्र को तो वे कब से होमा पक्षी कहते ही थे...
‘‘सहजानंद होने पर यों ही नशा हो जाता है, शराब पीनी नहीं पड़ती।’’ ठाकुर पुनः बोले, ‘‘माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता है। ठीक उतना, जितना पाँच बोतल शराब पीने से होता है।...इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता...।’’
नरेंद्र उनकी वाणी के प्रवाह के साथ और नहीं चल पाया। शिलावत् मार्ग में अड़ गया, ‘‘खाने-पीने के लिए जो कुछ मिले, वही बिना विचार के खाना अच्छा है।...’’ और नरेंद्र सहसा सजग हो गया...एक बार पहले भी वह अपने कुछ मित्रों के साथ होटल में खा आया था। तब भी उसने ठाकुर से कुछ नहीं छिपाया था। उसके सम्मुख पड़ते ही उसने बता दिया था, ‘‘महाराज ! आज एक होटल में वह खा आया हूँ, जिसे साधारण लोग निषिद्ध भोजन कहते हैं।...’
ठाकुर ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा था और जैसे उसके मन के आर-पार देखते हुए समझ गए थे कि नरेंद्र वीरता जताने के लिए यह सूचना नहीं दे रहा था। वह तो उन्हें सूचित कर रहा था कि वह ऐसा कार्य कर आया है। अब यदि ठाकुर को उसे स्पर्श करने में अथवा उसके द्वारा उनके बर्तन अथवा घड़े इत्यादि के उपयोग में उन्हें कोई आपत्ति हो तो कह दें। कहीं यह न कहें कि उसने इन बातों को उनसे छुपाया....
‘तुझे इसका दोष नहीं लगेगा। तूने निषिद्ध वस्तु खाई है, उससे मुझे कुछ भी बुरा महसूस नहीं हो रहा।’ ठाकुर ने शेष लोगों की ओर इंगित किया, ‘किंतु यदि इनमें से कोई आकर यही बात कहता, तो उसे मैं छू भी नहीं सकता था।’
किंतु आज स्थिति वह नहीं थी। आज नरेंद्र स्वयं ही अपनी बात पर चौंक उठा था...उसकी उस उक्ति के पीछे कहीं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति तो नहीं बोल रही ?...उसका परिवार इस स्थिति में ही नहीं था कि वह सोचे कि क्या खाना है, क्या नहीं। किसके हाथ का खाना है, किसके हाथ का नहीं...जहाँ भोजन के ही लाले पड़े हों, वहाँ यह कौन सोचता है कि भोजन कहाँ से आया और किसके माध्यम से आया।
किंतु ठाकुर का ध्यान उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अथवा नरेंद्र की अपनी मनःस्थिति की ओर नहीं था। वे तो भक्त की आध्यात्मिक स्थिति की चर्चा कर रहे थे, ‘‘यह बात एक विशेष अवस्था के लिए है। ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं। गीता के मत से, ज्ञानी स्वयं नहीं खाता, वह कुंडलिनी को आहुती देता है।...तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है। तुम इधर भी हो और उधर भी। इस समय तुम सब खा सकते हो। गाय-शूकर खा कर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुकाव हो, तो वह धन्य है, और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामिनी और कांचन पर लगा रहे, तो उसे धिक्कार है।’’
नरेंद्र को याद है। ठाकुर ने ऐसी ही बात एक बार पहले भी कही थी...कुछ व्यापारी भक्त ठाकुर के दर्शन करने आए थे और मिस्री, पिस्ता, किशमिश, बादाम, आदि वस्तुएँ भेंट कर गए थे। ठाकुर ने न तो उनमें से कुछ स्वयं ग्रहण किया, न उपस्थित किसी भक्त को ही दिया।
‘ये व्यापारी लोग निष्काम भाव से दान करना नहीं जानते। एक बीड़ा पान देते समय भी सोलहों कामनाएँ जोड़ देते हैं। इस प्रकार सकाम दाता का अन्न खाने से भक्ति की हानि होती है।’ ठाकुर ने कहा था।
‘तो इन वस्तुओं का क्या होगा महाराज ?’
‘जा, नरेंद्र को दे आ। इन्हें खाकर भी उसे कोई हानि नहीं होगी।’
ठाकुर अब अपनी चर्चा कर रहे थे, ‘‘मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊँ। बचपन की बात है। लोहार कहते थे, ब्राह्मण खाना पकाना क्या जाने। खैर, मैंने खाया, परंतु उसमें लोहारी बू मिल रही थी।’’ ठाकुर ने पुनः नरेंद्र की ओर देखा, ‘‘वेदों और पुराणों में शुद्धाचार की बात लिखी है। वेदों और पुराणों में जिसके लिए कहा है कि यह न करो, इससे अनाचार होता है, तंत्रों में उसी को अच्छा कहा है।...’’उन्हें जैसे कुछ याद आ गया, ‘‘मेरी कैसी-कैसी अवस्थाएँ बीत गई हैं। मुख आकाश और पाताल तक फैलाता था और तब मैं कहता था, ‘‘माँ !’ मानो माँ को पकड़ने के लिए आ रहा हूँ, जैसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर खींचना। रामप्रसाद का एक गीत है न ‘अब की बार ऐ काली, तुम्हें ही मैं खाऊँगा।...मैं अच्छी तरह बता दूँगा कि रामप्रसाद काली का बेटा है। या तो मंत्र की सिद्धि ही होगी, या मेरा यह शरीर ही न रह जाएगा।’...पागल की-सी अवस्था हो गई थी मेरी—यह व्याकुलता है।’’
नरेंद्र को अच्छा लगा...बात भोजन से हटकर भक्ति के पागलपन तक तो आई। विधि-निषेध की चर्चाओं में वैसे भी उसे कोई बहुत रुचि नहीं थी। उससे तो यह पागलखाना ही अच्छा।...
उसने ठाकुर को आगे बोलने ही नहीं दिया। उसका स्वर जैसे उन्मादपूर्ण हो उठा, ‘‘माँ ! मुझे पागल कर दे। ज्ञान के विचार से मुझे कोई काम नहीं है।...
पर ठाकुर आज बहुत मौज में थे। खूब बातें करना चाहते थे। लड़कों को भी उनकी बातें अच्छी लगती थीं। वे एक क्षण में भक्ति अथवा साधना का कोई गूढ़ रहस्य समझा रहे होते थे और अगले ही क्षण कोई रोचक कहानी आरंभ कर देते थे।....आज उसका मन पलट-पलटकर अपने पिछले दिनों की ओर जा रहा था। बोले, ‘‘हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता था कि ब्रह्म और शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों में अभेद है। जब वे निष्क्रिय हैं, तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, और जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हीं को शक्ति कहते हैं। हैं वे एक ही वस्तु—अभेद।...तब मैंने प्रार्थना की, ‘माँ ! हाजरा यहाँ का मत उलटा देना चाहता है। या तो तू उसे समझा दे, या उसे यहाँ से हटा दे।’ उसके दूसरे ही दिन उसने आकर कहा, ‘हाँ, मानता हूँ, विभु सब जगह है।’ ’’
प्रतापचंद्र हाजरा से ठाकुर का संबंध लड़के जानते थे। हाजरा ठाकुर के माध्यम से ही दक्षिणेश्वर आया था और अब ठाकुर से ही प्रतिस्पर्धा कर अन्य लोगों की दृष्टि में स्वयं को उनसे बड़ा बनाना चाहता था। ठाकुर के साथ लगा-लगा, उनके भक्तों का आतिथ्य भी ग्रहण कर आता था और अवसर मिलते ही उनके शिष्यों और भक्तों की दृष्टि में उन्हें छोटा बनाने का प्रयत्न भी करता रहता था। ठाकुर भी अपने स्थान पर शिष्यों को उससे सावधान करते रहते थे। किंतु न तो उसे दक्षिणेश्वर से निकालने का आदेश देते थे, न उससे स्वयं को सर्वथा पृथक् ही कर लेते थे...
भवनाथ हँसा, ‘‘हाजरा की इसी बात पर आपको इतना दुःख हुआ था ?’’
‘‘मेरी अवस्था बदल गई है।’’ ठाकुर बोले, ‘‘अब मैं वाद-विवाद नहीं कर सकता। इस समय मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि हाजरा जैसे लोगों के साथ तर्क और झगड़ा करता रहूँ।’’
‘‘आपने हृदय से भी तो यही कहा था।’’ नरेंद्र ने जैसे उन्हें याद दिलाया।
हृदयराम मुखोपाध्याय ठाकुर का भांजा था, जो उनकी सेवा और देखभाल के लिए दक्षिणेश्वर में लगभग पच्चीस वर्ष उनके साथ रहा था। नरेंद्र के पहली बार दक्षिणेश्वर आने से पहले ही, स्वामियों के आदेश से ‘1881 ई. में वह वहाँ से निष्काषित किया जा चुका था। नरेंद्र को अनेक बार आश्चर्य भी होता था। वह हृदय किस मिट्टी का बना हुआ था कि जिस ठाकुर के एक बार दर्शन मात्र से उन सबका मन इस प्रकार ईश्वरोन्मुख हो गया था, उनके साथ पच्चीस वर्ष रहकर भी उसके मन में वैराग्य नहीं जागा। वह धन, संपत्ति तथा अधिकार के मोह में धँसता चला गया। स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अधीन न मानकर ठाकुर पर ही आधिपत्य स्थापित कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता रहा। उनसे लड़ता-झगड़ता रहा, उन्हें डाँटता-डपटता रहा....
‘‘हाँ ! यदु मल्लिक के बगीचे में आकर हृदय ने कहा, ‘मामा ! क्या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है ? मैंने कहा, ‘नहीं ! अब मेरी वैसी अवस्था नहीं है कि तेरे साथ गला फाड़ता रहूँ।’ ’’
नरेंद्र बातों-ही-बातों में अधलेटा-सा हो गया था। कुछ और विश्राम की स्थिति में आने के लिए वह पेट के बल चटाई पर लेट गया। ठाकुर की बातें सुनने में कैसा आनंद था...
तभी ठाकुर ने गाया, ‘‘श्री दुर्गा नाम का जप करो ए मन।’’
दिन चढ़ आया था। भोग की आरती का घंटा बजा। प्रसाद पाने के इच्छुक लोग अतिथिशाला की ओर बढ़ गए। मंदिर के कर्मचारी जहाँ प्रसाद पाते थे, आगंतुक भक्तों को भी वहीं प्रसाद दिया जाता था।
‘‘जाओ, सब लोग वहीं जाकर प्रसाद पाओ।’’ ठाकुर ने अपने आसपास बैठे लोगों से कहा, और फिर वे नरेंद्र की ओर मुड़े, ‘‘नहीं ! तू नहीं ! तू यहीं भोजन कर।’’ उन्होंने कमरे से बाहर खड़ी वृंदा को पुकार कर कहा, ‘‘नरेंद्र और मेरे लिए, यहीं प्रसाद की व्यवस्था हो।’’
नरेंद्र की इच्छा हुई कि कहे, उसके लिए विशेष रूप से यहाँ व्यवस्था क्यों करवा रहे हैं ? वह भी वहीं अतिथिशाला में जाकर दूसरे लोगों के साथ ही प्रसाद पा लेगा।...किंतु फिर कुछ सोचकर, वह रुक गया।...पहले दिन से ही ठाकुर उसके खान-पान का विशेष ध्यान रखते थे। जब उसे स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयों का तनिक भी अभाव नहीं था, तब भी वे कितने आग्रह से, अपने हाथों से उसे खिलाया करते थे...और अब तो सबकुछ बदल गया था।...उसके घर की आर्थिक स्थिति वे जानते थे। वे जानते थे कि नरेंद्र ने या तो खाया नहीं होगा, या भरपेट नहीं खाया होगा...या फिर उसे अपना मनपसंद सुस्वादु भोजन नहीं मिला होगा...शायद इसीलिए उन्होंने उसे रोक लिया था कि वे स्वयं उसे अच्छी तरह भोजन करा सकें...शायद वे यह भी समझते थे कि अपने घर की इस आर्थिक स्थिति के कारण नरेंद्र बाहर खाने में संकोच करने लगा है कि कहीं कोई उसे लोभी न मान ले।...पहले दिन जो नरेंद्र उनके पास इस आग्रह के साथ आया था कि यदि उन्होंने रसगुल्लों से उसका भली प्रकार सत्कार नहीं किया, तो वह उनके कान उमेठ देगा, वह नरेंद्र अब दो दिन से भूखा होने पर भी अपनी जिह्वा से यह नहीं कहता कि उसे भूख लगी है, उसे कुछ खाने को चाहिए...
ठाकुर स्वयं उसे खिलाएँगे, तो उनके स्नेह और आग्रह के सम्मुख न नरेंद्र का संकोच टिक पाएगा, न उसकी सामाजिक सावधानियाँ।...नरेंद्र के अधरों पर सहज ही मुस्कान आ गई...ठाकुर ऊपर से जितने निर्लिप्त, असावधान और अजान लगते हैं, भीतर से वैसे हैं नहीं। उनकी करुणा न निर्लिप्त है, न असावधान और न अजान...
भोजनोपरांत विश्राम के पश्चात् ठाकुर भी बाहर बरामदे में आ बैठे। अपराह्न के दो बजे थे। बाहर बरामदे में बैठना, कमरे में बैठने की तुलना में कहीं अच्छा लग रहा था।
नरेंद्र की दृष्टि सहज ही उठी और उसने देखा कि उपस्थित लोगों में भवनाथ नहीं था। कहाँ गया वह ? उसे बिना बताए, वह घर तो नहीं गया होगा। अभी यहीं कहीं होगा...किंतु कहाँ ?....
उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। सहसा उसने देखा कि दक्षिण-पूर्व के बरामदे से भवनाथ चला आ रहा है...पर यह क्या ? इसने यह कैसा वेश बना रखा है...यहाँ कोई स्वाँग होने वाला है या बहरूपियों का कोई तमाशा...? भवनाथ ने भगवा धारण कर रखा था। हाथ में कमंडलु था और वह इस प्रकार प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहा था, जैसे उसे कोई असाधारण उपलब्धि हुई हो....
ठाकुर ने भी उसे देखा और उल्लसित होकर हँस पड़े, ‘‘उसके मन का यही भाव है—ब्रह्मचारी का। इसीलिए तो यह वेश धारण किया है।’’
नरेंद्र ठाकुर का भाव समझता था। किसी को भी संन्यासी की ओर प्रवृत्त होते देख—चाहे वह स्वाँग ही क्यों न हो—उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होती थी। नरेंद्र ने जिस समय संसार त्यागने का संकल्प किया था, ठाकुर ने उसे रोक लिया था, किंतु उसके विवाह-विरोध से वे प्रसन्न ही थे।...
किंतु इस समय नरेंद्र अपने ही मन को ठीक-ठीक समझ नहीं पा रहा था...इस समय वह भोजन कर अलसाया हुआ-सा था ?...अपने परिवार की परिस्थितियों के कारण इस सारे परिवेश से विरक्त सा हो रहा था...हो सकता है, यह विरक्ति न हो, उकताहट और खीझ हो, जो उसे कहीं भी रमने नहीं दे रही थी, कहीं रस नहीं लेने दे रही थी। वह नहीं जानता था कि वह खीझा खड़ा हुआ था, उखड़ा हुआ था या आक्रमक था।...एक सहज-सी वक्रता ने उसे घेर रखा था।...या भोजन और विश्राम के पश्चात् एक प्रकार की तृप्ति का अनुभव करता हुआ, वह हलके आह्लाद के मद की स्थित में था...नहीं। यह तृप्ति और मद की स्थिति नहीं थी। तृप्ति या मद में व्यक्ति इस प्रकार हर किसी से रूठा हुआ नहीं होता...
‘‘स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण।’’ वे बोले, ‘‘महाकारण में जाने पर चुप हैं। वहाँ बातचीत नहीं हो सकती।’’
नरेंद्र समझ गया, ठाकुर आध्यात्मिक अनुभव की बातें कर रहे हैं। अभी-अभी उनकी समाधि टूटी है। वे किसी उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव से होकर सामान्य भूमि पर लौटे हैं। महाकारण...संभवतः सृष्टि के महाकारण की बात कह रहे हैं। ठाकुर की तो चर्चा करने की पद्धति यही थी। वे विद्यालय के शिक्षक के समान यह मानकर नहीं चलते थे कि उनके सामने बैठा छात्र कुछ नहीं जानता, इसलिए उसे सब कुछ उसकी बुद्धि, ज्ञान और समझ के अनुसार समझाना है...कभी-कभी वैसा भी करते थे, किंतु जब समाधि के पश्चात् प्रकृतिस्थ होते थे तो उस भावक के समान होते थे, जिसने कुछ बहुत अद्भुत देखा हो, अनुभव किया हो और अब वह उसे अभिव्यक्ति देने के लिए तड़प रहा हो।...उस समय वे अध्यापक नहीं सर्जक कलाकार होते थे। अपने भीतर की सृष्टि को अभिव्यक्ति दे रहे होते थे।...भक्तों ने आत्मानुभव की चर्चा करते हुए कब चिंता की कि उनकी बात कोई समझ रहा है या नहीं, वे तो अपनी अनुभूति को बाँट रहे होते हैं।
‘‘ईश्वर-कोटि, महाकारण में पहुँचकर लौट आते हैं।’’ ठाकुर कह रहे थे, ‘‘वे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। वे ऊपर चढ़ भी सकते हैं और नीचे उतर भी सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर, फिर सीढ़ी से उतर कर, नीचे चल-फिर सकते हैं। अनुलोम और विलोम।...’’
नरेंद्र समझ रहा था कि ‘ईश्वर-कोटि’ के माध्यम से ठाकुर अपनी ही स्थिति समझा रहे थे। वे अपनी इच्छानुसार सृष्टि और स्रष्टा के मध्य कहीं भी स्वयं को स्थिर कर सकते थे, किंतु यह उन साधकों की स्थिति नहीं थी जो अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति से पतित हो जाते हैं, न उन साधकों की स्थिति थी जिनके लिए, एक बार आरोह करने के पश्चात् ‘अवरोह’ संभव नहीं रहता। ठाकुर तो उन ईश्वर-कोटि लोगों की बात कर रहे थे, जो भगवान् में रमे रहने के पश्चात् भी सामान्य व्यक्ति के धरातल पर उतर सकते हैं...
‘‘सात मंजिला मकान है। किसी की पहुँच बाहर के फाटक तक ही होती है, किसी की भीतरी फाटक तक। जो राजा का लड़का है, उसका तो वह अपना ही मकान है। वह सातों मंजिलों पर घूम-फिर सकता है।’’ निश्चय ही ठाकुर ईश्वर-कोटि जीवों की तुलना राजकुमार से कर रहे थे। और फिर उन्होंने एक नया उदाहरण दिया, ‘‘अनार कई प्रकार के होते हैं—दीपावली पर जलने वाले बारूद के अनार ! एक विशेष प्रकार का अनार होता है, जिसमें थोड़ी देर तक तो एक प्रकार की फुलझड़ियाँ छूटती हैं, फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे प्रकार के फूल निकलने लगते हैं, फिर किसी और प्रकार के...।’’ ठाकुर रुके, ‘‘एक प्रकार के अनार वे हैं...आग लगाने के थोड़ी ही देर बाद वे भुस्स से फूट जाते हैं। उसी प्रकार बहुत प्रयत्न करके कोई साधारण आदमी यदि ऊपर चला भी जाता है, तो वह लौटकर खबर नहीं देता। जीव-कोटि के जो साधक हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि तो हो सकती है, परंतु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उतरकर खबर ही दे सकते हैं।...’’ठाकुर बिना रुके ही कहते चले गए, ‘‘एक हैं नित्य-सिद्ध की तरह। वे जन्म से ही ईश्वर की आकांक्षा करते हैं। संसार की कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। वे होमा पक्षी होते हैं। अवतारों के संग आने वाले, नित्य-सिद्ध होते हैं, या फिर अन्तिम जन्म वाले प्राणी...।’’
नरेंद्र को लगा, ठाकुर आज बहुत कुछ कह देने को तत्पर थे। वे अपनी ध्यानावस्था की अनुभूतियाँ ही नहीं बाँट रहे थे, बहुत सारे संकेत भी दे रहे थे। उनसे स्पष्ट पूछे जाने पर कि क्या वे अवतार हैं, वे कभी प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देते थे। उलटे प्रश्न को पलटकर स्वयं ही पूछ बैठते थे, ‘‘वो जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं अवतार हूँ, उस विषय में तुम्हारा क्या विचार है ?’’...किंतु आज वे स्वयं अवतार ही नहीं, अपने साथ के लोगों को भी नित्य-सिद्ध अथवा अंतिम जन्म वाले लोग कह रहे थे। स्वयं नरेंद्र को तो वे कब से होमा पक्षी कहते ही थे...
‘‘सहजानंद होने पर यों ही नशा हो जाता है, शराब पीनी नहीं पड़ती।’’ ठाकुर पुनः बोले, ‘‘माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता है। ठीक उतना, जितना पाँच बोतल शराब पीने से होता है।...इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता...।’’
नरेंद्र उनकी वाणी के प्रवाह के साथ और नहीं चल पाया। शिलावत् मार्ग में अड़ गया, ‘‘खाने-पीने के लिए जो कुछ मिले, वही बिना विचार के खाना अच्छा है।...’’ और नरेंद्र सहसा सजग हो गया...एक बार पहले भी वह अपने कुछ मित्रों के साथ होटल में खा आया था। तब भी उसने ठाकुर से कुछ नहीं छिपाया था। उसके सम्मुख पड़ते ही उसने बता दिया था, ‘‘महाराज ! आज एक होटल में वह खा आया हूँ, जिसे साधारण लोग निषिद्ध भोजन कहते हैं।...’
ठाकुर ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा था और जैसे उसके मन के आर-पार देखते हुए समझ गए थे कि नरेंद्र वीरता जताने के लिए यह सूचना नहीं दे रहा था। वह तो उन्हें सूचित कर रहा था कि वह ऐसा कार्य कर आया है। अब यदि ठाकुर को उसे स्पर्श करने में अथवा उसके द्वारा उनके बर्तन अथवा घड़े इत्यादि के उपयोग में उन्हें कोई आपत्ति हो तो कह दें। कहीं यह न कहें कि उसने इन बातों को उनसे छुपाया....
‘तुझे इसका दोष नहीं लगेगा। तूने निषिद्ध वस्तु खाई है, उससे मुझे कुछ भी बुरा महसूस नहीं हो रहा।’ ठाकुर ने शेष लोगों की ओर इंगित किया, ‘किंतु यदि इनमें से कोई आकर यही बात कहता, तो उसे मैं छू भी नहीं सकता था।’
किंतु आज स्थिति वह नहीं थी। आज नरेंद्र स्वयं ही अपनी बात पर चौंक उठा था...उसकी उस उक्ति के पीछे कहीं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति तो नहीं बोल रही ?...उसका परिवार इस स्थिति में ही नहीं था कि वह सोचे कि क्या खाना है, क्या नहीं। किसके हाथ का खाना है, किसके हाथ का नहीं...जहाँ भोजन के ही लाले पड़े हों, वहाँ यह कौन सोचता है कि भोजन कहाँ से आया और किसके माध्यम से आया।
किंतु ठाकुर का ध्यान उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अथवा नरेंद्र की अपनी मनःस्थिति की ओर नहीं था। वे तो भक्त की आध्यात्मिक स्थिति की चर्चा कर रहे थे, ‘‘यह बात एक विशेष अवस्था के लिए है। ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं। गीता के मत से, ज्ञानी स्वयं नहीं खाता, वह कुंडलिनी को आहुती देता है।...तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है। तुम इधर भी हो और उधर भी। इस समय तुम सब खा सकते हो। गाय-शूकर खा कर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुकाव हो, तो वह धन्य है, और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामिनी और कांचन पर लगा रहे, तो उसे धिक्कार है।’’
नरेंद्र को याद है। ठाकुर ने ऐसी ही बात एक बार पहले भी कही थी...कुछ व्यापारी भक्त ठाकुर के दर्शन करने आए थे और मिस्री, पिस्ता, किशमिश, बादाम, आदि वस्तुएँ भेंट कर गए थे। ठाकुर ने न तो उनमें से कुछ स्वयं ग्रहण किया, न उपस्थित किसी भक्त को ही दिया।
‘ये व्यापारी लोग निष्काम भाव से दान करना नहीं जानते। एक बीड़ा पान देते समय भी सोलहों कामनाएँ जोड़ देते हैं। इस प्रकार सकाम दाता का अन्न खाने से भक्ति की हानि होती है।’ ठाकुर ने कहा था।
‘तो इन वस्तुओं का क्या होगा महाराज ?’
‘जा, नरेंद्र को दे आ। इन्हें खाकर भी उसे कोई हानि नहीं होगी।’
ठाकुर अब अपनी चर्चा कर रहे थे, ‘‘मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊँ। बचपन की बात है। लोहार कहते थे, ब्राह्मण खाना पकाना क्या जाने। खैर, मैंने खाया, परंतु उसमें लोहारी बू मिल रही थी।’’ ठाकुर ने पुनः नरेंद्र की ओर देखा, ‘‘वेदों और पुराणों में शुद्धाचार की बात लिखी है। वेदों और पुराणों में जिसके लिए कहा है कि यह न करो, इससे अनाचार होता है, तंत्रों में उसी को अच्छा कहा है।...’’उन्हें जैसे कुछ याद आ गया, ‘‘मेरी कैसी-कैसी अवस्थाएँ बीत गई हैं। मुख आकाश और पाताल तक फैलाता था और तब मैं कहता था, ‘‘माँ !’ मानो माँ को पकड़ने के लिए आ रहा हूँ, जैसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर खींचना। रामप्रसाद का एक गीत है न ‘अब की बार ऐ काली, तुम्हें ही मैं खाऊँगा।...मैं अच्छी तरह बता दूँगा कि रामप्रसाद काली का बेटा है। या तो मंत्र की सिद्धि ही होगी, या मेरा यह शरीर ही न रह जाएगा।’...पागल की-सी अवस्था हो गई थी मेरी—यह व्याकुलता है।’’
नरेंद्र को अच्छा लगा...बात भोजन से हटकर भक्ति के पागलपन तक तो आई। विधि-निषेध की चर्चाओं में वैसे भी उसे कोई बहुत रुचि नहीं थी। उससे तो यह पागलखाना ही अच्छा।...
उसने ठाकुर को आगे बोलने ही नहीं दिया। उसका स्वर जैसे उन्मादपूर्ण हो उठा, ‘‘माँ ! मुझे पागल कर दे। ज्ञान के विचार से मुझे कोई काम नहीं है।...
पर ठाकुर आज बहुत मौज में थे। खूब बातें करना चाहते थे। लड़कों को भी उनकी बातें अच्छी लगती थीं। वे एक क्षण में भक्ति अथवा साधना का कोई गूढ़ रहस्य समझा रहे होते थे और अगले ही क्षण कोई रोचक कहानी आरंभ कर देते थे।....आज उसका मन पलट-पलटकर अपने पिछले दिनों की ओर जा रहा था। बोले, ‘‘हाजरा किसी तरह भी विश्वास नहीं करना चाहता था कि ब्रह्म और शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों में अभेद है। जब वे निष्क्रिय हैं, तब उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, और जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हीं को शक्ति कहते हैं। हैं वे एक ही वस्तु—अभेद।...तब मैंने प्रार्थना की, ‘माँ ! हाजरा यहाँ का मत उलटा देना चाहता है। या तो तू उसे समझा दे, या उसे यहाँ से हटा दे।’ उसके दूसरे ही दिन उसने आकर कहा, ‘हाँ, मानता हूँ, विभु सब जगह है।’ ’’
प्रतापचंद्र हाजरा से ठाकुर का संबंध लड़के जानते थे। हाजरा ठाकुर के माध्यम से ही दक्षिणेश्वर आया था और अब ठाकुर से ही प्रतिस्पर्धा कर अन्य लोगों की दृष्टि में स्वयं को उनसे बड़ा बनाना चाहता था। ठाकुर के साथ लगा-लगा, उनके भक्तों का आतिथ्य भी ग्रहण कर आता था और अवसर मिलते ही उनके शिष्यों और भक्तों की दृष्टि में उन्हें छोटा बनाने का प्रयत्न भी करता रहता था। ठाकुर भी अपने स्थान पर शिष्यों को उससे सावधान करते रहते थे। किंतु न तो उसे दक्षिणेश्वर से निकालने का आदेश देते थे, न उससे स्वयं को सर्वथा पृथक् ही कर लेते थे...
भवनाथ हँसा, ‘‘हाजरा की इसी बात पर आपको इतना दुःख हुआ था ?’’
‘‘मेरी अवस्था बदल गई है।’’ ठाकुर बोले, ‘‘अब मैं वाद-विवाद नहीं कर सकता। इस समय मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि हाजरा जैसे लोगों के साथ तर्क और झगड़ा करता रहूँ।’’
‘‘आपने हृदय से भी तो यही कहा था।’’ नरेंद्र ने जैसे उन्हें याद दिलाया।
हृदयराम मुखोपाध्याय ठाकुर का भांजा था, जो उनकी सेवा और देखभाल के लिए दक्षिणेश्वर में लगभग पच्चीस वर्ष उनके साथ रहा था। नरेंद्र के पहली बार दक्षिणेश्वर आने से पहले ही, स्वामियों के आदेश से ‘1881 ई. में वह वहाँ से निष्काषित किया जा चुका था। नरेंद्र को अनेक बार आश्चर्य भी होता था। वह हृदय किस मिट्टी का बना हुआ था कि जिस ठाकुर के एक बार दर्शन मात्र से उन सबका मन इस प्रकार ईश्वरोन्मुख हो गया था, उनके साथ पच्चीस वर्ष रहकर भी उसके मन में वैराग्य नहीं जागा। वह धन, संपत्ति तथा अधिकार के मोह में धँसता चला गया। स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अधीन न मानकर ठाकुर पर ही आधिपत्य स्थापित कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता रहा। उनसे लड़ता-झगड़ता रहा, उन्हें डाँटता-डपटता रहा....
‘‘हाँ ! यदु मल्लिक के बगीचे में आकर हृदय ने कहा, ‘मामा ! क्या मुझे रखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है ? मैंने कहा, ‘नहीं ! अब मेरी वैसी अवस्था नहीं है कि तेरे साथ गला फाड़ता रहूँ।’ ’’
नरेंद्र बातों-ही-बातों में अधलेटा-सा हो गया था। कुछ और विश्राम की स्थिति में आने के लिए वह पेट के बल चटाई पर लेट गया। ठाकुर की बातें सुनने में कैसा आनंद था...
तभी ठाकुर ने गाया, ‘‘श्री दुर्गा नाम का जप करो ए मन।’’
दिन चढ़ आया था। भोग की आरती का घंटा बजा। प्रसाद पाने के इच्छुक लोग अतिथिशाला की ओर बढ़ गए। मंदिर के कर्मचारी जहाँ प्रसाद पाते थे, आगंतुक भक्तों को भी वहीं प्रसाद दिया जाता था।
‘‘जाओ, सब लोग वहीं जाकर प्रसाद पाओ।’’ ठाकुर ने अपने आसपास बैठे लोगों से कहा, और फिर वे नरेंद्र की ओर मुड़े, ‘‘नहीं ! तू नहीं ! तू यहीं भोजन कर।’’ उन्होंने कमरे से बाहर खड़ी वृंदा को पुकार कर कहा, ‘‘नरेंद्र और मेरे लिए, यहीं प्रसाद की व्यवस्था हो।’’
नरेंद्र की इच्छा हुई कि कहे, उसके लिए विशेष रूप से यहाँ व्यवस्था क्यों करवा रहे हैं ? वह भी वहीं अतिथिशाला में जाकर दूसरे लोगों के साथ ही प्रसाद पा लेगा।...किंतु फिर कुछ सोचकर, वह रुक गया।...पहले दिन से ही ठाकुर उसके खान-पान का विशेष ध्यान रखते थे। जब उसे स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयों का तनिक भी अभाव नहीं था, तब भी वे कितने आग्रह से, अपने हाथों से उसे खिलाया करते थे...और अब तो सबकुछ बदल गया था।...उसके घर की आर्थिक स्थिति वे जानते थे। वे जानते थे कि नरेंद्र ने या तो खाया नहीं होगा, या भरपेट नहीं खाया होगा...या फिर उसे अपना मनपसंद सुस्वादु भोजन नहीं मिला होगा...शायद इसीलिए उन्होंने उसे रोक लिया था कि वे स्वयं उसे अच्छी तरह भोजन करा सकें...शायद वे यह भी समझते थे कि अपने घर की इस आर्थिक स्थिति के कारण नरेंद्र बाहर खाने में संकोच करने लगा है कि कहीं कोई उसे लोभी न मान ले।...पहले दिन जो नरेंद्र उनके पास इस आग्रह के साथ आया था कि यदि उन्होंने रसगुल्लों से उसका भली प्रकार सत्कार नहीं किया, तो वह उनके कान उमेठ देगा, वह नरेंद्र अब दो दिन से भूखा होने पर भी अपनी जिह्वा से यह नहीं कहता कि उसे भूख लगी है, उसे कुछ खाने को चाहिए...
ठाकुर स्वयं उसे खिलाएँगे, तो उनके स्नेह और आग्रह के सम्मुख न नरेंद्र का संकोच टिक पाएगा, न उसकी सामाजिक सावधानियाँ।...नरेंद्र के अधरों पर सहज ही मुस्कान आ गई...ठाकुर ऊपर से जितने निर्लिप्त, असावधान और अजान लगते हैं, भीतर से वैसे हैं नहीं। उनकी करुणा न निर्लिप्त है, न असावधान और न अजान...
भोजनोपरांत विश्राम के पश्चात् ठाकुर भी बाहर बरामदे में आ बैठे। अपराह्न के दो बजे थे। बाहर बरामदे में बैठना, कमरे में बैठने की तुलना में कहीं अच्छा लग रहा था।
नरेंद्र की दृष्टि सहज ही उठी और उसने देखा कि उपस्थित लोगों में भवनाथ नहीं था। कहाँ गया वह ? उसे बिना बताए, वह घर तो नहीं गया होगा। अभी यहीं कहीं होगा...किंतु कहाँ ?....
उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। सहसा उसने देखा कि दक्षिण-पूर्व के बरामदे से भवनाथ चला आ रहा है...पर यह क्या ? इसने यह कैसा वेश बना रखा है...यहाँ कोई स्वाँग होने वाला है या बहरूपियों का कोई तमाशा...? भवनाथ ने भगवा धारण कर रखा था। हाथ में कमंडलु था और वह इस प्रकार प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहा था, जैसे उसे कोई असाधारण उपलब्धि हुई हो....
ठाकुर ने भी उसे देखा और उल्लसित होकर हँस पड़े, ‘‘उसके मन का यही भाव है—ब्रह्मचारी का। इसीलिए तो यह वेश धारण किया है।’’
नरेंद्र ठाकुर का भाव समझता था। किसी को भी संन्यासी की ओर प्रवृत्त होते देख—चाहे वह स्वाँग ही क्यों न हो—उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होती थी। नरेंद्र ने जिस समय संसार त्यागने का संकल्प किया था, ठाकुर ने उसे रोक लिया था, किंतु उसके विवाह-विरोध से वे प्रसन्न ही थे।...
किंतु इस समय नरेंद्र अपने ही मन को ठीक-ठीक समझ नहीं पा रहा था...इस समय वह भोजन कर अलसाया हुआ-सा था ?...अपने परिवार की परिस्थितियों के कारण इस सारे परिवेश से विरक्त सा हो रहा था...हो सकता है, यह विरक्ति न हो, उकताहट और खीझ हो, जो उसे कहीं भी रमने नहीं दे रही थी, कहीं रस नहीं लेने दे रही थी। वह नहीं जानता था कि वह खीझा खड़ा हुआ था, उखड़ा हुआ था या आक्रमक था।...एक सहज-सी वक्रता ने उसे घेर रखा था।...या भोजन और विश्राम के पश्चात् एक प्रकार की तृप्ति का अनुभव करता हुआ, वह हलके आह्लाद के मद की स्थित में था...नहीं। यह तृप्ति और मद की स्थिति नहीं थी। तृप्ति या मद में व्यक्ति इस प्रकार हर किसी से रूठा हुआ नहीं होता...
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i