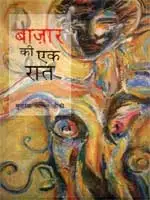|
कहानी संग्रह >> बाजार की एक रात बाजार की एक रातमुशर्रफ आलम ज़ौकी
|
411 पाठक हैं |
|||||||
इस संग्रह की ज़्यादातर कहानियाँ बाज़ार से जुड़ी हैं। बाजा़र, जिसने व्यक्ति से ‘व्यक्तित्व’ को ख़ारिज कर एक ठूँठ, उदासीन मोहरा बना दिया है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मुशर्रफ़ आलम ज़ौक़ी की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि वो जितने हिंदी के
हैं, उतने ही उर्दू के। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि वे जितने उर्दू के
हैं उतने ही भीतर तक हिंदी कथा-संसार में भी लोकप्रिय हैं। बदीउज़्ज़मां,
शानी, मंगूर एहतेशाम, असगर वजाहत और अब्दुल बिस्मिल्ला सरीखे रचनाकार जहाँ
केवल हिंदी के होकर रहे, वहाँ ज़ौक़ी को साहित्यक फलक का दायरा इन मायनो
में बड़ा है कि ‘कहानी’ रचने की अद्भुत शैली व क्षमता ने,
दोनों ही भाषाओं में उन्हें समान रूप से लोकप्रिय बनाया है।
ज़ौक़ी में यहाँ विषय की विविधताओं ने कहानी कहने की कला को बहुआयामी रंग दिया है। इस संग्रह की ज़्यादातर कहानियाँ बाज़ार से जुड़ी हैं। बाजा़र, जिसने व्यक्ति से ‘व्यक्तित्व’ को ख़ारिज कर एक ठूँठ, उदासीन मोहरा बना दिया है। वास्तव में भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण में उड़ते पंक्षी ने दुनिया को एक छोटा-सा गाँव या बाज़ार में परिवर्तित तो कर दिया, किन्तु मनुष्य होने के एहसान को ही छीन लिया। ज़ौक़ी के लिए ‘बाज़ार’ में संघर्ष कर रही विचारधारा किसी चिकनी मिट्टी के ‘क्ले’ की तरह है, जिसे समय के बहाव में अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के अनुसार आप कुछ भी बना सकते हैं। खिलौना, पक्षी या हवाई जहाज।
ज़ौक़ी की यह अद्भुत पाठनीयता है कि पाठक साँसें रोककर एक बार कहानी के भीतर प्रवेश कर गया तो फिर लौटना असंभव प्रतीत होता है।
ज़ौक़ी में यहाँ विषय की विविधताओं ने कहानी कहने की कला को बहुआयामी रंग दिया है। इस संग्रह की ज़्यादातर कहानियाँ बाज़ार से जुड़ी हैं। बाजा़र, जिसने व्यक्ति से ‘व्यक्तित्व’ को ख़ारिज कर एक ठूँठ, उदासीन मोहरा बना दिया है। वास्तव में भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण में उड़ते पंक्षी ने दुनिया को एक छोटा-सा गाँव या बाज़ार में परिवर्तित तो कर दिया, किन्तु मनुष्य होने के एहसान को ही छीन लिया। ज़ौक़ी के लिए ‘बाज़ार’ में संघर्ष कर रही विचारधारा किसी चिकनी मिट्टी के ‘क्ले’ की तरह है, जिसे समय के बहाव में अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के अनुसार आप कुछ भी बना सकते हैं। खिलौना, पक्षी या हवाई जहाज।
ज़ौक़ी की यह अद्भुत पाठनीयता है कि पाठक साँसें रोककर एक बार कहानी के भीतर प्रवेश कर गया तो फिर लौटना असंभव प्रतीत होता है।
आभार
यद्यपि इस संग्रह का अधिकतर पत्रक पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं, उनमें
से कुछ, उल्लेखनीय रूप से ‘पॉलिटिक्स ऐज ए सबजेक्ट फॉर
सोशियोलोजी’ (अध्याय-8) और, ‘इकोनोमिक्स एण्ड
सोशियोलोजी’ (अध्याय-9) तब लिखे गये थे जबकि संग्रह तैयार किया
जा
रहा था और इन लेखों को उसमें शामिल किया जाता था। अन्य शैक्षिक विषयों की
तरह ज्ञानपूर्ण प्रकाशनों के अवसरों के लिये व्यावसायिक जर्नलों पर मैं भी
निर्भर रहा हूँ। इनमें तीन प्रमुख हैं, जिनसे मुझे काफी सहारा और शक्ति
मिली है: इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (EPW), ‘सोशियोलोजिकल
बुलेटिन’ (SB), ‘कोन्ट्रिब्यूशन्स टु
इण्डियन
सोशियोलोजी’ (CIS), और उनके प्रति आभार प्रदर्शन द्वारा मैं
बड़ा
सन्तोष अनुभव कर रहा हूँ।
निम्नलिखित अध्याय पहले ‘इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली’ में प्रकाशित हुए थे : अध्याय-1, ‘सोशियोलोजी एण्ड कॉमनसैन्स’ (EPW, Vol.XXXI nos. 35, 36 & 37, pp. 2361-5, 1996); अध्याय-7 रेलीजन एज ए सबजैक्ट फॉर सोशियोलोजी (EPW,Vol.XXVII, nos. 35, pp 1865-70, 1992); अध्याय-9 इकोनोमिक्स एण्ड सोशियोलोजी, (EPW, Vol. XXXV, no. 18, pp. 1531-8,2000); और अध्याय-11 साइन्स एण्ड ट्रेडिशन (EPW, Vol.XXXIII, no. 10, pp, 529-32, 1998) दो अध्याय पहले सोशियोलोजिकल बुलेटिन में प्रकाशित हुए; अध्याय-5 ‘द कम्पेरेटिव मैथड एण्ड द स्टेण्ड-पाइण्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर (SB, Vol. 47, no. 2, pp. 137-54, 1998)। और अध्याय-12 न्यूनेस इन सोशियोलोजिकल एन्कवायरी (SB, Vol. 46, no. 1, pp. 97-110, 1997) अध्याय-3 सोशियोलोजिक एन्कवायरी (SB, Vol. 46, no. 1, pp. 97-110, 1997)) अध्याय-3, ‘सोशियोलोजी एण्ड एन्थ्रोपोलॉजी; देयर रिलेशन्स इन वन परसन्स करियर’ सर्वप्रथम ‘कन्ट्रीब्यूशन्स, टु इण्डियन सोशियोलोजी (CIS, Vol. 27, no. 2, pp. 291-304, 1993) में प्रकाशित हुआ।
अध्याय-6 ‘सोशियोलोजी एण्ड एरिया स्टडी’ मूलरूप से ‘जर्नल ऑफ द जापानीज एसोसियेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज’ (Vol. 11, pp.124-137, 1999) में प्रकाशित हुआ था। अध्याय-4 ‘सम ऑबसर्वेशन्स ऑन द कम्पेरेटिव मैथड’ प्रथम वर्दियेम व्याख्यान के रूप में 1990 में सेन्टर फॉर एशियन स्टडीज एम्सटर्डम द्वारा प्रकाशित किया गया था। अध्याय-10 ‘द प्लेस ऑफ ट्रेडिशन इन सोशियोलोजिकल एन्क्वायरी’ पंचम राधाकृष्णन मैमोरियल लेक्चर के रूप में इण्डियन इन्स्टीट्यूट फॉर एडवान्स्ड स्टडीज शिमला द्वारा प्रकाशित किया गया।
अध्याय-2 सोशियोलोजी एण्ड एन्थ्रोपोलॉजी ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले एक एन्साइक्लोपीडिया के लिये लिखा गया था, और अध्याय-8 की तरह ही यहाँ पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है।
परिशिष्ट-1 स्टाकहोम में स्टेफान मोलन्द द्वारा संचालित एक साक्षात्कार है और Anthropologiska Studier में no. 48, pp. 31-47, 1991 में प्रकाशित हुआ था। परिशिष्ट-2 में ही एसैज इन कम्पेरेटिव सोशियोलोजी ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, देहली 1987, 141-66 सेपुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
मैं प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव का इस संग्रह में तैयारी करने में उनके योगदान के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ और विशेषतौर पर विषय सूची तैयार करने में।
निम्नलिखित अध्याय पहले ‘इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली’ में प्रकाशित हुए थे : अध्याय-1, ‘सोशियोलोजी एण्ड कॉमनसैन्स’ (EPW, Vol.XXXI nos. 35, 36 & 37, pp. 2361-5, 1996); अध्याय-7 रेलीजन एज ए सबजैक्ट फॉर सोशियोलोजी (EPW,Vol.XXVII, nos. 35, pp 1865-70, 1992); अध्याय-9 इकोनोमिक्स एण्ड सोशियोलोजी, (EPW, Vol. XXXV, no. 18, pp. 1531-8,2000); और अध्याय-11 साइन्स एण्ड ट्रेडिशन (EPW, Vol.XXXIII, no. 10, pp, 529-32, 1998) दो अध्याय पहले सोशियोलोजिकल बुलेटिन में प्रकाशित हुए; अध्याय-5 ‘द कम्पेरेटिव मैथड एण्ड द स्टेण्ड-पाइण्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर (SB, Vol. 47, no. 2, pp. 137-54, 1998)। और अध्याय-12 न्यूनेस इन सोशियोलोजिकल एन्कवायरी (SB, Vol. 46, no. 1, pp. 97-110, 1997) अध्याय-3 सोशियोलोजिक एन्कवायरी (SB, Vol. 46, no. 1, pp. 97-110, 1997)) अध्याय-3, ‘सोशियोलोजी एण्ड एन्थ्रोपोलॉजी; देयर रिलेशन्स इन वन परसन्स करियर’ सर्वप्रथम ‘कन्ट्रीब्यूशन्स, टु इण्डियन सोशियोलोजी (CIS, Vol. 27, no. 2, pp. 291-304, 1993) में प्रकाशित हुआ।
अध्याय-6 ‘सोशियोलोजी एण्ड एरिया स्टडी’ मूलरूप से ‘जर्नल ऑफ द जापानीज एसोसियेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज’ (Vol. 11, pp.124-137, 1999) में प्रकाशित हुआ था। अध्याय-4 ‘सम ऑबसर्वेशन्स ऑन द कम्पेरेटिव मैथड’ प्रथम वर्दियेम व्याख्यान के रूप में 1990 में सेन्टर फॉर एशियन स्टडीज एम्सटर्डम द्वारा प्रकाशित किया गया था। अध्याय-10 ‘द प्लेस ऑफ ट्रेडिशन इन सोशियोलोजिकल एन्क्वायरी’ पंचम राधाकृष्णन मैमोरियल लेक्चर के रूप में इण्डियन इन्स्टीट्यूट फॉर एडवान्स्ड स्टडीज शिमला द्वारा प्रकाशित किया गया।
अध्याय-2 सोशियोलोजी एण्ड एन्थ्रोपोलॉजी ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले एक एन्साइक्लोपीडिया के लिये लिखा गया था, और अध्याय-8 की तरह ही यहाँ पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है।
परिशिष्ट-1 स्टाकहोम में स्टेफान मोलन्द द्वारा संचालित एक साक्षात्कार है और Anthropologiska Studier में no. 48, pp. 31-47, 1991 में प्रकाशित हुआ था। परिशिष्ट-2 में ही एसैज इन कम्पेरेटिव सोशियोलोजी ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, देहली 1987, 141-66 सेपुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
मैं प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव का इस संग्रह में तैयारी करने में उनके योगदान के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ और विशेषतौर पर विषय सूची तैयार करने में।
आन्द्रे बेतेइ
प्रस्तावना
(Introduction)
यह समाजशास्त्र की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है लेकिन इसमें पाठ्यपुस्तक के
प्रमुख अवयव मौजूद हैं। इसमें निबन्धों का एक समूह है जो देहली स्कूल ऑफ
इकोनोमिक्स में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में मेरे जीवन के विगत दस
वर्षों की अवधि में लिखे गये थे, जिनमें मैंने ज्ञान के विशिष्ट विषय
समाजशास्त्र की प्रकृति और महत्त्व की परीक्षा करने का प्रयास किया है।
निबन्ध पहले से योजना बनाकर नहीं लिखे गये, इस अर्थ में, जब इन सबको एक
साथ रखा जाए तो, वे पाठ्यपुस्तक का रूप नहीं लेते। लेकिन वे सब स्वयं मेरे
लिये तथा अन्य लोगों को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता को देखते हुए लिखे गये
कि समाजशास्त्रीय समझ और व्याख्या में क्या विशिष्टता है। ये निबन्ध
प्रमुख रूप से अपने साथी समाजशास्त्रियों और समाजशास्त्र के छात्रों को
सम्बोधित हैं लेकिन समाज और उसकी संस्थाओं में अधिक सामान्य रुचि रखने
वाले अन्य लोग भी इन्हें पढ़ सकते हैं। यद्यपि, जैसा कि मैंने प्रथम
अध्याय में ही स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि के समान कोई
वस्तु नहीं है, सामाजिक जीवन की प्रकृति और स्वरूप में रुचि रखने वाले
सामान्य पाठक को देने के लिये भी इसमें बहुत कुछ है।
इस प्रश्न का छोटा उत्तर देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है : समाजशास्त्र क्या है ? सम्भवत: यही बात अन्य विषयों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून के विषय में भी उतनी ही सही है। कोई भी बौद्धिक विषय पूर्ण रूप से निरूपित विषय सामग्री के साथ समापन की स्थिति में नहीं है, उसकी अवधारणाएँ व विधियाँ हमेशा-हमेशा के लिये परिभाषित नहीं है और न ही अन्य विषयों के साथ उसकी सीमाएँ अन्तिम रूप से बन्द हैं। संक्षेप में यह कहना कठिन है कि समाजशास्त्र क्या है, क्योंकि यह अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है; शायद यह कहना सरल होगा कि जीवन्त विषय के रूप में इसकी ख्याति कम होने के बाद यह क्या था।
समाजशास्त्र की औपचारिक परिभाषाओं की कोई कमी नहीं है। वास्तव में परिभाषाओं की संख्या और विविधता ही असमंजस का मुख्य स्रोत है। दुर्भाग्यवश एक औपचारिक परिभाषा केवल उन्हीं के काम की है जो पहले से ही विषय की मोटी रूप की जानकारी रखते हैं। नूतानाभ्यासी के लिये इसका महत्त्व कम ही होता है। यद्यपि यह प्रायः विद्वानों के बीच बहस में एक उपयोगी प्रस्थान बिन्दु का कार्य करता है जिनका इस विषय पर समान दृष्टिकोण नहीं है।
औपचारिक रूप में विषय की परिभाषा करने के बजाय कोई यह बात सीधे से कह सकता है कि समाजशास्त्र वह है जो समाजशास्त्री करते हैं’ यह विषय अब अपनी प्रारम्भिक स्थिति में नहीं है बल्कि पश्चिम में तो सौ वर्षों से भी अधिक समय से पनप रहा है और भारत में 1920 से। कई पीढ़ियों ने समाजशास्त्र पढ़ा है, पढ़ाया है और इसमें अनुसन्धान किया है। इस विषय के अपने व्यासायिक संगठन और अपनी सामयिक पत्रिकाएँ भी हैं। लेकिन जैसी कि अपेक्षा की जा सकती है, समाजशास्त्र का अभ्यास सभी स्थानों और सभी समयों में एक सा नहीं हुआ है। इसलिये यह कहना कि समाजशास्त्र वह है, जो समाजशास्त्र करते हैं, उत्तर की अपेक्षा प्रश्न को जन्म देना है।
समाजशास्त्री वास्तव में जो कुछ करते हैं वह बिल्कुल वह नहीं है, जो उनके विश्वास उनके बीच द्वन्दात्मक सम्बन्ध हैं, क्योंकि समाजशास्त्रियों के रूप में हमारा अभ्यास इस बात से बनता है कि हम और हमारे सहयोगी व्यवसायिक लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कि हमारे विचार से समाजशास्त्र क्या होना चाहिए ? अतः समाजशास्त्र क्या है ? इस बात का पता लगाने में व्यक्ति विषय के विस्तार, उद्देश्य और विधियों तथा विशिष्ट विषयों के वर्णन, समस्याओं और प्रकरणों के बीच ही घूमता रह जाता है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्रियों के दैनिक अभ्यास की वस्तुएँ होती हैं।
यहाँ एक साथ संकलित निबन्धों में मैंने, समाजशास्त्र क्या है ? विषय पर दोनों बिन्दुओं से विचार करने का प्रयत्न किया है, बार-बार आगे विचार करते हुए तथा एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिना ध्यान दिये भी। समाजशास्त्र के क्षेत्र और विधियों तथा मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति जैसे अन्य विषयों से इसके सम्बन्ध में विशेष गुणों पर भी सामान्य चर्चा भी इसमें है। लेकिन इसमें विशेष वर्णन भी है कि समाजशास्त्री वास्तव में क्या करते हैं, जब वे धर्म, राजनीति और असमानता पर अध्ययन करते हैं। दोनों प्रकार के वर्णन अन्तरसम्बद्ध हैं। यह अन्तरसम्बद्धता आंशिक ही हो सकी है, क्योंकि निबन्ध सोची समझी योजना के अनुसार नहीं लिखे गये थे। लेकिन सामान्य और विशिष्ट के बीच कठोर पृथकता बनाए रखने के लिये पहले से सोची गई योजना का परिणाम लगभग निश्चित रूप से बनावटी तथा अविश्वसनीय ही होगा।
सामान्य और विशिष्ट के बीच का चक्कर या अमूर्त्त तथा मूर्त्त-देहली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में समाजशास्त्र के अध्यापक के रूप में लम्बे समय से इस विषय पर मेरी चिन्ता को दर्शाता है। चालीस वर्ष की अवधि में मैं समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों से लेकर भारत के समाजशास्त्र तक सामाजिक स्तरीकरण, राजनैतिक समाजशास्त्र और धर्म का समाजशास्त्र के माध्यम से मुख्यतः स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाता रहा हूँ बल्कि कभी-कभी स्नातक छात्रों को भी पढ़ाता रहा हूँ। स्नातकोत्तर छात्रों को कोई भी पाठ्यक्रम यह प्रश्न बताए बगैर की चर्चा के विषय क्या है, पढ़ाना असम्भव है। समाजशास्त्र क्या है और क्या होना चाहिए विषय पर मेरा अपना दृष्टिकोण इसी प्रकार की चर्चाओं से विकसित हुआ है।
यदि कोई व्यक्ति पढ़ाने और अनुसन्धान के बारे में गम्भीर है तो वह अपने दृष्टिकोण पर बोलने के बाद उस पर चर्चा को छोड़ नहीं सकता। उसको अन्य दृष्टिकोणों से भी इसे जोड़ना चाहिए, उसके अपने समकालीन तथा पूर्णकालीन लोगों के विचारों से। ऐसा करने में उसे स्थान और समय की किस सीमा तक जाना चाहिए।
समाजशास्त्र क्या है, यदि यह विचार, समाजशास्त्री क्या करते हैं इस विचार से अलग रखकर नहीं समझा जा सकता तो इस विषय पर अन्य अवधारणाओं को खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्री क्या करते हैं, स्वयं इस विषय पर काफी भेद हैं। समाजशास्त्र एक अनुभवाश्रित अध्ययन विषय है जिसका विकास न केवल नये विचारों और सिद्धान्तों के निर्माण पर ही निर्भर रहा है बल्कि नवीन आधार सामग्री के विश्लेषण तथा अन्वेषण पर भी निर्भर रहा है। जितना यह तथ्यों से जुड़ा रहा है, उतना ही विचारों से जुड़ा रहा है। समाजशास्त्रीय तर्क तभी उपयोगी होते हैं जब वे सामाजिक सम्बन्धों सामाजिक प्रक्रियाओं तथा विशेष स्थानों और समयों की सामाजिक संस्थाओं पर प्रकाश डालते हों।
बौद्धिक अध्ययन विषय होने के नाते समाजशास्त्र पश्चिम की तुलना में भारत में देरी से आया, यद्यपि अवधि लम्बी नहीं थी। पश्चिम में पहले तो यह विषय विश्वविद्यालयों से बाहर विकसित हुआ और बाद में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक इसने विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर लिया लेकिन अध्ययन विषय के रूप में इसका विकास स्वतन्त्रता के बाद ही हुआ। भारत में ऑगस्ट, काम्टे या हरबर्ट स्पेन्सर जैसे लेखकों के समकक्ष लेखक नहीं थे, जिन्होंने पश्चिमी में विश्वविद्यालयों से बाहर समाजशास्त्र की नींव डाली थी, हाँ, ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के पठन पाठन के प्रारम्भ होने से पहले सामाजिक विचारों में योगदान किया था लेकिन इसमें सन्देह है कि टैगोर और गाँधी जैसे विचारकों को सही रूप में समाजशास्त्री या प्रथम समाजशास्त्री तक भी कहा जाय।
क्योंकि वे इस क्षेत्र में प्रथम थे अतः यूरोपीयन समाजशास्त्रियों जैसे वेबर और दुर्खीम में स्वयं को सभी प्रकार के समाजों के विषय में लिखने को स्वतन्त्र समझा और सरलतम से जटिलतम समाजों के बारे में लिखा न कि केवल अपने समाज के बारे में। समूचे संसार के मानव समाजों की समूची परिधि में इस रुचि और उसकी ओर ध्यान ने ही समाजशास्त्र को अपनी प्रारम्भिक अवस्था में तुलनात्मक अध्ययन का रूप प्रदान किया न कि मात्र अनुभवाश्रित अध्ययन क्षेत्र के रूप में। भारत में समाजशास्त्रियों की रुचि काफी सीमित रही है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् के प्रारंभिक दशकों में उन्होंने भारतीय अध्ययनों तक ही सीमित कहने की जोखिम उठायी। यह सत्य है कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर ही तुलनात्मक अध्ययन के अवसर प्रदान करता है लेकिन विषय के अध्ययन का विकास भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा अपने समाज के अलावा अन्य समाजों पर अच्छे अनुभवाश्रित कार्य के अभाव में निःसन्देह बाधित रहा। इस व्यवसाय में नवागन्तुक हताशा महसूस करते हैं, जब वे देखते हैं कि पश्चिमी समाजशास्त्री सभी समाजों के विषय में मुक्तहस्त लिखते हैं जबकि उनके अपने देश में इस व्यवसाय में अग्रणी लोगों के पास भारत से बाहर के समाजों के बारे में बहुत कम कहने को है।
यदि हम समाजशास्त्र का मानवशास्त्र से अलग विचार करें तो हमें पता चलेगा कि पश्चिमी समाजशास्त्र के अध्येताओं में से अधिकतर की रुचि का केन्द्र पश्चिमी समाज ही रहा है। पूर्व पीढ़ी की एक अग्रणी पश्चिमी समाजशास्त्री ने इस प्रकार कहा है, ‘‘अधिकतम समाजशास्त्री समकालीन पश्चिमी समाज का अध्ययन करते हैं’’ (शिल्स, 1997:225)। यह अपेक्षाकृत अनलंकृत कथन इसी लेखक द्वारा विस्तृत रचना के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किये गये समाज मुख्यतः उनके अपने समाज रहे हैं, उन्होंने अपना अधिकतर ध्यान, अपने समकालीन समाजों और उनको भी बिल्कुल हाल के ही समय में दिया है, (शिल्प 1985:801)। यदि हम इसको ही इस सन्दर्भ का एक अच्छा कथन स्वीकार लें तब पश्चिमी और भारतीय समाजशास्त्रियों के बीच की परिपाटियों का अन्तर केवल मात्रा का ही हो सकता है। साथ ही इस अन्तर को नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता।
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपने तुलनात्मक झुकाव के बावजूद भी समाजशास्त्र के सिद्धान्त और व्यवहार जैसा कि हम आज तक उनके विषय में जानते हैं, पश्चिमी या यूरोपीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। कुछ हद तक यह अपरिहार्य है, क्योंकि अब तक यह विषय क्षेत्र अधिकतर विकसित स्वरूप को प्राप्त कर चुके है। न केवल आधार सामग्री बल्कि समाजशास्त्र की अवधारणाओं और श्रेणियों पर भी उन समाजों की छाप है, जिनमें सर्वप्रथम उनका निर्माण तथा प्रयोग हुआ। लेकिन सभी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं और श्रेणियों पर यह छाप उसी सीमा तक नहीं दिखाई देती। संरचना प्रक्रियाएँ संस्था और यहाँ तक प्रस्थिति और शक्ति जैसी अवधारणाएँ विशेष समाजों में उनके ऐतिहासिक स्वरूप से लेकर काफी हद तक पृथक की जा सकती है; परम्परा आधुनिकता और यहाँ तक कि तर्क संगतता जैसी अन्य अवधारणाएँ ऐसी पृथकता के लिये अधिक अवरोध सिद्ध हुई हैं। समाजशास्त्र और बौद्धिक अध्ययन विषय होने के स्तर से थोड़ा नीचे आ जायेगा। यदि इसके योग्यतम अध्येयता अपनी मूल अवधारणाओं से उनके मूल स्थान से पूर्वरूपेण पृथक् करने में योग्यतम हो जाएँ। समकालीन समाजशास्त्र में वास्तव में पश्चिमी पूर्वाग्रह मौजूद है, लेकिन यह इसको व्यापक रूप प्रदान करने या इन्हीं विचारों से घिरे रखने में कोई भूमिका अदा नहीं करता।
जहाँ तक सिद्धान्त और विधि का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को लेटलतीफ होने के फायदे और नुकसान दोनों मिले हैं। अध्यापन और अनुसन्धान में उन्हें अपने काम के लिये आवश्यक सभी मूल अवधारणाओं और श्रेणियों निर्माण में प्रारम्भ से ही संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और सबसे ऊपर, उन्हें उन्नीसवीं, शताब्दी के अपने यूरोपीय पूर्वजों की तरह समाजशास्त्र को बौद्धिक अध्ययन विषय के रूप में गम्भीरता से इसकी वैधता को स्थापित करने के लिये संघर्ष नहीं करना पड़ा। 1920 तक जब समाजशास्त्र भारत में आया तब तक इसने पनी वैधता तो स्थापित कर लिया था; और कुछ पश्चिमी विश्वविद्यालयों में इसके लिये स्थान बनाने का दावा करना आसान हो गया।
अवधारणाओं और विधियों की रचना और परिष्कृत में समय लगता है और प्रयास करना पड़ता है। जब समाजशास्त्रियों ने भारत में अपना कार्य प्रारम्भ किया तो उन्हें पता लगा कि उनके शिल्प में काम आने वाले कई औजार (साधन) पहले से ही गढ़े जा चुके हैं, इसलिये उनके समय और प्रयास की बचत हो गई। अनुसन्धान से अध्यापन में अधिक भारतीय समाजशास्त्री, पहले तो पश्चिम में विकसित और अब सर्वत्र उपलब्ध जाँच और विश्लेषण के साधन, कुछ कुछ यन्त्रवत्, प्रयोग करने के लिये तत्पर रहे हैं। ऐसा करने में उन्होंने अन्य गैर पश्चिमी देशों के समाजशास्त्रियों से भिन्न कार्य नहीं किया है, जैसे मैक्सिको या जापान आदि के।
लेकिन बौद्धिक कार्यों में जो बहुत आसान दिखाई देता है वह पेचीदा फन्दा भी हो सकता है। विश्वभर में उपलब्ध सभी साधन प्रत्येक सामाजिक और ऐतिहासिक सन्दर्भ में उपयुक्त नहीं होते अनुपयुक्त दशाओं में उनका यान्त्रिक प्रयोग तुच्छ तथा गुमराह करने वाले नतीजे दे सकता है। इस व्यवसाय में तैयार साधनों की उपलब्धता ने अवधारणाओं तथा विधि में नवीनता लाने के विचार को आघात पहुँचाया है और भारतीय समाजशास्त्रियों को सामान्य समाजशास्त्र से सम्बन्धित मामलों पर लिखने में संकोची बनाया है।
यहाँ प्रस्तुत निबन्ध में यह विचार निहित है कि सामान्य समाजशास्त्र केवल एक है और एक ही हो सकता है। यद्यपि यह मान्यता है कि लक्ष्यों और उद्देश्यों के एक ही वृहद ढाँचे में मौजूद विविध समाजशास्त्रीय परिपाटियों से उत्पन्न विविध स्वरूप भी इसमें शामिल हैं। विविध राष्ट्रीयताओं, सभ्यताओं धर्मों या विचारधाराओं के विभिन्न समाजशास्त्रों का होना न तो सम्भव, है न ही वांछनीय यद्यपि विविध कालों में स्थानों पर समाजशास्त्रीय परिपाटियों में राष्ट्रीय, धार्मिक और अन्य भिन्नताओं का लक्षित होना स्वाभाविक है। बौद्धिक अध्ययन विषय के रूप में समाजशास्त्र इन भिन्नताओं को बढ़ाने के बजाय घटाने का प्रयास करता है। चाहे पश्चिम या भारत में समाजशास्त्र जैसा मैं समझता हूँ, कोई विचारधारा नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है जाँच तथा विश्लेषण के समान स्तर पर राष्ट्रीय धार्मिक या वैचारिक भिन्नताओं के विचार के बिना सभी समाजों को समझना।
भारत के लिए एक वैकल्पिक समाज की खोज के कोई ठोस नतीजे नहीं निकले हैं और न ही भविष्य में उसकी कोई सम्भावना है। कुछ भी हो यह एक अनमना प्रयत्न रहा है और इसने देश में मानक समाजशास्त्र के अभ्यास को गम्भीरता से नज़रअन्दाज़ नहीं कया है। यह अभ्यास विगत पचास वर्षों में खूब फूलाफला है और अब इसमें अति विविधता आ गई है। जैसा कि मैं पहले ही संकेत कर चुका हूँ, इसका अनुभवाश्रित होने का केन्द्र पूर्णरूपेण भारतीय समाजों पर ही रहा है, यह विश्वभर में समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सभी साधनों का मुक्तहस्त से प्रयोग कर रहा है।
समकालीन भारत में समाजशास्त्रियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का सन्तुलित आकलन करना कठिन है और ऐसा कार्य करने के प्रयत्न के लिये यह कोई स्थान भी नहीं है। अधिकतर कार्य बहुत घटिया किस्म का है-नीरस पुनरावृत्ति वाला और नकल मात्र है-यद्यपि भारतीय समाजशास्त्री इस मामले में कोई अनोखे नहीं रहे हैं। साथ ही यदि एक लम्बी काल अवधि समूचे कार्य पर विचार करें तो हम भारतीय समाजशास्त्र की विविधता और सजीवता का मिलना संदिग्ध है जहाँ, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, विषय का विकास लम्बे समय से हो रहा है।
प्रायः यह कहा जाता है कि भारतीय समाजशास्त्र ने अमेरिकन, फ्रैंच या जर्मन समाजशास्त्र की तुलना में विशिष्ट पहचान नहीं प्राप्त की है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इसके अनेक कारण हैं। लेकिन समयावधि में ऐसी कोई विशिष्टता इसके सामान्य उपागम और उन्मुखता में उत्पन्न होती है तो यह धर्म राजनीति, असमानता आदि के ठोस परिवेश के सम्बन्ध में सम्भवत आ सकती है, अपेक्षाकृत किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के जो भारतीय मिट्टी में निहित हो ऐसे वैकल्पिक उपागम और विधि के।
गम्भीर बौद्धिक अध्ययन विषय के रूप में समाजशास्त्र अध्ययन समाज और उसकी संस्थाओं को कुछ मूल्यों को प्रदान करने के लिये पूर्व अनुमान लगा लेता है-यह अनुभाव एक समान रूप से सकारात्मक ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि समाज का विचार स्वयं चलन से बाहर हो गया है-(इनगोल्ड, 1990) यह देखना कठिन है कि मानव व्यवहार के प्रति समाजशास्त्रीय उपागम का ऐसे विचारों के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। शिल्प के द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा का विस्तार करते हुए कह सकते हैं कि समाजशास्त्र आधुनिक न होकर एक उत्तर आधुनिक अध्ययन विषय है।
उत्तर आधुनिकतावाद समाज की संस्थाओं को हल्का करके दर्शाता है, जबकि मेरे विचार में संस्थाओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय अध्ययन का केन्द्रीय विषय है। यहाँ लिये गये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवीय क्रिया प्रतिबन्धित और मुक्त दोनों साथ हैं। यह सत्य है कि सभी मानव क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है बल्कि सामाजिक क्रिया कमोवेश इसका विशिष्ट स्वरूप है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक क्रिया एक सामाजिक ढाँचे के भीतर ही होती है, जो कि कर्त्ता या अभिकर्त्ता की दृष्टि से एक सुविधा और पाबन्दी दोनों है। निःसन्देह कर्त्ता अपनी सामाजिक स्थिति को परिभाषित करने के लिए मुक्त होत है, लेकिन वह उस सामाजिक ढाँचे को अकेले नहीं बनाता जिसके भीतर वह स्वयं को स्थित करता है।
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या कम से कम वह जो यहाँ प्रस्तुत निबन्धों में धारण किया गया है, कल्पना के विपरीत है। काल्पनिक परिप्रेक्ष्य भारतीय मनीषियों सहित भारतीय बुद्धिजीवियों के लिये अत्यधिक आकर्षक रहा है। यह बात उस समाज में चौकाने वाली नहीं है जिसमें उसने सुना था-एक पानी में तैरने वाली औरत...। बिस्तर जैसे हवा में उड़ रहा था...नहीं...बिस्तर चिंगारियाँ फेंक रहा था...एक बेहद हसीन चेहरा। लंबी गर्दन...किल्यूपेटरा की तरह, तना हुआ हसीन गठा हुआ शरीर-जैसे कमान से तीर छूटने भर की देर हो। दो नंगे पाँव। जैसे पानी में लहराती दो नंगी हसीन डालियाँ....
इस प्रश्न का छोटा उत्तर देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है : समाजशास्त्र क्या है ? सम्भवत: यही बात अन्य विषयों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून के विषय में भी उतनी ही सही है। कोई भी बौद्धिक विषय पूर्ण रूप से निरूपित विषय सामग्री के साथ समापन की स्थिति में नहीं है, उसकी अवधारणाएँ व विधियाँ हमेशा-हमेशा के लिये परिभाषित नहीं है और न ही अन्य विषयों के साथ उसकी सीमाएँ अन्तिम रूप से बन्द हैं। संक्षेप में यह कहना कठिन है कि समाजशास्त्र क्या है, क्योंकि यह अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है; शायद यह कहना सरल होगा कि जीवन्त विषय के रूप में इसकी ख्याति कम होने के बाद यह क्या था।
समाजशास्त्र की औपचारिक परिभाषाओं की कोई कमी नहीं है। वास्तव में परिभाषाओं की संख्या और विविधता ही असमंजस का मुख्य स्रोत है। दुर्भाग्यवश एक औपचारिक परिभाषा केवल उन्हीं के काम की है जो पहले से ही विषय की मोटी रूप की जानकारी रखते हैं। नूतानाभ्यासी के लिये इसका महत्त्व कम ही होता है। यद्यपि यह प्रायः विद्वानों के बीच बहस में एक उपयोगी प्रस्थान बिन्दु का कार्य करता है जिनका इस विषय पर समान दृष्टिकोण नहीं है।
औपचारिक रूप में विषय की परिभाषा करने के बजाय कोई यह बात सीधे से कह सकता है कि समाजशास्त्र वह है जो समाजशास्त्री करते हैं’ यह विषय अब अपनी प्रारम्भिक स्थिति में नहीं है बल्कि पश्चिम में तो सौ वर्षों से भी अधिक समय से पनप रहा है और भारत में 1920 से। कई पीढ़ियों ने समाजशास्त्र पढ़ा है, पढ़ाया है और इसमें अनुसन्धान किया है। इस विषय के अपने व्यासायिक संगठन और अपनी सामयिक पत्रिकाएँ भी हैं। लेकिन जैसी कि अपेक्षा की जा सकती है, समाजशास्त्र का अभ्यास सभी स्थानों और सभी समयों में एक सा नहीं हुआ है। इसलिये यह कहना कि समाजशास्त्र वह है, जो समाजशास्त्र करते हैं, उत्तर की अपेक्षा प्रश्न को जन्म देना है।
समाजशास्त्री वास्तव में जो कुछ करते हैं वह बिल्कुल वह नहीं है, जो उनके विश्वास उनके बीच द्वन्दात्मक सम्बन्ध हैं, क्योंकि समाजशास्त्रियों के रूप में हमारा अभ्यास इस बात से बनता है कि हम और हमारे सहयोगी व्यवसायिक लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कि हमारे विचार से समाजशास्त्र क्या होना चाहिए ? अतः समाजशास्त्र क्या है ? इस बात का पता लगाने में व्यक्ति विषय के विस्तार, उद्देश्य और विधियों तथा विशिष्ट विषयों के वर्णन, समस्याओं और प्रकरणों के बीच ही घूमता रह जाता है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्रियों के दैनिक अभ्यास की वस्तुएँ होती हैं।
यहाँ एक साथ संकलित निबन्धों में मैंने, समाजशास्त्र क्या है ? विषय पर दोनों बिन्दुओं से विचार करने का प्रयत्न किया है, बार-बार आगे विचार करते हुए तथा एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिना ध्यान दिये भी। समाजशास्त्र के क्षेत्र और विधियों तथा मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति जैसे अन्य विषयों से इसके सम्बन्ध में विशेष गुणों पर भी सामान्य चर्चा भी इसमें है। लेकिन इसमें विशेष वर्णन भी है कि समाजशास्त्री वास्तव में क्या करते हैं, जब वे धर्म, राजनीति और असमानता पर अध्ययन करते हैं। दोनों प्रकार के वर्णन अन्तरसम्बद्ध हैं। यह अन्तरसम्बद्धता आंशिक ही हो सकी है, क्योंकि निबन्ध सोची समझी योजना के अनुसार नहीं लिखे गये थे। लेकिन सामान्य और विशिष्ट के बीच कठोर पृथकता बनाए रखने के लिये पहले से सोची गई योजना का परिणाम लगभग निश्चित रूप से बनावटी तथा अविश्वसनीय ही होगा।
सामान्य और विशिष्ट के बीच का चक्कर या अमूर्त्त तथा मूर्त्त-देहली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में समाजशास्त्र के अध्यापक के रूप में लम्बे समय से इस विषय पर मेरी चिन्ता को दर्शाता है। चालीस वर्ष की अवधि में मैं समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों से लेकर भारत के समाजशास्त्र तक सामाजिक स्तरीकरण, राजनैतिक समाजशास्त्र और धर्म का समाजशास्त्र के माध्यम से मुख्यतः स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाता रहा हूँ बल्कि कभी-कभी स्नातक छात्रों को भी पढ़ाता रहा हूँ। स्नातकोत्तर छात्रों को कोई भी पाठ्यक्रम यह प्रश्न बताए बगैर की चर्चा के विषय क्या है, पढ़ाना असम्भव है। समाजशास्त्र क्या है और क्या होना चाहिए विषय पर मेरा अपना दृष्टिकोण इसी प्रकार की चर्चाओं से विकसित हुआ है।
यदि कोई व्यक्ति पढ़ाने और अनुसन्धान के बारे में गम्भीर है तो वह अपने दृष्टिकोण पर बोलने के बाद उस पर चर्चा को छोड़ नहीं सकता। उसको अन्य दृष्टिकोणों से भी इसे जोड़ना चाहिए, उसके अपने समकालीन तथा पूर्णकालीन लोगों के विचारों से। ऐसा करने में उसे स्थान और समय की किस सीमा तक जाना चाहिए।
समाजशास्त्र क्या है, यदि यह विचार, समाजशास्त्री क्या करते हैं इस विचार से अलग रखकर नहीं समझा जा सकता तो इस विषय पर अन्य अवधारणाओं को खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्री क्या करते हैं, स्वयं इस विषय पर काफी भेद हैं। समाजशास्त्र एक अनुभवाश्रित अध्ययन विषय है जिसका विकास न केवल नये विचारों और सिद्धान्तों के निर्माण पर ही निर्भर रहा है बल्कि नवीन आधार सामग्री के विश्लेषण तथा अन्वेषण पर भी निर्भर रहा है। जितना यह तथ्यों से जुड़ा रहा है, उतना ही विचारों से जुड़ा रहा है। समाजशास्त्रीय तर्क तभी उपयोगी होते हैं जब वे सामाजिक सम्बन्धों सामाजिक प्रक्रियाओं तथा विशेष स्थानों और समयों की सामाजिक संस्थाओं पर प्रकाश डालते हों।
बौद्धिक अध्ययन विषय होने के नाते समाजशास्त्र पश्चिम की तुलना में भारत में देरी से आया, यद्यपि अवधि लम्बी नहीं थी। पश्चिम में पहले तो यह विषय विश्वविद्यालयों से बाहर विकसित हुआ और बाद में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक इसने विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर लिया लेकिन अध्ययन विषय के रूप में इसका विकास स्वतन्त्रता के बाद ही हुआ। भारत में ऑगस्ट, काम्टे या हरबर्ट स्पेन्सर जैसे लेखकों के समकक्ष लेखक नहीं थे, जिन्होंने पश्चिमी में विश्वविद्यालयों से बाहर समाजशास्त्र की नींव डाली थी, हाँ, ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के पठन पाठन के प्रारम्भ होने से पहले सामाजिक विचारों में योगदान किया था लेकिन इसमें सन्देह है कि टैगोर और गाँधी जैसे विचारकों को सही रूप में समाजशास्त्री या प्रथम समाजशास्त्री तक भी कहा जाय।
क्योंकि वे इस क्षेत्र में प्रथम थे अतः यूरोपीयन समाजशास्त्रियों जैसे वेबर और दुर्खीम में स्वयं को सभी प्रकार के समाजों के विषय में लिखने को स्वतन्त्र समझा और सरलतम से जटिलतम समाजों के बारे में लिखा न कि केवल अपने समाज के बारे में। समूचे संसार के मानव समाजों की समूची परिधि में इस रुचि और उसकी ओर ध्यान ने ही समाजशास्त्र को अपनी प्रारम्भिक अवस्था में तुलनात्मक अध्ययन का रूप प्रदान किया न कि मात्र अनुभवाश्रित अध्ययन क्षेत्र के रूप में। भारत में समाजशास्त्रियों की रुचि काफी सीमित रही है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् के प्रारंभिक दशकों में उन्होंने भारतीय अध्ययनों तक ही सीमित कहने की जोखिम उठायी। यह सत्य है कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर ही तुलनात्मक अध्ययन के अवसर प्रदान करता है लेकिन विषय के अध्ययन का विकास भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा अपने समाज के अलावा अन्य समाजों पर अच्छे अनुभवाश्रित कार्य के अभाव में निःसन्देह बाधित रहा। इस व्यवसाय में नवागन्तुक हताशा महसूस करते हैं, जब वे देखते हैं कि पश्चिमी समाजशास्त्री सभी समाजों के विषय में मुक्तहस्त लिखते हैं जबकि उनके अपने देश में इस व्यवसाय में अग्रणी लोगों के पास भारत से बाहर के समाजों के बारे में बहुत कम कहने को है।
यदि हम समाजशास्त्र का मानवशास्त्र से अलग विचार करें तो हमें पता चलेगा कि पश्चिमी समाजशास्त्र के अध्येताओं में से अधिकतर की रुचि का केन्द्र पश्चिमी समाज ही रहा है। पूर्व पीढ़ी की एक अग्रणी पश्चिमी समाजशास्त्री ने इस प्रकार कहा है, ‘‘अधिकतम समाजशास्त्री समकालीन पश्चिमी समाज का अध्ययन करते हैं’’ (शिल्स, 1997:225)। यह अपेक्षाकृत अनलंकृत कथन इसी लेखक द्वारा विस्तृत रचना के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किये गये समाज मुख्यतः उनके अपने समाज रहे हैं, उन्होंने अपना अधिकतर ध्यान, अपने समकालीन समाजों और उनको भी बिल्कुल हाल के ही समय में दिया है, (शिल्प 1985:801)। यदि हम इसको ही इस सन्दर्भ का एक अच्छा कथन स्वीकार लें तब पश्चिमी और भारतीय समाजशास्त्रियों के बीच की परिपाटियों का अन्तर केवल मात्रा का ही हो सकता है। साथ ही इस अन्तर को नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता।
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपने तुलनात्मक झुकाव के बावजूद भी समाजशास्त्र के सिद्धान्त और व्यवहार जैसा कि हम आज तक उनके विषय में जानते हैं, पश्चिमी या यूरोपीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। कुछ हद तक यह अपरिहार्य है, क्योंकि अब तक यह विषय क्षेत्र अधिकतर विकसित स्वरूप को प्राप्त कर चुके है। न केवल आधार सामग्री बल्कि समाजशास्त्र की अवधारणाओं और श्रेणियों पर भी उन समाजों की छाप है, जिनमें सर्वप्रथम उनका निर्माण तथा प्रयोग हुआ। लेकिन सभी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं और श्रेणियों पर यह छाप उसी सीमा तक नहीं दिखाई देती। संरचना प्रक्रियाएँ संस्था और यहाँ तक प्रस्थिति और शक्ति जैसी अवधारणाएँ विशेष समाजों में उनके ऐतिहासिक स्वरूप से लेकर काफी हद तक पृथक की जा सकती है; परम्परा आधुनिकता और यहाँ तक कि तर्क संगतता जैसी अन्य अवधारणाएँ ऐसी पृथकता के लिये अधिक अवरोध सिद्ध हुई हैं। समाजशास्त्र और बौद्धिक अध्ययन विषय होने के स्तर से थोड़ा नीचे आ जायेगा। यदि इसके योग्यतम अध्येयता अपनी मूल अवधारणाओं से उनके मूल स्थान से पूर्वरूपेण पृथक् करने में योग्यतम हो जाएँ। समकालीन समाजशास्त्र में वास्तव में पश्चिमी पूर्वाग्रह मौजूद है, लेकिन यह इसको व्यापक रूप प्रदान करने या इन्हीं विचारों से घिरे रखने में कोई भूमिका अदा नहीं करता।
जहाँ तक सिद्धान्त और विधि का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को लेटलतीफ होने के फायदे और नुकसान दोनों मिले हैं। अध्यापन और अनुसन्धान में उन्हें अपने काम के लिये आवश्यक सभी मूल अवधारणाओं और श्रेणियों निर्माण में प्रारम्भ से ही संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और सबसे ऊपर, उन्हें उन्नीसवीं, शताब्दी के अपने यूरोपीय पूर्वजों की तरह समाजशास्त्र को बौद्धिक अध्ययन विषय के रूप में गम्भीरता से इसकी वैधता को स्थापित करने के लिये संघर्ष नहीं करना पड़ा। 1920 तक जब समाजशास्त्र भारत में आया तब तक इसने पनी वैधता तो स्थापित कर लिया था; और कुछ पश्चिमी विश्वविद्यालयों में इसके लिये स्थान बनाने का दावा करना आसान हो गया।
अवधारणाओं और विधियों की रचना और परिष्कृत में समय लगता है और प्रयास करना पड़ता है। जब समाजशास्त्रियों ने भारत में अपना कार्य प्रारम्भ किया तो उन्हें पता लगा कि उनके शिल्प में काम आने वाले कई औजार (साधन) पहले से ही गढ़े जा चुके हैं, इसलिये उनके समय और प्रयास की बचत हो गई। अनुसन्धान से अध्यापन में अधिक भारतीय समाजशास्त्री, पहले तो पश्चिम में विकसित और अब सर्वत्र उपलब्ध जाँच और विश्लेषण के साधन, कुछ कुछ यन्त्रवत्, प्रयोग करने के लिये तत्पर रहे हैं। ऐसा करने में उन्होंने अन्य गैर पश्चिमी देशों के समाजशास्त्रियों से भिन्न कार्य नहीं किया है, जैसे मैक्सिको या जापान आदि के।
लेकिन बौद्धिक कार्यों में जो बहुत आसान दिखाई देता है वह पेचीदा फन्दा भी हो सकता है। विश्वभर में उपलब्ध सभी साधन प्रत्येक सामाजिक और ऐतिहासिक सन्दर्भ में उपयुक्त नहीं होते अनुपयुक्त दशाओं में उनका यान्त्रिक प्रयोग तुच्छ तथा गुमराह करने वाले नतीजे दे सकता है। इस व्यवसाय में तैयार साधनों की उपलब्धता ने अवधारणाओं तथा विधि में नवीनता लाने के विचार को आघात पहुँचाया है और भारतीय समाजशास्त्रियों को सामान्य समाजशास्त्र से सम्बन्धित मामलों पर लिखने में संकोची बनाया है।
यहाँ प्रस्तुत निबन्ध में यह विचार निहित है कि सामान्य समाजशास्त्र केवल एक है और एक ही हो सकता है। यद्यपि यह मान्यता है कि लक्ष्यों और उद्देश्यों के एक ही वृहद ढाँचे में मौजूद विविध समाजशास्त्रीय परिपाटियों से उत्पन्न विविध स्वरूप भी इसमें शामिल हैं। विविध राष्ट्रीयताओं, सभ्यताओं धर्मों या विचारधाराओं के विभिन्न समाजशास्त्रों का होना न तो सम्भव, है न ही वांछनीय यद्यपि विविध कालों में स्थानों पर समाजशास्त्रीय परिपाटियों में राष्ट्रीय, धार्मिक और अन्य भिन्नताओं का लक्षित होना स्वाभाविक है। बौद्धिक अध्ययन विषय के रूप में समाजशास्त्र इन भिन्नताओं को बढ़ाने के बजाय घटाने का प्रयास करता है। चाहे पश्चिम या भारत में समाजशास्त्र जैसा मैं समझता हूँ, कोई विचारधारा नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है जाँच तथा विश्लेषण के समान स्तर पर राष्ट्रीय धार्मिक या वैचारिक भिन्नताओं के विचार के बिना सभी समाजों को समझना।
भारत के लिए एक वैकल्पिक समाज की खोज के कोई ठोस नतीजे नहीं निकले हैं और न ही भविष्य में उसकी कोई सम्भावना है। कुछ भी हो यह एक अनमना प्रयत्न रहा है और इसने देश में मानक समाजशास्त्र के अभ्यास को गम्भीरता से नज़रअन्दाज़ नहीं कया है। यह अभ्यास विगत पचास वर्षों में खूब फूलाफला है और अब इसमें अति विविधता आ गई है। जैसा कि मैं पहले ही संकेत कर चुका हूँ, इसका अनुभवाश्रित होने का केन्द्र पूर्णरूपेण भारतीय समाजों पर ही रहा है, यह विश्वभर में समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सभी साधनों का मुक्तहस्त से प्रयोग कर रहा है।
समकालीन भारत में समाजशास्त्रियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का सन्तुलित आकलन करना कठिन है और ऐसा कार्य करने के प्रयत्न के लिये यह कोई स्थान भी नहीं है। अधिकतर कार्य बहुत घटिया किस्म का है-नीरस पुनरावृत्ति वाला और नकल मात्र है-यद्यपि भारतीय समाजशास्त्री इस मामले में कोई अनोखे नहीं रहे हैं। साथ ही यदि एक लम्बी काल अवधि समूचे कार्य पर विचार करें तो हम भारतीय समाजशास्त्र की विविधता और सजीवता का मिलना संदिग्ध है जहाँ, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, विषय का विकास लम्बे समय से हो रहा है।
प्रायः यह कहा जाता है कि भारतीय समाजशास्त्र ने अमेरिकन, फ्रैंच या जर्मन समाजशास्त्र की तुलना में विशिष्ट पहचान नहीं प्राप्त की है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इसके अनेक कारण हैं। लेकिन समयावधि में ऐसी कोई विशिष्टता इसके सामान्य उपागम और उन्मुखता में उत्पन्न होती है तो यह धर्म राजनीति, असमानता आदि के ठोस परिवेश के सम्बन्ध में सम्भवत आ सकती है, अपेक्षाकृत किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के जो भारतीय मिट्टी में निहित हो ऐसे वैकल्पिक उपागम और विधि के।
गम्भीर बौद्धिक अध्ययन विषय के रूप में समाजशास्त्र अध्ययन समाज और उसकी संस्थाओं को कुछ मूल्यों को प्रदान करने के लिये पूर्व अनुमान लगा लेता है-यह अनुभाव एक समान रूप से सकारात्मक ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि समाज का विचार स्वयं चलन से बाहर हो गया है-(इनगोल्ड, 1990) यह देखना कठिन है कि मानव व्यवहार के प्रति समाजशास्त्रीय उपागम का ऐसे विचारों के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। शिल्प के द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा का विस्तार करते हुए कह सकते हैं कि समाजशास्त्र आधुनिक न होकर एक उत्तर आधुनिक अध्ययन विषय है।
उत्तर आधुनिकतावाद समाज की संस्थाओं को हल्का करके दर्शाता है, जबकि मेरे विचार में संस्थाओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय अध्ययन का केन्द्रीय विषय है। यहाँ लिये गये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवीय क्रिया प्रतिबन्धित और मुक्त दोनों साथ हैं। यह सत्य है कि सभी मानव क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है बल्कि सामाजिक क्रिया कमोवेश इसका विशिष्ट स्वरूप है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक क्रिया एक सामाजिक ढाँचे के भीतर ही होती है, जो कि कर्त्ता या अभिकर्त्ता की दृष्टि से एक सुविधा और पाबन्दी दोनों है। निःसन्देह कर्त्ता अपनी सामाजिक स्थिति को परिभाषित करने के लिए मुक्त होत है, लेकिन वह उस सामाजिक ढाँचे को अकेले नहीं बनाता जिसके भीतर वह स्वयं को स्थित करता है।
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या कम से कम वह जो यहाँ प्रस्तुत निबन्धों में धारण किया गया है, कल्पना के विपरीत है। काल्पनिक परिप्रेक्ष्य भारतीय मनीषियों सहित भारतीय बुद्धिजीवियों के लिये अत्यधिक आकर्षक रहा है। यह बात उस समाज में चौकाने वाली नहीं है जिसमें उसने सुना था-एक पानी में तैरने वाली औरत...। बिस्तर जैसे हवा में उड़ रहा था...नहीं...बिस्तर चिंगारियाँ फेंक रहा था...एक बेहद हसीन चेहरा। लंबी गर्दन...किल्यूपेटरा की तरह, तना हुआ हसीन गठा हुआ शरीर-जैसे कमान से तीर छूटने भर की देर हो। दो नंगे पाँव। जैसे पानी में लहराती दो नंगी हसीन डालियाँ....
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i