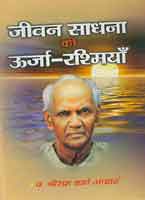|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> मनःस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले मनःस्थिति बदले तो परिस्थिति बदलेश्रीराम शर्मा आचार्य
|
421 पाठक हैं |
||||||
मनःस्थिति बदले तो परिस्थिति बदलें...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
युग धर्म का परिपालन अनिवार्य
छोटे बच्चों के कपड़े किशोरों के लिए फिट नहीं बैठते और किशोरों के लिए
सिलवाए गए कपड़ों से प्रौढ़ों का काम नहीं चलता। आयु वृद्धि के साथ-साथ
परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। भोजन ताजा बनाने से ही काम चलता है।
विद्यार्थी जैसे-जैसे कक्षा चढ़ते जाते हैं, वैसे ही वैसे उन्हें अगले
पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीदनी पड़ती है। सर्दी और गर्मी के कपड़े अलग तरह
के होते हैं। परिवर्तन होते चलने के साथ, तदनुकूल व्यवस्था बनाते रहना भी
एक प्रकार से अनिवार्य है।
समय सदा एक जैसा नहीं रहता। वह बदलता एवं आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार नए नियम निर्धारण भी करने पड़ते हैं। आदिम काल में मनुष्य बिना वस्त्रों के ही रहता था। मध्यकाल में धोती और दुपट्टा दो ही, बिना सिले वस्त्र काम आने लगे थे। प्रारंभ में अनगढ़ औजारों-हथियारों से ही काम चल जाता था। मध्यकाल में भी धनुष बाण और ढाल- तलवार ही युद्ध के प्रमुख उपकरण थे, अब आग्नेयास्त्रों के बिना काम चल ही नहीं सकता। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं और फिर उनके समाधान खोजने पड़ते हैं।
प्राचीनकाल के वर्णाश्रम पर आधारित प्रायः सभी विभाजन बदल गए। अब उसका स्थान नई व्यवस्था ने ले लिया है। दो सौ वर्ष पुराने समय में काम आने वाली पोशाकों का अब कहीं-कहीं प्रदर्शनिकों के रूप में ही अस्तित्व दीख पड़ता है। जब साइकिलें चली थीं तब अगला पहिया बहुत बड़ा और पिछला बहुत छोटा था। अब उनका दर्शन किन्हीं पुरातन प्रदर्शनियों में ही दीख पड़ता है। कुदाली से जमीन खोद कर खेती करना किसी समय खेती का प्रमुख आधार रहा होगा, पर अब तो सुधरे हुए हल ही काम आते हैं। उन्हें जानवरों या मशीनों द्वारा चलाया जाता है। लकड़ियाँ घिसकर आग पैदा करने की प्रथा मध्यकाल में थी, पर अब तो माचिस का प्रचलन हो जाने पर कोई भी उस कष्टसाध्य प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार न होगा।
विकास क्रम में ऐसे बदलाव अनायास ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस परिवर्तन क्रम को रोका नहीं जा सकता। जो पुरानी प्रथाओं पर ही अड़ा रहेगा उसे न केवल घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा, वरन् उपहासास्पद भी बनना पड़ेगा।
मान्यताएँ, विचारणाएँ, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादाओं में बँधे रहे हैं और उनमें प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। स्मृतियाँ और सूत्र ग्रंथ भी भिन्न-भिन्न ऋषियों ने अपने समय के अनुसार, नए सिरे से लिखने की आवश्यकता समझी और वह सुधार ही जनजीवन में मान्यता प्राप्त करता रहा। इसका कारण उन निर्माताओं में परस्पर विवाद या विग्रह होना नहीं है, वरन् यह है कि बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म प्रचलन के स्वरूप में भी भारी हेर-फेर किया गया।
प्राचीनकाल में जमीन में गड्ढा खोदकर गुफाएँ विनिर्मित कर ली जाती थीं। बाद में कुटिया बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक लगा। इसके बाद अब तो भूमि संबंधी कठिनाई को देखते हुए, आगे बढ़कर सीमेंट और लोहे के सहारे भवन निर्माण का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। लकड़ी और गोबर से ईंधन की आवश्यकता पूरी करने की प्रथा पिछले दिनों रही है, पर उनका पर्याप्त मात्रा में न मिलना, इस प्रयास को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है कि गोबर गैस या खनिज गैस से काम लिया जाए। जहाँ इफरात है, वहाँ बिजली से भी ईंधन का काम लिया जा रहा है। खनिज तेल भी किसी प्रकार उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। अब तो सूर्य की धूप भी ईंधन की जगह प्रयुक्त होने लगी है। इन परिवर्तनों में आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार होते चलने की उक्ति ही सार्थक सिद्ध होती है।
समय पीछे नहीं लौटता, वह निरंतर आगे ही बढ़ता है। उसके साथ ही मान्यताओं में, प्रचलनों में भी परिवर्तन होता चलता है। ऐसा आग्रह कोई कदाचित् ही करता हो, कि जो पहले दिनों माना या किया जाता रहा है, वही पत्थर की तरह सदा सर्वदा जारी रहना चाहिए। ऐसे दुराग्रही तो शायद बिजली का प्रयोग करने और नल का पानी पीने से भी ऐतराज कर सकते हैं ? उन्हें शायद गुफा बनाकर रहने का भी आग्रह हो, क्योंकि पूर्वपुरुषों ने निवास के लिए उसी प्रक्रिया को सरल समझा था।
कभी मिट्टी के खपरों पर लेखन काम लिया जाता था, बाद में चमड़े, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लेखन कार्य चलने लगा। कुछ दिनों हाथ का बना कागज भी चला, पर अब तो सर्वत्र मिलों का बना कागज ही काम में आता है। हाथ से ग्रंथों की नकल करने का उपक्रम लंबे समय तक चलता रहा है, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधाएँ छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तब रेल मोटर आदि की आवश्यकता न थी, पर अब तो उनके बिना परिवहन और यातायात का काम नहीं चलता। डाक से पत्र व्यवहार करने की अपेक्षा घोड़ों पर लंबी दूरी पर संदेश भेजने की प्रथा अब एक प्रकार से समाप्त ही हो गई है।
परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नए आयाम विकसित करने की आवश्यकता अब इतनी अनिवार्य हो गई है कि उसे अपनाने से कदाचित् ही कोई इनकार करता हो ? घड़ी का उपयोग करने से अब कदाचित् ही कहीं एतराज किया जाता हो ? समय हर किसी को बाधित करता है कि युग धर्म पहचाना जाए और उसे अपनाने में आनाकानी न की जाए। नीति-निष्ठा एवं समाज निष्ठा के संबंध में शाश्वत हो सकता है, पर रीति रिवाजों, क्रिया कलापों, उपकरणों, आदि प्रचलित नियम अनुशासन के संबंध में पुरातन परपाटी के भक्त तो कहे जा सकते हैं, पर अपने अतिरिक्त और किसी को इसके लिए सहमत नहीं कर सकते कि लकीर के फकीर बने रहने में ही धर्म का पालन सन्निहित है, जो पुरातन काल में चलता रहा है, उसमें हेर-फेर करने की बात किसी को सोचनी ही नहीं चाहिए, ऐसा करने को अधर्म कहा जाएगा और उसे करने वाले पर पाप चढ़ेगा।
किसी भी भली-बुरी प्रथा को अपनी ओर पूर्वजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर उस पर अड़ा और डटा तो रहा जा सकता है, पर उसमें बुद्धिमानी का समावेश तनिक भी नहीं है। मनुष्य प्रगतिशील रहा है और रहेगा। वह सृष्टि के आदि से लेकर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरता हुआ आज की स्थिति तक पहुँचा है। यह क्रम आगे भी चलता ही रहने वाला है। पुरातन के लिए हठवादी बने रहना किसी भी प्रकार, किसी के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता। युग धर्म को अपनाकर ही मनुष्य आगे बढ़ता है और आगे भी उसके लिए तैयार रहेगा। समय का यह ऐसा तकाजा है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।
समय सदा एक जैसा नहीं रहता। वह बदलता एवं आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार नए नियम निर्धारण भी करने पड़ते हैं। आदिम काल में मनुष्य बिना वस्त्रों के ही रहता था। मध्यकाल में धोती और दुपट्टा दो ही, बिना सिले वस्त्र काम आने लगे थे। प्रारंभ में अनगढ़ औजारों-हथियारों से ही काम चल जाता था। मध्यकाल में भी धनुष बाण और ढाल- तलवार ही युद्ध के प्रमुख उपकरण थे, अब आग्नेयास्त्रों के बिना काम चल ही नहीं सकता। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं और फिर उनके समाधान खोजने पड़ते हैं।
प्राचीनकाल के वर्णाश्रम पर आधारित प्रायः सभी विभाजन बदल गए। अब उसका स्थान नई व्यवस्था ने ले लिया है। दो सौ वर्ष पुराने समय में काम आने वाली पोशाकों का अब कहीं-कहीं प्रदर्शनिकों के रूप में ही अस्तित्व दीख पड़ता है। जब साइकिलें चली थीं तब अगला पहिया बहुत बड़ा और पिछला बहुत छोटा था। अब उनका दर्शन किन्हीं पुरातन प्रदर्शनियों में ही दीख पड़ता है। कुदाली से जमीन खोद कर खेती करना किसी समय खेती का प्रमुख आधार रहा होगा, पर अब तो सुधरे हुए हल ही काम आते हैं। उन्हें जानवरों या मशीनों द्वारा चलाया जाता है। लकड़ियाँ घिसकर आग पैदा करने की प्रथा मध्यकाल में थी, पर अब तो माचिस का प्रचलन हो जाने पर कोई भी उस कष्टसाध्य प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार न होगा।
विकास क्रम में ऐसे बदलाव अनायास ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस परिवर्तन क्रम को रोका नहीं जा सकता। जो पुरानी प्रथाओं पर ही अड़ा रहेगा उसे न केवल घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा, वरन् उपहासास्पद भी बनना पड़ेगा।
मान्यताएँ, विचारणाएँ, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादाओं में बँधे रहे हैं और उनमें प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। स्मृतियाँ और सूत्र ग्रंथ भी भिन्न-भिन्न ऋषियों ने अपने समय के अनुसार, नए सिरे से लिखने की आवश्यकता समझी और वह सुधार ही जनजीवन में मान्यता प्राप्त करता रहा। इसका कारण उन निर्माताओं में परस्पर विवाद या विग्रह होना नहीं है, वरन् यह है कि बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म प्रचलन के स्वरूप में भी भारी हेर-फेर किया गया।
प्राचीनकाल में जमीन में गड्ढा खोदकर गुफाएँ विनिर्मित कर ली जाती थीं। बाद में कुटिया बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक लगा। इसके बाद अब तो भूमि संबंधी कठिनाई को देखते हुए, आगे बढ़कर सीमेंट और लोहे के सहारे भवन निर्माण का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। लकड़ी और गोबर से ईंधन की आवश्यकता पूरी करने की प्रथा पिछले दिनों रही है, पर उनका पर्याप्त मात्रा में न मिलना, इस प्रयास को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है कि गोबर गैस या खनिज गैस से काम लिया जाए। जहाँ इफरात है, वहाँ बिजली से भी ईंधन का काम लिया जा रहा है। खनिज तेल भी किसी प्रकार उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। अब तो सूर्य की धूप भी ईंधन की जगह प्रयुक्त होने लगी है। इन परिवर्तनों में आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार होते चलने की उक्ति ही सार्थक सिद्ध होती है।
समय पीछे नहीं लौटता, वह निरंतर आगे ही बढ़ता है। उसके साथ ही मान्यताओं में, प्रचलनों में भी परिवर्तन होता चलता है। ऐसा आग्रह कोई कदाचित् ही करता हो, कि जो पहले दिनों माना या किया जाता रहा है, वही पत्थर की तरह सदा सर्वदा जारी रहना चाहिए। ऐसे दुराग्रही तो शायद बिजली का प्रयोग करने और नल का पानी पीने से भी ऐतराज कर सकते हैं ? उन्हें शायद गुफा बनाकर रहने का भी आग्रह हो, क्योंकि पूर्वपुरुषों ने निवास के लिए उसी प्रक्रिया को सरल समझा था।
कभी मिट्टी के खपरों पर लेखन काम लिया जाता था, बाद में चमड़े, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लेखन कार्य चलने लगा। कुछ दिनों हाथ का बना कागज भी चला, पर अब तो सर्वत्र मिलों का बना कागज ही काम में आता है। हाथ से ग्रंथों की नकल करने का उपक्रम लंबे समय तक चलता रहा है, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधाएँ छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तब रेल मोटर आदि की आवश्यकता न थी, पर अब तो उनके बिना परिवहन और यातायात का काम नहीं चलता। डाक से पत्र व्यवहार करने की अपेक्षा घोड़ों पर लंबी दूरी पर संदेश भेजने की प्रथा अब एक प्रकार से समाप्त ही हो गई है।
परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नए आयाम विकसित करने की आवश्यकता अब इतनी अनिवार्य हो गई है कि उसे अपनाने से कदाचित् ही कोई इनकार करता हो ? घड़ी का उपयोग करने से अब कदाचित् ही कहीं एतराज किया जाता हो ? समय हर किसी को बाधित करता है कि युग धर्म पहचाना जाए और उसे अपनाने में आनाकानी न की जाए। नीति-निष्ठा एवं समाज निष्ठा के संबंध में शाश्वत हो सकता है, पर रीति रिवाजों, क्रिया कलापों, उपकरणों, आदि प्रचलित नियम अनुशासन के संबंध में पुरातन परपाटी के भक्त तो कहे जा सकते हैं, पर अपने अतिरिक्त और किसी को इसके लिए सहमत नहीं कर सकते कि लकीर के फकीर बने रहने में ही धर्म का पालन सन्निहित है, जो पुरातन काल में चलता रहा है, उसमें हेर-फेर करने की बात किसी को सोचनी ही नहीं चाहिए, ऐसा करने को अधर्म कहा जाएगा और उसे करने वाले पर पाप चढ़ेगा।
किसी भी भली-बुरी प्रथा को अपनी ओर पूर्वजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर उस पर अड़ा और डटा तो रहा जा सकता है, पर उसमें बुद्धिमानी का समावेश तनिक भी नहीं है। मनुष्य प्रगतिशील रहा है और रहेगा। वह सृष्टि के आदि से लेकर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरता हुआ आज की स्थिति तक पहुँचा है। यह क्रम आगे भी चलता ही रहने वाला है। पुरातन के लिए हठवादी बने रहना किसी भी प्रकार, किसी के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता। युग धर्म को अपनाकर ही मनुष्य आगे बढ़ता है और आगे भी उसके लिए तैयार रहेगा। समय का यह ऐसा तकाजा है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।
गरीबों द्वारा अमीरी का आडम्बर
रोम के एक दार्शनिक के मन में भारत की महत्ता देखने की ललक उठी। समय और धन
खर्च करके आए, घूमे और रहे। लौटे तो उदास थे। साथियों ने पूछा तो केवल
इतना कहा, ‘‘भारत में जहाँ गरीब अधिकांश रहते हैं,
वहाँ भी
अमीरों जैसा स्वाँग बनाया जाता है।’’ ऐसा ही कथन एक
जापानी
शिष्ट मंडल का भी है। उन्होंने भ्रमण के बाद कहा था, यहाँ अमीरी का माहौल
है, परंतु उसकी छाया में पिछड़े गए-गुजरे लोग रहते हैं।
प्रश्न उठता है कि ऐसी विडम्बना क्यों कर बन पड़ी ? अमीरों में जो दुर्गुण पाए जाते हैं, वे यहाँ जन-जन में विद्यमान हैं, किंतु प्रगतिशीलों में जो सद्गुण पाए जाने चाहिए, उनका बुरी तरह अभाव है। इस कमी के रहते गरीबी ही नहीं, अशिक्षा, गंदगी, कामचोरी जैसी अनेकों पिछड़ेपन की निशानियाँ बनी ही रहेंगी। वे किसी बाहरी संपत्ति के बलबूते दूर न हो सकेंगी। भूमि की अपनी उर्वरता न रहे, तो बीज बोने वाला, सिंचाई- रखवाली करने वाला भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त न कर सकेगा।
मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है। वह जीवंत स्तर का हो तो उसमें वह खेत-उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदाएँ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकती हैं, पर चट्टान पर हरियाली कैसे उगे ? व्यक्तित्व अनायास ही नहीं बन जाता। वह इर्द-गिर्द के वातावरण से अपने लिए प्राणवायु खींचता है। जहाँ विषाक्तता छाई हुई हो, वहाँ साँस लेना तक कठिन हो जाएगा। लंबे समय तक जीवित रहने की बात तो वहाँ बन ही कैसे पड़ेगी ?
लंबे समय तक दुर्बलता के शिकार रहने वालों को धीरे-धीरे कई प्रकार की बीमारियाँ घेरती और दबोचती रहती हैं। छूत की बीमारियाँ एक से दूसरों को लगती और भले चंगों को चपेट में लेती चली जाती हैं। लंबे समय की गुलामी और अवांछनीयता स्तर की मूढ़ मान्यताओं दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में भी यही बात है। वे यदि निर्बाध गति से बढ़ती रहें, तो किसी भी समुदाय को खोखला किए बिना नहीं रहतीं।
देश की दरिद्रता प्रख्यात है। अशिक्षा, गंदगी और कुटेबों की बात भी छिपी हुई नहीं है। पर इस बात को समझने में जरा अधिक जोर लगाना पड़ेगा कि भारत में अमीरी का प्रदर्शन क्यों होता है ? यहां अमीरों के साथ जुड़े हुए, प्रमुख दीख पड़ने वाले काले पक्ष को विशेष रूप से देखना होगा। यों इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। अमीरी सदा अवांछनीयताएँ ही उत्पन्न नहीं करतीं। सदुपयोग कर सकने वाले, उसका अपने तथा दूसरों के लिए समुचित लाभ भी उठा लेते हैं, पर आमतौर से वैसा कुछ नहीं बन पड़ता।
प्रश्न उठता है कि ऐसी विडम्बना क्यों कर बन पड़ी ? अमीरों में जो दुर्गुण पाए जाते हैं, वे यहाँ जन-जन में विद्यमान हैं, किंतु प्रगतिशीलों में जो सद्गुण पाए जाने चाहिए, उनका बुरी तरह अभाव है। इस कमी के रहते गरीबी ही नहीं, अशिक्षा, गंदगी, कामचोरी जैसी अनेकों पिछड़ेपन की निशानियाँ बनी ही रहेंगी। वे किसी बाहरी संपत्ति के बलबूते दूर न हो सकेंगी। भूमि की अपनी उर्वरता न रहे, तो बीज बोने वाला, सिंचाई- रखवाली करने वाला भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त न कर सकेगा।
मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है। वह जीवंत स्तर का हो तो उसमें वह खेत-उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदाएँ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकती हैं, पर चट्टान पर हरियाली कैसे उगे ? व्यक्तित्व अनायास ही नहीं बन जाता। वह इर्द-गिर्द के वातावरण से अपने लिए प्राणवायु खींचता है। जहाँ विषाक्तता छाई हुई हो, वहाँ साँस लेना तक कठिन हो जाएगा। लंबे समय तक जीवित रहने की बात तो वहाँ बन ही कैसे पड़ेगी ?
लंबे समय तक दुर्बलता के शिकार रहने वालों को धीरे-धीरे कई प्रकार की बीमारियाँ घेरती और दबोचती रहती हैं। छूत की बीमारियाँ एक से दूसरों को लगती और भले चंगों को चपेट में लेती चली जाती हैं। लंबे समय की गुलामी और अवांछनीयता स्तर की मूढ़ मान्यताओं दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में भी यही बात है। वे यदि निर्बाध गति से बढ़ती रहें, तो किसी भी समुदाय को खोखला किए बिना नहीं रहतीं।
देश की दरिद्रता प्रख्यात है। अशिक्षा, गंदगी और कुटेबों की बात भी छिपी हुई नहीं है। पर इस बात को समझने में जरा अधिक जोर लगाना पड़ेगा कि भारत में अमीरी का प्रदर्शन क्यों होता है ? यहां अमीरों के साथ जुड़े हुए, प्रमुख दीख पड़ने वाले काले पक्ष को विशेष रूप से देखना होगा। यों इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। अमीरी सदा अवांछनीयताएँ ही उत्पन्न नहीं करतीं। सदुपयोग कर सकने वाले, उसका अपने तथा दूसरों के लिए समुचित लाभ भी उठा लेते हैं, पर आमतौर से वैसा कुछ नहीं बन पड़ता।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i