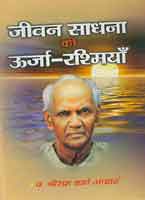|
पुराण एवं उपनिषद् >> प्रज्ञा पुराण भाग 3 प्रज्ञा पुराण भाग 3श्रीराम शर्मा आचार्य
|
90 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है परिवार खंड.....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्राक्कथन
भारतीय इतिहास-पुराणों मे ऐसे अगणित उपख्यान हैं, जिनमें मनुष्य के सम्मुख
आने वाली अगणित समस्याओं के समाधान विद्यमान है। उन्हीं में से सामयिक
परिस्थित एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ का ऐसा चयन किया गया गया
है, जो युद्ध समस्याओं के समाधान में आज की स्थिति के अनुरूप योगदान दे
सकें।
सर्वविदित है कि दार्शनिक और विवेचनात्मक प्रवचन-प्रतिपादित उन्हीं के गले उतरने हैं, जिसकी मनोभूमि सुवकसित है, परन्तु कथानकों की यह विशेषता है कि बाल, वृद्ध नर-नारी, शिक्षित-अशिक्षित सभी की समझ में आते हैं और उनके आधार पर ही किसी निष्कर्ष तक पहुँच सकना सम्भव होता है। लोकरंजन के साथ लोकमंगल का यह सर्वसुलभ लाभ है।
कथा-सहित्य की लोकप्रियता के संबंध में कुछ कहना व्यर्थ होगा। प्राचीन काल में 18 पुराण लिखे गए। उनसे भी काम न चला तो 18 उपपुराणों की रचना हुई। इन सब में कुल मिलाकर 10,000,000 श्लोक हैं, जबकि चारों वेदों में मात्र 20 हजार मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त भी संसार भर में इतना कथा साहित्य सृजा गया है कि उन सबको तराजू के पलड़े पर रखा जाए और अन्य साहित्य को दूसरे पर कथाऐं भी भारी पड़ेंगी।
समय परिवर्तनशील है। उसकी परिस्थितियाँ, मान्यताएं, प्रथाऐं, समस्याऐं एवं आवश्यकताऐं भी बदलती रहती हैं। तदनुरुप ही उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। इस आश्वत सृष्टिक्रम को ध्यान में रखते हुए ऐसे युग साहित्य की आवश्यकता पड़ती रही है, जिसमें प्रस्तुत प्रसंगो प्रकाश मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनेकानेक मनःस्थिति वालों के लिए उनकी परिस्थिति के अनुरूप समाधान ढूँढ़ निकालने में सुविधा दे सकने की दृष्टि से इस प्रज्ञा पुराण की रचना की गई, इसे चार खण्डों में प्रकाशित किया गया है।
प्रथम किस्त में प्रज्ञा पुराण के पाँच खण्ड प्रकाशित किए जा रहे हैं। प्रथम खण्ड का प्रथम संस्करण तो आज से चार वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। तदुपरान्त उसकी अनेकों आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। अब चार खण्ड एक साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इतने सुविस्तृत सृजन के लिए इन दिनों की एकान्त साधना में अवकाश भी मिल गया था। भविष्य का हमारा कार्यक्रम एवं जीवन काल अनिश्चित है। लेखनी तो सतत क्रियाशील रहेगी, चिन्तन हमारा ही सक्रिय रहेगा, हाथ भले ही किन्हीं के भी हों, यदि अवसर मिल सका, तो और भी अनेकों खण्ड प्रकाशित होते चले जायेंगे।
इन पाँच खण्डों में समग्र मानव धर्म के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त इतिहास-पुराणों की कथाएं है। इनमें अन्य धर्मालम्बियों के क्षेत्र में प्रचलित कथाओं का भी समावेश है, पर वह नगण्य सा ही है। बन पड़ा तो अगले दिनों अन्य धर्मों में प्रचलित कथानकों के भी संकलन इसी दृष्टि से चयन किए जाएँगे जैसे कि इस पहली पाँच खण्डों की प्रथम किस्त में किया गया है। कामना तो यह है कि युग पुराण के प्रज्ञा-पुराणों के भी पुरातन 18 खण्डों का सृजन बन पड़े।
संस्कृत श्लोंकों तथा उसके अर्थों के उपनिषद् पक्ष के साथ उसकी व्याख्या एवं कथानकों के प्रयोजनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास इनमें किया गया है। वस्तुतः इसमें युग दर्शन का नर्म निहित है। सिद्धांन्तों एवं तथ्यों को महत्व देने वालों के लिए यह अंग भी समाधानकारक होगा। जो संस्कृति नहीं जानते, उनके लिए अर्थ व उसकी पढ़ लेने से भी काम चल सकता है। इन श्लोकों की रचना नवीन है, पर जिस तत्यों का समावेश किया गया है, वे शाश्वत हैं।
प्रस्तुत ग्रन्थ का पठन निजी स्वास्थ्य के रूप में भी किया जा सकता है और सामूहिक सत्संग के रूप में भी। रात्रि के समय पारिवारिक लोक शिक्षण की दृष्टि से भी इसका उपयोग हो सकता है। बच्चे कथाऐं सुनने को उत्सुक रहते हैं। बड़ो को धर्म परम्पराऐं समझने की इच्छा रहती है। इनकी पूर्ति भी घर में इस आधार पर कथा क्रम और समय निर्धारित करके की जा सकती है।
कथा आयोजनों की समूहिक धर्मानुष्ठान के रूप में भी सम्पन्न किए जाने की परम्परा है। उस आधार पर भी इस कथावाचन का प्रयोग हो सकता है। आरम्भ का एक दिन वेद पूजन, व्रत धारण, महात्म्य आदि के मंगलाचरण में लगाया जा सकता है। चार दिन में चार खण्डों का सार संक्षेप, प्रातः और सायंकाल की दो बैठकों में सुनाया जा सकता है। अन्तिम दिन पूर्णाहुति का सामूहिक समारोह हो। बन पड़े तो अमृतशन (उबले धान्य, खीर, खिचड़ी आदि) कि व्यवस्था कि जा सकती है और विसर्जन शोभा यात्रा मिशन के बैनरो सहित निकाली जा सकती है। प्रज्ञा मिशन के प्रतिभोजों में अमृताशन कि परम्परा इसलिए रखी गयी है कि वह मात्र उबलने के कारण बनाने में सुगण, लागत में करते हुए मनुष्य मात्र को एक बिरादरी बनाने के लक्ष्य की ओर क्रमशः कदम बढ़ सकने का पथ-प्रशस्त करता है।
लोक शिक्षण के लिए गोष्ठियों-समारोहों में प्रवचनों-वक्तृताओं का आवश्यकता पड़ती है। उन्हें ही चुना जाने का वक्ता को पलायन करना पड़ता है। जिसकी कठिनाई का समाधान इस ग्रन्थ से ही हो सकता है। विवेचनों, प्रसंगों के साथ कथानकों का समन्वय करते-चलने पर वक्त के पास इतनी बड़ी निधि हो जाती है कि उसे महीनों कहता रहे। न कहने वाला पर भार पड़े, न सुनने वाले पर भार पड़े, न सुनने वाले ऊबें। इस दृष्टि के युग सृजेताओं के लिए लोक शिक्षण का एक उपयुक्त आधार उपलब्ध होता है। प्रज्ञा-पीठों और प्रज्ञा संस्थानों में तो ऐसे कथा प्रसंग नियमित रूप से चलने ही चाहिए ऐसे आयोजन एक स्थान या मुहल्ले में अदल-बदल के भी किए जा सकते हैं ताकि युग सन्देश को अधिकाधिक लोग निरटवर्ती स्थान में जाकर सरलतापूर्वक सुन सकें। ऐसे ही विचार इस सृजन के साथ-साथ मन में उठते रहे हैं, जिन्हें पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है।
प्रज्ञा पुराण के इस तीसरे खण्ड में एक ऐसे प्रसंग को लिया गया है, जो हमारे दैनंदिन जीवन का अंग है, जिसकी उपेक्षा के कारण आज चारों ओर कलह-विग्रह खड़े दृष्टिगोचर होते हैं। गृहस्थ जीवन, सह जीवन, पारिवारिकता की धुरी पर ही इस विश्व परिवार का समग्र ढांचा विनिर्मित है। मनुष्य जीवन की यह अवधि ऐसी है, जिस पर यदि सर्वाधिक ध्यान दिया जा सके, तो मानव में देवत्व एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण की द्विविध उद्देश्य भली-भाँति पूरे होते रह सकते हैं। सतयुग के मूल में यही ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का दर्शन समाहित नजर आता है।
परिवार संस्था के विभिन्न पक्षों तथा दांपत्य जीवन, गृहस्थ दायित्व, नारी, शिशु, वृद्धजन, सुसंस्कारिता संवर्धन एवं अंत में विश्व परिवार को इस खंड में कथा-उपाख्यानों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सुग्रह्य ढंग से प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। सभी परिवारों में पढ़ी-पढ़ाई जाने वाली गीता-उपनिष्द् सार के रूप में समझा जा सकता है।
इस समग्र प्रतिपादन में जहां कहीं अनुपयुक्तता, लेखन या मुद्रण की भूल दृष्टिगोचर हो, उन्हें विज्ञजन सूचित करने का अनुग्रह करें ताकि अगले संस्करणों में संशोदन किया जा सके।
सर्वविदित है कि दार्शनिक और विवेचनात्मक प्रवचन-प्रतिपादित उन्हीं के गले उतरने हैं, जिसकी मनोभूमि सुवकसित है, परन्तु कथानकों की यह विशेषता है कि बाल, वृद्ध नर-नारी, शिक्षित-अशिक्षित सभी की समझ में आते हैं और उनके आधार पर ही किसी निष्कर्ष तक पहुँच सकना सम्भव होता है। लोकरंजन के साथ लोकमंगल का यह सर्वसुलभ लाभ है।
कथा-सहित्य की लोकप्रियता के संबंध में कुछ कहना व्यर्थ होगा। प्राचीन काल में 18 पुराण लिखे गए। उनसे भी काम न चला तो 18 उपपुराणों की रचना हुई। इन सब में कुल मिलाकर 10,000,000 श्लोक हैं, जबकि चारों वेदों में मात्र 20 हजार मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त भी संसार भर में इतना कथा साहित्य सृजा गया है कि उन सबको तराजू के पलड़े पर रखा जाए और अन्य साहित्य को दूसरे पर कथाऐं भी भारी पड़ेंगी।
समय परिवर्तनशील है। उसकी परिस्थितियाँ, मान्यताएं, प्रथाऐं, समस्याऐं एवं आवश्यकताऐं भी बदलती रहती हैं। तदनुरुप ही उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। इस आश्वत सृष्टिक्रम को ध्यान में रखते हुए ऐसे युग साहित्य की आवश्यकता पड़ती रही है, जिसमें प्रस्तुत प्रसंगो प्रकाश मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनेकानेक मनःस्थिति वालों के लिए उनकी परिस्थिति के अनुरूप समाधान ढूँढ़ निकालने में सुविधा दे सकने की दृष्टि से इस प्रज्ञा पुराण की रचना की गई, इसे चार खण्डों में प्रकाशित किया गया है।
प्रथम किस्त में प्रज्ञा पुराण के पाँच खण्ड प्रकाशित किए जा रहे हैं। प्रथम खण्ड का प्रथम संस्करण तो आज से चार वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। तदुपरान्त उसकी अनेकों आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। अब चार खण्ड एक साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इतने सुविस्तृत सृजन के लिए इन दिनों की एकान्त साधना में अवकाश भी मिल गया था। भविष्य का हमारा कार्यक्रम एवं जीवन काल अनिश्चित है। लेखनी तो सतत क्रियाशील रहेगी, चिन्तन हमारा ही सक्रिय रहेगा, हाथ भले ही किन्हीं के भी हों, यदि अवसर मिल सका, तो और भी अनेकों खण्ड प्रकाशित होते चले जायेंगे।
इन पाँच खण्डों में समग्र मानव धर्म के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त इतिहास-पुराणों की कथाएं है। इनमें अन्य धर्मालम्बियों के क्षेत्र में प्रचलित कथाओं का भी समावेश है, पर वह नगण्य सा ही है। बन पड़ा तो अगले दिनों अन्य धर्मों में प्रचलित कथानकों के भी संकलन इसी दृष्टि से चयन किए जाएँगे जैसे कि इस पहली पाँच खण्डों की प्रथम किस्त में किया गया है। कामना तो यह है कि युग पुराण के प्रज्ञा-पुराणों के भी पुरातन 18 खण्डों का सृजन बन पड़े।
संस्कृत श्लोंकों तथा उसके अर्थों के उपनिषद् पक्ष के साथ उसकी व्याख्या एवं कथानकों के प्रयोजनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास इनमें किया गया है। वस्तुतः इसमें युग दर्शन का नर्म निहित है। सिद्धांन्तों एवं तथ्यों को महत्व देने वालों के लिए यह अंग भी समाधानकारक होगा। जो संस्कृति नहीं जानते, उनके लिए अर्थ व उसकी पढ़ लेने से भी काम चल सकता है। इन श्लोकों की रचना नवीन है, पर जिस तत्यों का समावेश किया गया है, वे शाश्वत हैं।
प्रस्तुत ग्रन्थ का पठन निजी स्वास्थ्य के रूप में भी किया जा सकता है और सामूहिक सत्संग के रूप में भी। रात्रि के समय पारिवारिक लोक शिक्षण की दृष्टि से भी इसका उपयोग हो सकता है। बच्चे कथाऐं सुनने को उत्सुक रहते हैं। बड़ो को धर्म परम्पराऐं समझने की इच्छा रहती है। इनकी पूर्ति भी घर में इस आधार पर कथा क्रम और समय निर्धारित करके की जा सकती है।
कथा आयोजनों की समूहिक धर्मानुष्ठान के रूप में भी सम्पन्न किए जाने की परम्परा है। उस आधार पर भी इस कथावाचन का प्रयोग हो सकता है। आरम्भ का एक दिन वेद पूजन, व्रत धारण, महात्म्य आदि के मंगलाचरण में लगाया जा सकता है। चार दिन में चार खण्डों का सार संक्षेप, प्रातः और सायंकाल की दो बैठकों में सुनाया जा सकता है। अन्तिम दिन पूर्णाहुति का सामूहिक समारोह हो। बन पड़े तो अमृतशन (उबले धान्य, खीर, खिचड़ी आदि) कि व्यवस्था कि जा सकती है और विसर्जन शोभा यात्रा मिशन के बैनरो सहित निकाली जा सकती है। प्रज्ञा मिशन के प्रतिभोजों में अमृताशन कि परम्परा इसलिए रखी गयी है कि वह मात्र उबलने के कारण बनाने में सुगण, लागत में करते हुए मनुष्य मात्र को एक बिरादरी बनाने के लक्ष्य की ओर क्रमशः कदम बढ़ सकने का पथ-प्रशस्त करता है।
लोक शिक्षण के लिए गोष्ठियों-समारोहों में प्रवचनों-वक्तृताओं का आवश्यकता पड़ती है। उन्हें ही चुना जाने का वक्ता को पलायन करना पड़ता है। जिसकी कठिनाई का समाधान इस ग्रन्थ से ही हो सकता है। विवेचनों, प्रसंगों के साथ कथानकों का समन्वय करते-चलने पर वक्त के पास इतनी बड़ी निधि हो जाती है कि उसे महीनों कहता रहे। न कहने वाला पर भार पड़े, न सुनने वाले पर भार पड़े, न सुनने वाले ऊबें। इस दृष्टि के युग सृजेताओं के लिए लोक शिक्षण का एक उपयुक्त आधार उपलब्ध होता है। प्रज्ञा-पीठों और प्रज्ञा संस्थानों में तो ऐसे कथा प्रसंग नियमित रूप से चलने ही चाहिए ऐसे आयोजन एक स्थान या मुहल्ले में अदल-बदल के भी किए जा सकते हैं ताकि युग सन्देश को अधिकाधिक लोग निरटवर्ती स्थान में जाकर सरलतापूर्वक सुन सकें। ऐसे ही विचार इस सृजन के साथ-साथ मन में उठते रहे हैं, जिन्हें पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है।
प्रज्ञा पुराण के इस तीसरे खण्ड में एक ऐसे प्रसंग को लिया गया है, जो हमारे दैनंदिन जीवन का अंग है, जिसकी उपेक्षा के कारण आज चारों ओर कलह-विग्रह खड़े दृष्टिगोचर होते हैं। गृहस्थ जीवन, सह जीवन, पारिवारिकता की धुरी पर ही इस विश्व परिवार का समग्र ढांचा विनिर्मित है। मनुष्य जीवन की यह अवधि ऐसी है, जिस पर यदि सर्वाधिक ध्यान दिया जा सके, तो मानव में देवत्व एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण की द्विविध उद्देश्य भली-भाँति पूरे होते रह सकते हैं। सतयुग के मूल में यही ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का दर्शन समाहित नजर आता है।
परिवार संस्था के विभिन्न पक्षों तथा दांपत्य जीवन, गृहस्थ दायित्व, नारी, शिशु, वृद्धजन, सुसंस्कारिता संवर्धन एवं अंत में विश्व परिवार को इस खंड में कथा-उपाख्यानों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सुग्रह्य ढंग से प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। सभी परिवारों में पढ़ी-पढ़ाई जाने वाली गीता-उपनिष्द् सार के रूप में समझा जा सकता है।
इस समग्र प्रतिपादन में जहां कहीं अनुपयुक्तता, लेखन या मुद्रण की भूल दृष्टिगोचर हो, उन्हें विज्ञजन सूचित करने का अनुग्रह करें ताकि अगले संस्करणों में संशोदन किया जा सके।
श्रीराम शर्मा आचार्य
प्रज्ञा पुराण
अथ प्रथमोऽध्यायः
परिवार-व्यवस्था प्रकरणम्
एकदा तु हरिद्वारे कुम्भपर्वणि पुण्यदे।
पर्वस्नानस्य सञ्जातः समारोहोऽत्र धार्मिकः।।1।।
देशान्तरादसंख्यास्ते सद्गृहस्थाश्च संगताः।
अवसरे च शुभे सर्वे पुण्यलाभाप्तिकाम्यया।।2।।
सद्भिर्महत्मभिश्चाऽपि संगत्यात्र परस्परम्।
सन्दर्भे समयोत्पन्नस्थितीनां विधयः शुभाः।।3।।
मृग्यास्तथा स्वसम्पर्कक्षेत्रजानां नृणामपि।
समस्यास्ताः समाधातुं सत्प्रवृत्तेर्विवर्धने।।4।।
मार्गदर्शनमिष्टं च राष्ट्रकल्याणकारकम्।
भागीरथीतटे तस्मात् सम्मर्दः सुमहानभूत्।।5।।
पुण्यारण्येषु गत्वा च सर्वे देवालयेष्वपि।
प्रेरणाः प्राप्रुवन्त्युच्चा धार्मिकास्ते जनः समे।।6।।
पर्वस्नानस्य सञ्जातः समारोहोऽत्र धार्मिकः।।1।।
देशान्तरादसंख्यास्ते सद्गृहस्थाश्च संगताः।
अवसरे च शुभे सर्वे पुण्यलाभाप्तिकाम्यया।।2।।
सद्भिर्महत्मभिश्चाऽपि संगत्यात्र परस्परम्।
सन्दर्भे समयोत्पन्नस्थितीनां विधयः शुभाः।।3।।
मृग्यास्तथा स्वसम्पर्कक्षेत्रजानां नृणामपि।
समस्यास्ताः समाधातुं सत्प्रवृत्तेर्विवर्धने।।4।।
मार्गदर्शनमिष्टं च राष्ट्रकल्याणकारकम्।
भागीरथीतटे तस्मात् सम्मर्दः सुमहानभूत्।।5।।
पुण्यारण्येषु गत्वा च सर्वे देवालयेष्वपि।
प्रेरणाः प्राप्रुवन्त्युच्चा धार्मिकास्ते जनः समे।।6।।
भावार्थ—
एक बार पुण्यदायी कुम्भपर्व पर हरिद्वार
क्षेत्र में
विशाल
पर्व-स्नान का धर्म समारोह हुआ। देश-देशांतरों से अगणित सद्गृहस्थ उस अवसर
पर पुण्य-लाभ पाने के लिए एकत्र हुए। साधु-संतों को भी परस्पर मिल-जुलकर
सामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में उपाय खोजने थे, साथ ही अपने संपर्क
क्षेत्र के लोगों की समस्यायें सुलझाने एवं सत्प्रवृत्तियाँ बढ़ाने के
संदर्भ में राष्ट्र-कल्याणकारी मार्गदर्शन भी करना था। भागीरथी के तट पर
अपार भीड़ थी, तीर्थ आरण्यकों और देवालयों में पहुँचकर धर्मप्रेमी
उच्चस्तरीय प्रेरणाएँ प्राप्त कर रहे थे।।5-6।।
व्याख्या—
कुम्भ आदि पर्वों, तीर्थस्थानों पर भारी
संख्या में
संतों
और गृहस्थों के संगम होते रहने के प्रमाण स्थान-स्थान पर मिलते रहते हैं।
मोटी मान्यता यह है कि समय विशेष पर स्नान आदि का विशेष पुण्य
प्राप्त करने के लिए ही लोग पहुँचते हैं। वह भी एक पुण्य हो
सकता
है; किंतु प्रस्तुत संदर्भ में अनेक महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों की चर्चा की
गयी है।
अनादिकाल से ऋषियों का, संतों का एक देशव्यापी तंत्र कार्य करता रहा है। अपनी-अपनी साधनाओं से उपलब्ध महत्त्वपूर्ण सूत्रों एकीकरण, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप धर्म-तंत्र के क्रियात्मक सूत्रों का मनिर्धार्ण, सामाजिक-राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में सर्वसम्मत हल तथा तदनुरूप मार्गदर्शन की व्यवस्था जैसे महत्त्वपूर्ण पुण्यदायी कार्य ऐसे अवसरों पर किए जाते थे। इनका लाभ जनसामान्य भी उठाते थे और जन-जन तक पहुँचाने का क्रम भी चलाता रहता था।
अनादिकाल से ऋषियों का, संतों का एक देशव्यापी तंत्र कार्य करता रहा है। अपनी-अपनी साधनाओं से उपलब्ध महत्त्वपूर्ण सूत्रों एकीकरण, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप धर्म-तंत्र के क्रियात्मक सूत्रों का मनिर्धार्ण, सामाजिक-राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में सर्वसम्मत हल तथा तदनुरूप मार्गदर्शन की व्यवस्था जैसे महत्त्वपूर्ण पुण्यदायी कार्य ऐसे अवसरों पर किए जाते थे। इनका लाभ जनसामान्य भी उठाते थे और जन-जन तक पहुँचाने का क्रम भी चलाता रहता था।
अस्मिन् एवर्णि धौम्यश्च महर्षिः स व्यधाच्छुभम्।
सत्रं तत्र गृहस्थानां मार्गदर्शनहेतवे।।7।।
तस्या आयोजनस्येयं सूचना विहिताऽत्र च।
शंखनादेन घण्टानां निनादेनाऽपि सर्वतः।।8।।
सत्रं तत्र गृहस्थानां मार्गदर्शनहेतवे।।7।।
तस्या आयोजनस्येयं सूचना विहिताऽत्र च।
शंखनादेन घण्टानां निनादेनाऽपि सर्वतः।।8।।
भावार्थ—
इस पूर्व आयोजन के बीच महर्षि धौम्य ने
सद्गृहस्थों के
मार्गदर्शन हेतु एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इस आयोजन की सूचना शंख
बजाते हुए सभी को दे दी गयी।।7-8।।
व्याख्या—
प्राचीनकाल के ऋषियों ने अपने समय की
समस्याओं पर उसी
समय
की परिस्थतियों का ध्यान रखते हुए प्रकाश डाला था। आज की स्थिति उस समय से
भिन्न है। आज वे समस्याएँ नहीं रहीं जो प्राचीनकाल में थीं। तब परिवार
सीमित और सुसंस्कारी होते थे, साधन भी पर्याप्त थे। परंतु अब नयी समस्याएँ
सामने हैं, उनके समाधान आज के हिसाब से ही ढ़ूँढ़ने होंगे। यह काम
युगदृष्टाओं और काल पुरुषों का है। वे ही समय-समय पर युगानुरूप समस्याओं
के समाधान प्रस्तुत करते रहे हैं। यहाँ महर्षि ने बदली परिस्थितियों में
समयानुकूल समाधान प्रस्तुत करने के लिए सद्गृहस्थों-सामान्यजनों को
आमंत्रित किया है।
सत्रसप्तामारब्धं विषयेष्वपि च सप्तसु।
प्रथमें दिवसे चाभूदौतसुक्यमधिकं नृणाम्।।9।।
जिज्ञासवो गृहस्थाश्च बहवस्तस्त्र संगताः।
गृहिण्योऽपि विवेकिन्यो बह्लयस्तत्र समागताः।.10।।
उपस्थितान् गृहस्ताँश्च संबोध्योवाच तत्र सः ।
ऋषिर्धौम्यो गहस्थास्य गरिम्णो विषयेऽद्भुतम्।।11।।
पुण्यदं घोषितं तच्च गृहेऽपि वसतां नृणाम्।
वातावृतेस्तपोभूमेः समानाया विनिर्मितेः।।12।।
गुरुकुलस्य विशालस्य संचालनविधेरिव।
ओजस्विन्यां गम्भीरायां वाचि वक्तव्यमाह च।।13।।
प्रथमें दिवसे चाभूदौतसुक्यमधिकं नृणाम्।।9।।
जिज्ञासवो गृहस्थाश्च बहवस्तस्त्र संगताः।
गृहिण्योऽपि विवेकिन्यो बह्लयस्तत्र समागताः।.10।।
उपस्थितान् गृहस्ताँश्च संबोध्योवाच तत्र सः ।
ऋषिर्धौम्यो गहस्थास्य गरिम्णो विषयेऽद्भुतम्।।11।।
पुण्यदं घोषितं तच्च गृहेऽपि वसतां नृणाम्।
वातावृतेस्तपोभूमेः समानाया विनिर्मितेः।।12।।
गुरुकुलस्य विशालस्य संचालनविधेरिव।
ओजस्विन्यां गम्भीरायां वाचि वक्तव्यमाह च।।13।।
भावार्थ—
सत्र प्रारंभ हुआ। इसे सात दिन चलना था और
सात विषयों
पर
प्रकाश डाला जाना था। प्रथम दिन उत्सुकता अधिक थी। बहुत से जिज्ञासु
गृहस्थ उपस्थित हुए। विचारशील महिलायें भी उसमें बड़ी संख्या में उपस्थित
थीं। उपस्थित सद्गृहस्थों को संबोधित करते हुए महर्षि धौम्य ने
गृहस्थ-धर्म की अद्भुत गरिमा बताई। उसे घर में रहते हुए तपोवन का वातावरण
बनाने और गुरुकुल चलाने के समान् पुण्यफलदायक बताया। गम्भीर ओजस्वी वाणी
में अपना प्रतिपादन प्रस्तुत करते हुए वे बोले—।।9-13।।
व्याख्या—
गृहस्थ धर्म जीवन का एक पुनीत, आवश्यक एवं
उपयोगी
अनुष्ठान
है। आत्मोन्नति करने के लिए यह एक प्राकृतिक, स्वाभाविक और सर्वसुलभ योग
है। गृहस्थ-धर्म के परिपालन से ही आत्मभाव की सीमा बढ़ती है, एक से अनेक
तक आत्मीयता फैलती-विकसित होती है। इसमें मनुष्य अपनी दिन-दिन की खुदगर्जी
के ऊपर अंकुश लगाता जाता है, आत्मसंयम सीखता और स्त्री, पुत्र, संबंधी,
परिजन आदि में अपनी आत्मीयता बढ़ाता जाता है। यही उन्नति धीरे-धीरे आगे
बढ़ती जाती है और मनुष्य संपूर्ण चर-अचर में, जड़-चेतन में आत्मसत्ता को
ही समाया देखता है। उसे परमात्मा की दिव्य ज्योति जगमगाती दीखती है।
गृहस्थाश्रम को ऐसा आश्रम कहा है, जिसकी परिधि में आज के विश्व की बहुसंख्यक जनसंख्या समा जाती है। इस दृष्टि से इस आश्रम की मर्यादाओं में किसी भी भले-बुरे परिवर्तन का प्रभाव सर्वाधिक लोगों को प्रभावित करता है, जो कि समाज की एक इकाई है। समाज का एक स्वरूप ही मनुष्य का अपना परिवार है। परिवार संख्या को लौकिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए अतीव उपयोगी माना गया है। परिवार जीवन की परिभाषा करते हुए ऋषि-मनीषियों ने कहा है—‘‘परिवार परमात्मा की ओर से स्थापित एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा हम अपना आत्म-विकास सहज ही कर सकते हैं और आत्मा में सतोगुण को परिपुष्ट कर सुखी, समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं।। मानव जीवन की सर्वांगीण सुव्यवस्था के लिए पारिवारिक जीवन प्रथम सोपान है। मनुष्य केवल सेवा, कर्म और साधना में ही पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है।
जिस प्रकार परमात्मा और आत्मा में सिवाय छोटे-बड़े स्वरूप के और कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार समाज और परिवार में कोई अंतर नहीं है। परिवार को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाना समाज के उत्थान करने की एक छोटी प्रक्रिया है। उसको क्रियात्मक रूप देने की प्रयोगशाला परिवार है। समाज सेवा का परिपूर्ण अवसर अपने परिवार के छोटे-से क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है और उतने का सुधार कर सकना सरल एवं साध्य भी है। यदि हम सब अपने कौशल, ज्ञान और क्षमता का पूरा-पूरा लाभ देकर परिवार के माध्यम से समाज सेवा का उत्तरदायित्व निभाते चलें, तो जल्दी ही वे परिस्थितियाँ आ सकतीं हैं, वह सुकाल आ सकता है जो कभी प्राचीन युग में रही हैं, शास्त्र का वचन है—
गृहस्थाश्रम को ऐसा आश्रम कहा है, जिसकी परिधि में आज के विश्व की बहुसंख्यक जनसंख्या समा जाती है। इस दृष्टि से इस आश्रम की मर्यादाओं में किसी भी भले-बुरे परिवर्तन का प्रभाव सर्वाधिक लोगों को प्रभावित करता है, जो कि समाज की एक इकाई है। समाज का एक स्वरूप ही मनुष्य का अपना परिवार है। परिवार संख्या को लौकिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए अतीव उपयोगी माना गया है। परिवार जीवन की परिभाषा करते हुए ऋषि-मनीषियों ने कहा है—‘‘परिवार परमात्मा की ओर से स्थापित एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा हम अपना आत्म-विकास सहज ही कर सकते हैं और आत्मा में सतोगुण को परिपुष्ट कर सुखी, समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं।। मानव जीवन की सर्वांगीण सुव्यवस्था के लिए पारिवारिक जीवन प्रथम सोपान है। मनुष्य केवल सेवा, कर्म और साधना में ही पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है।
जिस प्रकार परमात्मा और आत्मा में सिवाय छोटे-बड़े स्वरूप के और कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार समाज और परिवार में कोई अंतर नहीं है। परिवार को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाना समाज के उत्थान करने की एक छोटी प्रक्रिया है। उसको क्रियात्मक रूप देने की प्रयोगशाला परिवार है। समाज सेवा का परिपूर्ण अवसर अपने परिवार के छोटे-से क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है और उतने का सुधार कर सकना सरल एवं साध्य भी है। यदि हम सब अपने कौशल, ज्ञान और क्षमता का पूरा-पूरा लाभ देकर परिवार के माध्यम से समाज सेवा का उत्तरदायित्व निभाते चलें, तो जल्दी ही वे परिस्थितियाँ आ सकतीं हैं, वह सुकाल आ सकता है जो कभी प्राचीन युग में रही हैं, शास्त्र का वचन है—
तथा तथैव कार्याऽत्र न कालस्य विधीयते।
अभिन्नेव प्रयुञ्जनो ह्यमिन्नेव प्रलीयते।।
अभिन्नेव प्रयुञ्जनो ह्यमिन्नेव प्रलीयते।।
अर्थात् इस संसार के साथ हमारा संयोग है, इसी संसार में हमारा लय हो
जायेगा, तब हमें जिस समय जो कर्तव्य हो, वही करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत
सुविधा अथवा असुविधा को लेकर कर्तव्य के पुण्य पथ पर चलते रहना चाहिए।
इसीलिए धर्म ने गृहस्थाश्रम को तपोभूमि कहकर उसकी महत्ता स्वीकार की है।
गृहस्थ एव इज्यते गृहस्थस्तप्यते तपः।
चुतुर्णामाश्रमाणान्तु गृहस्थस्तु विशिष्यते।।
चुतुर्णामाश्रमाणान्तु गृहस्थस्तु विशिष्यते।।
अर्थात् गृहस्थ ही वास्तव में यज्ञ करते हैं। गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी
हैं। इसलिए चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सबका सिरमौर है। गृहस्थ जीवन
एक तप है, एक साधना है। इसका समुचित प्रयोग करके ही वास्तविक जीवन लक्ष्य
को प्राप्त किया जा सकता है।
यहाँ ऋषि श्रेष्ठ ने गृहस्थाश्रम को तपोवन बताते हुए उसकी गरिमा बताने एवं इस आश्रम को एक समग्र गुरुकुल व्यवस्था के रूप में चलाने, विकसित करने की महत्ता दर्शाने का प्रयास आरंभ किया है। उन्होंने अपने उद्बोधन का शुभारंभ ही गृहस्थाश्रम के माहात्म्य से किया है। जो स्पष्टतः इस प्रकरण की गंभीरता जताता है।
यहाँ ऋषि श्रेष्ठ ने गृहस्थाश्रम को तपोवन बताते हुए उसकी गरिमा बताने एवं इस आश्रम को एक समग्र गुरुकुल व्यवस्था के रूप में चलाने, विकसित करने की महत्ता दर्शाने का प्रयास आरंभ किया है। उन्होंने अपने उद्बोधन का शुभारंभ ही गृहस्थाश्रम के माहात्म्य से किया है। जो स्पष्टतः इस प्रकरण की गंभीरता जताता है।
धन्यो गृहस्थाश्रमः
गृहस्थाश्रम समाज को सुनागरिक देने की खान है। भक्त, ज्ञानी, संत,
महात्मा, सुधारक, महापुरुष, विद्वान, पंडित, गृहस्थाश्रम से ही निकलकर आते
हैं। उनके जन्म से लेकर शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण, ज्ञानवर्धन,
गृहस्थाश्रम के बीच होता है। परिवार के बीच ही मनुष्य की सर्वोपरि शिक्षा
होती है। गृहस्थाश्रम की समाज के संगठन, मानवीय मूल्यों की स्थापना, समाज
निष्ठा, भौतिक विकास के साथ-साथ मनुष्य के आध्यात्मिक-मानसिक विकास का
क्षेत्र है। गृहस्थाश्रम ही समाज के व्यक्तित्व स्वरूप का मूलाधार है।
गृहस्थ धर्म मानव जीवन का एक पवित्र, आवश्यक एवं उपयोगी अनुष्ठान है। आत्मोन्नति का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा स्थान-आश्रम स्थल अपना घर-परिवार ही है। इसीलिए गृहस्थ धर्म अन्य धर्मों से अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है महर्षि व्यास के शब्दों में ‘गार्हस्थ्येव हि धर्माणां सर्वेषां मूलमुच्यते।’ गृहस्थाश्रम ही सर्वधर्मों का आधार है। ‘धन्यो गृहस्थाश्रमः’ चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम धन्य है। जिस तरह समस्त प्राणी माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी तरह आश्रम गृहस्ताश्रम पर आधारित हैं।
गृहस्थ धर्म मानव जीवन का एक पवित्र, आवश्यक एवं उपयोगी अनुष्ठान है। आत्मोन्नति का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा स्थान-आश्रम स्थल अपना घर-परिवार ही है। इसीलिए गृहस्थ धर्म अन्य धर्मों से अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है महर्षि व्यास के शब्दों में ‘गार्हस्थ्येव हि धर्माणां सर्वेषां मूलमुच्यते।’ गृहस्थाश्रम ही सर्वधर्मों का आधार है। ‘धन्यो गृहस्थाश्रमः’ चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम धन्य है। जिस तरह समस्त प्राणी माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी तरह आश्रम गृहस्ताश्रम पर आधारित हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i