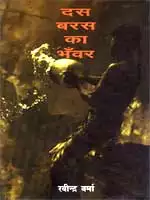|
उपन्यास >> दस बरस का भँवर दस बरस का भँवररवीन्द्र वर्मा
|
37 पाठक हैं |
|||||||
बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992) और गुजरात नरसंहार (2002) के बीच फैले दस वर्ष हमारे समकालीन इतिहास का ऐसा समय रचते हैं, जिनकी प्रतिध्वनियाँ देर और दूर तक जाएँगी।
Dus Baras Ka Bhaver
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992) और गुजरात नरसंहार (2002) के बीच फैले दस वर्ष हमारे समकालीन इतिहास का ऐसा समय रचते हैं, जिनकी प्रतिध्वनियाँ देर और दूर तक जाएँगी। इस दशक में केवल साम्प्रदायिकता परवान नहीं चढ़ी, बल्कि नव-उदारवाद ने भी हमारे समाज में जड़ें पकड़ीं-जैसे दोनों सगी बहनें हों। उपभोक्तावाद मूल्य बना। सामाजिक सरोकार तिरोहित होने लगे। यह उपन्यास इसी आरोह-अवरोह को एक परिवार की कहानी द्वारा पकड़ने की कोशिश की है, जिसके केन्द्र में रतन का तथा-कथित ‘शिज़ोफ्रिनिया’ है और उसका सामना करते बाँके बिहारी हैं।
रतन के भाइयों की संवेदनहीनता जाने-अनजाने एक चक्रव्यूह की रचना करती है, जिससे बाँके बिहारी अपने छोटे बेटे को निकालते हैं। रतन अपने उन्माद में अपनी प्रेमिका का बलात्कार करता है। पत्रकार बाँकेबिहारी के लिए यह ‘गुजरात’ का रूपक बन जाता है।
इन्हीं कथा-सूत्रों के इर्द-गिर्द लेखकीय चिन्ताएँ बिखरी हैं, जो समकालीनता का अतिक्रमण करती हुई मनुष्य की नियति की पड़ताल करती हैं। यह प्रकृतवाद से परहेज करती हुई किस्सागोई है, जो नए यथार्थ के मुहावरे को रचने का प्रयास करती है। उपन्यास में समय और शिल्प का लचीलापन इसी मुहारवरे की तलाश है।
रतन के भाइयों की संवेदनहीनता जाने-अनजाने एक चक्रव्यूह की रचना करती है, जिससे बाँके बिहारी अपने छोटे बेटे को निकालते हैं। रतन अपने उन्माद में अपनी प्रेमिका का बलात्कार करता है। पत्रकार बाँकेबिहारी के लिए यह ‘गुजरात’ का रूपक बन जाता है।
इन्हीं कथा-सूत्रों के इर्द-गिर्द लेखकीय चिन्ताएँ बिखरी हैं, जो समकालीनता का अतिक्रमण करती हुई मनुष्य की नियति की पड़ताल करती हैं। यह प्रकृतवाद से परहेज करती हुई किस्सागोई है, जो नए यथार्थ के मुहावरे को रचने का प्रयास करती है। उपन्यास में समय और शिल्प का लचीलापन इसी मुहारवरे की तलाश है।
1.1
जब पुष्पक एक्सप्रेस झाँसी के प्लेटफ़ॉर्म पर सरकते-सरकते थमी तो सूने प्लेटफ़ॉर्म पर बिजली की रोशनियाँ चमकीं। रोशनियाँ प्लेटफ़ॉर्म की छत से उल्टी लटकी थीं। छत के परे आधी रात का अँधेरा था—जो आसमान में छिटपुट तारों के इर्द-गिर्द जमा हो रहा था।
प्लेटफ़ॉर्म पर उतरकर रतन और दो अटैचियों के साथ अकेले खड़े हुए बाँके बिहारी को याद आया कि पिछली बार भी आधी रात इसी तरह पुष्पक से उतरकर वे यहीं खड़े थे। फ़र्क यही था कि तब पुष्पक विपरीत दिशा से आई थी।
‘चाय’, रतन ने चायवाले को रोककर बाँके बिहारी की ओर देखते हुए कहा, ‘पापा, मैं चाय पिऊँगा।’
एक और चायवाला रुक गया था। दूसरी ओर दोनों अटैचियों के पास एक कुली भी आकर खड़ा हो गया।
‘तीन चाय’, बाँके बिहारी ने संदिग्ध मुस्कान के साथ कहा। असल में उन्हें अचानक यह याद आ गया था कि पिछली बार भी रतन ने इसी तरह चाय की माँग की थी, जब वे लखनऊ से लौटे थे। और तब भी कुली के साथ दोनों ने चाय पी थी। बाँके बिहारी की वह उम्र कब की शुरू हो गई थी जब चीजें अपने को दुहराती हुई लगती हैं जैसे निरन्तर फैलती हुई सृष्टि की भी सीमाएँ हों।
कुली अधेड़ और चौकन्ना था। उसकी मूँछ और बढ़ी दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद थे। उसने प्लास्टिक के कप से चाय सुड़ककर पहले बाँके बिहारी को देखा : एक श्वेत-धवल दाढ़ी और सन-से बालों से घिरा चेहरा था, जो सीधी काठी पर रखा था। फिर रतन को : नया गबरू जवान था जो गाड़ी से उतर आया था, मगर अभी जागा नहीं था। दूसरी बार चाय सुड़ककर कुली ने दोनों को एक बार फिर देखा और सोचा कि गबरू जवान को बूढ़े की फ़िक्र करनी चाहिए। मगर गंगा उल्टी बह रही थी।
बाँके बिहारी वीरान प्लेटफ़ॉर्म को हसरत से देख रहे थे जैसे कोई लौटकर अपने घर को देखता है। प्लेटफ़ॉर्म पर भरपूर उजाला था। पर उजाला सूना था। सारे स्टॉल बन्द थे। सिर्फ़ चाय का स्टॉल खुला था। उसके सामने दो आदमी खड़े थे। पुष्पक से उतरे छिटपुट लोग चले गए थे। चाय पीने और कोई नहीं रुका था। सामने प्लेटफ़ॉर्म को जोड़ता लोहे का पुल था जिस पर कुछ लोग धब्बों-से नज़र आते थे। रोशनी पुल के ऊपर और प्लेटफ़ॉर्म के बाहर कुछ कदम चलती थी ओर थककर बैठ जाती थी। चारों ओर अँधेरे का समुद्र ठाठें मार रहा था।
जब वे चले, सबसे आगे कुली था। कुली के पीछे बाँके बिहारी और बाँके बिहारी के पीछे रतन। रतन को बाँके बिहारी मुड़-मुड़कर देख लेते थे जैसे आगे अटैचियाँ थामे कुली को देखते थे। अँधेरे में उनकी सफ़ेद मुंडी आगे-पीछे घूमती। कुली के पैर चपल थे। बड़ी अटैची उसने सिर पर रख ली थी। छोटी उसके हाथ में थी। उसकी चाल तेज़ थी। बाँके बिहारी तेज़ चलते हुए मुड़-मुड़कर पीछे देखते जाते। उन्हें लगा, पुल की सीढ़ियों पर लगी रोशनी ने उनके कानों में फुसफुसाया : सँभलकर, ज़रा सँभलकर। हँसकर उन्होंने पीछे रतन को देखा। रतन आँखें नीची किए चुपचाप चला आ रहा था जैसे उसे रोशनी या अँधेरे या शहर से कोई मतलब न हो।
ऑटो-रिक्शा में बैठकर रतन ने आँखें मूँद लीं। बाँके बिहारी आँखें फाड़-फाड़कर शहर को देखने लगा, जो सो रहा था। ठंडी हवा का पहला झोंका ऑटो पर झपटा जैसे वह भर्र-भर्र करके आगे बढ़ा। बाँके बिहारी ने शॉल पूरी लपेटने से पहले रतन से पूछा, ‘‘ठंड तो नहीं लग रही ?’ ‘नहीं’, रतन ने आँखें बन्द किए हुए कहा। वह सिर्फ़ स्वेटर पहने था। मार्च शुरू हो गया था। सर्दी ऑटो पर ठंडी हवाओं में लिपटी झपट-झपट पड़ती थी। बाँके बिहारी अँधेरे में रेलवे का ऑफिस, कोठियाँ पहचानते और सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों को देखते रहे, जो कुछ दूर जाकर गहरे होते जाते, पेड़ों के पीछे पेड़ और उनके पीछे पेड़...जो अँधेरे में डूब जाते। सड़क पर बिजली के खम्भे जल रहे थे। फिर कुछ बन्द, अँधेरे मकानों में अपनी चीखें छो़ड़ता हुआ ऑटो इलाइट सिनेमा के चौराहे पर पहुँचकर बाईं ओर घूम गया। बाँके बिहारी की आँखें बन्द हो गई थीं। जब एक झटके से आँखें खुलीं तो सामने दूर पहाड़ी पर किला खड़ा था जैसे अँधेरे का किला हो, समूचे शहर को अपनी बाँहों में छिपाए हुए। ऊपर आसमान में छिटपुट तारे थे—तारों के अवशेष की तरह।
एक बार सहसा आसमान चमका और पहाड़ी पर किला उजागर हो गया जैसे अँधेरे में नंगा खड़ा हो।
‘अम्माँ, अम्माँ’, रतन की आवाज़ किवाड़ पर बिजली साँकल के साथ मोहल्ले में गूँजी।
ऑटोवाला दोनों अटैचियाँ चबूतरे पर रखकर चला गया था। अँधेरे में ऑटो की भर्र-भर्र की घुलती हुई अनुगूँजें थीं।
दरवाज़ा खुला।
‘छोटे’, अम्माँ की आवाज़ थी जैसे किवाड़ खोलकर बाहर आई हो।
बाँके बिहारी और रतन अटैचियाँ उठाए पौर में घुसे। रतन ने आँगन में खड़े-खड़े दालान में अटैची रखी, फिर पेड़ के पीछे रखे घड़े से एक गिलास पानी लेकर पिया। उसने गायत्री से कहा कि मुझे बहुत नींद लगी है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वह सीढ़ियों पर धड़-धड़ चढ़ने लगा।
अम्माँ ने आँगन में खड़े-खड़े फ़ौरन ऊपर की बत्ती जलाई और पूछा—‘भूख तो नहीं लगी ?’ नहीं’, रतन ने आखिरी सीढ़ी पर कहा और छत पर चला गया। छत पर उसके अटारी में जाते क़दमों की आहट होती रही।
‘पचास बरस से कह रही हूँ’, गायत्री ने बाँके बिहारी की ओर देखकर कहा, ‘कि सीढ़ियों पर ओट बनवा लो, तुमने नहीं माना। अभी नंगी सीढ़ियों पर छोटे के पैर काँपे थे।’
‘वह आधा नींद में है’, बाँके बिहारी बोले।
‘उसकी तबियत कैसी है ?’
‘आधी ठीक है।’
‘आधी !’ गायत्री ने पति को हैरत से देखा।
‘हाँ।’
‘बम्बई के डॉक्टर भी ठीक न कर सके ?’
‘बम्बई नहीं मुम्बई !’
‘यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है।’
आँगन में खड़े पेड़ की पत्तियों में उलझी हवाएँ छूटने को कसमसाईं। शाखों के झूमकर एक-दूसरे से टकराने की आवाज़ें आईं। फिर हवाओं की हवाओं से टकराने की आवाज़ें...हू-हू...सूँ-सूँ...जैसे आँगन में एक पेड़ न हो, जंगल हो।
‘आधा तो ठीक है’, बाँके बिहारी ने कहा।
‘क्या ?’
‘जवाब और रतन, दोनों।’ आवाज़ ठंडी थी जैसे पेड़ की हवा बोली हो।
जैसे अपने से बोली हों, गायत्री बोलीं, ‘मँझले तो कहता था कि बम्बई में जो डॉक्टर हैं, वे और कहीं नहीं।
‘अब मँझले मुम्बई में रहता है, गायत्री। बम्बई नहीं रही। कल सुबह बताऊँगा।’
शायद ऑटो की मोहल्ले की सड़क पर खिंची चीख से दो कुत्ते जाग गए थे और रह-रह कर भौंक रहे थे। जब वे चुप हो गए, तभी बाँके बिहारी को नींद आई। नींद में उतरना सीढ़ियों पर उतरने की तरह था, जिनका एक सिरा खाली था और आँगन में खुलता था। बाँके बिहारी की आँखें आधी खुली थीं। उनके पैर अचानक पाँचवी सीढ़ी पर काँपे। आँखें अपने आप पूरी खुल गईं : नीचे आँगन नहीं था, समुद्र था। सीढ़ी के ऊपर आसमान था, नीचे समुद्र था। वे आँखें बन्द किए नीचे उतरते गए। सीढ़ी खत्म ही नहीं होती थी जैसे समुद्र पाताल में उतरता जाता हो। जब नीचे उतरते हुए उन्हें अपने पैर तैरते पैरों की तरह लगे तो उनकी आँखें खुल गईं : न कहीं सीढ़ी थी, न आँगन था। केवल समुद्र था। वे समुद्र के प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े थे, जिसके सामने पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी। रेलगाड़ी के सारे दरवाज़े और खिड़कियाँ बन्द थीं। रतन कहीं नहीं था। बाँके बिहारी की आँखें रतन को ढूँढ़ रही थीं। आँखें समुद्र की लहरों पर पक्षियों की तरह घूमतीं...दूर-दूर...बहुत दूर...चारों ओर...चारों ओर गोल धरती पर समुद्र नीचे लुढ़क रहा था जैसे जुहू-तट पर सागर दूर क्षितिज पर दूसरी ओर झरने-सा गिरता लगता था...अभी चारों ओर जुहू-क्षितिज था और चारों ओर रात थी। रात में आँखें सागर-क्षितिज पर अटकी चीख़ रही थीं...रतन, रतन...। एकाएक सामने खड़ी पुष्पक का एक दरवाज़ा खुला। दरवाज़े में बड़े, मँझले और भैया खड़े हाथ हिला रहे थे और मुस्करा रहे थे। ये तीनों एक-साथ कहाँ जा रहे हैं ? भैया अमरीका से कब आया ? छोटे इनके साथ क्यों नहीं है ?
‘छोटे कहाँ है ?’ बाँके बिहारी चीख़ते हैं।
गाड़ी के दरवाज़े में खड़े तीनों के होंठ हिलते हैं। मगर कोई आवाज़ नहीं आती।
‘क्या ?’ बाँके बिहारी फिर चीख़ते हैं।
तीनों हाथ हिलाते हैं। गाड़ी चल देती है।
जब गाड़ी की जगह खाली होती है तो उसी ख़ाली जगह के पीछे छोटे खड़ा नज़र आता है। बाँके बिहारी समुद्र पर दौड़कर छोटे को गले लगा लेते हैं। वे हाँफ रहे हैं। उनकी आँखों में आँसू नहीं हैं। आँखें सागर की फेनिल लहरों को निहार रही हैं।
वे देखते हैं कि सीधी गाड़ी अचानक बाएँ मुड़ती है, फिर यू-टर्न लेकर दाएँ मुड़ जाती है जैसे रेलगाड़ी न हो, कोई ऑटो-रिक्शा हो जिसे पटरी की जरूरत नहीं होती।
धरती की पनीली गेंद पर बाँके बिहारी रतन को छाती से चपेटे अकेले खड़े थे।
सुबह चाय पीते हुए बाँके बिहारी ने पत्नी से कहा :
‘सुनो।’
‘हाँ।’
‘पचास साल से तुम ठीक कह रही थीं।’
‘क्या ?’ वे हँसी।
‘आँगन में सीढ़ी नंगी है। उसे ढँक देना चाहिए।’
‘हाँ’, उन्होंने आह भरी, ‘बड़े मझले और भैया इन्हीं सीढ़ियों पर नंगे खेलते हुए बड़े हो गए।’
बाँके बिहारी क्षण-भर गायत्री को देखते रहे। फिर बोले—‘छोटे बड़े होकर सीढ़ियों पर फँस गए हैं। हमें सीढ़ियों को ढँकना होगा।’
‘एक ईंट की दीवार कमर तक काफ़ी होगी,’ गायत्री ने कहा।
‘मिस्त्री से पूछ लेंगे।’
फिर बाँके बिहारी ने गायत्री से पूछा :
‘छोटे उठ गए ?’
‘नहीं।’
‘ठीक है। सोने दो।’
गायत्री भीतर चली गईं। बाँके बिहारी चाय का कप नीचे रखकर पौर में गावतकिए पर सिर टिकाए पसर गए। दरवाज़ा खुला था। ताज़ी धूप सड़क पर नर्म कालीन-सी बिछी थी। आँगन में धूप नहीं थी, जब वे अन्दर से कोठे से पौर में आए। अब शायद नीम की पत्तियों से छनकर तने पर फिसलती हुई धूप नंगे फ़र्श पर आ गई होगी। घर के बाहर चबूतरे पर भी धूप घर की दीवार की ओर सरकती हुई लगती थी। घर धूप से घिर गया था।
बाँके बिहारी ने आँखें मूँद लीं। उन्हें लगा, वे अभी पैदा हुए हैं। वे अपने घर की सुबह देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। यह सुबह अपने घर में गायत्री और उनके बीच तनी थी। अलबत्ता छोटे अटारी में सो रहे थे। छोटे शायद अब कभी पूरी तरह ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर यही कहते हैं। वे कहते हैं कि छोटे को देखभाल, दवा-दारू चाहिए। मर्ज दस साल पुराना था। पहले पता ही नहीं चला। फिर कुछ वक़्त शक में गुज़रा। जिस दिन छोटे नूर मंजिल से घर आए, उसी शाम बाँके बिहारी ने बहू को दूसरे कमरे में बोलते सुना था, ‘यह नीम-पागल घर में रहेगा, तो मुन्ना पर क्या असर पड़ेगा ?’ वे दो दिन बाद ही छोटे को लेकर झाँसी आ गए थे। दो बरस बाद मँझले ने छोटे को मुम्बई बुलाया। मँझले की बेटी पँचगनी में पढ़ती थी और उसका तीन कमरे का बड़ा फ़्लैट था। उसने नई फ़ैक्टरी डाली थी। दस माह बाद छोटे ने फोन पर रोते हुए कहा—‘पापा, यहाँ मैं घर का नौकर हो गया हूँ, जिसे वेतन नहीं मिलता।’ तब बाँके बिहारी मुम्बई गए थे और कल रात छोटे को लेकर लौटे थे।
यह सच है कि बाँके बिहारी दस बरस इसी झिलमिल भरोसे में रहे कि छोटे को उसके तीनों बड़े भाई सँभाल लेंगे। भैया अमरीका में था। उसने लिखा था कि पापा, मैं छोटे को यहाँ बुला तो नहीं सकता, मगर इलाज के लिए डॉलर भेज सकता हूँ। डॉलर से क्या नहीं हो सकता, पापा ? भैया, बाँकेलाल बुदबुदाए, डॉलर से नीम-पागल और घर के नौकर ही बनेंगे ! उन्होंने आँखें खोली। एक गौरैया पौर में घुस आई थी और चूँ-चूँ, चूँ-चूँ बोल रही थी। वह एक कोने से दूसरे कोने में उड़ी, फिर तीसरे से चौथे कोने में—और फिर दरवाज़े से फुर्र हो गई।
डॉलर नहीं लूँगा, बाँके बिहारी ने सोचा। नीम-पागल या घर के नौकर के लिए डॉलर दान ही हुआ न ! दान नहीं लूँगा। छोटे मेरा बेटा है। मैं उसे पालूँगा। उन्हें पता ही नहीं चला था। पहले वे उठकर बैठे, फिर खड़े हो गए थे गोया किसी महायात्रा का संकल्प हो।
बाँके बिहारी पौर के चबूतरे पर खड़े थे, जब दरवाज़े की धूप में कोई आकर चुपचाप खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई छाया हो।
‘दद्दा, आप कब आए ?’ छाया बोली।
‘अरे मोहन, कैसे हो ?’ बाँके बिहारी ने सिर घुमाया, ‘मैं रात आया। एक्सप्रेस भी देना।’
मोहन ने पीछे मुड़कर साइकिल के कैरियर से दो अख़बार निकाले और उनके हाथ में थमा दिए। वे खड़े-खड़े एक्सप्रेस देखने लगे। मुख्य ख़बर गुजरात में दंगों की ही थी। कल ट्रेन में दिन-भर कुछ छिटपुट खबरें कानों में पड़ती रही थीं। यह पक्की खबर थी। परसों घटे ‘गोधरा’ का बदला कल गुजरात में लिया था। गोधरा कहाँ था ? गोधरा यदि गुजरात में था तो क्या गुजरात ने गुजरात से बदला लिया ? हत्या लूट, और आगजनी का तांडव हुआ था। पता नहीं क्या-क्या हुआ था ? यह तो पहली खबर थी। ट्रेन में एक गुजराती अहमदाबाद का ‘संदेश’ लिये था—जिसमें गोधरा में हुए बलात्कारों की खबर थी। कल प्रतिशोध अभियान शुरू हुआ। शहर जले थे। अहमदाबाद का चरम पूर्व सांसद एहसान जाफ़री का कल अपराह्न दहन था। भीड़ से घिरे अपने घर के सामने दौड़ते लहूलुहान जाफ़री को ज़िन्दा जला दिया गया था। अहसान ज़ाफरी !
बाँके बिहारी की जीभ पर यह नाम घूमा, जो नूरजहाँ में बदल गया। नूरजहाँ—जो मेरे पोते की माँ है ! बाँके बिहारी अख़बार हाथ में लिए बैठ गए। धूप दरवाज़े की चौखट पर आ गई थी। उन्होंने धूप को घूरते हुए सोचा : आग का कोई भरोसा नहीं। बाबरी मस्जिद ढहने के तुरन्त बाद दस साल पहले नूरजहाँ के पिता लखनऊ में खो गए थे। नूरजहाँ रोई थी। क्या नूरजहाँ फिर रोएगी ? दरवाज़े पर एकाएक धूप चमकी जैसे सूर्य ने कोण बदला हो। बाँके बिहारी को अचानक भैया याद आया जो सिलिकन वैली में जेब में डॉलर खनखनाता घूमता था। उसने पिछली बार बताया था कि वह और उसके दोस्त अमरीका में विश्व हिन्दू परिषद को चन्दा देते हैं। आख़िरकार, उसने कहा था, गोरों के देश में हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहा है। आप नहीं जानते, पापा, उसने कहा था—परदेस में अपना देश कैसे-कैसे याद आता है ! तब शाहरुख खान की फिल्म देखना या मन्दिर जाना बहुत काम आता है। वही समय गुजरात के गाँवों में त्रिशूल-यज्ञ और भगवा-पट्टी बनकर फैला था। उन्हीं हाथों में तलवारें थमी थीं। वही हाथ गुजरात जला रहे थे। गुजरात गुजरात से बदला ले रहा था। क्या मेरा एक बेटा दूसरे बेटे से बदला लेगा ? बाँके बिहारी की आँखों के सामने नूरजहाँ का चेहरा आ गया। उन्होंने उसे फिर एक मुसलमान की तरह देखा जैसे ब्याह के वक़्त देखा था। फिर भूल गए थे। भूला हुआ शिद्दत से दिसम्बर 1992 में याद आया था। फिर लगातार याद आता रहा। जब-जब बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि का मसला गरमाता, बाँके बिहारी को नूरजहाँ का मुसलमान होना याद आता जैसे कोई दर्द बार-बार उठता हो।
अटारी में छोटे की आँख जब खुली तो हल्का-सा अँधेरा था, जो कोनों में गाढ़ा हो रहा था—नीचे फ़र्श पर कोनों में ज़्यादा। छप्पर पर उजाले के कुछ छेद थे। सुबह का समाँ था। मगर आँगन के पेड़ से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। चिड़ियों की बातें मुम्बई के फ़्लैट में बहुत याद आती थीं—क्योंकि वे वहाँ नहीं थीं। वहाँ ऐसा दरवाज़ा भी नहीं था, जो छत पर खुलता हो। छत पर सुबह का उजाला था।
धूप नहीं थी।
छोटे निकर पहने सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसने सिर ऊपर घुमाया। नीम की पत्तियाँ हौले-हौले हिल रही थीं। चिड़ियाँ नहीं थीं। कहाँ गईं सारी चिड़ियाँ ? क्या अपना पेड़ भूल गईं ? या कोई और पेड़ याद आ गया ? सारी चिड़ियाँ आसमान में एक-साथ मर तो नहीं सकतीं ? चिड़ियों में सामूहिक हत्या या आगजनी का रिवाज़ भी नहीं था।
‘अम्माँ’, छोटे ने चौके में बैठते हुए कहा।
‘‘हाँ’, गायत्री दूसरी ओर चूल्हे के बगल में बैठे हुए बोलीं।
‘चिड़ियाँ कहाँ गईं ?’
‘कौन-सी चिड़ियाँ ?’ गायत्री ने आँखें घुमाईं।
‘अपने नीम की चिड़ियाँ ?’
‘घूमने गई हैं’, गायत्री हँसी।
‘कहाँ ?’
‘दूसरे पेड़ों या घरों या आसमान में।’
‘क्यों ?’
‘यही उनका दिन-भर का काम है।’
‘वे भी काम करती हैं ?’
‘हाँ’, गायत्री ने छोटे की ओर देखा।
चूल्हे से धुआँ उठा। गायत्री की आँखों में भर गया। उन्होंने आँखें मूँदकर खोलीं। आँखों में आँसू डबडबा आए। डबडबाई आँखों में छोटे की आकृति काँपने लगी।
धुआँ चौके के दोनों मेहराबों से अपने गुंजलक बनाते हुए आँगन में बिखर गया। छोटे चौके में दूसरी ओर मेड़ पर उकडूँ बैठा था। वह आँगन में लहराते धुएँ को देख रहा था। एकाएक उसे लगा कि पेड़ से आँगन में अँधेरा चू रहा है। वह देखता ! पेड़ से अँधेरा सूखी पत्तियों की तरह गिर रहा था।
सूर्य कहाँ गया ?
‘अम्माँ’, छोटे ने अचानक कहा, ‘आज क्या दिन नहीं होगा ? सुबह के बाद रात होगी ?’
‘यह सुबह नहीं है’, गायत्री हँसी, ‘शाम है।’
‘पर’, छोटे ने सिर चारों ओर घुमाया, ‘पर दिन कहाँ गया ?’
‘दिन-भर तुम सोते रहे।’
छोटे ने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा।
वह चौके में बैठा कुछ देर चाय पीता रहा और आँगन में गिरता अँधेरा देखता रहा। कोई पक्षी पेड़ पर बोला। क्या आज पक्षी पेड़ पर चुपचौप लौटे थे ?
प्लेटफ़ॉर्म पर उतरकर रतन और दो अटैचियों के साथ अकेले खड़े हुए बाँके बिहारी को याद आया कि पिछली बार भी आधी रात इसी तरह पुष्पक से उतरकर वे यहीं खड़े थे। फ़र्क यही था कि तब पुष्पक विपरीत दिशा से आई थी।
‘चाय’, रतन ने चायवाले को रोककर बाँके बिहारी की ओर देखते हुए कहा, ‘पापा, मैं चाय पिऊँगा।’
एक और चायवाला रुक गया था। दूसरी ओर दोनों अटैचियों के पास एक कुली भी आकर खड़ा हो गया।
‘तीन चाय’, बाँके बिहारी ने संदिग्ध मुस्कान के साथ कहा। असल में उन्हें अचानक यह याद आ गया था कि पिछली बार भी रतन ने इसी तरह चाय की माँग की थी, जब वे लखनऊ से लौटे थे। और तब भी कुली के साथ दोनों ने चाय पी थी। बाँके बिहारी की वह उम्र कब की शुरू हो गई थी जब चीजें अपने को दुहराती हुई लगती हैं जैसे निरन्तर फैलती हुई सृष्टि की भी सीमाएँ हों।
कुली अधेड़ और चौकन्ना था। उसकी मूँछ और बढ़ी दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद थे। उसने प्लास्टिक के कप से चाय सुड़ककर पहले बाँके बिहारी को देखा : एक श्वेत-धवल दाढ़ी और सन-से बालों से घिरा चेहरा था, जो सीधी काठी पर रखा था। फिर रतन को : नया गबरू जवान था जो गाड़ी से उतर आया था, मगर अभी जागा नहीं था। दूसरी बार चाय सुड़ककर कुली ने दोनों को एक बार फिर देखा और सोचा कि गबरू जवान को बूढ़े की फ़िक्र करनी चाहिए। मगर गंगा उल्टी बह रही थी।
बाँके बिहारी वीरान प्लेटफ़ॉर्म को हसरत से देख रहे थे जैसे कोई लौटकर अपने घर को देखता है। प्लेटफ़ॉर्म पर भरपूर उजाला था। पर उजाला सूना था। सारे स्टॉल बन्द थे। सिर्फ़ चाय का स्टॉल खुला था। उसके सामने दो आदमी खड़े थे। पुष्पक से उतरे छिटपुट लोग चले गए थे। चाय पीने और कोई नहीं रुका था। सामने प्लेटफ़ॉर्म को जोड़ता लोहे का पुल था जिस पर कुछ लोग धब्बों-से नज़र आते थे। रोशनी पुल के ऊपर और प्लेटफ़ॉर्म के बाहर कुछ कदम चलती थी ओर थककर बैठ जाती थी। चारों ओर अँधेरे का समुद्र ठाठें मार रहा था।
जब वे चले, सबसे आगे कुली था। कुली के पीछे बाँके बिहारी और बाँके बिहारी के पीछे रतन। रतन को बाँके बिहारी मुड़-मुड़कर देख लेते थे जैसे आगे अटैचियाँ थामे कुली को देखते थे। अँधेरे में उनकी सफ़ेद मुंडी आगे-पीछे घूमती। कुली के पैर चपल थे। बड़ी अटैची उसने सिर पर रख ली थी। छोटी उसके हाथ में थी। उसकी चाल तेज़ थी। बाँके बिहारी तेज़ चलते हुए मुड़-मुड़कर पीछे देखते जाते। उन्हें लगा, पुल की सीढ़ियों पर लगी रोशनी ने उनके कानों में फुसफुसाया : सँभलकर, ज़रा सँभलकर। हँसकर उन्होंने पीछे रतन को देखा। रतन आँखें नीची किए चुपचाप चला आ रहा था जैसे उसे रोशनी या अँधेरे या शहर से कोई मतलब न हो।
ऑटो-रिक्शा में बैठकर रतन ने आँखें मूँद लीं। बाँके बिहारी आँखें फाड़-फाड़कर शहर को देखने लगा, जो सो रहा था। ठंडी हवा का पहला झोंका ऑटो पर झपटा जैसे वह भर्र-भर्र करके आगे बढ़ा। बाँके बिहारी ने शॉल पूरी लपेटने से पहले रतन से पूछा, ‘‘ठंड तो नहीं लग रही ?’ ‘नहीं’, रतन ने आँखें बन्द किए हुए कहा। वह सिर्फ़ स्वेटर पहने था। मार्च शुरू हो गया था। सर्दी ऑटो पर ठंडी हवाओं में लिपटी झपट-झपट पड़ती थी। बाँके बिहारी अँधेरे में रेलवे का ऑफिस, कोठियाँ पहचानते और सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों को देखते रहे, जो कुछ दूर जाकर गहरे होते जाते, पेड़ों के पीछे पेड़ और उनके पीछे पेड़...जो अँधेरे में डूब जाते। सड़क पर बिजली के खम्भे जल रहे थे। फिर कुछ बन्द, अँधेरे मकानों में अपनी चीखें छो़ड़ता हुआ ऑटो इलाइट सिनेमा के चौराहे पर पहुँचकर बाईं ओर घूम गया। बाँके बिहारी की आँखें बन्द हो गई थीं। जब एक झटके से आँखें खुलीं तो सामने दूर पहाड़ी पर किला खड़ा था जैसे अँधेरे का किला हो, समूचे शहर को अपनी बाँहों में छिपाए हुए। ऊपर आसमान में छिटपुट तारे थे—तारों के अवशेष की तरह।
एक बार सहसा आसमान चमका और पहाड़ी पर किला उजागर हो गया जैसे अँधेरे में नंगा खड़ा हो।
‘अम्माँ, अम्माँ’, रतन की आवाज़ किवाड़ पर बिजली साँकल के साथ मोहल्ले में गूँजी।
ऑटोवाला दोनों अटैचियाँ चबूतरे पर रखकर चला गया था। अँधेरे में ऑटो की भर्र-भर्र की घुलती हुई अनुगूँजें थीं।
दरवाज़ा खुला।
‘छोटे’, अम्माँ की आवाज़ थी जैसे किवाड़ खोलकर बाहर आई हो।
बाँके बिहारी और रतन अटैचियाँ उठाए पौर में घुसे। रतन ने आँगन में खड़े-खड़े दालान में अटैची रखी, फिर पेड़ के पीछे रखे घड़े से एक गिलास पानी लेकर पिया। उसने गायत्री से कहा कि मुझे बहुत नींद लगी है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वह सीढ़ियों पर धड़-धड़ चढ़ने लगा।
अम्माँ ने आँगन में खड़े-खड़े फ़ौरन ऊपर की बत्ती जलाई और पूछा—‘भूख तो नहीं लगी ?’ नहीं’, रतन ने आखिरी सीढ़ी पर कहा और छत पर चला गया। छत पर उसके अटारी में जाते क़दमों की आहट होती रही।
‘पचास बरस से कह रही हूँ’, गायत्री ने बाँके बिहारी की ओर देखकर कहा, ‘कि सीढ़ियों पर ओट बनवा लो, तुमने नहीं माना। अभी नंगी सीढ़ियों पर छोटे के पैर काँपे थे।’
‘वह आधा नींद में है’, बाँके बिहारी बोले।
‘उसकी तबियत कैसी है ?’
‘आधी ठीक है।’
‘आधी !’ गायत्री ने पति को हैरत से देखा।
‘हाँ।’
‘बम्बई के डॉक्टर भी ठीक न कर सके ?’
‘बम्बई नहीं मुम्बई !’
‘यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है।’
आँगन में खड़े पेड़ की पत्तियों में उलझी हवाएँ छूटने को कसमसाईं। शाखों के झूमकर एक-दूसरे से टकराने की आवाज़ें आईं। फिर हवाओं की हवाओं से टकराने की आवाज़ें...हू-हू...सूँ-सूँ...जैसे आँगन में एक पेड़ न हो, जंगल हो।
‘आधा तो ठीक है’, बाँके बिहारी ने कहा।
‘क्या ?’
‘जवाब और रतन, दोनों।’ आवाज़ ठंडी थी जैसे पेड़ की हवा बोली हो।
जैसे अपने से बोली हों, गायत्री बोलीं, ‘मँझले तो कहता था कि बम्बई में जो डॉक्टर हैं, वे और कहीं नहीं।
‘अब मँझले मुम्बई में रहता है, गायत्री। बम्बई नहीं रही। कल सुबह बताऊँगा।’
शायद ऑटो की मोहल्ले की सड़क पर खिंची चीख से दो कुत्ते जाग गए थे और रह-रह कर भौंक रहे थे। जब वे चुप हो गए, तभी बाँके बिहारी को नींद आई। नींद में उतरना सीढ़ियों पर उतरने की तरह था, जिनका एक सिरा खाली था और आँगन में खुलता था। बाँके बिहारी की आँखें आधी खुली थीं। उनके पैर अचानक पाँचवी सीढ़ी पर काँपे। आँखें अपने आप पूरी खुल गईं : नीचे आँगन नहीं था, समुद्र था। सीढ़ी के ऊपर आसमान था, नीचे समुद्र था। वे आँखें बन्द किए नीचे उतरते गए। सीढ़ी खत्म ही नहीं होती थी जैसे समुद्र पाताल में उतरता जाता हो। जब नीचे उतरते हुए उन्हें अपने पैर तैरते पैरों की तरह लगे तो उनकी आँखें खुल गईं : न कहीं सीढ़ी थी, न आँगन था। केवल समुद्र था। वे समुद्र के प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े थे, जिसके सामने पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी। रेलगाड़ी के सारे दरवाज़े और खिड़कियाँ बन्द थीं। रतन कहीं नहीं था। बाँके बिहारी की आँखें रतन को ढूँढ़ रही थीं। आँखें समुद्र की लहरों पर पक्षियों की तरह घूमतीं...दूर-दूर...बहुत दूर...चारों ओर...चारों ओर गोल धरती पर समुद्र नीचे लुढ़क रहा था जैसे जुहू-तट पर सागर दूर क्षितिज पर दूसरी ओर झरने-सा गिरता लगता था...अभी चारों ओर जुहू-क्षितिज था और चारों ओर रात थी। रात में आँखें सागर-क्षितिज पर अटकी चीख़ रही थीं...रतन, रतन...। एकाएक सामने खड़ी पुष्पक का एक दरवाज़ा खुला। दरवाज़े में बड़े, मँझले और भैया खड़े हाथ हिला रहे थे और मुस्करा रहे थे। ये तीनों एक-साथ कहाँ जा रहे हैं ? भैया अमरीका से कब आया ? छोटे इनके साथ क्यों नहीं है ?
‘छोटे कहाँ है ?’ बाँके बिहारी चीख़ते हैं।
गाड़ी के दरवाज़े में खड़े तीनों के होंठ हिलते हैं। मगर कोई आवाज़ नहीं आती।
‘क्या ?’ बाँके बिहारी फिर चीख़ते हैं।
तीनों हाथ हिलाते हैं। गाड़ी चल देती है।
जब गाड़ी की जगह खाली होती है तो उसी ख़ाली जगह के पीछे छोटे खड़ा नज़र आता है। बाँके बिहारी समुद्र पर दौड़कर छोटे को गले लगा लेते हैं। वे हाँफ रहे हैं। उनकी आँखों में आँसू नहीं हैं। आँखें सागर की फेनिल लहरों को निहार रही हैं।
वे देखते हैं कि सीधी गाड़ी अचानक बाएँ मुड़ती है, फिर यू-टर्न लेकर दाएँ मुड़ जाती है जैसे रेलगाड़ी न हो, कोई ऑटो-रिक्शा हो जिसे पटरी की जरूरत नहीं होती।
धरती की पनीली गेंद पर बाँके बिहारी रतन को छाती से चपेटे अकेले खड़े थे।
सुबह चाय पीते हुए बाँके बिहारी ने पत्नी से कहा :
‘सुनो।’
‘हाँ।’
‘पचास साल से तुम ठीक कह रही थीं।’
‘क्या ?’ वे हँसी।
‘आँगन में सीढ़ी नंगी है। उसे ढँक देना चाहिए।’
‘हाँ’, उन्होंने आह भरी, ‘बड़े मझले और भैया इन्हीं सीढ़ियों पर नंगे खेलते हुए बड़े हो गए।’
बाँके बिहारी क्षण-भर गायत्री को देखते रहे। फिर बोले—‘छोटे बड़े होकर सीढ़ियों पर फँस गए हैं। हमें सीढ़ियों को ढँकना होगा।’
‘एक ईंट की दीवार कमर तक काफ़ी होगी,’ गायत्री ने कहा।
‘मिस्त्री से पूछ लेंगे।’
फिर बाँके बिहारी ने गायत्री से पूछा :
‘छोटे उठ गए ?’
‘नहीं।’
‘ठीक है। सोने दो।’
गायत्री भीतर चली गईं। बाँके बिहारी चाय का कप नीचे रखकर पौर में गावतकिए पर सिर टिकाए पसर गए। दरवाज़ा खुला था। ताज़ी धूप सड़क पर नर्म कालीन-सी बिछी थी। आँगन में धूप नहीं थी, जब वे अन्दर से कोठे से पौर में आए। अब शायद नीम की पत्तियों से छनकर तने पर फिसलती हुई धूप नंगे फ़र्श पर आ गई होगी। घर के बाहर चबूतरे पर भी धूप घर की दीवार की ओर सरकती हुई लगती थी। घर धूप से घिर गया था।
बाँके बिहारी ने आँखें मूँद लीं। उन्हें लगा, वे अभी पैदा हुए हैं। वे अपने घर की सुबह देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। यह सुबह अपने घर में गायत्री और उनके बीच तनी थी। अलबत्ता छोटे अटारी में सो रहे थे। छोटे शायद अब कभी पूरी तरह ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर यही कहते हैं। वे कहते हैं कि छोटे को देखभाल, दवा-दारू चाहिए। मर्ज दस साल पुराना था। पहले पता ही नहीं चला। फिर कुछ वक़्त शक में गुज़रा। जिस दिन छोटे नूर मंजिल से घर आए, उसी शाम बाँके बिहारी ने बहू को दूसरे कमरे में बोलते सुना था, ‘यह नीम-पागल घर में रहेगा, तो मुन्ना पर क्या असर पड़ेगा ?’ वे दो दिन बाद ही छोटे को लेकर झाँसी आ गए थे। दो बरस बाद मँझले ने छोटे को मुम्बई बुलाया। मँझले की बेटी पँचगनी में पढ़ती थी और उसका तीन कमरे का बड़ा फ़्लैट था। उसने नई फ़ैक्टरी डाली थी। दस माह बाद छोटे ने फोन पर रोते हुए कहा—‘पापा, यहाँ मैं घर का नौकर हो गया हूँ, जिसे वेतन नहीं मिलता।’ तब बाँके बिहारी मुम्बई गए थे और कल रात छोटे को लेकर लौटे थे।
यह सच है कि बाँके बिहारी दस बरस इसी झिलमिल भरोसे में रहे कि छोटे को उसके तीनों बड़े भाई सँभाल लेंगे। भैया अमरीका में था। उसने लिखा था कि पापा, मैं छोटे को यहाँ बुला तो नहीं सकता, मगर इलाज के लिए डॉलर भेज सकता हूँ। डॉलर से क्या नहीं हो सकता, पापा ? भैया, बाँकेलाल बुदबुदाए, डॉलर से नीम-पागल और घर के नौकर ही बनेंगे ! उन्होंने आँखें खोली। एक गौरैया पौर में घुस आई थी और चूँ-चूँ, चूँ-चूँ बोल रही थी। वह एक कोने से दूसरे कोने में उड़ी, फिर तीसरे से चौथे कोने में—और फिर दरवाज़े से फुर्र हो गई।
डॉलर नहीं लूँगा, बाँके बिहारी ने सोचा। नीम-पागल या घर के नौकर के लिए डॉलर दान ही हुआ न ! दान नहीं लूँगा। छोटे मेरा बेटा है। मैं उसे पालूँगा। उन्हें पता ही नहीं चला था। पहले वे उठकर बैठे, फिर खड़े हो गए थे गोया किसी महायात्रा का संकल्प हो।
बाँके बिहारी पौर के चबूतरे पर खड़े थे, जब दरवाज़े की धूप में कोई आकर चुपचाप खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई छाया हो।
‘दद्दा, आप कब आए ?’ छाया बोली।
‘अरे मोहन, कैसे हो ?’ बाँके बिहारी ने सिर घुमाया, ‘मैं रात आया। एक्सप्रेस भी देना।’
मोहन ने पीछे मुड़कर साइकिल के कैरियर से दो अख़बार निकाले और उनके हाथ में थमा दिए। वे खड़े-खड़े एक्सप्रेस देखने लगे। मुख्य ख़बर गुजरात में दंगों की ही थी। कल ट्रेन में दिन-भर कुछ छिटपुट खबरें कानों में पड़ती रही थीं। यह पक्की खबर थी। परसों घटे ‘गोधरा’ का बदला कल गुजरात में लिया था। गोधरा कहाँ था ? गोधरा यदि गुजरात में था तो क्या गुजरात ने गुजरात से बदला लिया ? हत्या लूट, और आगजनी का तांडव हुआ था। पता नहीं क्या-क्या हुआ था ? यह तो पहली खबर थी। ट्रेन में एक गुजराती अहमदाबाद का ‘संदेश’ लिये था—जिसमें गोधरा में हुए बलात्कारों की खबर थी। कल प्रतिशोध अभियान शुरू हुआ। शहर जले थे। अहमदाबाद का चरम पूर्व सांसद एहसान जाफ़री का कल अपराह्न दहन था। भीड़ से घिरे अपने घर के सामने दौड़ते लहूलुहान जाफ़री को ज़िन्दा जला दिया गया था। अहसान ज़ाफरी !
बाँके बिहारी की जीभ पर यह नाम घूमा, जो नूरजहाँ में बदल गया। नूरजहाँ—जो मेरे पोते की माँ है ! बाँके बिहारी अख़बार हाथ में लिए बैठ गए। धूप दरवाज़े की चौखट पर आ गई थी। उन्होंने धूप को घूरते हुए सोचा : आग का कोई भरोसा नहीं। बाबरी मस्जिद ढहने के तुरन्त बाद दस साल पहले नूरजहाँ के पिता लखनऊ में खो गए थे। नूरजहाँ रोई थी। क्या नूरजहाँ फिर रोएगी ? दरवाज़े पर एकाएक धूप चमकी जैसे सूर्य ने कोण बदला हो। बाँके बिहारी को अचानक भैया याद आया जो सिलिकन वैली में जेब में डॉलर खनखनाता घूमता था। उसने पिछली बार बताया था कि वह और उसके दोस्त अमरीका में विश्व हिन्दू परिषद को चन्दा देते हैं। आख़िरकार, उसने कहा था, गोरों के देश में हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहा है। आप नहीं जानते, पापा, उसने कहा था—परदेस में अपना देश कैसे-कैसे याद आता है ! तब शाहरुख खान की फिल्म देखना या मन्दिर जाना बहुत काम आता है। वही समय गुजरात के गाँवों में त्रिशूल-यज्ञ और भगवा-पट्टी बनकर फैला था। उन्हीं हाथों में तलवारें थमी थीं। वही हाथ गुजरात जला रहे थे। गुजरात गुजरात से बदला ले रहा था। क्या मेरा एक बेटा दूसरे बेटे से बदला लेगा ? बाँके बिहारी की आँखों के सामने नूरजहाँ का चेहरा आ गया। उन्होंने उसे फिर एक मुसलमान की तरह देखा जैसे ब्याह के वक़्त देखा था। फिर भूल गए थे। भूला हुआ शिद्दत से दिसम्बर 1992 में याद आया था। फिर लगातार याद आता रहा। जब-जब बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि का मसला गरमाता, बाँके बिहारी को नूरजहाँ का मुसलमान होना याद आता जैसे कोई दर्द बार-बार उठता हो।
अटारी में छोटे की आँख जब खुली तो हल्का-सा अँधेरा था, जो कोनों में गाढ़ा हो रहा था—नीचे फ़र्श पर कोनों में ज़्यादा। छप्पर पर उजाले के कुछ छेद थे। सुबह का समाँ था। मगर आँगन के पेड़ से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। चिड़ियों की बातें मुम्बई के फ़्लैट में बहुत याद आती थीं—क्योंकि वे वहाँ नहीं थीं। वहाँ ऐसा दरवाज़ा भी नहीं था, जो छत पर खुलता हो। छत पर सुबह का उजाला था।
धूप नहीं थी।
छोटे निकर पहने सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसने सिर ऊपर घुमाया। नीम की पत्तियाँ हौले-हौले हिल रही थीं। चिड़ियाँ नहीं थीं। कहाँ गईं सारी चिड़ियाँ ? क्या अपना पेड़ भूल गईं ? या कोई और पेड़ याद आ गया ? सारी चिड़ियाँ आसमान में एक-साथ मर तो नहीं सकतीं ? चिड़ियों में सामूहिक हत्या या आगजनी का रिवाज़ भी नहीं था।
‘अम्माँ’, छोटे ने चौके में बैठते हुए कहा।
‘‘हाँ’, गायत्री दूसरी ओर चूल्हे के बगल में बैठे हुए बोलीं।
‘चिड़ियाँ कहाँ गईं ?’
‘कौन-सी चिड़ियाँ ?’ गायत्री ने आँखें घुमाईं।
‘अपने नीम की चिड़ियाँ ?’
‘घूमने गई हैं’, गायत्री हँसी।
‘कहाँ ?’
‘दूसरे पेड़ों या घरों या आसमान में।’
‘क्यों ?’
‘यही उनका दिन-भर का काम है।’
‘वे भी काम करती हैं ?’
‘हाँ’, गायत्री ने छोटे की ओर देखा।
चूल्हे से धुआँ उठा। गायत्री की आँखों में भर गया। उन्होंने आँखें मूँदकर खोलीं। आँखों में आँसू डबडबा आए। डबडबाई आँखों में छोटे की आकृति काँपने लगी।
धुआँ चौके के दोनों मेहराबों से अपने गुंजलक बनाते हुए आँगन में बिखर गया। छोटे चौके में दूसरी ओर मेड़ पर उकडूँ बैठा था। वह आँगन में लहराते धुएँ को देख रहा था। एकाएक उसे लगा कि पेड़ से आँगन में अँधेरा चू रहा है। वह देखता ! पेड़ से अँधेरा सूखी पत्तियों की तरह गिर रहा था।
सूर्य कहाँ गया ?
‘अम्माँ’, छोटे ने अचानक कहा, ‘आज क्या दिन नहीं होगा ? सुबह के बाद रात होगी ?’
‘यह सुबह नहीं है’, गायत्री हँसी, ‘शाम है।’
‘पर’, छोटे ने सिर चारों ओर घुमाया, ‘पर दिन कहाँ गया ?’
‘दिन-भर तुम सोते रहे।’
छोटे ने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा।
वह चौके में बैठा कुछ देर चाय पीता रहा और आँगन में गिरता अँधेरा देखता रहा। कोई पक्षी पेड़ पर बोला। क्या आज पक्षी पेड़ पर चुपचौप लौटे थे ?
1.2
दीवार खड़ी हो रही थी।
गायत्री ने पचास वर्ष पहले कहा था जब बड़े पैदा हुए। फिर बड़े और मँझले और भैया बड़े होते रहे और वे भूल गईं। अब जब छोटे मुम्बई से लौटे तो उन्हें फिर याद आया जो उन्होंने पचास वर्ष पहले कहा था। यह छोटे का आख़िरी लौटना था।
नीम की पत्तियों में अपनी चहचहाहट को छोड़कर चिड़ियाँ उड़ गई थीं। सूर्य आसमान में कुछ ऊपर उठ आया था। छत को लाँघकर धूप आँगन में पसर गई थी। सीढ़ियों पर नीम के नीचे पेड़ की छाया थी, जहाँ दीवार खड़ी हो रही थी। बाँके बिहारी सुबह की छाया में खड़े थे। मिस्त्री ईंट पर ईंट रख रहा था। मजदूर उसे ईंट देता जाता था। पास में तसले में सीमेंट और बालू का मसाला था, जो दो ईंटों के बीच में भरा जाता था। बाँके बिहारी उसी ओर मुँह किए खड़े थे।
गायत्री ने पचास वर्ष पहले कहा था जब बड़े पैदा हुए। फिर बड़े और मँझले और भैया बड़े होते रहे और वे भूल गईं। अब जब छोटे मुम्बई से लौटे तो उन्हें फिर याद आया जो उन्होंने पचास वर्ष पहले कहा था। यह छोटे का आख़िरी लौटना था।
नीम की पत्तियों में अपनी चहचहाहट को छोड़कर चिड़ियाँ उड़ गई थीं। सूर्य आसमान में कुछ ऊपर उठ आया था। छत को लाँघकर धूप आँगन में पसर गई थी। सीढ़ियों पर नीम के नीचे पेड़ की छाया थी, जहाँ दीवार खड़ी हो रही थी। बाँके बिहारी सुबह की छाया में खड़े थे। मिस्त्री ईंट पर ईंट रख रहा था। मजदूर उसे ईंट देता जाता था। पास में तसले में सीमेंट और बालू का मसाला था, जो दो ईंटों के बीच में भरा जाता था। बाँके बिहारी उसी ओर मुँह किए खड़े थे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i