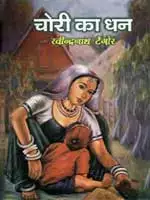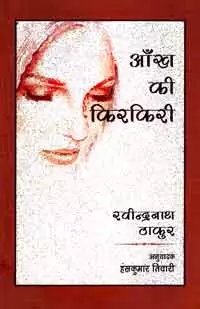|
कहानी संग्रह >> चोरी का धन चोरी का धनरबीन्द्रनाथ टैगोर
|
236 पाठक हैं |
|||||||
श्रेष्ठ कहानी-संग्रह...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पोस्टमास्टर
काम शुरू करते ही पहले पहल पोस्टमास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा। गांव
बहुत साधारण था। गांव के पास ही एक नील-कोठी थी। इसीलिए कोठी के स्वामी ने
बहुत कोशिश करके यह नया पोस्टऑफिस खुलवाया था।
हमारे पोस्टमास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है वही दशा इस बड़े गांव में आकर इन पोस्टमास्टर की हुई। एक अंधेरी आठचाला1 में उनका ऑफिस था, पास ही काई से घिरा एक तालाब था, जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमाश्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे उन्हें अक्सर फुर्सत नहीं रहती थी, न वे शिष्टजनों से मिलने-जुलने के योग्य ही थे।
खासतौर से कलकत्ता के बाबू ठीक तरह से मिलना-जुलना नहीं जानते। नई जगह में पहुंचकर वे या तो उद्धत हो जाते हैं या अप्रतिभ। इसलिए स्थानीय लोगों से उनका मेल-जोल नहीं हो पाता। इधर काम भी ज्यादा नहीं था। कभी-कभी एकाध कविता लिखने की कोशिश करते। उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त करते-दिनभर तरु-पल्लवों का कम्पन और आकाश के बादल देखते-देखते जीवन बड़े सुख से कट जाता है। लेकिन अन्तर्यामी जानते हैं कि यदि अलिफलैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में तरु-पल्लव समेत इन सारे पेड़-पौधों को काटकर पक्का रास्ता तैयार कर देता और पंक्तिबद्ध अट्टालिकाओं द्वारा बादलों को दृष्टि से ओझल कर देता तो यह मृतप्राय भद्र वंशधर नवीन जीवन-लाभ कर लेता।
पोस्टमास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथों बनाकर खाना पड़ता और गांव की एक मातृ-पितृ-हीन अनाथ बालिका इनका काम-काज कर देती थी। उसको थोड़ा-बहुत खाना मिल जाता। लड़की का नाम था रतन। उम्र बारह-तेरह। उसके विवाह की कोई विशेष सम्भावना नहीं दिखाई देती थी।
शाम को जब गांव की गोशाला से कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झींगुर बोलते दूर के गांव में पियक्कड़ बाउलों का दल ढोल-करताल बजाकर ऊंचे स्वर
------------------------
1. फूस के अठपहलू से ढका बड़ा घर।
में गीत छेड़ देता-जब अन्दर बरामदे में अकेले बैठे-बैठे वृक्षों का कम्पन देखकर कवि-हृदय में भी ईषत् हृत्कंप होने लगता तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्टमास्टर आवाज लगाते-‘रतन’।
रतन दरवाजे पर बैठी इस आवाज की प्रतीक्षा करती रहती। लेकिन पहली आवाज पर ही अन्दर न आती। वहीं से कहती, ‘‘क्या है बाबू, किसलिए बुला रहे हो ?’’
पोस्टमास्टर, ‘‘तू क्या कर रही है ?’’
रतन, ‘‘बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूं, रसोईघर में।’’
पोस्टमास्टर, ‘‘तेरा रसोई का काम पीछे हो जायेगा। पहले हुक्का भर ला !’’
थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती-मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्टमास्टर चट से पूछ बैठते, ‘‘अच्छा रतन, तुझे अपनी मां की याद है ?’’
बड़ी लम्बी बातें हैं, बहुत-सी याद हैं, बहुत-सी याद भी नहीं। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी-थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से दो-एक शामों की याद उसके मन में चित्र के समान अंकित है। उन्हीं की बात करते-करते धीरे-धीरे रतन पोस्टमास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाती। उसे ध्यान आता, उसका एक भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ-मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद उसे अधिक आती। इस तरह बातें करते-करते कभी-कभी काफी रात हो जाती। तब आलस के मारे पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सबेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लेती। उन्हीं से दोनों के रात्रि-भोजन का काम चल जाता।
कभी-कभी शाम को उस बृहत् आठचाला के एक कोने में ऑफिस की काठ की कुर्सी पर बैठे-बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बात चलाते-छोटे-भाई की बात, मां और दीदी की बात, प्रवास में एकान्त कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता उनकी बात। जो बातें उनके मन में बार-बार उदय होती रहतीं, पर जो नील-कोठी के गुमाश्तों के सामने किसी भी तरह नहीं उठाई जा सकती थीं, उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल संकोच न लगता। अन्त में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिरपरिचितों के समान खुद भी मां, दादा, दीदी कहने लगी। यहां तक कि अपने नन्हे-से हृदयपट पर उसने उनकी काल्पनिक मूर्ति भी चित्रित कर ली थी।
एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छंट गए थे और हलका-सा ताप लिये सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़-पौधों से एक प्रकार की गन्ध निकल रही थी; ऐसा लगता था मानो क्लान्त धरती का उष्ण निःश्वास अंगों को छू रहा हो और न जाने कहां का एक हठी पक्षी दोपहर-भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यन्त करुण स्वर में अपनी नालिश दुहरा रहा था। उस दिन पोस्टमास्टर के हाथ खाली थे। वर्षों के धुले लहलहाते चिकने मृदुल तरु-पल्लव और धूप में चमकते पराजित वर्षा के भग्नावशिष्ट स्तूपाकार बादल सचमुच देखने योग्य थे।
पोस्टमास्टर उन्हें देखते जाते और सोचते जाते कि इस समय यदि कोई आत्मीय अपने पास होता, हृदय के साथ एकान्त संलग्न कोई स्नेह की प्रतिमा मानव-मूर्ति। धीरे-धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वह पक्षी भी बार-बार यही कह रहा हो, और मानो उस निर्जन में तरु-छाया में डूबी दोपहर के पल्लव-मर्मर का भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। न तो कोई विश्वास कर सकता, न जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतन भोगी उस सब-पोस्टमास्टर के मन में छुट्टी के लम्बे दिनों में गम्भीर सुनसान दोपहर में इसी प्रकार के भाव उदय होते रहते।
पोस्टमास्टर ने एक दीर्घ निःश्वास लिया और फिर आवाज लगाई, ‘‘रतन !’’
रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी वह मालिक की आवाज सुनते ही तुरन्त दौड़ी हुई आई और हांफती-हांफती बोली, ‘‘भैयाजी, बुला रहे थे ?’
पोस्टमास्टर ने कहा, ‘‘मैं तुझे थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा।’’ और फिर दोपहर-भर उसके साथ ‘छोटा अ’, ‘बड़ा अ’ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिए।
सावन का महीना था। लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब, सब पानी से भर गए थे। रात-दिन मेढक की टर्र-टर्र और वर्षा की आवाज। गांव के रास्तों में चलना-फिरना लगभग बन्द हो गया था। हाट के लिए नाव में चढ़कर जाना पड़ता।
एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथासमय उसकी बुलाहट न हुई तो खुद किताबों का थैला लिये धीरे-धीरे भीतर आई। देखा, पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वह चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा ‘रतन !’ झपटकर लौटकर भीतर जाकर उसने कहा, ‘‘भैयाजी, सो रहे थे ?’’
पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, ‘‘तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर तो देख !’’
घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तप्त ललाट पर शंख की चूड़ियां पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवास में रोग की पीड़ा में यह सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता और दीदी बैठी हैं और प्रवासी के मन की यह अभिलाषा व्यर्थ नहीं गई। बालिका रतन बालिका न रही। उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई, यथासमय गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, ‘‘भैयाजी कुछ आराम है क्या ?’’
बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग-शय्या छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया, अब और नहीं। जैसे भी हो, अब यहां से बदली करानी चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी।
रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया। लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी। वह बीच-बीच में झांककर देखती-पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। जिस समय इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वे अधीर होकर अपनी दरख्वास्त के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दुहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा उसकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ न हो जाय इसकी उसे आशंका थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उस की पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, ‘‘भैयाजी, मुझे बुलाया था ?’’
पोस्टमास्टर ने कहा, ‘‘रतन, मैं कल ही चला जाऊंगा।’’
रतन, ‘‘कहां चले जाओगे भैयाजी !’’
पोस्टमास्टर, ‘‘घर जाऊंगा।’’
रतन, ‘‘फिर कब लौटोगे ?’’
पोस्टमास्टर, ‘‘अब नहीं लौटूंगा।’’
रतन ने और कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी थी, पर दरख्वास्त नामंजूर हो गई इसलिए वे इस्तीफा देकर घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने और कोई बात नहीं की। दीया टिमटिमाता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेदकर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप-टप करता टपकता रहा।
बड़ी देर के बाद इतने धीरे उठकर रसोईघर में रोटियां बनाने चली गई। पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी-जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह-रहकर तरह-तरह की आशंकाएं उठ रही थीं। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, ‘‘भैयाजी, मुझे अपने घर ले चलोगे ?’’
पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, ‘‘वाह, यह कैसे हो सकता है !’’ किन कारणों से यह बात सम्भव न थी, बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा।
रातभर जागते और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी-मिश्रित स्वर गूंजते रहे, ‘वाह, यह कैसे हो सकता है।’
सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वे ताजे पानी से ही स्नान करते थे। न जाने क्यों बालिका यह नहीं पूछ सकी थी कि वे सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़के ही जरूरत न पड़ जाय, यह सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भरकर ले आई थी। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखा।
मालिक ने कहा, ‘‘रतन, मेरी जगह जो सज्जन आयेंगे मैं उन्हें कह जाऊंगा। वे मेरी ही तरह तेरी देख-भाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।’’ इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये बातें अत्यन्त स्नेहपूर्ण और दयार्द्र हृदय से निकली थीं, किन्तु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है ! रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वह सहन न कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते-रोते कहा, ‘‘नहीं, नहीं। तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती।’’
पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे अवाक् रह गए।
नया पोस्टमास्टर आया। उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते-चलते रतन को बुलाकर बोले, ‘‘रतन, तुझे मैं कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूं, इससे कुछ दिन तेरा काम चल जायेगा।’’
तनख्वाह में जो रुपये मिले थे उनमें से राह-खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपये जेब से निकाले। यह देखकर रतन धूल में लोटकर उनके पैरों से लिपटकर बोली, ‘‘भैयाजी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मेरे लिए किसी को कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं।’’ और यह कहते-कहते वह तुरन्त वहां से भाग गई।
भूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ निःश्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कन्धे पर छाता रखे, कुली के सिर पर नीली-सफेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीरे-धीरे नाव की ओर चल दिए।
जब वे नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती अश्रु-धारा के समान चारों ओर छलछल करने लगी, तब वे अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्व-व्यापी बृहत् अव्यक्त मर्म-व्यथा प्रकट करने लग गया।
एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जायें और जगत् की गोद से वंचित उस अनाथिनी को साथ ले आयें। लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी, वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी-किनारे का श्मशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए पथिक के उदास हृदय में यह सत्य उदित हो रहा था, ‘‘जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने के क्या लाभ ! संसार में कौन किसका है !’
लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्टऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद उसके मन में हल्की-सी आशा जीवित थी कि हो सकता है, भैयाजी, लौट आयें। आशा के इसी बन्धन से बंधी वह किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी।
हाय रे बुद्धिहीन मानव-हृदय ! तेरी भ्रान्ति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद मस्तिष्क में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके मिथ्या आशा को अपनी दोनों बांहों से जकड़कर तू भरसक छाती से चिपकाए रहता है। अन्त में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर, हृदय का सारा रक्त चूसकर वह निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रान्ति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल हो उठता है।
हमारे पोस्टमास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है वही दशा इस बड़े गांव में आकर इन पोस्टमास्टर की हुई। एक अंधेरी आठचाला1 में उनका ऑफिस था, पास ही काई से घिरा एक तालाब था, जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमाश्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे उन्हें अक्सर फुर्सत नहीं रहती थी, न वे शिष्टजनों से मिलने-जुलने के योग्य ही थे।
खासतौर से कलकत्ता के बाबू ठीक तरह से मिलना-जुलना नहीं जानते। नई जगह में पहुंचकर वे या तो उद्धत हो जाते हैं या अप्रतिभ। इसलिए स्थानीय लोगों से उनका मेल-जोल नहीं हो पाता। इधर काम भी ज्यादा नहीं था। कभी-कभी एकाध कविता लिखने की कोशिश करते। उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त करते-दिनभर तरु-पल्लवों का कम्पन और आकाश के बादल देखते-देखते जीवन बड़े सुख से कट जाता है। लेकिन अन्तर्यामी जानते हैं कि यदि अलिफलैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में तरु-पल्लव समेत इन सारे पेड़-पौधों को काटकर पक्का रास्ता तैयार कर देता और पंक्तिबद्ध अट्टालिकाओं द्वारा बादलों को दृष्टि से ओझल कर देता तो यह मृतप्राय भद्र वंशधर नवीन जीवन-लाभ कर लेता।
पोस्टमास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथों बनाकर खाना पड़ता और गांव की एक मातृ-पितृ-हीन अनाथ बालिका इनका काम-काज कर देती थी। उसको थोड़ा-बहुत खाना मिल जाता। लड़की का नाम था रतन। उम्र बारह-तेरह। उसके विवाह की कोई विशेष सम्भावना नहीं दिखाई देती थी।
शाम को जब गांव की गोशाला से कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झींगुर बोलते दूर के गांव में पियक्कड़ बाउलों का दल ढोल-करताल बजाकर ऊंचे स्वर
------------------------
1. फूस के अठपहलू से ढका बड़ा घर।
में गीत छेड़ देता-जब अन्दर बरामदे में अकेले बैठे-बैठे वृक्षों का कम्पन देखकर कवि-हृदय में भी ईषत् हृत्कंप होने लगता तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्टमास्टर आवाज लगाते-‘रतन’।
रतन दरवाजे पर बैठी इस आवाज की प्रतीक्षा करती रहती। लेकिन पहली आवाज पर ही अन्दर न आती। वहीं से कहती, ‘‘क्या है बाबू, किसलिए बुला रहे हो ?’’
पोस्टमास्टर, ‘‘तू क्या कर रही है ?’’
रतन, ‘‘बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूं, रसोईघर में।’’
पोस्टमास्टर, ‘‘तेरा रसोई का काम पीछे हो जायेगा। पहले हुक्का भर ला !’’
थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती-मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्टमास्टर चट से पूछ बैठते, ‘‘अच्छा रतन, तुझे अपनी मां की याद है ?’’
बड़ी लम्बी बातें हैं, बहुत-सी याद हैं, बहुत-सी याद भी नहीं। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी-थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से दो-एक शामों की याद उसके मन में चित्र के समान अंकित है। उन्हीं की बात करते-करते धीरे-धीरे रतन पोस्टमास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाती। उसे ध्यान आता, उसका एक भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ-मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद उसे अधिक आती। इस तरह बातें करते-करते कभी-कभी काफी रात हो जाती। तब आलस के मारे पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सबेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लेती। उन्हीं से दोनों के रात्रि-भोजन का काम चल जाता।
कभी-कभी शाम को उस बृहत् आठचाला के एक कोने में ऑफिस की काठ की कुर्सी पर बैठे-बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बात चलाते-छोटे-भाई की बात, मां और दीदी की बात, प्रवास में एकान्त कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता उनकी बात। जो बातें उनके मन में बार-बार उदय होती रहतीं, पर जो नील-कोठी के गुमाश्तों के सामने किसी भी तरह नहीं उठाई जा सकती थीं, उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल संकोच न लगता। अन्त में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिरपरिचितों के समान खुद भी मां, दादा, दीदी कहने लगी। यहां तक कि अपने नन्हे-से हृदयपट पर उसने उनकी काल्पनिक मूर्ति भी चित्रित कर ली थी।
एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छंट गए थे और हलका-सा ताप लिये सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़-पौधों से एक प्रकार की गन्ध निकल रही थी; ऐसा लगता था मानो क्लान्त धरती का उष्ण निःश्वास अंगों को छू रहा हो और न जाने कहां का एक हठी पक्षी दोपहर-भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यन्त करुण स्वर में अपनी नालिश दुहरा रहा था। उस दिन पोस्टमास्टर के हाथ खाली थे। वर्षों के धुले लहलहाते चिकने मृदुल तरु-पल्लव और धूप में चमकते पराजित वर्षा के भग्नावशिष्ट स्तूपाकार बादल सचमुच देखने योग्य थे।
पोस्टमास्टर उन्हें देखते जाते और सोचते जाते कि इस समय यदि कोई आत्मीय अपने पास होता, हृदय के साथ एकान्त संलग्न कोई स्नेह की प्रतिमा मानव-मूर्ति। धीरे-धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वह पक्षी भी बार-बार यही कह रहा हो, और मानो उस निर्जन में तरु-छाया में डूबी दोपहर के पल्लव-मर्मर का भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। न तो कोई विश्वास कर सकता, न जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतन भोगी उस सब-पोस्टमास्टर के मन में छुट्टी के लम्बे दिनों में गम्भीर सुनसान दोपहर में इसी प्रकार के भाव उदय होते रहते।
पोस्टमास्टर ने एक दीर्घ निःश्वास लिया और फिर आवाज लगाई, ‘‘रतन !’’
रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी वह मालिक की आवाज सुनते ही तुरन्त दौड़ी हुई आई और हांफती-हांफती बोली, ‘‘भैयाजी, बुला रहे थे ?’
पोस्टमास्टर ने कहा, ‘‘मैं तुझे थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा।’’ और फिर दोपहर-भर उसके साथ ‘छोटा अ’, ‘बड़ा अ’ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिए।
सावन का महीना था। लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब, सब पानी से भर गए थे। रात-दिन मेढक की टर्र-टर्र और वर्षा की आवाज। गांव के रास्तों में चलना-फिरना लगभग बन्द हो गया था। हाट के लिए नाव में चढ़कर जाना पड़ता।
एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथासमय उसकी बुलाहट न हुई तो खुद किताबों का थैला लिये धीरे-धीरे भीतर आई। देखा, पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वह चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा ‘रतन !’ झपटकर लौटकर भीतर जाकर उसने कहा, ‘‘भैयाजी, सो रहे थे ?’’
पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, ‘‘तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर तो देख !’’
घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तप्त ललाट पर शंख की चूड़ियां पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवास में रोग की पीड़ा में यह सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता और दीदी बैठी हैं और प्रवासी के मन की यह अभिलाषा व्यर्थ नहीं गई। बालिका रतन बालिका न रही। उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई, यथासमय गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, ‘‘भैयाजी कुछ आराम है क्या ?’’
बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग-शय्या छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया, अब और नहीं। जैसे भी हो, अब यहां से बदली करानी चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी।
रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया। लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी। वह बीच-बीच में झांककर देखती-पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। जिस समय इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वे अधीर होकर अपनी दरख्वास्त के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दुहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा उसकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ न हो जाय इसकी उसे आशंका थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उस की पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, ‘‘भैयाजी, मुझे बुलाया था ?’’
पोस्टमास्टर ने कहा, ‘‘रतन, मैं कल ही चला जाऊंगा।’’
रतन, ‘‘कहां चले जाओगे भैयाजी !’’
पोस्टमास्टर, ‘‘घर जाऊंगा।’’
रतन, ‘‘फिर कब लौटोगे ?’’
पोस्टमास्टर, ‘‘अब नहीं लौटूंगा।’’
रतन ने और कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी थी, पर दरख्वास्त नामंजूर हो गई इसलिए वे इस्तीफा देकर घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने और कोई बात नहीं की। दीया टिमटिमाता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेदकर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप-टप करता टपकता रहा।
बड़ी देर के बाद इतने धीरे उठकर रसोईघर में रोटियां बनाने चली गई। पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी-जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह-रहकर तरह-तरह की आशंकाएं उठ रही थीं। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, ‘‘भैयाजी, मुझे अपने घर ले चलोगे ?’’
पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, ‘‘वाह, यह कैसे हो सकता है !’’ किन कारणों से यह बात सम्भव न थी, बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा।
रातभर जागते और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी-मिश्रित स्वर गूंजते रहे, ‘वाह, यह कैसे हो सकता है।’
सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वे ताजे पानी से ही स्नान करते थे। न जाने क्यों बालिका यह नहीं पूछ सकी थी कि वे सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़के ही जरूरत न पड़ जाय, यह सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भरकर ले आई थी। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखा।
मालिक ने कहा, ‘‘रतन, मेरी जगह जो सज्जन आयेंगे मैं उन्हें कह जाऊंगा। वे मेरी ही तरह तेरी देख-भाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।’’ इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये बातें अत्यन्त स्नेहपूर्ण और दयार्द्र हृदय से निकली थीं, किन्तु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है ! रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वह सहन न कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते-रोते कहा, ‘‘नहीं, नहीं। तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती।’’
पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे अवाक् रह गए।
नया पोस्टमास्टर आया। उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते-चलते रतन को बुलाकर बोले, ‘‘रतन, तुझे मैं कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूं, इससे कुछ दिन तेरा काम चल जायेगा।’’
तनख्वाह में जो रुपये मिले थे उनमें से राह-खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपये जेब से निकाले। यह देखकर रतन धूल में लोटकर उनके पैरों से लिपटकर बोली, ‘‘भैयाजी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मेरे लिए किसी को कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं।’’ और यह कहते-कहते वह तुरन्त वहां से भाग गई।
भूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ निःश्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कन्धे पर छाता रखे, कुली के सिर पर नीली-सफेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीरे-धीरे नाव की ओर चल दिए।
जब वे नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती अश्रु-धारा के समान चारों ओर छलछल करने लगी, तब वे अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्व-व्यापी बृहत् अव्यक्त मर्म-व्यथा प्रकट करने लग गया।
एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जायें और जगत् की गोद से वंचित उस अनाथिनी को साथ ले आयें। लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी, वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी-किनारे का श्मशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए पथिक के उदास हृदय में यह सत्य उदित हो रहा था, ‘‘जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने के क्या लाभ ! संसार में कौन किसका है !’
लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्टऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद उसके मन में हल्की-सी आशा जीवित थी कि हो सकता है, भैयाजी, लौट आयें। आशा के इसी बन्धन से बंधी वह किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी।
हाय रे बुद्धिहीन मानव-हृदय ! तेरी भ्रान्ति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद मस्तिष्क में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके मिथ्या आशा को अपनी दोनों बांहों से जकड़कर तू भरसक छाती से चिपकाए रहता है। अन्त में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर, हृदय का सारा रक्त चूसकर वह निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रान्ति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल हो उठता है।
एक रात
एक ही पाठशाला में सुरबाला के साथ पढ़ा हूं, और बउ-बउ1 खेला हूं। उसके घर
जाने पर सुरबाला की मां मुझे बड़ा प्यार करतीं और हम दोनों को साथ बिठाकर
कहतीं, ‘वाह, कितनी सुन्दर जोड़ी है।’
छोटा था, किन्तु बात का अभिप्राय प्रायः समझ लेता था। सुरबाला पर अन्य सर्वसाधारण की अपेक्षा मेरा कुछ विशेष अधिकार था, यह धारणा मेरे मन में बद्धमूल हो गई थी। इस अधिकार-मद से मत्त होकर उस पर मैं शासन और अत्याचार न करता होऊं, ऐसी बात न थी। वह भी सहिष्णुभाव से हर तरह से मेरी फरमाइश पूरी करती और दण्ड वहन करती। मुहल्ले में उसके रूप की प्रशंसा थी, किन्तु बर्बर बालक की दृष्टि में उस सौन्दर्य का कोई महत्त्व नहीं था-मैं तो बस यही जानता था कि सुरबाला ने अपने पिता के घर में मेरा प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए ही जन्म लिया है, इसीलिए वह विशेष रूप से मेरी अवहेलना की पात्री है।
मेरे पिता चौधरी जमींदार के नायब थे। उनकी इच्छा थी, मेरे काम करने योग्य होते ही मुझे जमींदारी-सरिश्ते का काम सिखाकर कहीं गुमाश्तागिरी दिला दें। किन्तु मैं मन-ही-मन इसका विरोधी था। हमारे मुहल्ले के नीलरतन जिस तरह भागकर कलकत्ता में पढ़ना-लिखना सीखकर कलक्टर साहब के नाजिर हो गए थे उसी तरह मेरे जीवन का लक्ष्य भी अत्युच्च था, ‘कलक्टर का नाजिर न बन सका तो जजी अदालत का हेड क्लर्क हो जाऊंगा’, मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था।
मैं हमेशा देखता कि मेरे पिता इन अदालतजीवियों का बहुत सम्मान करते थे-अनेक अवसरों पर मछली-तरकारी, रुपये पैसे से उनकी पूजार्चना करनी पड़ती, यह बात भी मैं बाल्यावस्था से ही जानता था; इसलिए मैंने अदालत के छोटे कर्मचारी, यहां तक कि हरकारों को भी अपने हृदय में बड़े सम्मान का स्थान दे रखा था। ये हमारे बंगाल के पूज्य देवता थे, तेतीस कोटि देवताओं के छोटे-छोटे नवीन संस्करण। कार्य-सिद्धि-लाभ के सम्बन्ध में स्वयं सिद्धिदाता गणेश की
------------------------------
1. छोटी बालिकाओं का खेल; जिसमें बहू के समान सजकर, घूंघट निकालकर गृहिणी का अभिनय करती हैं।
अपेक्षा इनके प्रति लोगों में आन्तरिक निर्भरता कहीं अधिक थी, अतएव पहले गणेश को जो कुछ प्राप्त होता था वह आजकल इन्हें मिलता था।
नीलरतन के दृष्टांत से उत्साहित होकर मैं एक दिन विशेष सुविधा पाकर कलकत्ता भाग गया। पहले तो गांव के एक परिचित व्यक्ति के घर ठहरा, उसके बाद पढ़ाई के लिए पिता से भी थोड़ी-बहुत सहायता मिलने लग गई। पढ़ना-लिखना नियमपूर्वक चलने लगा। इसके अतिरिक्त मैं सभा-समितियों में भी योग देता। देश के लिए प्राण-विसर्जन करने की तत्काल आवश्यकता है, इस विषय में मुझे कोई सन्देह न था। किन्तु, यह दुस्साध्य कार्य किस, प्रकार किया जा सकता है, यह मैं नहीं जानता था; न इसका कोई दृष्टांत ही दिखाई पड़ता था। पर इससे मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हम देहाती थे, कम उम्र में ही प्रौढ़ बुद्धि रखने वाले कलकत्ता वालों की तरह हर चीज का मजाक उड़ाना हमने नहीं सीखा था; इसलिए हम लोग चन्दे की किताब लेकर भूखे-प्यासे दोपहर की धूप से दर-दर भीख मांगते फिरते, किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटते, सभा-स्थल में जोकर बेंच-कुर्सी लगाते, दलपति के बारे में किसी के कुछ कहने पर कमर बांधकर मार-पीट करने पर उतारू हो जाते। शहर के लड़के हमारे ये लक्षण देखकर हमें गंवार कहते।
आया तो था नाजिर सरिश्तेदार बनने, पर मैजिनी, गैरीबाल्डी बनने की तैयारी करने लग गया।
इसी समय मेरे पिता और सुरबाला के पिता ने एकमत होकर सुरबाला के साथ मेरा विवाह कर देने का निश्चय किया।
मैं पन्द्रह वर्ष की अवस्था में कलकत्ता भाग आया था, उस समय सुरबाला की अवस्था आठ वर्ष थी; अब मैं अठारह वर्ष का था। पिता के अनुसार मेरे विवाह की आयु धीरे-धीरे निकली जा रही थी। पर मैंने मन-ही-मन यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन अविवाहित रहकर स्वदेश के लिए मर मिटूंगा। मैंने पिता से कहा, ‘पढ़ाई पूरी किये बिना मैं विवाह नहीं कर सकता।’’
दो-चार महीने के बाद ही खबर मिली कि वकील रामलोचन बाबू के साथ सुरबाला का विवाह हो गया है। मैं तो पतित भारत की चंदा-वसूली के काम में व्यस्त था, मुझे यह समाचार अत्यन्त तुच्छ मालूम पड़ा।
एन्ट्रेंस पास कर लिया था, फर्स्ट ईयर आर्ट्स में जाने का विचार था कि तभी पिता की मृत्यु हो गई। परिवार में मैं अकेला नहीं था; माता थीं और दो बहनें। अतएव कॉलेज छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद नोआखाली डिवीजन के एक छोटे-से शहर के एन्ट्रेंस स्कूल में असिस्टैण्ट मास्टर का पद मिला।
सोचा, ‘मेरे उपयुक्त काम मिल गया। उपदेश तथा उत्साह प्रदान करके प्रत्येक विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा।’
काम आरम्भ कर दिया। देखा, भारतवर्ष के भविष्य की अपेक्षा आसन्न इम्तहान की चिन्ता कहीं ज्यादा की जाती थी। छात्रों को ग्रामर और एलजेबरा के बाहर की कोई बात बताते ही हेडमास्टर नाराज हो जाते। दो एक महीने में मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया।
हमारे जैसे प्रतिभाहीन लोग घर में बैठकर तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, पर अन्त में कर्म-क्षेत्र में उतरते ही कन्धे पर हल का बोझ ढोते हुए पीछे से पूंछ मरोड़ी जाने पर भी सिर झुकाए सहिष्णु भाव से प्रतिदिन खेत गोड़ने का काम कर संध्या को भर-पेट चारा पाकर ही सन्तुष्ट रहते हैं; फिर कूद-फांद करने का उत्साह नहीं बचता।
आग लगने के डर से एक-न-एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता। मैं अकेला था, इसलिए यह भार मेरे ही ऊपर आ पड़ा। स्कूल के बड़े आठचाला से सटी हुई एक झोंपड़ी में मैं रहता।
स्कूल बस्ती से कुछ दूर एक बड़ी पुष्कणी के किनारे था। चारों ओर सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ तथा स्कूल से लगे आपस में सटे हुए नीम के दो पुराने विशाल पेड़ छाया देते रहते।
अभी तक मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया, न मैंने उसे उस योग्य ही समझा। यहां के सरकारी वकील रामलोचन राय का घर हमारे स्कूल के पास ही था और उनके साथ उनकी स्त्री मेरी बाल्य-सखी सुरबाला थी, यह मैं जानता था।
रामलोचन बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ। सुरबाला के साथ मेरा बचपन में परिचय था यह रामलोचन बाबू जानते थे या नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने भी नया परिचय होने के कारण उस विषय में कुछ कहना उचित न समझा। यही नहीं सुरबाला किसी समय मेरे जीवन के साथ किसी रूप में जुड़ी हुई थी, यह बात मेरे मन में ठीक तरह से उठी ही नहीं।
एक दिन छुट्टी के रोज रामलोचन बाबू से भेंट करने उनके घर गया था। याद नहीं किस विषय पर बातचीत हो रही थी, शायद वर्तमान भारतवर्ष दुरव्यस्था के सम्बन्ध में। यह बात न थी कि वे उसके लिए विशेष चिंतित और उदास थे, किन्तु विषय ऐसा था कि हुक्का पीते-पीते उस पर एक-डेढ़ घण्टे तक यों ही शौकिया दुःख प्रकट किया जा सकता था।
तभी बगल के कमरे में चूड़ियों की हल्की-सी खनखनाहट, साड़ी की सरसराहट और पैरों की भी कुछ आहट सुनाई पड़ी। मैं अच्छी तरह समझ गया कि जंगले की संध से कोई कौतूहलपूर्ण आंखें मुझे देख रही हैं।
मुझे तत्काल वे आंखें याद ही आईं-विश्वास, सरलता और बालसुलभ प्रीति से छलछलाती दो बड़ी-बड़ी आंखें, काली-काली पुतलियां घनी काली पलकें, और स्थिर स्निग्ध दृष्टि। सहसा मेरे हृत्पिंड को मानो किसी ने अपनी कड़ी मुट्ठी में भींच लिया। वेदना से मेरा अन्तर झनझना उठा।
लौटकर घर आ गया, किन्तु वह व्यथा बनी रही। पढ़ना-लिखना, जो भी करता किसी तरह मन का भार दूर न हो पाता, मन सहसा एक भारी बोझ के समान हृदय की शिराओं को पकड़कर झूलने लग गया।
छोटा था, किन्तु बात का अभिप्राय प्रायः समझ लेता था। सुरबाला पर अन्य सर्वसाधारण की अपेक्षा मेरा कुछ विशेष अधिकार था, यह धारणा मेरे मन में बद्धमूल हो गई थी। इस अधिकार-मद से मत्त होकर उस पर मैं शासन और अत्याचार न करता होऊं, ऐसी बात न थी। वह भी सहिष्णुभाव से हर तरह से मेरी फरमाइश पूरी करती और दण्ड वहन करती। मुहल्ले में उसके रूप की प्रशंसा थी, किन्तु बर्बर बालक की दृष्टि में उस सौन्दर्य का कोई महत्त्व नहीं था-मैं तो बस यही जानता था कि सुरबाला ने अपने पिता के घर में मेरा प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए ही जन्म लिया है, इसीलिए वह विशेष रूप से मेरी अवहेलना की पात्री है।
मेरे पिता चौधरी जमींदार के नायब थे। उनकी इच्छा थी, मेरे काम करने योग्य होते ही मुझे जमींदारी-सरिश्ते का काम सिखाकर कहीं गुमाश्तागिरी दिला दें। किन्तु मैं मन-ही-मन इसका विरोधी था। हमारे मुहल्ले के नीलरतन जिस तरह भागकर कलकत्ता में पढ़ना-लिखना सीखकर कलक्टर साहब के नाजिर हो गए थे उसी तरह मेरे जीवन का लक्ष्य भी अत्युच्च था, ‘कलक्टर का नाजिर न बन सका तो जजी अदालत का हेड क्लर्क हो जाऊंगा’, मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था।
मैं हमेशा देखता कि मेरे पिता इन अदालतजीवियों का बहुत सम्मान करते थे-अनेक अवसरों पर मछली-तरकारी, रुपये पैसे से उनकी पूजार्चना करनी पड़ती, यह बात भी मैं बाल्यावस्था से ही जानता था; इसलिए मैंने अदालत के छोटे कर्मचारी, यहां तक कि हरकारों को भी अपने हृदय में बड़े सम्मान का स्थान दे रखा था। ये हमारे बंगाल के पूज्य देवता थे, तेतीस कोटि देवताओं के छोटे-छोटे नवीन संस्करण। कार्य-सिद्धि-लाभ के सम्बन्ध में स्वयं सिद्धिदाता गणेश की
------------------------------
1. छोटी बालिकाओं का खेल; जिसमें बहू के समान सजकर, घूंघट निकालकर गृहिणी का अभिनय करती हैं।
अपेक्षा इनके प्रति लोगों में आन्तरिक निर्भरता कहीं अधिक थी, अतएव पहले गणेश को जो कुछ प्राप्त होता था वह आजकल इन्हें मिलता था।
नीलरतन के दृष्टांत से उत्साहित होकर मैं एक दिन विशेष सुविधा पाकर कलकत्ता भाग गया। पहले तो गांव के एक परिचित व्यक्ति के घर ठहरा, उसके बाद पढ़ाई के लिए पिता से भी थोड़ी-बहुत सहायता मिलने लग गई। पढ़ना-लिखना नियमपूर्वक चलने लगा। इसके अतिरिक्त मैं सभा-समितियों में भी योग देता। देश के लिए प्राण-विसर्जन करने की तत्काल आवश्यकता है, इस विषय में मुझे कोई सन्देह न था। किन्तु, यह दुस्साध्य कार्य किस, प्रकार किया जा सकता है, यह मैं नहीं जानता था; न इसका कोई दृष्टांत ही दिखाई पड़ता था। पर इससे मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हम देहाती थे, कम उम्र में ही प्रौढ़ बुद्धि रखने वाले कलकत्ता वालों की तरह हर चीज का मजाक उड़ाना हमने नहीं सीखा था; इसलिए हम लोग चन्दे की किताब लेकर भूखे-प्यासे दोपहर की धूप से दर-दर भीख मांगते फिरते, किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटते, सभा-स्थल में जोकर बेंच-कुर्सी लगाते, दलपति के बारे में किसी के कुछ कहने पर कमर बांधकर मार-पीट करने पर उतारू हो जाते। शहर के लड़के हमारे ये लक्षण देखकर हमें गंवार कहते।
आया तो था नाजिर सरिश्तेदार बनने, पर मैजिनी, गैरीबाल्डी बनने की तैयारी करने लग गया।
इसी समय मेरे पिता और सुरबाला के पिता ने एकमत होकर सुरबाला के साथ मेरा विवाह कर देने का निश्चय किया।
मैं पन्द्रह वर्ष की अवस्था में कलकत्ता भाग आया था, उस समय सुरबाला की अवस्था आठ वर्ष थी; अब मैं अठारह वर्ष का था। पिता के अनुसार मेरे विवाह की आयु धीरे-धीरे निकली जा रही थी। पर मैंने मन-ही-मन यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन अविवाहित रहकर स्वदेश के लिए मर मिटूंगा। मैंने पिता से कहा, ‘पढ़ाई पूरी किये बिना मैं विवाह नहीं कर सकता।’’
दो-चार महीने के बाद ही खबर मिली कि वकील रामलोचन बाबू के साथ सुरबाला का विवाह हो गया है। मैं तो पतित भारत की चंदा-वसूली के काम में व्यस्त था, मुझे यह समाचार अत्यन्त तुच्छ मालूम पड़ा।
एन्ट्रेंस पास कर लिया था, फर्स्ट ईयर आर्ट्स में जाने का विचार था कि तभी पिता की मृत्यु हो गई। परिवार में मैं अकेला नहीं था; माता थीं और दो बहनें। अतएव कॉलेज छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद नोआखाली डिवीजन के एक छोटे-से शहर के एन्ट्रेंस स्कूल में असिस्टैण्ट मास्टर का पद मिला।
सोचा, ‘मेरे उपयुक्त काम मिल गया। उपदेश तथा उत्साह प्रदान करके प्रत्येक विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा।’
काम आरम्भ कर दिया। देखा, भारतवर्ष के भविष्य की अपेक्षा आसन्न इम्तहान की चिन्ता कहीं ज्यादा की जाती थी। छात्रों को ग्रामर और एलजेबरा के बाहर की कोई बात बताते ही हेडमास्टर नाराज हो जाते। दो एक महीने में मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया।
हमारे जैसे प्रतिभाहीन लोग घर में बैठकर तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, पर अन्त में कर्म-क्षेत्र में उतरते ही कन्धे पर हल का बोझ ढोते हुए पीछे से पूंछ मरोड़ी जाने पर भी सिर झुकाए सहिष्णु भाव से प्रतिदिन खेत गोड़ने का काम कर संध्या को भर-पेट चारा पाकर ही सन्तुष्ट रहते हैं; फिर कूद-फांद करने का उत्साह नहीं बचता।
आग लगने के डर से एक-न-एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता। मैं अकेला था, इसलिए यह भार मेरे ही ऊपर आ पड़ा। स्कूल के बड़े आठचाला से सटी हुई एक झोंपड़ी में मैं रहता।
स्कूल बस्ती से कुछ दूर एक बड़ी पुष्कणी के किनारे था। चारों ओर सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ तथा स्कूल से लगे आपस में सटे हुए नीम के दो पुराने विशाल पेड़ छाया देते रहते।
अभी तक मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया, न मैंने उसे उस योग्य ही समझा। यहां के सरकारी वकील रामलोचन राय का घर हमारे स्कूल के पास ही था और उनके साथ उनकी स्त्री मेरी बाल्य-सखी सुरबाला थी, यह मैं जानता था।
रामलोचन बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ। सुरबाला के साथ मेरा बचपन में परिचय था यह रामलोचन बाबू जानते थे या नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने भी नया परिचय होने के कारण उस विषय में कुछ कहना उचित न समझा। यही नहीं सुरबाला किसी समय मेरे जीवन के साथ किसी रूप में जुड़ी हुई थी, यह बात मेरे मन में ठीक तरह से उठी ही नहीं।
एक दिन छुट्टी के रोज रामलोचन बाबू से भेंट करने उनके घर गया था। याद नहीं किस विषय पर बातचीत हो रही थी, शायद वर्तमान भारतवर्ष दुरव्यस्था के सम्बन्ध में। यह बात न थी कि वे उसके लिए विशेष चिंतित और उदास थे, किन्तु विषय ऐसा था कि हुक्का पीते-पीते उस पर एक-डेढ़ घण्टे तक यों ही शौकिया दुःख प्रकट किया जा सकता था।
तभी बगल के कमरे में चूड़ियों की हल्की-सी खनखनाहट, साड़ी की सरसराहट और पैरों की भी कुछ आहट सुनाई पड़ी। मैं अच्छी तरह समझ गया कि जंगले की संध से कोई कौतूहलपूर्ण आंखें मुझे देख रही हैं।
मुझे तत्काल वे आंखें याद ही आईं-विश्वास, सरलता और बालसुलभ प्रीति से छलछलाती दो बड़ी-बड़ी आंखें, काली-काली पुतलियां घनी काली पलकें, और स्थिर स्निग्ध दृष्टि। सहसा मेरे हृत्पिंड को मानो किसी ने अपनी कड़ी मुट्ठी में भींच लिया। वेदना से मेरा अन्तर झनझना उठा।
लौटकर घर आ गया, किन्तु वह व्यथा बनी रही। पढ़ना-लिखना, जो भी करता किसी तरह मन का भार दूर न हो पाता, मन सहसा एक भारी बोझ के समान हृदय की शिराओं को पकड़कर झूलने लग गया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i