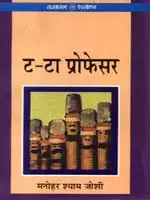|
उपन्यास >> ट-टा प्रोफेसर ट-टा प्रोफेसरमनोहर श्याम जोशी
|
441 पाठक हैं |
|||||||
प्रेम और काम जैसे अति सम्वेदनशील विषयों को केन्द्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास मज़ाक को भी त्रासदी में तब्दील कर देता है...
T-Ta Professor - A Hindi Book - by Manohar Shyam Joshi
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
स्वीकृत मानदण्डों की दृष्टि से पूरी तरह तर्कसंगत और प्रासंगिक नहीं होने के बावजूद ट-टा प्रोफेसर हिन्दी उपन्यासों में विशिष्ट दर्जा रखता है। दरअसल दास्ताने अलिफ़ लैला की शैली में वह ऐसी उत्तर-आधुनिक कथा है, जिसके अन्दर कई-कई कथा निर्बाध गतिमान है, सीमित कलेवर में होने के बाद भी कहानी पूरे उपन्यास का रसास्वादन कराती है। ट-टा प्रोफेसर एक पात्र की ही नहीं, एक कहानी की भी कहानी है। ऐसी कहानी जिसका आदि और अन्त, लेखक के आदि और अन्त के साथ होता है।
प्रेम और काम जैसे अति सम्वेदनशील विषयों को केन्द्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास मज़ाक को भी त्रासदी में तब्बीत कर देता है। कहीं ‘कॉमिक’ कामुकता में परिवर्तित नज़र आता है, लेकिन जीवन और मर्म की धड़कन निरन्तर सुनाई पड़ती रहती है। सत्य, कल्पना और अनुमति की प्रामाणिकता और भाषा के सहज प्रवाह के चलते कथा पाठक को आद्यान्त बाँधे रखती है।
अपने विलक्षण लेखन के नाते जाने जाने-वाले मनोहर श्याम जोशी ने एक सामान्य प्रोफेसर को केन्द्र में रखकर इस कृति में अपने कथा-कौशल का अद्भुत प्रमाण दिया है। उपन्यास के मुखर स्वरानुसार काम मनुष्य को ‘कामुक’ से अधिक ‘कॉमिक’ बनाता है और अस्तित्व को एक कॉमिक-कामुक और कास्मिक त्रासदी बना देता है।
‘‘कवियों को जवानी में ही मर जाना चाहिए और कथाकारों को बुढ़ापे में ही पैदा होना चाहिए।’’-यह उक्ति पता नहीं मैंने अपनी जवानी में किस किताब में पढ़ी थी ? लेखक का नाम भी अब याद नहीं रहा। जाने वह कौन था ? कोई विफल अधेड़ कवि होने की सम्भावना ही अधिक नजर आती है मुझे तो। कोई ऐसा अधेड़ जर्मन कवि, जिसकी चाँद गंजी और आत्मा रोएँदार होने लगी होगी और जिसकी प्रशंसक किशोरियाँ उसके बीयर-बेडौल शरीर में उसकी जवानी के गीतों को आत्मघाती रोमानी हीरो ढूँढ़ने में अपने को असमर्थ पाने लगीं होंगी।
देखिए, सफल न सही, वृद्ध कथाकार तो मैं भी हूँ और मेरा अनुभव यह है कि जीने के लिए लिख भले ही लूँ, लिखने के लिए मुझसे अब जीया नहीं जाता। अपने कथाकार के बुढ़ापे में पैदा होने के इन्तजार में मैंने जो ढेर सारी कहानियाँ जवानी में नहीं लिखीं, वे मेरे साथ-साथ बूढ़ी होती चली गयी हैं और जिस हद तक मैं मृत्यु के निकट पहुँच चुका हूँ, उसी हद तक वे भी पहुँच चुकी है। मरती हुई कहानियाँ लिखकर अमर हुआ जा सकता है भला ?
जिस जमाने में मैं इस तरह की अपने से मुग्ध और दूसरों को मुग्ध करने को आतुर उक्तियों से भरी पड़ी किताबें पढ़ा करता था, मैं भी अपने साथी लेखकों की तरह सोचता था कि साहित्य से जुड़कर मैं अनश्वरता से जुड़ रहा हूँ। गोया ऐसी ही उक्तियों से भरी जो दर्जनों कृतियाँ मेरी लेखनी से निकलेंगी, उन्हें आने वाली पीढ़ियों के मेरे ही जैसे लोग, किसी धूप-खिले या बादल-घिरे दिन, मेरी रचना के मौसम का अपने बाहरी और भीतरी मौसम से तादात्म्य बैठाते हुए पढ़ेंगे, और मेरी किसी उक्ति पर अटककर, किताब के पृष्ठों के बीच अँगुली रखकर उठेंगे कि किसी को सुनाये कि किसी के लिखे में उन्होंने क्या-क्या सुन लिया है।
और फिर सामने खिड़की से दीखती रोजमर्रा की दुनिया पर नजर डालने के बाद तय पायेंगे कि नहीं, जो हमने सुना है, उसे ऐसे सुनाने बैठ गये तो सिरफिरे समझे जायेंगे। इसे तो अपने ढंग से फिर लिख डालना होगा, लेखक बनना होगा और शब्द-सिद्धों की उस बिरादरी से जुड़ना होगा जो शब्दातीत की साधक है और अमरता की अधिकारिणी। लेकिन आज जब मुझे अपने चारों ओर अपनी लेखनी की पुरानी दुनिया मरती हुई नजर आती है और उस पुरानी दुनिया की कहानियों की स्मृतियाँ भी सठियाई हुई प्रतीत होती है, मुझे अपनी या किसी की भी अमरता में विश्वास नहीं रहा। इसीलिए अब मुझसे लिखा नहीं जाता और सच कहूँ तो किसी दूसरे का लिखा पढा़ भी नहीं जाता उस तरह मुग्ध होकर।
अब मेरे लिए उस जवान कथाकार की कल्पना तक कर पाना मुश्किल हो चला है, जिसके भीतर से कहानियाँ बेसाख्ता हँसी या बिला-वजह रुलाई की तरह फूट निकला करती थीं। क्या वह मैं था जो विश्वविद्यालय के पिछवाड़े के रेस्तोराँ में बैठा चाय पीते-पीते फिच्च से हँस पड़ता था और नीम-पागल समझे जाने का खतरा उठाते हुए हँसता-हँसता बाहर निकल पड़ता था किसी दोस्त की की तलाश में, जिसे हँसी के दौरे की वजह समझाई जा सके ? गोया राह चलते हँसते-हँसाते एक पूरी कहानी सुना दी जा सके ? और क्या वह भी मैं ही था जो कहीं दूर रेडियो पर बजता कोई पुराना गीत सुनकर, या ‘कवियों को जवानी में ही मर जाना चाहिए’ मार्का कोई काव्यात्मक पंक्ति पढ़कर गले में कुछ अटकता-सा और आँखों में कुछ भरता-सा महसूस करता था ? और जिसे फिर किसी दोस्त की नहीं, गुसलखाने के अकेलेपन की तलाश रहती, जहाँ उसका आँसुओं से लड़ना और हारना वाशबेसिन के आईने में उभरा हुआ उसका अक्स ही देख पाता और वह सुनता रहता उन आँसुओं के साथ निकलती, उन आँसुओं जितनी ही गरमागरम एक ताजा भाव-विह्वल कहानी।
वह ‘लेखक’ क्या सचमुच मैं था कि वह भी मेरी किसी कहानी का ही पात्र था ? जो हो, वह मेरे बस का, या कहूँ मैं उसके बस का अब रहा नहीं। वह जो रचनात्मक भावुकता का, बेसाख्ता हँसी और बिला-वजह रुलाई का, एक सक्रिय तन्त्र था मेरे भीतर उम्र बढ़ने के साथ पहले गड़बड़ाने लगा - हँसी की जगह रुलाई या रुलाई की जगह हँसी या कभी-कभी दोनों एक साथ - और अन्ततः ठप्प पड़ गया। तो जो कहानियाँ जवानी में लिखी नहीं गयीं, मेरे साथ-साथ बुढ़ाती चली गयीं, मरती चली गयीं - मेरे बाहर भी, मेरे भीतर भी।
इन कहानियों में से भी कुछ की मैं बीच-बीच में वैसे ही सुध लेता रहा जैसे कि स्वयं अपनी। अपने बुढापे से लड़ने की कोशिश करते हुए उनके बुढापे से भी लड़ा। यही कारण है कि मेरी फाइलों में उन कहानियों के आरम्भिक पृष्ठों के, लम्बे अन्तरालों पर लिखे गये, कई-कई संस्करण मौजूद है, जो मूक साक्षी है मेरी कल्पना और मेरी लिखावट के बुढ़ाते चले जाने के। लेकिन कुछ अभागी कहानियाँ ऐसी भी है, जो मन में ही लिख-लिखकर मन में ही मिटा दी गयी। कभी उतारी नहीं गयीं कागज पर। जो भीतर ही जन्मी, पली-बढ़ी और भीतर ही घुटकर मर गयीं। ऐसी ही एक कहानी का मर्सिया लिखने बैठा हूँ मैं।
इस कहानी की याद मुझे पिछली गर्मियों में पूरे एक दशक के बाद, अपने पुश्तैनी शहर अल्मोड़ा जाने पर इसी कहानी के एक गौण पात्र ने दिलवायी। सो भी चलती बस से। मैं अपने पैतृक निवास के सूखे हुए खुबानी के पेड़ पर गौर करते हुए अपने उस बुजुर्ग को याद कर रहा था, जिसने यह पेड़ लगाया था जिसे बागवानी से बेहद प्यार था कि ऊपर गाड़ी-सड़क से किसी ने पुकारा-‘‘जोशी माट सैप !’’
मैंने चौंककर निगाह उठायी। ऊपर सड़क पर बागेश्वर जाने वाली प्राइवेट बस मेरे मुहल्ले की किसी सवारी को बैठाने के लिए रुकी खड़ी थी और उसकी एक खिड़की से एक बूढ़ा मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसको पहचानने की कोशिश करते हुए मैं खेत-खेत चढ़ता हुआ गाड़ी-सड़क की ओर बढ़ा। उसने मुझे ‘माट सैप’ पुकारा था इसलिए इतना तो स्पष्ट था कि उसका सम्बन्ध सुनौली धार गाँव से रहा होगा क्योंकि मैंने जिन्दगी में पहली और आखिरी बार मास्टरी वहीं की थी। वहीं के लोग मुझे ‘माट सैप’ यानी मास्टर साहब पुकारा करते थे।
मैं गाड़ी-सड़क पर पहुँचा। बस से झाँकता वह व्यक्ति मुझे बधाई देने लगा, इस बीच बहुत बड़ा आदमी बन जाने के लिए और मैं उसके बूढ़े चेहरे में सुनौलीधार में देखा हुआ कोई जवान चेहरा तलाश लेने की विफल कोशिश करते हुए अपने चेहरे पर एक आश्वासनप्रद और आत्मीय मुस्कान सँजोये रहा कि हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मगर मैं उसे पहचाना तभी जब उसने साहित्य की दौड़ में अपनी लेखनी के मेरी लेखनी से पिछड़ जाने को भी नसीब का खेल बताकर एक गहरा साँस भरा। अच्छा, तो वह सुनौलीधार के स्कूल का जूनियर क्लर्क था जो छायावादी किस्म की कविताएँ लिखा करता था। लेकिन कमबख्त का नाम मुझे याद नहीं आया कि लेकर उसे खुश कर सकूँ।
तभी बस चल पड़ी। चलती बस से उसने चिल्लाकर पूछा, ‘‘माट सैप, तुम प्रोफेसर षष्टीबल्लभ पन्त ट-टा डबुल एम० ए० की कथा नहीं लिखोगे क्या ?’’
मैं उत्तर में चीखकर कुछ कह सकूँ इतना अवसर न मिला। उसने हाथ हिलाकर षष्टीबल्लभ की तरह ‘ट-टा’ कहा और मैंने भी हाथ हिलाकर ‘टा-टा’ बुदबुदा दिया। मैं उसके चेहरे से जुड़ा हुआ नाम ढूँढने की कोशिश करता हुआ गाड़ी-सड़क से अपने घर लौटा। लेकिन भले ही उसकी किसी कविता की एक पंक्ति मुझे याद आ गयीं-‘विहग-विहीन सखी मन तरुवर।’’-लेकिन उसका नाम याद नहीं आया। जिसके लिए चेहरों पर से नाम मिट चुके हैं और नामों से चेहरे नहीं रह गये है, ऐसे सठियाए कथाकार को वहाँ गाड़ी-सड़क पर पीछे छोड़कर जाते हुए, किसी बहुत ही पीछे छूटी कहानी की याद दिला जाने की विडम्बना उसने निश्चिय ही समझी होगी क्योंकि वह भी कवि था। कवि और जूनियर क्लर्क। तब जब मैं लेखक था। लेखक और अस्थायी अध्यापक। उस सुदूर पहाड़ी गाँव सुनौलीधार में, जिसके क्षितिज पर हिमालय घोड़े की नाल की तरह जड़ा हुआ था।
पढ़ाई से विद्रोह करते हुए स्नातक परीक्षा में अपना डिवीजन बिगाड़ लेने के बाद मैं परिवार से विद्रोह करते हुए सुनौलीधार में मास्टरी करने जा पहुँचा था ताकि मुझसे आगे पढ़ने को अथवा गम्भीरता से किसी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करने को न कहा जा सके। मैंने घरवालों से तो यह कह दिया था कि मास्टरी करते हुए मैं प्राइवेट एम० ए० कर लूँगा, लेकिन मेरा सुनौलीधार में रहकर पढ़ने का नहीं, सुरम्य वातावरण में रम्य रचनाएँ लिखने का इरादा था। स्कूल में पहुँचने के पहले दिन ही मालूम हो गया कि सुनौलीधार का वातावरण रम्य कम है रोचक अधिक है। रोचक भी कॉमिक’ वाले अर्थ में।
सबसे पहले मैं मिला स्कूल के नये हैडमास्टर शोभनसिंह से। उन्होंने हैडमास्टर सम्बोधन पर आपत्ति की और कहा-मुझे प्रिंसिपल कहा कीजिए हैडमास्टर तो षष्टीबल्लभ पन्त है, जिन्हें लोग-बाग आम तौर पर प्रोफेसर पुकारते हैं। उसी वर्ष मिडिल से हाई बने स्कूल में प्रिंसिपल और प्रोफेसर ! सुनकर मैं मन-ही-मन हँसा। यह आन्तरिक हँसी तब और भी बढ़ गयी जब प्रिंसिपल सैप ने अपने और षष्टीबल्लभ पन्त के द्वन्द्व का विषद वर्णन करके सुनौलीधार को मेरे लिए काव्यात्मक से कहीं अधिक नाटकीय और राजनीतिक बना दिया। यही नहीं, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े इस नये अध्यापक को प्रभावित करने के लिए लखनऊ के कई बड़े लोगों से अपने नजदीकी नाते का ब्योरा देना जरूरी समझा। उन्होंने कुछ गैर-जरूरी समझा तो मुझे अपने क्वार्टर में जगह देना जब कि अल्मोड़ा में मेरा सलेक्शन करते हुए स्कूल मैनेजर ने कहा था कि प्रिसिपल सैप के लिए जो क्वार्टर बनाया गया है, वह उसमें एक कमरा आपको दे देंगे। प्रिसिपल सैप ने मुझे सुझाव दिया कि आप अधबनी प्रयोगशाला के स्टोर रूम में जूनियर क्लर्क के साथ रह लीजिए।
तो मैं प्रयोगशाला के स्टोर रूम में पहुँचा और वहाँ मैंने पाया कि जूनियर क्लर्क एक लम्बे लिफाफे पर सम्पादक सरस्वती का नाम-पता लिख रहा है। मैंने अपना परिचय और प्रिंसिपल का सन्देह दिया और सामान रखने की अनुमति माँगी। उसने इसे प्रिंसिपल सैप की एक और ज्यादती का नमूना ठहराया। बोला-सामान तो वह अपने ऑफिस में भी रखवा सकते थे। मैंने इस पर कोई टिप्पणी न करके यह जिज्ञासा की कि क्या आप लेखक हैं ?
उसने तुनककर जवाब दिया, ‘‘मै पोयट हूँ पोयट, लेखक-वेखक नहीं।’’
मैंने उसे बताया कि मैं लेखक हूँ और मेरा एक वैज्ञानिक लेख ‘संगम’ में छप चुका है। उसने कहा कि वैज्ञानिक लेख लिखने से लेखक जो थोड़ी हो जाता है कोई। कहानियाँ-उपन्यास लिखने पड़ते हैं। मैं अपनी कविता सरस्वती में छपने भेज रहा हूँ। मुझे डाकखाने जाना है। सामान यहाँ रखना हो तो रख लो लेकिन मैं तुम्हे यहाँ अकेला छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। स्टोर का सामान है, मेरा अपना सामान है। कुछ खो-खा गया तो बबाला होगा। ओल-टोल मेरे सिर पर आयेगी।
मैंने प्रस्ताव किया कि मैं भी साथ ही चले चलता हूँ। मुझे भी ‘संगम’ के लिए एक कहानी भेजनी है।
तो हम दोनों सुनौलीधार के बाजार में पहुँचें, जिसमें कुल दो दुकाने थीं। पहली दुकान जीतसिंह की थी, जिसमें नमक-तेल से लेकर जूते-कपड़े तक कई तरह की चीजे सीमित मात्रा में उपलब्ध थीं। इसी में गाँव का डाकखाना भी था। जूनियर क्लर्क इस बीच यह अनुमान लगा चुका था कि ‘संगम’ सम्पादक इलाचन्द्र जोशी मेरे भाई-वाई होंगे। उसने अनुरोध किया कि मैं अपने लिफाफे में उसकी भी कुछ कविताएँ अपने सिफारिश पत्र के साथ रख दूँ।
प्रेम और काम जैसे अति सम्वेदनशील विषयों को केन्द्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास मज़ाक को भी त्रासदी में तब्बीत कर देता है। कहीं ‘कॉमिक’ कामुकता में परिवर्तित नज़र आता है, लेकिन जीवन और मर्म की धड़कन निरन्तर सुनाई पड़ती रहती है। सत्य, कल्पना और अनुमति की प्रामाणिकता और भाषा के सहज प्रवाह के चलते कथा पाठक को आद्यान्त बाँधे रखती है।
अपने विलक्षण लेखन के नाते जाने जाने-वाले मनोहर श्याम जोशी ने एक सामान्य प्रोफेसर को केन्द्र में रखकर इस कृति में अपने कथा-कौशल का अद्भुत प्रमाण दिया है। उपन्यास के मुखर स्वरानुसार काम मनुष्य को ‘कामुक’ से अधिक ‘कॉमिक’ बनाता है और अस्तित्व को एक कॉमिक-कामुक और कास्मिक त्रासदी बना देता है।
‘‘कवियों को जवानी में ही मर जाना चाहिए और कथाकारों को बुढ़ापे में ही पैदा होना चाहिए।’’-यह उक्ति पता नहीं मैंने अपनी जवानी में किस किताब में पढ़ी थी ? लेखक का नाम भी अब याद नहीं रहा। जाने वह कौन था ? कोई विफल अधेड़ कवि होने की सम्भावना ही अधिक नजर आती है मुझे तो। कोई ऐसा अधेड़ जर्मन कवि, जिसकी चाँद गंजी और आत्मा रोएँदार होने लगी होगी और जिसकी प्रशंसक किशोरियाँ उसके बीयर-बेडौल शरीर में उसकी जवानी के गीतों को आत्मघाती रोमानी हीरो ढूँढ़ने में अपने को असमर्थ पाने लगीं होंगी।
देखिए, सफल न सही, वृद्ध कथाकार तो मैं भी हूँ और मेरा अनुभव यह है कि जीने के लिए लिख भले ही लूँ, लिखने के लिए मुझसे अब जीया नहीं जाता। अपने कथाकार के बुढ़ापे में पैदा होने के इन्तजार में मैंने जो ढेर सारी कहानियाँ जवानी में नहीं लिखीं, वे मेरे साथ-साथ बूढ़ी होती चली गयी हैं और जिस हद तक मैं मृत्यु के निकट पहुँच चुका हूँ, उसी हद तक वे भी पहुँच चुकी है। मरती हुई कहानियाँ लिखकर अमर हुआ जा सकता है भला ?
जिस जमाने में मैं इस तरह की अपने से मुग्ध और दूसरों को मुग्ध करने को आतुर उक्तियों से भरी पड़ी किताबें पढ़ा करता था, मैं भी अपने साथी लेखकों की तरह सोचता था कि साहित्य से जुड़कर मैं अनश्वरता से जुड़ रहा हूँ। गोया ऐसी ही उक्तियों से भरी जो दर्जनों कृतियाँ मेरी लेखनी से निकलेंगी, उन्हें आने वाली पीढ़ियों के मेरे ही जैसे लोग, किसी धूप-खिले या बादल-घिरे दिन, मेरी रचना के मौसम का अपने बाहरी और भीतरी मौसम से तादात्म्य बैठाते हुए पढ़ेंगे, और मेरी किसी उक्ति पर अटककर, किताब के पृष्ठों के बीच अँगुली रखकर उठेंगे कि किसी को सुनाये कि किसी के लिखे में उन्होंने क्या-क्या सुन लिया है।
और फिर सामने खिड़की से दीखती रोजमर्रा की दुनिया पर नजर डालने के बाद तय पायेंगे कि नहीं, जो हमने सुना है, उसे ऐसे सुनाने बैठ गये तो सिरफिरे समझे जायेंगे। इसे तो अपने ढंग से फिर लिख डालना होगा, लेखक बनना होगा और शब्द-सिद्धों की उस बिरादरी से जुड़ना होगा जो शब्दातीत की साधक है और अमरता की अधिकारिणी। लेकिन आज जब मुझे अपने चारों ओर अपनी लेखनी की पुरानी दुनिया मरती हुई नजर आती है और उस पुरानी दुनिया की कहानियों की स्मृतियाँ भी सठियाई हुई प्रतीत होती है, मुझे अपनी या किसी की भी अमरता में विश्वास नहीं रहा। इसीलिए अब मुझसे लिखा नहीं जाता और सच कहूँ तो किसी दूसरे का लिखा पढा़ भी नहीं जाता उस तरह मुग्ध होकर।
अब मेरे लिए उस जवान कथाकार की कल्पना तक कर पाना मुश्किल हो चला है, जिसके भीतर से कहानियाँ बेसाख्ता हँसी या बिला-वजह रुलाई की तरह फूट निकला करती थीं। क्या वह मैं था जो विश्वविद्यालय के पिछवाड़े के रेस्तोराँ में बैठा चाय पीते-पीते फिच्च से हँस पड़ता था और नीम-पागल समझे जाने का खतरा उठाते हुए हँसता-हँसता बाहर निकल पड़ता था किसी दोस्त की की तलाश में, जिसे हँसी के दौरे की वजह समझाई जा सके ? गोया राह चलते हँसते-हँसाते एक पूरी कहानी सुना दी जा सके ? और क्या वह भी मैं ही था जो कहीं दूर रेडियो पर बजता कोई पुराना गीत सुनकर, या ‘कवियों को जवानी में ही मर जाना चाहिए’ मार्का कोई काव्यात्मक पंक्ति पढ़कर गले में कुछ अटकता-सा और आँखों में कुछ भरता-सा महसूस करता था ? और जिसे फिर किसी दोस्त की नहीं, गुसलखाने के अकेलेपन की तलाश रहती, जहाँ उसका आँसुओं से लड़ना और हारना वाशबेसिन के आईने में उभरा हुआ उसका अक्स ही देख पाता और वह सुनता रहता उन आँसुओं के साथ निकलती, उन आँसुओं जितनी ही गरमागरम एक ताजा भाव-विह्वल कहानी।
वह ‘लेखक’ क्या सचमुच मैं था कि वह भी मेरी किसी कहानी का ही पात्र था ? जो हो, वह मेरे बस का, या कहूँ मैं उसके बस का अब रहा नहीं। वह जो रचनात्मक भावुकता का, बेसाख्ता हँसी और बिला-वजह रुलाई का, एक सक्रिय तन्त्र था मेरे भीतर उम्र बढ़ने के साथ पहले गड़बड़ाने लगा - हँसी की जगह रुलाई या रुलाई की जगह हँसी या कभी-कभी दोनों एक साथ - और अन्ततः ठप्प पड़ गया। तो जो कहानियाँ जवानी में लिखी नहीं गयीं, मेरे साथ-साथ बुढ़ाती चली गयीं, मरती चली गयीं - मेरे बाहर भी, मेरे भीतर भी।
इन कहानियों में से भी कुछ की मैं बीच-बीच में वैसे ही सुध लेता रहा जैसे कि स्वयं अपनी। अपने बुढापे से लड़ने की कोशिश करते हुए उनके बुढापे से भी लड़ा। यही कारण है कि मेरी फाइलों में उन कहानियों के आरम्भिक पृष्ठों के, लम्बे अन्तरालों पर लिखे गये, कई-कई संस्करण मौजूद है, जो मूक साक्षी है मेरी कल्पना और मेरी लिखावट के बुढ़ाते चले जाने के। लेकिन कुछ अभागी कहानियाँ ऐसी भी है, जो मन में ही लिख-लिखकर मन में ही मिटा दी गयी। कभी उतारी नहीं गयीं कागज पर। जो भीतर ही जन्मी, पली-बढ़ी और भीतर ही घुटकर मर गयीं। ऐसी ही एक कहानी का मर्सिया लिखने बैठा हूँ मैं।
इस कहानी की याद मुझे पिछली गर्मियों में पूरे एक दशक के बाद, अपने पुश्तैनी शहर अल्मोड़ा जाने पर इसी कहानी के एक गौण पात्र ने दिलवायी। सो भी चलती बस से। मैं अपने पैतृक निवास के सूखे हुए खुबानी के पेड़ पर गौर करते हुए अपने उस बुजुर्ग को याद कर रहा था, जिसने यह पेड़ लगाया था जिसे बागवानी से बेहद प्यार था कि ऊपर गाड़ी-सड़क से किसी ने पुकारा-‘‘जोशी माट सैप !’’
मैंने चौंककर निगाह उठायी। ऊपर सड़क पर बागेश्वर जाने वाली प्राइवेट बस मेरे मुहल्ले की किसी सवारी को बैठाने के लिए रुकी खड़ी थी और उसकी एक खिड़की से एक बूढ़ा मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसको पहचानने की कोशिश करते हुए मैं खेत-खेत चढ़ता हुआ गाड़ी-सड़क की ओर बढ़ा। उसने मुझे ‘माट सैप’ पुकारा था इसलिए इतना तो स्पष्ट था कि उसका सम्बन्ध सुनौली धार गाँव से रहा होगा क्योंकि मैंने जिन्दगी में पहली और आखिरी बार मास्टरी वहीं की थी। वहीं के लोग मुझे ‘माट सैप’ यानी मास्टर साहब पुकारा करते थे।
मैं गाड़ी-सड़क पर पहुँचा। बस से झाँकता वह व्यक्ति मुझे बधाई देने लगा, इस बीच बहुत बड़ा आदमी बन जाने के लिए और मैं उसके बूढ़े चेहरे में सुनौलीधार में देखा हुआ कोई जवान चेहरा तलाश लेने की विफल कोशिश करते हुए अपने चेहरे पर एक आश्वासनप्रद और आत्मीय मुस्कान सँजोये रहा कि हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मगर मैं उसे पहचाना तभी जब उसने साहित्य की दौड़ में अपनी लेखनी के मेरी लेखनी से पिछड़ जाने को भी नसीब का खेल बताकर एक गहरा साँस भरा। अच्छा, तो वह सुनौलीधार के स्कूल का जूनियर क्लर्क था जो छायावादी किस्म की कविताएँ लिखा करता था। लेकिन कमबख्त का नाम मुझे याद नहीं आया कि लेकर उसे खुश कर सकूँ।
तभी बस चल पड़ी। चलती बस से उसने चिल्लाकर पूछा, ‘‘माट सैप, तुम प्रोफेसर षष्टीबल्लभ पन्त ट-टा डबुल एम० ए० की कथा नहीं लिखोगे क्या ?’’
मैं उत्तर में चीखकर कुछ कह सकूँ इतना अवसर न मिला। उसने हाथ हिलाकर षष्टीबल्लभ की तरह ‘ट-टा’ कहा और मैंने भी हाथ हिलाकर ‘टा-टा’ बुदबुदा दिया। मैं उसके चेहरे से जुड़ा हुआ नाम ढूँढने की कोशिश करता हुआ गाड़ी-सड़क से अपने घर लौटा। लेकिन भले ही उसकी किसी कविता की एक पंक्ति मुझे याद आ गयीं-‘विहग-विहीन सखी मन तरुवर।’’-लेकिन उसका नाम याद नहीं आया। जिसके लिए चेहरों पर से नाम मिट चुके हैं और नामों से चेहरे नहीं रह गये है, ऐसे सठियाए कथाकार को वहाँ गाड़ी-सड़क पर पीछे छोड़कर जाते हुए, किसी बहुत ही पीछे छूटी कहानी की याद दिला जाने की विडम्बना उसने निश्चिय ही समझी होगी क्योंकि वह भी कवि था। कवि और जूनियर क्लर्क। तब जब मैं लेखक था। लेखक और अस्थायी अध्यापक। उस सुदूर पहाड़ी गाँव सुनौलीधार में, जिसके क्षितिज पर हिमालय घोड़े की नाल की तरह जड़ा हुआ था।
पढ़ाई से विद्रोह करते हुए स्नातक परीक्षा में अपना डिवीजन बिगाड़ लेने के बाद मैं परिवार से विद्रोह करते हुए सुनौलीधार में मास्टरी करने जा पहुँचा था ताकि मुझसे आगे पढ़ने को अथवा गम्भीरता से किसी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करने को न कहा जा सके। मैंने घरवालों से तो यह कह दिया था कि मास्टरी करते हुए मैं प्राइवेट एम० ए० कर लूँगा, लेकिन मेरा सुनौलीधार में रहकर पढ़ने का नहीं, सुरम्य वातावरण में रम्य रचनाएँ लिखने का इरादा था। स्कूल में पहुँचने के पहले दिन ही मालूम हो गया कि सुनौलीधार का वातावरण रम्य कम है रोचक अधिक है। रोचक भी कॉमिक’ वाले अर्थ में।
सबसे पहले मैं मिला स्कूल के नये हैडमास्टर शोभनसिंह से। उन्होंने हैडमास्टर सम्बोधन पर आपत्ति की और कहा-मुझे प्रिंसिपल कहा कीजिए हैडमास्टर तो षष्टीबल्लभ पन्त है, जिन्हें लोग-बाग आम तौर पर प्रोफेसर पुकारते हैं। उसी वर्ष मिडिल से हाई बने स्कूल में प्रिंसिपल और प्रोफेसर ! सुनकर मैं मन-ही-मन हँसा। यह आन्तरिक हँसी तब और भी बढ़ गयी जब प्रिंसिपल सैप ने अपने और षष्टीबल्लभ पन्त के द्वन्द्व का विषद वर्णन करके सुनौलीधार को मेरे लिए काव्यात्मक से कहीं अधिक नाटकीय और राजनीतिक बना दिया। यही नहीं, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े इस नये अध्यापक को प्रभावित करने के लिए लखनऊ के कई बड़े लोगों से अपने नजदीकी नाते का ब्योरा देना जरूरी समझा। उन्होंने कुछ गैर-जरूरी समझा तो मुझे अपने क्वार्टर में जगह देना जब कि अल्मोड़ा में मेरा सलेक्शन करते हुए स्कूल मैनेजर ने कहा था कि प्रिसिपल सैप के लिए जो क्वार्टर बनाया गया है, वह उसमें एक कमरा आपको दे देंगे। प्रिसिपल सैप ने मुझे सुझाव दिया कि आप अधबनी प्रयोगशाला के स्टोर रूम में जूनियर क्लर्क के साथ रह लीजिए।
तो मैं प्रयोगशाला के स्टोर रूम में पहुँचा और वहाँ मैंने पाया कि जूनियर क्लर्क एक लम्बे लिफाफे पर सम्पादक सरस्वती का नाम-पता लिख रहा है। मैंने अपना परिचय और प्रिंसिपल का सन्देह दिया और सामान रखने की अनुमति माँगी। उसने इसे प्रिंसिपल सैप की एक और ज्यादती का नमूना ठहराया। बोला-सामान तो वह अपने ऑफिस में भी रखवा सकते थे। मैंने इस पर कोई टिप्पणी न करके यह जिज्ञासा की कि क्या आप लेखक हैं ?
उसने तुनककर जवाब दिया, ‘‘मै पोयट हूँ पोयट, लेखक-वेखक नहीं।’’
मैंने उसे बताया कि मैं लेखक हूँ और मेरा एक वैज्ञानिक लेख ‘संगम’ में छप चुका है। उसने कहा कि वैज्ञानिक लेख लिखने से लेखक जो थोड़ी हो जाता है कोई। कहानियाँ-उपन्यास लिखने पड़ते हैं। मैं अपनी कविता सरस्वती में छपने भेज रहा हूँ। मुझे डाकखाने जाना है। सामान यहाँ रखना हो तो रख लो लेकिन मैं तुम्हे यहाँ अकेला छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। स्टोर का सामान है, मेरा अपना सामान है। कुछ खो-खा गया तो बबाला होगा। ओल-टोल मेरे सिर पर आयेगी।
मैंने प्रस्ताव किया कि मैं भी साथ ही चले चलता हूँ। मुझे भी ‘संगम’ के लिए एक कहानी भेजनी है।
तो हम दोनों सुनौलीधार के बाजार में पहुँचें, जिसमें कुल दो दुकाने थीं। पहली दुकान जीतसिंह की थी, जिसमें नमक-तेल से लेकर जूते-कपड़े तक कई तरह की चीजे सीमित मात्रा में उपलब्ध थीं। इसी में गाँव का डाकखाना भी था। जूनियर क्लर्क इस बीच यह अनुमान लगा चुका था कि ‘संगम’ सम्पादक इलाचन्द्र जोशी मेरे भाई-वाई होंगे। उसने अनुरोध किया कि मैं अपने लिफाफे में उसकी भी कुछ कविताएँ अपने सिफारिश पत्र के साथ रख दूँ।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i