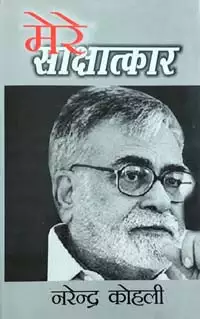|
अतिरिक्त >> मेरा साथी कोई नहीं मेरा साथी कोई नहींनरेन्द्र कोहली
|
96 पाठक हैं |
|||||||
मेरा साथी कोई नहीं...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
...मेरे अनुभव कहानियों के रूप में ही ढलते थे, शायद इसीलिए कि प्रत्येक घटना को स्वतः संपूर्ण तथा स्वतंत्र मानकर मेरा सर्जक मन उस घटना को उसी की संपूर्णता से बुनता था...कहानी उसी एक बिंदु के चारों ओर बुनी जाती थी।...
नरेन्द्र कोहली
नरेन्द्र कोहली की ही यह कथा-ऊर्जा है, जिसने उन्हें वृहदाकार उपन्यासों से सृजन में शिखर तक पहुंचाया। यह मानना ही पड़ेगा कि उनके कथा-बीज कहानी की उर्वर जमीन में रोपे गए थे, जिन्होंने उनके भव्य और विशाल लेखन को करवाया। आधुनिक संदर्भों की विसंगतियों को उकेरने में उनके व्यंग्यों ने अपना कमाल दिखाया और वास्तव में वह एक चुस्त-दुरुस्त और संवेदनशील कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। व्यापक दृष्टिकोण रखने के कारण वह बारीक-से-बारीक स्थितियों, घटनाओं और प्रसंगों को भी अपनी संवेदना के रंग से भरने में सिद्धहस्त हैं। ये सब मिलाकर ही वह पाठक के चहेते और सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार हैं।
कहानी का चरम
मुझे लगता है, मैं घर से दूर परदेश में अकेला बैठा हूं। ज़िन्दगी इसी तरह की उदास शाम है, जिसमें दूसरे को हंसता देख, अपनी उदासी याद आती है।...
...जब अकेली शामें इस तरह कटती है, साथी कोई नहीं होता ...तो पढ़ाई नहीं होती ...मैं नहीं पढ़ता। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा साथी कोई नहीं। मैं अकेला हूं।
...जब अकेली शामें इस तरह कटती है, साथी कोई नहीं होता ...तो पढ़ाई नहीं होती ...मैं नहीं पढ़ता। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा साथी कोई नहीं। मैं अकेला हूं।
- ‘मेरा साथी कोई नहीं’ से
सुकरात के ये वचन सत्संग की महिमा की ओर संकेत करते हैं। ‘विवेक’ किसी भी मूल्य पर मिले, वह सस्ता है, क्योंकि, इसके बिना जीवन में उपलब्धि नहीं होती। तुलसीदास जी ने विवेक प्राप्ति का प्रमुख साधन सत्संग को माना है-‘बिनु सत्संग विवेक न होई।’
सुंदरकाण्ड में लंकिनी द्वारा कहे गए ये शब्द सत्संग की महिमा पर ही तो प्रकाश डालते हैं -
सुंदरकाण्ड में लंकिनी द्वारा कहे गए ये शब्द सत्संग की महिमा पर ही तो प्रकाश डालते हैं -
कथा-भूमि
मेरा लेखन कहानियों से आरम्भ हुआ या कविताओं से, यह कहना कठिन है, किन्तु इसमें कोई भ्रम नहीं है कि मेरे लेखन का विकास कहानियों के माध्यम से ही हुआ। अपनी कॉपियों में तो कविताएं भी खूब लिखी थीं, पर न तो उनका विकास हुआ और न प्रकाशन, किन्तु कहानियों की बात और थी। जिधर दृष्टि जाती थी, कोई-न-कोई कहानी दिख जाती थी, अपने भीतर भी और अपने बाहर भी, फिर भी मेरी आरम्भिक कहानियाँ इस अर्थ में काफी आत्मकेन्द्रित रही हैं कि उनकी सामग्री मैंने अपने परिवार और निकट संबंधियों के व्यक्तिगत जीवन से ही ली हैं। अबोध शैशव को पीछे छोड़ आए, पहली बार आँखें खोलते हुए तरुण मन के लिए शायद यही स्वाभाविक था। प्रतिदिन पारिवारिक-सामाजिक जीवन के किसी-न-किसी नए तथ्य का उद्घाटन हो रहा था। अपने आस-पास घटती घटनाओं की अनुभूतियों का ताज़ापन और उनके प्रति तीखी प्रतिक्रिया मुझे कहानी लिखने का बाध्य कर रही थी। कॉलेज के नए-नए अनुभव, हलके-हलके रोमांस, घर में पहला विवाह, नए बनते संबंध और पुराने संबंधो के प्रति विद्रोह जैसे उपकरण मुझे अकस्मात् ही सुलभ हो गए थे और मेरे पास था मस्ती से भरा तथा लोगों को कोंचने को आतुर चुलबुला मन, चुहल से कटाक्ष और विद्रूप तक जाती वाणी, स्वयं को बड़ों के बराबर मनवाने का किशोर प्रयास, क्योंकि बड़ों के गरिमायुक्त व्यक्तित्व क्रमश: हलके पड़ते जा रहे थे। आरंभिक कहानियों में घटनाओं के नाटकीय संयोजन से विसंगतियों तथा दोहरे मानदंडों पर प्रहार करना ही शायद मेरा प्रमुख उद्देश्य था। आज सोचता हूँ, तो लगता है कि शायद अपने विद्रोह की घोषणा करने के लिए ही मैंने कहानियाँ लिखी थीं। ‘पानी का जग, गिलास और केतली,’ ‘दो हाथ,’ ‘बदतमीज़ी,’ ‘ज्ञान की पिपासा,’ ‘दो ढाई-आठ,’ ‘उजड़े दयार में’ आदि कहानियाँ मेरे इसी मूड की अत्यन्त आरंभिक कहानियाँ हैं।
इसी अवधि में कुछ कहानियाँ केवल इसलिए लिखी गईं, क्योंकि कहानियाँ बन गई थीं। कहानीपन का भी अपना मज़ा होता है। उसको छोड़ पाना कठिन होता है, विशेषकर आरंभिक दौर में। ऐसा भी हुआ कि परस्पर चर्चा में किसी ने कोई रोचक घटना सुना दी अथवा किसी की बातचीत में से कोई पक्ष उभर आया, तो उसकी भी कहानी बन गई। ‘राजा दशरथ के बेटे’ तथा ‘मम्मी, पापा और उनकी बेबी’ ऐसी ही कहानियाँ हैं।
प्रेम-कथाएँ मैंने बहुत कम लिखी हैं, किन्तु आरंभ में कुछ रोमानी कहानियाँ अवश्य लिखी थीं। ‘स्नेह का उदय,’ ‘संगिनी,’ ‘उसने ग़लत नहीं कहा था’ तथा ‘मालिनी’ जैसी कुछ कहानियाँ याद आ रही हैं, किन्तु इनमें से कोई भी गंभीर प्रेम-कथा नहीं है। प्रेम-कथा लिखने में न मुझे तब संकोच था, न अब है, किन्तु प्रेम को कहानी बनने में शायद लम्बी अवधि चाहिए। लम्बे अरसे के बाद मैंने ‘कथा पुरानी मैत्री की,’ ‘त्रासदियाँ प्रेम की’ तथा ‘प्रीति-कथा’ इत्यादि रचनाएँ अवश्य लिखीं, किन्तु उनमें ‘प्रेम’ कम, विश्लेषण और व्यंग्य ही अधिक सघन हुआ है, क्योंकि प्रेम की वास्तविकता अब उतनी अबूझ नहीं रह गई थी।
फिर जैसे अपने-आप से अवकाश पाकर मेरा लेखक अपने दुःख-दर्द के साथ-साथ दूसरों के दुःख-दर्द को भी पहचानने लगा था। इस समय की मेरी कहानियाँ, मेरे जीवन को छूते हुए अन्य लागो के अनुभवों की कहानियाँ। मेरी लेखनीय सहानुभूति इन्हीं दिनों विकसित होनी आरंभ हुई थी। ‘आहत-प्यार’, ‘भूखे बच्चे : सूखी डाली,’ ‘मेरा अपना संसार’ बहुत भावुक और आहत भावनाओं की कहानियाँ है ? उनके साथ-साथ ‘कहानी का अभाव,’ ‘होने वाली पत्नी’ तथा ‘एक ही विकल्प’ परिस्थितियों की विडंबना की कहानियाँ हैं। ‘कहानी का अभाव’ यद्यपि मेरी आरंभिक कहानियों में से है, किन्तु मुझे अब भी बहुत प्रिय है। इसकी सामग्री मैंने अपने बड़े भाई के जीवन से ली थी, जो अत्यंत नीरस, शुष्क तथा मशीनी हो चुका था। उनकी पीड़ा तो मेरे लिए महत्वपूर्ण भी है, किन्तु यह कहानी मुझे अन्य कारणों से भी प्रिय है। यह कहानी की संरचना के परंपरागत अकादमीय-ढाँचे पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। ‘एक ही विकल्प’ कहानी मैंने तीन बार लिखी थी। पहली बार यह ‘अंधेरे का जीवन’ नाम से ‘कहानी’ पत्रिका में प्रकशित हुई थी। उसे लिखने ही नहीं, प्रकाशित करवा देने के पश्चात् भी मेरे मन में एक बात सदा कौंधती रही कि उस कहानी में और बहुत कुछ कहने और चित्रित करने का अवकाश था, किन्तु मैंने उसे बहुत विरल रूप में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि मैंने उसे पुनः उपन्यास के रूप मे लिखा, किन्तु लिखने के साथ ही मुझे लगा कि उसे उपन्यास बनाने के अविवेकी प्रयत्न में मैंने उसे अनावश्यक विस्तार दे दिया है और उस रचना की प्रखरता तथा प्रहारकता क्षीण कर दी है। उसे तीसरी बार लिखा और वह ‘एक ही विकल्प’ के रूप में सामने आई।
जीवन के केन्द्र में अब भी कॉलेज ही था, किन्तु छात्र से अध्यापक बनने की प्रक्रिया से गुज़र चुका था। नई-नई नौकरी, विवाह, दांपत्य जीवन की कुछ आरंभिक समस्याएँ... और इनके कारण अपने तथा अपने निकट के लोगों के जीवन में उत्पन्न हुई जटिलताएँ...जीवन के इन नए अनुभवों ने अपनी आकस्मिकता के कारण वाणी की वक्रता को गौण बना दिया था, अनुभूति ही प्रधान हो गई थी। ‘मॉरिस नगर’, ‘कपूर’, ‘दूसरे कगार का निषेध’ तथा ‘सीमा के आर-पार’ इन्हीं दिनों लिखी गई कहानियाँ हैं।
1966-67 के दो वर्ष मेरे जीवन में घटनाओं की दृष्टि से अधिक हलचल भरे थे। पहली सन्तान का जन्म, छोटे बच्चे के पालन-पोषण की समस्याएँ और फिर चार ही महीनों में उसकी मृत्यु ! मैंने अनुभव किया कि विवाह अपने-आपमें जीवन की एक बहुत बड़ी घटना हो सकता है, किन्तु सन्तान का जन्म तथा उसका पालन-पोषण, भावना, व्यवहार तथा परिस्थितियों आदि के धरातल पर कहीं अधिक सघन अनुभव है, जो जीवन-क्रम को आपादमस्तक लील लेता है। ‘परिणति’, ‘दूसरी आया’ और ‘किरचें’ आदि कहानियों की पृष्ठभूमि में ये ही घटनाएँ हैं। रोमानियत को छोड़, जीवन कठोर यथार्थ के ढर्रे पर आ रहा था। पारिवारिक संबंधों की अनेक जटिलताएँ अपने केंचुल खोल रही थीं। मृत्यु को इस प्रकार आमने-सामने देखकर व्यक्ति रोमानी रह ही कैसे सकता है !
तब तक मेरे अनुभव कहानियों के रूप में ही ढलते थे, शायद इसलिए कि प्रत्येक घटना को स्वत: संपूर्ण तथा स्वतन्त्र मानकर मेरा सर्जक मन उस घटना को उसी की संपूर्णता में बुनता था। उसे कार्य और कारण की लम्बी श्रृंखला से स्वतन्त्र ही रखता था। कहानी उसी एक बिन्दु के चारों ओर बुनी जाती थी, उसे एक विराट जाल के अंग के रूप में बुनने की चेतना अभी नहीं जागी थी। तब तक ‘व्यंग्य’ भी पूरी तरह से मुझ पर हावी नहीं हुआ था, धीरे-धीरे अपनी आँखें अवश्य खोल रहा था। ‘सार्थकता’ में उसके अंकुर फूटते अवश्य दिखाई पड़ रहे थे। उपन्यास-लेखन की और बढ़ने की छटपटाहट भी चल रही थी। ‘द कॉलेज’ शायद इन दोनों के मिश्रण का ही परिणाम था। आज ‘वृत्त’ को पढ़ता हूँ, तो वह भी किसी बड़े सामाजिक-राजनीतिक उपन्यास का कथानक-सा ही दिखाई पड़ता है। ‘साथ सहा गया दुःख’ का प्रथम प्रारूप भी इन्हीं कहानियों का समकालीन है।
1967-68 में लिखी गई कहानियों की पृष्ठभूमि पिछले वर्ष की कहानियों से विशेष भिन्न नहीं है। ...दूसरी सन्तान का जन्म हो चुका था। इस बार जुड़वाँ बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की चौबीस दिनों की ही आयु लेकर आई थी। ...इस काल में लिखी कहानियों में इन घटनाओं की प्रत्यक्ष चर्चा नहीं है। हाँ, पिछले दो वर्षो के अनुभवों को कटुता के कारण विनोद की वक्रता अब यथार्थ की कटुता में बदलती अवश्य लग रही थी। इसी प्रक्रिया का आभास ‘हिन्दुस्तानी’ में मिलता है।
स्वयं पिता बनकर अपने पिता को मैंने और भी निकट से जाना। शायद इसीलिए वृद्धावस्था के प्रति संवेदना और सहानुभूति जागी। ‘शटल’ ‘दृष्टिदेश में एकाएक’, ‘नमक की क़ैदी’ तथा ‘ख़र्च, डायरी और अस्पताल’ आदि कहानियाँ तो पिता जी से संबंधित हैं ही, ‘चारहान का जंगल’ भी उन्हीं के जीवन में घटित एक घटना पर आधृत कहानी है।
जहाँ घटनाओं का चित्रण न कर उस पर प्रतिक्रिया और वह भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ी, वहाँ कहानी नहीं बनी, व्यंग्य ही बना। 1969 में कहानियों से अधिक मैं व्यंग्य लिख रहा था। बीच-बीच में कुछ कहानियाँ भी लिखी जा रही थीं, किन्तु क्रमशः कहानियों का स्रोत सूख रहा था। वैसे तो व्यंग्य में भी घटनाओं का उपयोग होता ही है, किन्तु व्यंग्य कथानक विहीन विधा है, तो मेरे भीतर का कथा-तत्व कहाँ जा रहा था ? 1970 में जब उपन्यास-लेखन आरंभ हुआ, तो कहानी-लेखन प्रायः बन्द हो गया। शायद तब छोटी घटनाओं का स्वतंत्र महत्व कम लगने लगा था। वे घटनाएँ तो एक बड़ी व्यवस्था की कड़ियाँ थीं और व्यवस्था का चित्रण उपन्यास लिखे बिना नहीं हो सकता था। संभवतः मेरा आक्रोश व्यंग्य का रूप ग्रहण कर रहा था और कथा-तत्व उपन्यास में ढ़ल रहा था।
1970-75 की अवधि में बहुत कम कहानियाँ लिखी गईं। व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पड़ाव (जो व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं) मैं प्रायः पार कर आया था। पढ़ाई, नौकरी, विवाह, संतान का जन्म, उनका रोग-शोक, गृहस्थी के तनाव और परेशानियाँ, सामाजिक संबंध, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक दबाव, यह सब कुछ देख चुका था। ...मेरी रचना-प्रक्रिया में एक विचित्र अंतर आता जा रहा था। सृजन-प्रक्रिया के वृक्ष के तने में से दो शाखाएँ उग आई थीं, व्यंग्य और उपन्यास। बीज आ जाने पर फूल झड़ जाते हैं। इन दो टहनियों के विकास से कहानी अनायास ही सूख गई थी।
मेरे सृजन-वृक्ष का तना अब भी कथा ही है, किन्तु विधा के रूप में कहानी जैसे विलीन हो गई है। कथा-तत्व उपन्यास में समा गया और आक्रोश व्यंग्य में। इसके बाद पन्द्रह वर्षों में मैंने कहानियाँ बहुत कम लिखी हैं, न के बराबर। अब तो स्वतन्त्र रचना के रूप में व्यंग्य भी कभी-कभार लिख लेता हूँ, अन्यथा वह भी उपन्यास में ही समाहित हो गया है। लोग पूछते हैं, ‘आपने कहानी लिखनी बन्द कर दी ?’ मैं स्वीकार में सिर हिला नहीं पाता, क्योंकि न तो मैंने ऐसा कोई संकल्प ही किया है और न ही मुझे कहानी से किसी भी प्रकार का विरोध है। कहानियाँ लिख नहीं रहा, तो इसलिए नहीं कि लिखना नहीं चाहता। हुआ यह है कि उपन्यास अधिक प्रबल हो उठा है या यह कहना अधिक उचित होगा कि वह मुझ पर हावी हो गया है।
इसी अवधि में कुछ कहानियाँ केवल इसलिए लिखी गईं, क्योंकि कहानियाँ बन गई थीं। कहानीपन का भी अपना मज़ा होता है। उसको छोड़ पाना कठिन होता है, विशेषकर आरंभिक दौर में। ऐसा भी हुआ कि परस्पर चर्चा में किसी ने कोई रोचक घटना सुना दी अथवा किसी की बातचीत में से कोई पक्ष उभर आया, तो उसकी भी कहानी बन गई। ‘राजा दशरथ के बेटे’ तथा ‘मम्मी, पापा और उनकी बेबी’ ऐसी ही कहानियाँ हैं।
प्रेम-कथाएँ मैंने बहुत कम लिखी हैं, किन्तु आरंभ में कुछ रोमानी कहानियाँ अवश्य लिखी थीं। ‘स्नेह का उदय,’ ‘संगिनी,’ ‘उसने ग़लत नहीं कहा था’ तथा ‘मालिनी’ जैसी कुछ कहानियाँ याद आ रही हैं, किन्तु इनमें से कोई भी गंभीर प्रेम-कथा नहीं है। प्रेम-कथा लिखने में न मुझे तब संकोच था, न अब है, किन्तु प्रेम को कहानी बनने में शायद लम्बी अवधि चाहिए। लम्बे अरसे के बाद मैंने ‘कथा पुरानी मैत्री की,’ ‘त्रासदियाँ प्रेम की’ तथा ‘प्रीति-कथा’ इत्यादि रचनाएँ अवश्य लिखीं, किन्तु उनमें ‘प्रेम’ कम, विश्लेषण और व्यंग्य ही अधिक सघन हुआ है, क्योंकि प्रेम की वास्तविकता अब उतनी अबूझ नहीं रह गई थी।
फिर जैसे अपने-आप से अवकाश पाकर मेरा लेखक अपने दुःख-दर्द के साथ-साथ दूसरों के दुःख-दर्द को भी पहचानने लगा था। इस समय की मेरी कहानियाँ, मेरे जीवन को छूते हुए अन्य लागो के अनुभवों की कहानियाँ। मेरी लेखनीय सहानुभूति इन्हीं दिनों विकसित होनी आरंभ हुई थी। ‘आहत-प्यार’, ‘भूखे बच्चे : सूखी डाली,’ ‘मेरा अपना संसार’ बहुत भावुक और आहत भावनाओं की कहानियाँ है ? उनके साथ-साथ ‘कहानी का अभाव,’ ‘होने वाली पत्नी’ तथा ‘एक ही विकल्प’ परिस्थितियों की विडंबना की कहानियाँ हैं। ‘कहानी का अभाव’ यद्यपि मेरी आरंभिक कहानियों में से है, किन्तु मुझे अब भी बहुत प्रिय है। इसकी सामग्री मैंने अपने बड़े भाई के जीवन से ली थी, जो अत्यंत नीरस, शुष्क तथा मशीनी हो चुका था। उनकी पीड़ा तो मेरे लिए महत्वपूर्ण भी है, किन्तु यह कहानी मुझे अन्य कारणों से भी प्रिय है। यह कहानी की संरचना के परंपरागत अकादमीय-ढाँचे पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। ‘एक ही विकल्प’ कहानी मैंने तीन बार लिखी थी। पहली बार यह ‘अंधेरे का जीवन’ नाम से ‘कहानी’ पत्रिका में प्रकशित हुई थी। उसे लिखने ही नहीं, प्रकाशित करवा देने के पश्चात् भी मेरे मन में एक बात सदा कौंधती रही कि उस कहानी में और बहुत कुछ कहने और चित्रित करने का अवकाश था, किन्तु मैंने उसे बहुत विरल रूप में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि मैंने उसे पुनः उपन्यास के रूप मे लिखा, किन्तु लिखने के साथ ही मुझे लगा कि उसे उपन्यास बनाने के अविवेकी प्रयत्न में मैंने उसे अनावश्यक विस्तार दे दिया है और उस रचना की प्रखरता तथा प्रहारकता क्षीण कर दी है। उसे तीसरी बार लिखा और वह ‘एक ही विकल्प’ के रूप में सामने आई।
जीवन के केन्द्र में अब भी कॉलेज ही था, किन्तु छात्र से अध्यापक बनने की प्रक्रिया से गुज़र चुका था। नई-नई नौकरी, विवाह, दांपत्य जीवन की कुछ आरंभिक समस्याएँ... और इनके कारण अपने तथा अपने निकट के लोगों के जीवन में उत्पन्न हुई जटिलताएँ...जीवन के इन नए अनुभवों ने अपनी आकस्मिकता के कारण वाणी की वक्रता को गौण बना दिया था, अनुभूति ही प्रधान हो गई थी। ‘मॉरिस नगर’, ‘कपूर’, ‘दूसरे कगार का निषेध’ तथा ‘सीमा के आर-पार’ इन्हीं दिनों लिखी गई कहानियाँ हैं।
1966-67 के दो वर्ष मेरे जीवन में घटनाओं की दृष्टि से अधिक हलचल भरे थे। पहली सन्तान का जन्म, छोटे बच्चे के पालन-पोषण की समस्याएँ और फिर चार ही महीनों में उसकी मृत्यु ! मैंने अनुभव किया कि विवाह अपने-आपमें जीवन की एक बहुत बड़ी घटना हो सकता है, किन्तु सन्तान का जन्म तथा उसका पालन-पोषण, भावना, व्यवहार तथा परिस्थितियों आदि के धरातल पर कहीं अधिक सघन अनुभव है, जो जीवन-क्रम को आपादमस्तक लील लेता है। ‘परिणति’, ‘दूसरी आया’ और ‘किरचें’ आदि कहानियों की पृष्ठभूमि में ये ही घटनाएँ हैं। रोमानियत को छोड़, जीवन कठोर यथार्थ के ढर्रे पर आ रहा था। पारिवारिक संबंधों की अनेक जटिलताएँ अपने केंचुल खोल रही थीं। मृत्यु को इस प्रकार आमने-सामने देखकर व्यक्ति रोमानी रह ही कैसे सकता है !
तब तक मेरे अनुभव कहानियों के रूप में ही ढलते थे, शायद इसलिए कि प्रत्येक घटना को स्वत: संपूर्ण तथा स्वतन्त्र मानकर मेरा सर्जक मन उस घटना को उसी की संपूर्णता में बुनता था। उसे कार्य और कारण की लम्बी श्रृंखला से स्वतन्त्र ही रखता था। कहानी उसी एक बिन्दु के चारों ओर बुनी जाती थी, उसे एक विराट जाल के अंग के रूप में बुनने की चेतना अभी नहीं जागी थी। तब तक ‘व्यंग्य’ भी पूरी तरह से मुझ पर हावी नहीं हुआ था, धीरे-धीरे अपनी आँखें अवश्य खोल रहा था। ‘सार्थकता’ में उसके अंकुर फूटते अवश्य दिखाई पड़ रहे थे। उपन्यास-लेखन की और बढ़ने की छटपटाहट भी चल रही थी। ‘द कॉलेज’ शायद इन दोनों के मिश्रण का ही परिणाम था। आज ‘वृत्त’ को पढ़ता हूँ, तो वह भी किसी बड़े सामाजिक-राजनीतिक उपन्यास का कथानक-सा ही दिखाई पड़ता है। ‘साथ सहा गया दुःख’ का प्रथम प्रारूप भी इन्हीं कहानियों का समकालीन है।
1967-68 में लिखी गई कहानियों की पृष्ठभूमि पिछले वर्ष की कहानियों से विशेष भिन्न नहीं है। ...दूसरी सन्तान का जन्म हो चुका था। इस बार जुड़वाँ बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की चौबीस दिनों की ही आयु लेकर आई थी। ...इस काल में लिखी कहानियों में इन घटनाओं की प्रत्यक्ष चर्चा नहीं है। हाँ, पिछले दो वर्षो के अनुभवों को कटुता के कारण विनोद की वक्रता अब यथार्थ की कटुता में बदलती अवश्य लग रही थी। इसी प्रक्रिया का आभास ‘हिन्दुस्तानी’ में मिलता है।
स्वयं पिता बनकर अपने पिता को मैंने और भी निकट से जाना। शायद इसीलिए वृद्धावस्था के प्रति संवेदना और सहानुभूति जागी। ‘शटल’ ‘दृष्टिदेश में एकाएक’, ‘नमक की क़ैदी’ तथा ‘ख़र्च, डायरी और अस्पताल’ आदि कहानियाँ तो पिता जी से संबंधित हैं ही, ‘चारहान का जंगल’ भी उन्हीं के जीवन में घटित एक घटना पर आधृत कहानी है।
जहाँ घटनाओं का चित्रण न कर उस पर प्रतिक्रिया और वह भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ी, वहाँ कहानी नहीं बनी, व्यंग्य ही बना। 1969 में कहानियों से अधिक मैं व्यंग्य लिख रहा था। बीच-बीच में कुछ कहानियाँ भी लिखी जा रही थीं, किन्तु क्रमशः कहानियों का स्रोत सूख रहा था। वैसे तो व्यंग्य में भी घटनाओं का उपयोग होता ही है, किन्तु व्यंग्य कथानक विहीन विधा है, तो मेरे भीतर का कथा-तत्व कहाँ जा रहा था ? 1970 में जब उपन्यास-लेखन आरंभ हुआ, तो कहानी-लेखन प्रायः बन्द हो गया। शायद तब छोटी घटनाओं का स्वतंत्र महत्व कम लगने लगा था। वे घटनाएँ तो एक बड़ी व्यवस्था की कड़ियाँ थीं और व्यवस्था का चित्रण उपन्यास लिखे बिना नहीं हो सकता था। संभवतः मेरा आक्रोश व्यंग्य का रूप ग्रहण कर रहा था और कथा-तत्व उपन्यास में ढ़ल रहा था।
1970-75 की अवधि में बहुत कम कहानियाँ लिखी गईं। व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पड़ाव (जो व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं) मैं प्रायः पार कर आया था। पढ़ाई, नौकरी, विवाह, संतान का जन्म, उनका रोग-शोक, गृहस्थी के तनाव और परेशानियाँ, सामाजिक संबंध, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक दबाव, यह सब कुछ देख चुका था। ...मेरी रचना-प्रक्रिया में एक विचित्र अंतर आता जा रहा था। सृजन-प्रक्रिया के वृक्ष के तने में से दो शाखाएँ उग आई थीं, व्यंग्य और उपन्यास। बीज आ जाने पर फूल झड़ जाते हैं। इन दो टहनियों के विकास से कहानी अनायास ही सूख गई थी।
मेरे सृजन-वृक्ष का तना अब भी कथा ही है, किन्तु विधा के रूप में कहानी जैसे विलीन हो गई है। कथा-तत्व उपन्यास में समा गया और आक्रोश व्यंग्य में। इसके बाद पन्द्रह वर्षों में मैंने कहानियाँ बहुत कम लिखी हैं, न के बराबर। अब तो स्वतन्त्र रचना के रूप में व्यंग्य भी कभी-कभार लिख लेता हूँ, अन्यथा वह भी उपन्यास में ही समाहित हो गया है। लोग पूछते हैं, ‘आपने कहानी लिखनी बन्द कर दी ?’ मैं स्वीकार में सिर हिला नहीं पाता, क्योंकि न तो मैंने ऐसा कोई संकल्प ही किया है और न ही मुझे कहानी से किसी भी प्रकार का विरोध है। कहानियाँ लिख नहीं रहा, तो इसलिए नहीं कि लिखना नहीं चाहता। हुआ यह है कि उपन्यास अधिक प्रबल हो उठा है या यह कहना अधिक उचित होगा कि वह मुझ पर हावी हो गया है।
- नरेन्द्र कोहली
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i